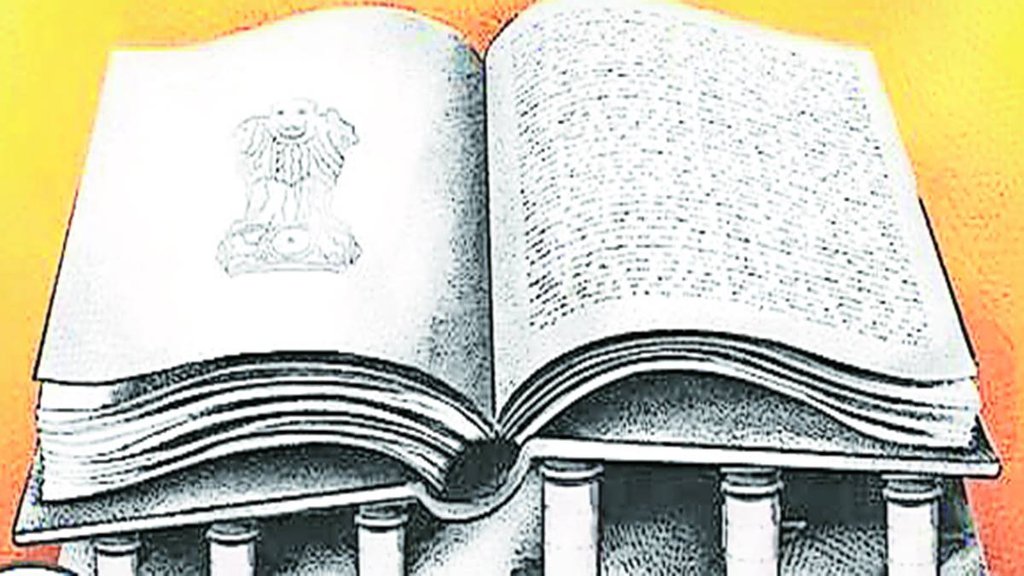कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक विधायिका है जिसके लिए न्यूनतम शिक्षा की शर्त नहीं है। आरोप लगते हैं कि विधायिका जनता से ज्यादा नौकरशाही को खुश रखने में जुट जाती है क्योंकि वह बौद्धिक और तार्किक स्तर पर हावी होती है। अब यह भी चलन है कि सदन में डिग्रीधारियों की कतार होते हुए भी किसी कमतर शिक्षा वाले को अहम महकमा दे दिया जाता है। उच्च शिक्षित कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किताबों और डिग्रियों से दूर विधायिका पर बेबाक बोल।
पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां
कदे अपने आप नूं पढ़या नईं
जां जां वड़दे मंदर, मसीती
कदे मन अपने विच्च वड़या नईं
-बुल्ले शाह
भक्ति काल में संतों, सूफियों ने इस तथ्य को स्थापित किया कि ज्ञान सिर्फ किताबों में ही नहीं है। अगर है भी तो खुद को पहचाने बिना फिजूल है। ज्ञान की दिशा तय करनी और भी जरूरी है। जब जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, या दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान नहीं थे तब सब गुरुकुलों का ही रुख करते थे। जो, इसमें सक्षम नहीं थे वे गुरु के चरणों में लोट कर कबीर हो जाते थे। पोथी से ज्यादा प्रेम का पाठ पढ़ते थे। बुल्ले शाह ने इससे आगे की बात कही कि ज्ञान के लिए जितना खुद को पहचानना जरूरी है, उतना ही भगवान को अंतर्मन में ढूंढना जरूरी है। खुद को पहचाने बिना सिर्फ मंदिर, मस्जिद से कुछ भी हासिल नहीं होगा। शायरों ने प्रेम की पहचान किताब की बजाय आंखों से परखी। लब्बोलुआब यही कि जब तक खुद को नहीं पहचानेंगे कागज पर की डिग्री सजावटी ही रहेगी।
पढ़ाई कैसी हो, भारत में इस पर हर काल में सवाल उठे हैं। वहीं भारतीय राजनीति में चुनाव सुधारों की बात होते ही राजनीतिक दलों के किताबी ज्ञान यानी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का सवाल कोई नया नहीं है। अदालत में पहुंचे नेताओं के भाषणों को बचाने के लिए वकील जितनी मोटी-मोटी किताबों का हवाला देकर दलील देते हैं उसे देख कर लगता है कि हिंदी पत्रकारिता का कालजयी जुमला संसद से सड़क तक अब संसद से अदालत तक बन जाएगा।
सुकरात शिक्षा के लिए वित्तीय पारिश्रमिक के खिलाफ थे
सभ्यता के विकास में नदी किनारे पैदा होने वाले अनाज के बाद किसी से मानव बस्तियों का वर्गीकरण हुआ है, तो वह शिक्षा ही है। प्राचीन यूनानी सभ्यताओं में समाज के साथ ही राजनीति शास्त्र का जन्म होता है। अगर हम कह रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसी वक्त यह भी कह रहे हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। इसलिए यहां समाज के साथ राजनीतिक शिक्षा भी शुरू होती है। जैसे, मां अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, पिता उसे रात में बिस्तर पर सुलाने के लिए पारिश्रमिक की मांग नहीं करते उसी तरह सुकरात शिक्षा के लिए वित्तीय पारिश्रमिक के खिलाफ थे। एक दार्शनिक ने तो शिक्षा के लिए शुल्क को वेश्यावृत्ति के दायरे में रखा।
लोकतंत्र की मातृ-शक्तियों ने शिक्षापान से जिस सभ्यता-संस्कृति को खड़ा किया था, जहां शिक्षा, साहित्य और कला से विहीन लोगों को पूंछ रहित पशु कहा गया था, जहां गुरु को गोविंद से प्रथम दर्जे पर रखा गया था, वहां का आधुनिक लोकतंत्र इतना पीछे कैसे चला गया कि राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए शिक्षा अनिवार्य हो या नहीं जैसा सवाल पूछना पड़े। यूनानी से लेकर प्राचीन भारतीय संस्कृति में शिक्षा किसी कागज के टुकड़े पर लिखा प्रमाणपत्र नहीं है। यह शिक्षा वैसे सरोकार का प्रमाणपत्र देती है जिसमें मनुष्य मानवीय मूल्यों से लैस होता है। हर युग में शिक्षा अपने साकार उद्देश्य के साथ खड़ी मिलती है। तो, आज उनके लिए न्यूनतम शिक्षा की मांग क्यों नहीं जिन्हें पूरे देश के लिए शिक्षा नीति, आर्थिक नीति बनानी है?
हर साल सिविल सेवा परीक्षा में उच्चतम अंक लाने वालों के साक्षात्कार दिखते हैं। किसी नेता की संतान, उद्योगपति की संतान से लेकर कमजोर तबके के लोगों की संतानों के साक्षात्कार छपते हैं। अब वे सिर्फ होनहार विद्यार्थी हैं और सिविल सेवक बनते ही उन सबका तबका एक ही है। उनके अंकों, साक्षात्कार का विश्लेषण पढ़ते हुए हम गर्व महसूस करते हैं कि पढ़-लिख कर मेहनत से आए लोग देश चलाने के अहम पायदान पर होंगे। अमीर घरों में उन बच्चों के उदाहरण दिए जाते हैं कि देखो इतने अभाव में पढ़-लिख कर अफसर बना।
जनता को खुश रखना पहली प्राथमिकता होती है
कार्यपालिका के लिए सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई निर्विवादित है। फिर हम विधायिका की ओर चलें जहां हमारे नेताजी चुनाव जीत कर सरकार और मंत्रिमंडल बनाते हैं। इन्हीं के साथ कदमताल करती है कार्यपालिका। एक कानून बनाएगी तो दूसरा कानून पारित करवाएगी। आरोप लगते रहे हैं कि विधायिका और कार्यपालिका दो अलग ध्रुव बन जाते हैं। राजनेता जनता के बीच से चुन कर आते हैं तो उनका लक्ष्य बहुमत को अपने पक्ष में रखना होता है। जनता को खुश रखना पहली प्राथमिकता होती है।
वहीं, नौकरशाह शासक वर्ग का वो हिस्सा बन जाते हैं जिनका ध्येय रहता है कि नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। नौकरशाह मूल रूप से आएं जिस भी वर्ग से लेकिन पदभार संभालते ही वे पूंजीपति वर्ग के साथ दिखते हैं। यानी उनका हित और जनता का हित एक नहीं होता है। यहां पर हितों के संघर्ष की टकराहट भी दिखती है जो जनता और शासक वर्ग के हितों का अक्षांश-देशांतर ही अलग कर देता है।
सरकार के राजनीतिक एजंडे पर भी नौकरशाही हावी हो जाएगी
विधायिका का प्रमुख चुनावी राजनीति से चुनकर आया होता है। वहीं से फिर मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक चुने जाते हैं। अब अगर मंत्री पढ़े-लिखे नहीं होंगे तो उनका एकमात्र ध्येय नौकरशाही को खुश करना रह जाएगा, आखिर सारे काम उसे इन्हीं से करवाने हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार के राजनीतिक एजंडे पर भी नौकरशाही हावी हो जाएगी। इसी वजह से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत में ही ज्यादातर मंत्रालय उससे संबंधित विशेषज्ञों को ही संभालने देने की रवायत रही।
खास कर वित्त, कानून, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम मंत्रालय। लेकिन, हम इस परंपरा को भी कायम नहीं रख सके। दिल्ली सरकार को ही देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल शिक्षा के मसले पर आसमान सिर पर उठाए रहते हैं। उन्होंने अपनी सरकार में शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा उन्हें दिया है, जिनके पास शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री नहीं है। इतना ही नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी सिसोदिया को विश्व का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री करार देती है। उनके लिए भारत रत्न की भी मांग कर दी जाती है। दीगर है कि सिसोदिया इन दिनों शराब घोटाले के कथित भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में हैं।
विरोधी दलों की सरकार वाली राज्यों में भी नौकरशाही हावी
जिन राज्यों में केंद्रीय शक्ति पार्टी से इतर दूसरे दलों की सरकार होती है, वहां भी नौकरशाही की अहम भूमिका होती है। सबसे अहम मसला होता है कि वहां केंद्रीय नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए? अगर विधायिका का नेतृत्व पढ़ा-लिखा नहीं हो तो नौकरशाही का उसे नियंत्रित करना, जनता की चाहत और उसके राजनीतिक एजंडे के खिलाफ ले जाना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब राजनीतिक नेतृत्व सदिच्छा होते हुए भी जनहितकारी योजनाओं को लागू नहीं करवा पाता क्योंकि वह बौद्धिक से लेकर तार्किक स्तर पर कार्यपालिका से कमतर हो जाता है।
वित्त और विदेश जैसे मंत्रालय पढ़े-लिखे राजनेताओं के पास
आज के एकध्रुवीय विश्व में कूटनीति का जिम्मा सिर्फ विदेश मंत्री के कंधों पर नहीं होता है जो वर्तमान की सरकार में जेएनयू के पढ़े-लिखे हैं। यह जिम्मा प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री व सत्ताधारी पार्टी से जुड़े प्रवक्ताओं से भी होता है जिन्हें भविष्य का राजनेता बनना है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राजनेताओं के बौद्धिक और तार्किक शक्ति का पहला नमूना हम संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर देखते हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि वित्त और विदेश जैसे मंत्रालय पढ़े-लिखे राजनेताओं के पास हैं। लेकिन, अन्य मंत्रालय से लेकर सभी सांसदों तक भी शिक्षा का स्तर उच्च हो तो शायद हम बेहतर संसद देख पाएंगे।
राजनेताओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की मांग करते ही स्त्री, हाशिये पर पड़े लोग, जातीय पूर्वग्रह से उत्पन्न हालात जैसी चुनौतियां सामने आती हैं। देश के हालात के लिहाज से इस सवाल पर ही सवाल उठ जाते हैं। पर, क्या आजादी के 75 साल में हम संकल्प कर सकते हैं कि सबको एक बराबरी पर लाना होगा? लेकिन, तब तक क्या हम उस आदर्श स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई नेता अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत में निरक्षर हो भी तो अगले बीस से तीस सालों के दौरान वह शिक्षा हासिल कर ले।
सांसद व विधायक बनने के बाद सिर्फ उसकी संपत्ति में नहीं बल्कि शिक्षा में भी इजाफा हो। चुनावी हलफनामे में सांसद का पर्चा देख कर हम कह सकें कि पांच साल या दस साल में उन्होंने फलां पाठ्यक्रम कर लिया तो फलां डिग्री ले ली। अगर कोई जनप्रतिनिधि फलां मंत्रालय देख रहा है तो उससे जुड़ा कोई पाठ्यक्रम कर लिया। पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक देखिए, जिस देश में राजनेताओं ने किताबों से नाता तोड़ा है वहां लोकतंत्र का भी जनता से नाता टूट जाता है। आजाद भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक संविधान की किताब है तो उस किताब को पढ़ने और समझने की सलाहियत जनता से लेकर उसके प्रतिनिधि तक में हो।