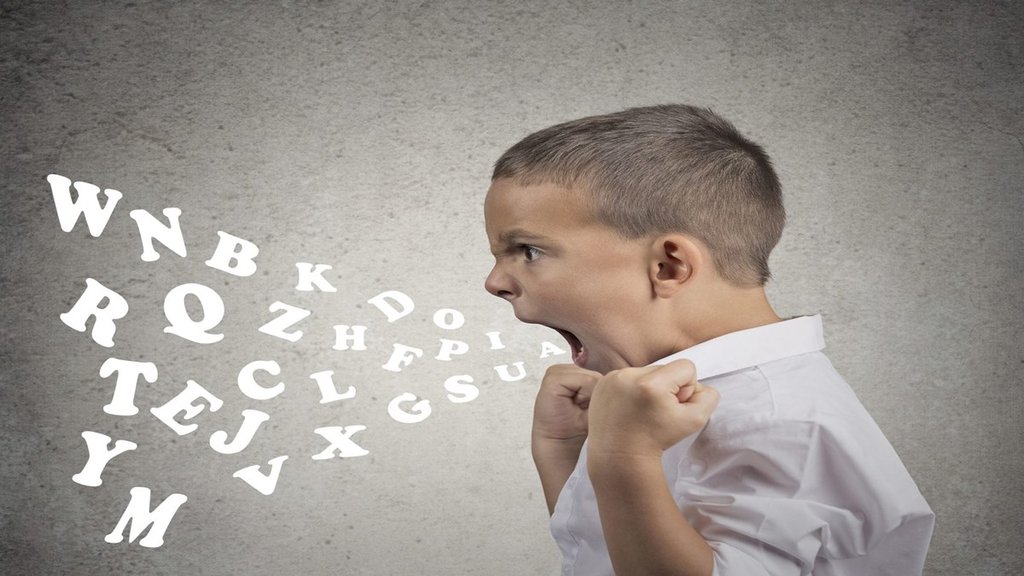संगीता सहाय
वक्त पल-प्रतिपल तेज गति से भाग रहा है और हर तरफ बदलाव के रंग भी बिखेरता जा रहा है। यह बदलाव बच्चे, वृद्ध, युवा- सभी के जीवन शैली, व्यवहार में स्पष्टता से दिख रहा है। स्वाभाविक रूप से इस लय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों किस्म के राग-विराग मौजूद हैं। पर गौरतलब यह है कि आज के समय में नकारात्मकता के खटराग ही ज्यादा प्रभावी हैं।
सामाजिकता, लोकाचार, बात व्यवहार- हर स्तर पर इन तथ्यों को देखा जा सकता है। विशेषकर वर्तमान युवा पीढ़ी के संदर्भ में ये बातें ज्यादा दृश्यमान हैं। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। लेकिन वह नकारात्मक दिशा में अग्रसर हो, तो वह मनुष्य के पतन का पर्याय बनने लगता है। हर रोज हमारे आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं, जो युवाओं में बढ़ती उग्रता, कम होते अनुशासन के भाव, बड़े-बुजुर्गों के प्रति असम्मान आदि को दिखाती हैं।
उनमें स्वयं को श्रेष्ठ मानने, दिखावा करने, अपनी पसंदीदा चीज को हर हालत में पाने की प्रवृत्ति घर करती जा रही है। युवाओं में बढ़ती ये प्रवृत्तियां एक तरफ उन्हें जीवन की सच्चाई से दूर कर रही हैं तो दूसरी ओर आत्मघाती कदम उठाने को भी उकसा रही हैं। बीते कुछ वर्षों में गांवों, कस्बों, छोटे-बड़े शहरों हर जगह युवाओं के आत्महत्या की दर लगातार बढ़ी है।
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश पाने का ख्वाब पाले बच्चों के लिए सफलता की राह प्रशस्त करने की बात करने वाला कोटा शहर हाल के दिनों में उन बच्चों के बीच बढ़ती आत्महत्या की दर के कारण चर्चा के केंद्र में है। सपने देखने, उसे जीने और उड़ान भरने की उम्र में ऐसी आत्मघाती प्रवृत्ति शोचनीय है, क्योंकि जिन पर देश और समाज का वर्तमान और भविष्य टिका है, उनके कदम किस दिशा में हैं।
आज गांवों, कस्बों, शहरों में हर तरफ हाथों में स्मार्टफोन, कानों में हेडफोन, कंधे पर बैग लिए लड़कों की भीड़ शिक्षा के नाम पर घूमते-टहलते, कुकुरमुत्ते की तरह उग आए कोचिंग संस्थानों में बढ़ती भीड़, चौराहों पर पान-गुटका चबाते और उच्छृंखलता करते किशोर और युवा दिखते रहते हैं। बात-बेबात मारपीट, गाली-गलौज इनके लिए आम है।
दुखद यह भी कि पढ़ने के नाम पर निकले बहुत सारे युवा आधुनिक बनने की होड़ में ऐसे माहौल का हिस्सेदार बन जाते हैं। इसकी छोटी-बड़ी कई वजहें हो सकती हैं। खराब परिवेश और परवरिश, बिगड़े सामाजिक माहौल, मोबाइल और इंटरनेट का प्रकोप, पंगु शिक्षा व्यवस्था आदि। हालांकि यह भी सच है कि इन्हीं व्यवस्थाओं से निकलकर लड़के, लड़कियां बेहतर पद-प्रतिष्ठा हासिल कर रहे हैं।
समाज को नई दिशा दे रहे हैं। पर यहां मुद्दा कुछेक के बेहतर हो जाने का नहीं, बल्कि अधिसंख्य के दिग्भ्रमित और दिशाहिन होने का है। यह भी कि आम से खास बनने निकली युवाओं की भीड़ खास तो क्या आम भी क्यों नहीं बन पा रही है? शिक्षा का उद्देश्य लोगों को सुविचारित ढंग से अपनी राहें तलाशना सिखाना और उन्हें योग्य बनाना होता है। उस शिक्षा का क्या मतलब, जो सही राह पर चलना ही न सिखा सके? आज ज्यादातर शिक्षा और शिक्षार्थी इसी बदहाल स्थिति से गुजर रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बाई शहरों की स्थिति इस संदर्भ में ज्यादा चिंतनीय है, जहां देश की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है। शिक्षा के हर स्तर पर सरकारी व्यवस्था की कमियों, तेजी से बढ़ते निजीकरण, बाजारीकरण, माफियाकरण आदि ने इसके असल उद्देश्य को ही गुम कर दिया है। महानगरों, नगरों, गांवों हर जगह यही सोच काबिज हो चुकी है। अधिकतर युवा पढ़ाई के नाम पर अधकचरा ज्ञान लिए बेरोजगारी के गर्त में समाते जा रहे हैं।
प्रतिभा पलायन की समस्या भारत सहित दुनिया के तमाम विकासशील देशों की एक कड़वी सच्चाई है। बेहतर आर्थिक संभावनाएं, अवसर, उच्च वेतन आदि के लिए अक्सर उच्च शिक्षित लोग दूसरे देशों में चले जाते हैं। उनका जाना देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को गहन रूप से प्रभावित करता है। यह किसी भी देश और समाज से बेहतर मस्तिष्क के निकास और प्रतिभा के लोप होते जाने की भी कहानी है।
ठीक इसी तरह लगातार गांवों से शहरों की ओर युवाओं का पलायन भी वहां से प्रतिभा और मस्तिष्क के लोप होते जाने की बात है। आज युवाओं से रिक्त गांव बुजुर्गों के वीराने में तब्दील होते जा रहे हैं। यह स्थिति वहां रह रहे लोगों की जिंदगी और जिंदादिली को तो छीन ही रहा है, साथ ही उनके आत्मविश्वास को भी समाप्त कर रहा है।
उन्हें लगने लगा है कि या तो यहां से पलायन करो या कैसे भी करके नौकरी प्राप्त करो। अपने गुणों और क्षमताओं को तो जैसे वो भूलते जा रहे हैं। तमाम लोग झूठी मृगमरीचिका से मोहग्रस्त होकर बिना विचारे एक अंधी दौड़ में शामिल होते जा रहे हैं।
कहा जा सकता है कि शिक्षा के वास्तविक अर्थ को खोता, विकास के भ्रामक जाल में उलझता हमारा समाज एक अंतहीन लिप्सा में फंसता जा रहा है। हर स्तर पर शिक्षा की दुकान खोले लोग इसी का फायदा उठा रहे हैं। आवश्यकता यह है कि हम अपने होने के महत्त्व को जानें, मनुष्यता को पहचानें, मिथ्या द्वंद्व और दंभ में फंसे बिना सही अर्थों में अपनी बेहतरी की राहों को जानते, पहचानते हुए आगे बढ़ें।