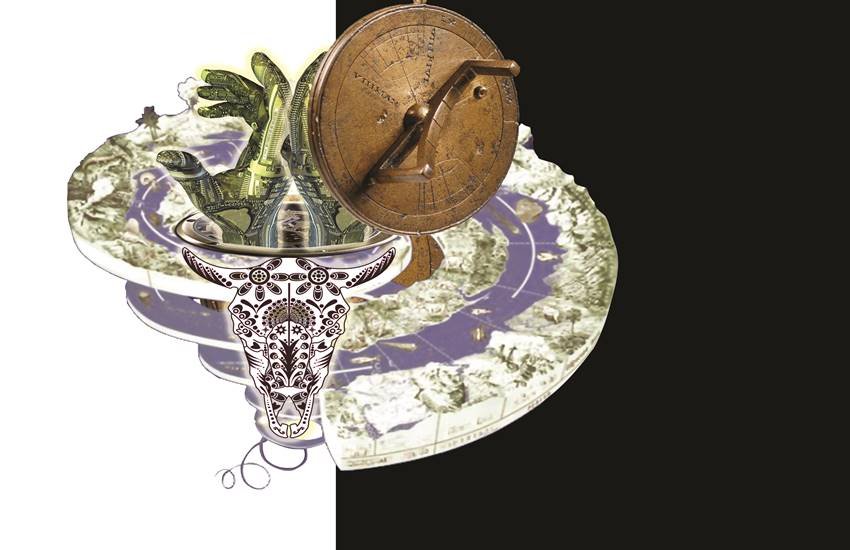राजशेखर व्यास
विक्रम संवत्’ के दो हजार वर्ष का समाप्त होना भारतीय इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। धूमिल अतीत में विक्रम के स्मारक स्वरूप जिस विक्रम संवत् का प्रवर्तन हुआ था, उसके पथ की वर्तमान रेखा हालांकि तमसाछन्न है, लेकिन इस डोर के सहारे हम अपने आपको उस शृंखला के क्रम में पाते हैं, जिसके अनेक अंश अत्यंत उज्ज्वल और गौरवमय रहे हैं। ये दो हजार वर्ष तो भारतीय इतिहास के उत्तरकाल के ही अंश हैं। विक्रम उद्भव तक विशुद्ध वैदिक संस्कृति का काल, रामायण और महाभारत का युग, महावीर और गौतम बुद्ध का समय, पराक्रमी चंद्रगुप्त मौर्य और प्रियदर्शी अशोक का काल, अंतत: पुष्यमित्र शुंग की साहस गाथा सुदूरभूत की बातें बन चुकी थीं। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, सूत्र-ग्रंथ और मुख्य स्मृतियों की रचना हो चुकी थी। वैयाकरण पाणिनी और पतंजलि अपनी कृतियों से पंडितों को चकित कर चुके थे और कौटिल्य की ख्याति सफल राजनीतिज्ञता के कारण फैल चुकी थी। उन पिछले दो हजार वर्षों की लंबी यात्रा में भी भारत के शौर्य ने उसकी प्रतिभा और विद्वता ने जो मान स्थित कर दिए हैं, वे विगत शताब्दियों के बहुत कुछ अनुरूप हैं। विक्रम संवत् के प्रथम हजार वर्षों में हमने मात्र शिवनागों, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, यशोधर्मद, विष्णुवर्धन आदि के बल और प्रताप के सम्मुख विदेशी शक्तियों को थर-थर कांपते हुए देखा, भारत के उपनिवेश बसते देखे, भारत की संस्कृति और उसके धर्म का प्रसार बाहर के देशों में देखा। हालांकि दूसरे सहस्राब्द में भाग्य चक्र की गति विपरीत हो गई। उसने उपनिवेशों का उजड़ना दिखाया और भारतीयों की हार तथा बहुमुखी पतन। लेकिन उनकी आतंरिक जीवन-शक्ति का ह्रास नहीं हुआ और यह दिखा दिया कि गिर कर भी कैसे उठा जा सकता है।
भारतीय संस्कृति के अभिमानियों के लिए यह कम गौरव की बात नहीं है। आज भारतवर्ष में प्रवर्तित विक्रम संवत्, बुद्ध-निर्वाण और काल-गणना को छोड़ कर संसार के लगभग सभी प्रचलित ऐतिहासिक संवतों से अधिक प्राचीन है। ‘विक्रम’, ‘यह था’ या ‘वह’ का विवाद केवल अनुसंधान-प्रिय पंडितों का समीक्षार्थ विषय है। आज संपूर्ण विश्व में जिस प्रकाशपुंज की कीर्ति फैल रही है, उसका उद्भव कहां से और कैसे हो गया है, वह तो इतिहासकारों की अनुसंधानशाला तक मर्यादित है। उसमें उच्च कोटि के मानसमूह तो ‘विक्रम’ को अपने हृदय में संजोए बैठे हैं। दरअसल, ‘विक्रम’ में हम अपने विशाल देश की परतंत्र पाश-पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाली समर्थ शक्ति की अभ्यर्थना करते हैं। विक्रम, कालिदास और उज्जयिनी हमारे स्वाभिमान, शौर्य और स्वर्णयुग के अभिमान का विषय है। उसी उज्जयिनी में महर्षि संदीपनी वंश में उत्पन्न पद्मभूषण, साहित्य वाचस्पति दिवंगत पंडित सूर्यनारायण व्यास ने विक्रम संवत् के दो हजार वर्ष पूरे होने पर एक मासिक पत्र ‘विक्रम’ का प्रकाशन आरंभ किया। ‘विक्रम’ (मासिक विक्रम) का प्रकाशन एक विशेष उद्देश्य को लेकर किया था। पंडित व्यास का उज्जैन जैसे छोटे-से कस्बे में ‘विक्रम’ का प्रकाशन दुस्साहस ही कहा जाएगा। अरसे से हमें पढ़ाया जा रहा था कि हम मुगलों और अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। हम शोषित, पीड़ित और गुलामों को पंडित व्यास ने एक प्रबल बल, विक्रम और पराक्रमी नायक, चरित्र नायक, संवत् प्रवर्तक सम्राट विक्रमादित्य दिया था और बताया कि हम आरंभ से ही परास्त, पराजित, पराभूत और शोषित नहीं रहे हैं, बल्कि ‘शक’ और ‘हूणों’ को परास्त करने वाला हमारा नायक शंकारि विक्रमादित्य विजय और विक्रम का दूसरा प्रतीक है। कालिदास समारोह के जन्म से भी पुरानी घटना है यह, जब उज्जयिनी में पंडित व्यास ने विक्रम द्विसहस्राब्दी समारोह समिति का गठन कर सम्राट विक्रम की पावन स्मृति में चार महान उद्देश्यों की स्थापना का संकल्प लिया।
वे उद्देश्य थे विक्रम के नाम पर एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना, जो साहित्य, शिक्षा, कला, संस्कृति की त्रिवेणी हो। दूसरा, ‘विक्रम कीर्ति मंदिर’, तीसरा, ‘विक्रम स्मृति ग्रंथ’ और चौथा, विक्रम स्तंभ। विशेषकर वीर सावरकर और केएम मुंशी ने अपने पत्र ‘सोशल वेलफेयर’ में इस योजना का प्रारूप विस्तार से प्रकाशित किया और सारे देश से इस पुण्य कार्य में पूर्ण सहयोग देने की प्रार्थना की। महाराजा देवास ने इस आयोजन के लिए सारा धन देना स्वीकार किया, मगर शर्त यह रखी गई कि सारे सूत्र उनके हाथ में रखे जाएं। मगर विधि को कुछ और ही मंजूर था। पंडित व्यास अपने व्यक्तिगत कार्यवश मुंबई गए और मुंशी जी से मिल कर योजना पर विस्तार से चर्चा की। तभी महाराजा सिंधिया का उन्हें निमंत्रण मिला। महाराजा जीवाजीराव सिंधिया ने पंडित व्यास के साथ लगभग ढाई घंटे चर्चा की। इस तरह पंडित व्यास सप्ताह भर ग्वालियर रुके और रोजाना घंटों विचार विनिमय हुआ। महाराजा का विचार, ‘विक्रम उत्सव’ के लिए पचास लाख की धनराशि एकत्रित कर अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य करना था, विश्वविद्यालय के लिए धनराशि शासन की ओर से दी जानी थी। इसके सिवा उज्जैन के प्रमुख धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थानों के सुधार के लिए शासन के अनेक विभागों द्वारा सहयोग देने का निश्चय किया गया। तदनुसार महाकाल मंदिर, हरसिद्धि मंदिर और क्षिप्रा तट पर सुधार कार्य आरंभ हो गए थे। जहां-जहां ये सुधार कार्य हुए, वहां पंडित व्यास ने, जो खुद संस्कृत के सुकवि थे, यह श्लोक अंकित करवा दिया था- ‘द्विसहस्रमिते वर्षे चैत्रे विक्रम संवत्सरे, महोत्सव सभा सम्यकरू जीर्णोद्धारमकरायत।’
जैसे-जैसे समारोह का कार्य प्रगति कर रहा था, देश के विभिन्न भागों में एक सांस्कृतिक वातावरण बन गया था। लगभग उसी समय पत्र-पत्रिकाओं में रवींद्र बाबू, निराला, नागार्जुन ने भी ‘विक्रम’ पर कविताओं का सृजन किया था। रवींद्र बाबू की ‘दूर बहुत दूर क्षिप्रातीरे…’ और निराला की ‘द्विसहस्राब्दि’ कविता पठनीय ही नहीं, संग्रहणीय भी है। इसी दरमियान जिन्ना ने अपने एक भाषण में इस उत्सव का विरोध किया। जिन्ना के विरोध से सरकार के भी कान खड़े हो गए। चूंकि यह समय भी ऐसा था, विश्व-युद्ध के आसार सामने थे, ब्रिटिश सरकार चौकन्नी हो गई। उन्हें पंडित व्यास के इस आयोजन में क्रांति या विद्रोह की बू दिखी, क्योंकि एक साथ एक सौ चौदह देशों के महाराजा एक जगह विक्रम उत्सव के नाम पर इकट्ठा हो रहे थे। निस्संदेह इस पर्वरंग में पंडित व्यास की यह परिकल्पना भी थी कि शौर्य और विक्रम उत्सव के इस अवसर पर हमारे खोए बल और पराक्रम की चर्चा देशी राजाओं के रक्त में उबाल अवश्य ले आएगी। यों इस आयोजन में हिंदू-मुसलिम भेदभाव की कोई जगह नहीं थी, लेकिन जिन्ना के विरोध से वातावरण में विकार पैदा हो गया। उस समय पंडित व्यास ने नवाब भोपाल को शासकीय स्तर पर समारोह मनाने के लिए लिखा। नवाब साहब ने अपने कैबिनेट में योग्य विचार करने का आश्वासन दिया। चेतना फैल रही थी, जागृति फैल रही थी। मुंबई में बड़े पैमाने पर यह समारोह आयोजित किया गया। देश की हजारों सभा-संस्थाओं ने समारोह की तैयारी की। उसी समय प्रख्यात फिल्म निर्माता-निर्देशक विजय भट्ट ने पंडित व्यास के आग्रह पर ‘विक्रमादित्य’ सिनेमा का निर्माण आरंभ किया, जिसके संवाद, पटकथा और गीत लेखन का कार्य भी उन्होंने व्यास जी के परामर्श से किया। इस फिल्म में विक्रमादित्य की मुख्य भूमिका भारतीय सिनेमा जगत के महानायक पृथ्वीराज कपूर ने निभाई थी। पृथ्वीराज उस समय पंडित व्यास के आवास ‘भारती भवन’ में ठहरे थे। तब से जो आत्मीयता उन दोनों के मध्य स्थापित हुई थी, वह अंत तक बनी रही। बाद के दिनों में पृथ्वीराज ने ‘कालिदास समारोह’ में अपनी नाटक मंडली को लाकर खुद नाटक भी किए और अपने नाटकों से होने वाली सारी आय कालिदास समारोह के लिए प्रदान कर दी। विक्रम कीर्ति मंदिर का निर्माण कर उसमें पुरातत्व संग्रहालय, चित्रकला-कक्ष, प्राचीन ग्रंथ संग्रहालय आदि रखने का निश्चय किया गया। कुछ समय बाद ही रियासतों का विलीनीकरण हुआ, मध्य भारत का निर्माण हुआ और विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर अनेक उलझन, प्रपंच और अड़ंगे लगाए गए। चूंकि उस वक्त तक इंदौर और भोपाल तक में विश्वविद्यालय नहीं थे, इसलिए वहां के अखबारों और स्वार्थी राजनेताओं ने पंडित व्यास के इस महान कार्य में असंख्य बाधाएं उपस्थित कीं।
उज्जयिनी में हर वर्ष बारह वर्षों में सिंहस्थ पर्व मनाया जाता था। 1944 में जब सिंहस्थ पर्व आया तब देशभर के असंख्य आचार्य, संत-साधु, संत-महंत उज्जयिनी आए, तब पंडित व्यास ने अपने व्यक्तिगत संपर्कों से प्रयास कर उन्हीं के नेतृत्व में विक्रम महोत्सव तीन रोज तक मनाया। साधु-संतों के एक सौ इक्कीस हाथियों, लाजमों, लवाजमों के साथ लाखों लोगों की उपस्थिति में तीन दिनों तक यह भव्य आयोजन बड़े पैमाने पर मनाया गया। देशभर में विक्रमादित्य का बहुत-सा साहित्य विविध भाषाओं में प्रकाशित हुआ। देशभर में सांस्कृतिक लहर आ गई। ‘विक्रम द्विसहस्राब्दि समारोह समिति’ ने भी ‘विक्रम स्मृति ग्रंथ’ का प्रकाशन किया, जैसा कि अक्सर महाभारत के बारे में कहा जाता है कि जो महाभारत में है, वही भारत में है और जो महाभारत में नहीं है, वह कहीं भी नहीं है। ऐसे ही यह ग्रंथ ‘न भूतो न भविष्यति है।’ क्या किसी नगर के इतिहास में यह कम महत्त्वपूर्ण घटना है कि पद और अधिकार से वंचित एक व्यक्ति ने एक पूरे शहर को एक युग से दूसरे युग में रख दिया। व्यास जी ने विक्रम, कालिदास या उज्जयिनी के नाम पर मंदिर मठ नहीं बनवाए, बल्कि शिक्षा अनुसंधान और कला संस्कृति के शोध संस्थान और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। हालांकि उनकी यह प्रक्रिया समाज को भरने के प्रयास में खुद को खाली करने की रही। आज जब भारत को आजाद हुए एकहत्तर वर्ष से भी ऊपर होने जा रहे हैं, तब भी हम अपने सांस्कृतिक-साहित्यिक मूल्यों और अवदानों से कितने अपरिचित हैं। तरस आता है हमारे राष्ट्र के कर्णधारों पर जो राष्ट्र को इक्कीसवीं शताब्दी में ले जाने की बात करते हैं। वे ईसा सन-संवत् से सोचते हैं। संभवत: इन ‘शक’ और ‘हूण’ वंशजों को यह ज्ञात नहीं होगा कि हम इक्कीसवीं शताब्दी में पहले से ही मौजूद हैं। मगर अभी भी कानों में कोई पिघला हुआ सीसा डालता है, जब हम सुबह आकाशवाणी से रेडियो के कान उमेठते ही सुनते हैं, आज दिनांक… है, तदनुसार शक संवत्…!