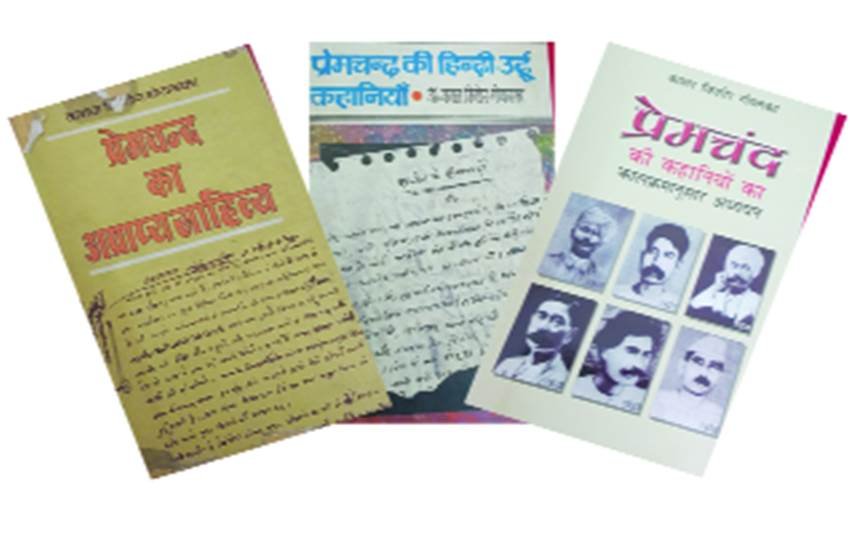प्रेमचंद का मानना है कि इतिहास की किताबों में तारीखों के अलावा सब कुछ कल्पना होती है। उपन्यासों में तारीखें काल्पनिक होती हैं और बाकी सब सच होता है। प्रेमचंद का साहित्य अपने कालखंड का इतिहास ही है। वहीं इतिहासकार इएच कार कहते हैं कि इतिहास अतीत से लेकर आज तक का निरंतर संवाद है। प्रेमचंद औपनिवेशिक काल में ऐसा साहित्य रच गए थे, जो आज आजादी के छह दशक बाद भी समाज के साथ कदमताल करता है। इसलिए खासकर हिंदी पट्टी में राजनीति और समाज का हर खेमा प्रेमचंद को अपना बनाना चाहता है। कमल किशोर गोयनका सीधे प्रेमचंद के साहित्य से जुड़ते हैं। प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन के लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। गोयनका का कहना है कि प्रेमचंद के साहित्य पर शोध करने के लिए पूरा एक जीवन भी कम है। साथ ही वे आगाह करते हैं कि शोध कार्य में भावुकता नहीं, सिर्फ तथ्य चलते हैं। पेश है उनके साथ बातचीत का संक्षिप्त अंश:
प्रश्न – हिंदी साहित्य का एक विद्यार्थी खासतौर पर प्रेमचंद का अध्येता कैसे बना?
उत्तर – मैं उत्तर प्रदेश के एक गोयनका परिवार का इकलौता आदमी था, जिसने अपनी आजीविका के लिए कारोबार के बजाय अकादमिक क्षेत्र को चुना। मैंने 1961 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया और 1975 में पीएचडी। मेरे शोध का विषय था, ‘प्रेमचंद का शिल्प-विधान’। इसके साथ ही प्रेमंचद पर शोध का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब भी चल रहा है। अब मुझे लगता है कि प्रेमचंद जितना काम कर गए हैं, उसके लिए एक पूरा जीवन कम है।
प्रश्न – हिंदी साहित्य में शोध की जो स्थिति है, उसके बरक्स आपका काम काफी महत्त्वपूर्ण है। एक अध्येता के रूप में शोध और साहित्य पर क्या कहना चाहेंगे?
उत्तर – शोध के लिए ज्ञान की निरंतरता, उसकी सोच की निरंतरता बहुत जरूरी है। शोध में गलतियां होंगी और आपको अपने किए कठिन परिश्रम को खारिज करके आगे बढ़ना होगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदी में पीएचडी के बाद लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। लोग तथ्यों पर कम और अपनी विचारधारा पर ज्यादा ध्यान देते हैं।
प्रश्न – प्रेमचंद को लेकर स्थापित स्थापनाओं को आपके शोध ने खारिज कर दिया। प्रेमचंद की स्थापित छवि को आपने तथ्यों के साथ तोड़ा और एक नए प्रेमचंद को सामने लेकर आए।
उत्तर – प्रेमंचद के बारे में सबसे बड़ा भ्रम यह फैलाया गया कि वे गरीबी में रहे। दरअसल, भारतीय कम्युनिस्ट प्रेमचंद की सर्वहारा की छवि बना कर हिंदी पट्टी में अपने विमर्श की पैठ बनाना चाहते थे। उनके पास हिंदी पट्टी में पैर जमाने का कोई आधार नहीं था। इसलिए सर्वहारा वर्ग से जोड़ने के लिए उनकी छवि ऐसी बनाई गई कि निधन के बाद उनके पास कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। मैंने प्रेमचंद के निजी दस्तावेजों तक अपनी पहुंच बनाई। उनकी सर्विस बुक, उनके बैंक खाते बताते हैं कि वे कभी भी गरीब नहीं थे। वे एक मध्यवर्गीय व्यक्ति थे, जिनकी अपने समय के हिसाब से ठीक-ठाक आमदनी थी। एक छोटा-सा उदाहरण: वे 1936 में दिल्ली आए थे। दो कहानियों का पाठ किया था, जिसके लिए उन्हें सौ रुपए मिले, जो उस समय के हिसाब से बड़ी रकम थी। 1929 में उन्होंने अपनी बेटी की शादी में सात हजार रुपए खर्च किए। 1929 में वे बंबई गए और फिल्म कंपनी में उनकी तनख्वाह आठ सौ रुपए महीना थी। उनके देहांत के चौदह दिन पहले बनारस बैंक के उनके खाते में लगभग चौवालीस सौ रुपए थे। कहने का मतलब यह है कि उनकी छवि ऐसी बनाई गई कि वे ऐसे सर्वहारा वर्ग से थे, जिसने समाज को बहुत कुछ दिया, लेकिन समाज से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। प्रेमचंद के साधारण कपड़े और फटे जूतों की भी चर्चा होती है। यह तो उस समय की संस्कृति थी कि लोग अपनी हैसियत का दिखावा नहीं करते थे! हां, यह सच है कि उन्होंने धन की सत्ता का विरोध किया। लेकिन उनके पास कफन लायक भी पैसे नहीं थे, इससे बड़ा झूठ कुछ और नहीं हो सकता।
प्रश्न – प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। तो प्रेमंचद की मशाल कहां थी?
उत्तर – दावा किया जाता रहा है कि प्रेमचंद अपने अंतिम समय में मार्क्सवादी हो गए थे। ये पंक्तियां प्रेमचंद की हैं कि रूस विचार का साम्राज्य स्थापित करना चाहता है… साम्यवाद पूंजीवाद से भी भयानक हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर साम्यवाद जनता के विरोध में होगा, तो जनता उसे बदल देगी। ‘गोदान’ के प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि कम्युनिस्ट हो तो कम्युनिस्ट की तरह रहो। प्रगतिशील लेखक संघ के बहुप्रचारित भाषण में वे छह से सात जगह आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक संतोष की बात करते हैं। मन के संस्कार की बात करते हैं। यह मार्क्सवाद की शब्दावली नहीं है। वे प्रगतिशील शब्द को ही निरर्थक मानते हैं, क्योंकि लेखक होता ही प्रगतिशील है। वे प्रगतिशीलता की मार्क्सवादी व्याख्या ग्रहण नहीं करते हैं। सितंबर 1936 के ‘हंस’ के आखिरी अंक में उनका बहुप्रसिद्ध लेख ‘महाजनी सभ्यता’ छपा है, जिसका मार्क्सवादी अक्सर उल्लेख करते हैं। लेकिन इसी अंक में उनकी कहानी ‘रहस्य’ भी छपी है। ‘रहस्य’ मनुष्य में देवत्व की खोज की कहानी है। यह शुद्ध आदर्शवाद है। उन्होंने कहा कि मेरे साहित्य के दो उद्देश्य हैं- स्वराज प्राप्ति और भारतीय आत्मा की रक्षा करना। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता का पुरजोर विरोध किया। वे पश्चिम की कृत्रिमता पर भारतीयता की छाप लगाना चाहते हैं। उन जैसा सांस्कृतिक और राष्टÑीय लेखक उस काल में नहीं है। उनके साहित्य का आधार भारतीय आत्मा से जुड़ा हुआ है। साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, लेकिन मार्क्सवादियों ने राजनीति को साहित्य के आगे खड़ा कर दिया।
प्रश्न – ’‘महाजनी सभ्यता’ और ‘रहस्य’… दोनों में प्रेमचंद की वसीयत क्या होगी?
उत्तर – ‘रहस्य’ शुद्ध आदर्शवादी और मनुष्य के सेवाभाव की कहानी है। इसे आप विवेकानंद का प्रभाव कह सकते हैं। प्रेमचंद का एक भी चरित्र अहिंसा पर हिंसा की विजय नहीं दिखाता है। उन पर गांधी छाए हुए हैं। उनकी एक कहानी है, ‘कैदी’ जिसकी चर्चा बहुत कम की जाती है। इसके किरदार बताते हैं कि लेनिन के कॉमरेड कैसे एक-दूसरे को धोखा दे रहे हैं। मैंने इन सबकी व्याख्या की तो मुझ पर आरोप लगे कि गोयनका प्रेमचंद को हिंदू बना रहे हैं।
प्रश्न – उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद के बरक्स अगर आज हम राष्ट्र-राज्य, राष्टÑवाद और अस्मिता संबंधी विमर्श देखें तो क्या प्रेमचंद यहां भी प्रासंगिक हैं?
उत्तर – तब और क्या! प्रेमचंद की कहानी शुरू होती है 1928 में सोजे-वतन से। प्रेमचंद दूसरे देशों से भी चरित्र लाते हैं। हिंदू-मुसलिम झगड़े और आतंकवाद के नजरिए से भी उनकी कहानी है। उनकी कहानी ‘जिहाद’ 1928-29 की है, जो अफगानिस्तान की है। पश्चिमोत्तर के पर्वत-प्रदेश में पठानों के जिरगे हमेशा लड़ते रहते थे। यहां पर हिंदू परिवार शांति से रहता था। लेकिन एक मुल्ला ने पठानों में धर्म का भाव जागृत कर दिया, जिसके बाद वे हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं। नायिका श्यामा जिहादियों के डर से खुदा पर ईमान जताने वाले धर्मदास की इसलिए भर्त्सना करती है कि उसने प्राणों के लिए धर्म का त्याग किया। वहीं जिहादी की तलवार की नोक पर खड़ा किरदार खजानचंद कहता है, ‘तुम एक हिंदू से यह प्रश्न कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि जान के खौफ से वह अपना ईमान बेच डालेगा? हिंदू को अपने ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी नबी, वली या पैगंबर की जरूरत नहीं है’। यही खजानचंद जिहादियों से कहता है, ‘मैं अपने को तुमसे ज्यादा खुदापरस्त समझता हूं। मैं उस धर्म को मानता हूं, जिसकी बुनियाद अक्ल पर है। आदमी में अक्ल ही खुदा का नूर है और हमारा ईमान हमारी अक्ल’। प्रेमंचद सांप्रदायिक एकता को आवश्यक मानते थे, लेकिन मतांध मुसलमानों द्वारा हिंदू जनता पर किए अत्याचारों का भी उल्लेख करते थे। लेकिन वे इस्लाम धर्म की शर्तों और ईमानदारी का भी सम्मान करते हैं। उनकी ही कहानी है, ‘भारत माता की जय’। 1908 की कहानी है ‘दुनिया का सबसे अनमोल रत्न’। इसका किरदार अपने देश की मिट्टी को ही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मानता है। अट्ठाईस साल की उम्र में लिख रहे प्रेमचंद का किरदार बोलता है, ‘यही मेरी मातृभूमि है’। उनके चरित्रों में राष्ट्रीय चेतना का उभार है। जनसंख्या जैसी बड़ी समस्या जिस पर आज भी कोई राजनीतिक दल या नेता ईमानदारी से बोलने में परहेज करता है, प्रेमचंद उसे अपनी कहानी में उठा चुके हैं। उनकी कहानी ‘गमी’ परिवार नियोजन पर है। इसमें तीसरा बच्चा होने पर परिवार का मुखिया गमी का आयोजन करता है। प्रेमचंद के समय में भारत की जनसंख्या तीस करोड़ हो चुकी थी। तो उनकी सोच का विस्तार देखिए।
प्रश्न – प्रेमंचद बनाम दलित मुद्दे पर भी काफी सवाल उठते रहे हैं।
उत्तर – ‘रंगभूमि’ जलाई गई थी। ‘निर्मला’ को हटा कर ‘ज्यों मेहंदी के रंग’ का पाठ लगाया गया था। रंगभूमि के संक्षिप्त संस्करण से ‘चमार’ शब्द हटा दिया गया था। प्रेमचंद को ‘कफन’ के सहारे बदनाम किया जाता रहा है। लेकिन प्रेमंचद का दलित किरदार मंदिर का ताला तोड़ता है। समय के हिसाब से इसे ऐतिहासिक साहस कहा जा सकता है। ‘सद्गति’ में वे कोई समाधान नहीं देते, लेकिन ब्राह्मणों की चरम क्रूरता को दिखा कर उनके प्रति घृणा भाव पैदा करते हैं।
प्रश्न – प्रेमचंद भातीय समाज के आगे के स्वरूप को भी देख रहे थे..!
उत्तर – आपको आश्चर्य होगा कि उस दौर में प्रेमचंद ने अपनी कहानी में सहजीवन जैसा मुद्दा उठाया था। ‘मिस पद्मा’ अपने पुरुष साथी के साथ बिना शादी के रहने का फैसला करती है। इस रिश्ते का अपना उतार-चढ़ाव है। कहानी के अंत में नायिका अपने छत से बग्घी पर जाते हुए एक यूरोपीय परिवार को देखती है और अपनी स्थिति से उसकी तुलना करती है। परिवार बरक्स साथी के साथ अकेले रहने का चुनाव। समय और समाज की पहचान में प्रेमचंद का कोई सानी नहीं। उनके साहित्य में तीन हजार से ज्यादा किरदार हैं। दुनिया के इतिहास में इतने ज्यादा चरित्र कहीं नहीं मिलते हैं। यही ‘वेरायटी’ उन्हें अमरत्व प्रदान करती है।