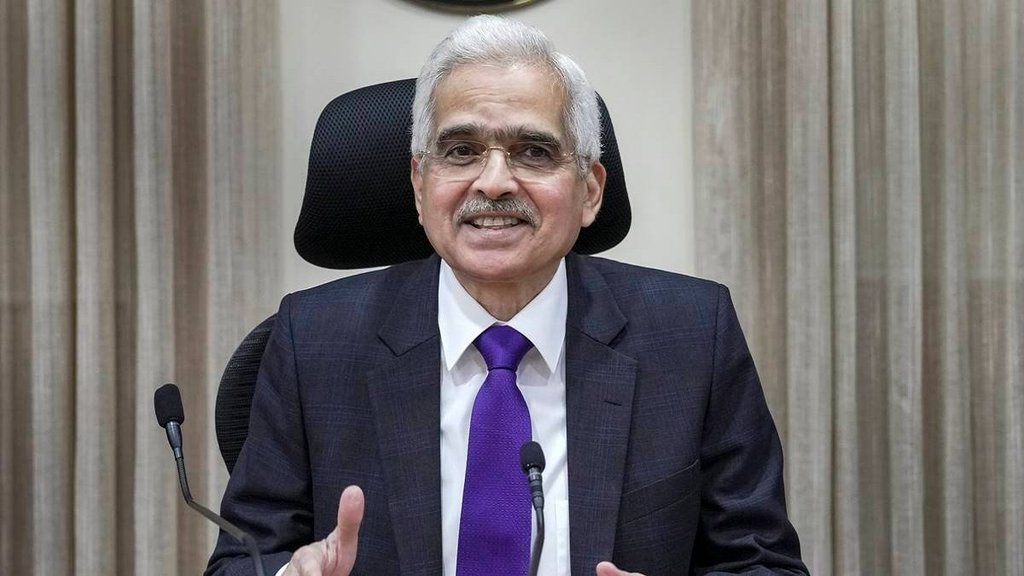एक वक्त था, जब भारतीय रिजर्व बैंक तमाम आर्थिक मामलों के लिए ‘खुदमुख्तार’ निकाय हुआ करता था। इस तक आम लोगों की पहुंच दुर्गम थी, मगर इसे स्वतंत्र और समझदार संस्था माना जाता था। कई बड़ी विफलताओं के बावजूद इसकी प्रतिष्ठा पर कोई दाग नहीं लगा था। इसकी सबसे उल्लेखनीय विफलता उस वित्तीय घोटाले को पहचानने में हुई चूक थी, जिसमें शेयर दलालों और बैंक अधिकारियों ने उसकी नाक के नीचे रचा (1992) और हजारों करोड़ रुपए लूट लिए थे।
‘आरबीआइ ने सरकार के साथ खुद मिलीभगत की थी’
बिल्कुल हाल की विफलता सरकार का नोटबंदी (2016) का लापरवाह साहसिक फैसला है, जिसमें आरबीआइ ने सरकार के साथ खुद मिलीभगत की थी। केंद्रीय बैंकों के फैसलों के मद्देनजर, ब्याज दरें निर्धारित करने के मामले में कई मौकों पर आरबीआइ के फैसलों को अनुचित माना गया है।
फिर भी, मेरा मानना है कि आरबीआइ ज्ञान का भंडार है। खासकर, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग और सांख्यिकीय विश्लेषण तथा कंप्यूटर सेवा विभाग डेटा के सबसे विश्वसनीय भंडारगृह हैं। दोनों विभागों में आला दर्जे के कर्मचारी हैं, जो उत्तम विश्लेषण करने और नीतिगत सलाह देने में सक्षम हैं।
आरबीआइ ने बौद्धिक आलस्य या बाहरी मजबूरियों से प्रतिष्ठा को धूमिल होने दिया
आरबीआइ के मासिक बुलेटिन को बैंकर, अर्थशास्त्री, विद्वान और नीति निर्माता व्यापक रूप से पढ़ते और उस पर भरोसा करते हैं। मगर यह अफसोस की बात है कि आरबीआइ ने अपने बौद्धिक आलस्य या बाहरी मजबूरियों के चलते अपनी अच्छी-खासी प्रतिष्ठा को धूमिल होने दिया।
मार्च 2023 की मासिक आरबीआइ बुलेटिन में ‘अर्थव्यवस्था की स्थिति’ पर एक नियमित आलेख है। इसके साथ सामान्य चेतावनी प्रकाशित है कि ‘इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं, ये विचार भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते’! जबकि तथ्य यह है कि लेखक ‘आर्थिक विश्लेषण और नीति’ विभाग से जुड़े हैं और फिलहाल आरबीआइ के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा के नेतृत्व में काम करते हैं।
बयानबाजी
मेरी तकलीफ इस बात को लेकर है कि जिस लेख में अर्थव्यवस्था को लेकर एक तर्कपूर्ण और शालीन मूल्यांकन होना चाहिए था, उसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में असाधारण दावे किए गए हैं। उनमें से कुछ दावे यहां प्रस्तुत हैं:
- इस विस्तार की अंतर्निहित शक्ति उच्च मुद्रास्फीति के बने रहने में स्पष्ट है।
- श्रम बाजार की शक्ति आश्चर्यजनक रूप से उभर कर सामने आई है, यह दरअसल ढांचागत बदलावों को दर्शाती है: बड़ी तकनीकी कंपनियों में जो नौकरियां चली गई थीं, उनकी भरपाई आतिथ्य, खुदरा और स्वास्थ्य देखभाल आदि क्षेत्र बड़ी तेजी से कर रहे हैं।
- भारत महामारी के दौर से उबर आया है और शुरू में जितना सोचा गया था उससे कहीं अधिक मजबूत हुआ है… इस तेज रफ्तार सुधार का आकलन साल-दर-साल की विकास दर से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे निर्माण द्वारा सांख्यिकीय आधार के प्रभावों से प्रभावित होते हैं।
- क्या होगा अगर केंद्रीय बजट में प्रस्तावित 35,000 करोड़ रुपए की कर राहत का कम से कम पचास फीसद करदाताओं द्वारा उपभोग के लिए उपयोग किया जाए और निजी अंतिम उपभोग व्यय में जोड़ा जाए?
- अगर प्रभावी पूंजीगत व्यय के लिए बजट में रखे गए 3.2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन का एक तिहाई हिस्सा भी सकल स्थिर पूंजी निर्माण में जुड़ जाए, तो क्या होगा?
- वैश्विक अर्थव्यवस्था के बरक्स, भारत की आर्थिक विकास दर धीमी नहीं होगी- इसमें 2022-23 में पर्याप्त विकास की गति बनी रहेगी।
निस्संदेह, ये बहुत साहसिक बयान हैं। चलिए अब, जो कुछ हमने सुना, देखा, पढ़ा और अनुभव किया है, उनके आलोक में इन बयानों की बारीकी से जांच करते हैं। इन बयानों के विरोधाभासी आंकड़े ये हैं कि: *मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और इसने निजी खपत को नीचे धकेल दिया है। *तकनीकी कंपनियों द्वारा की गई छंटनी, आतिथ्य या खुदरा उद्योगों में उपलब्ध नौकरियों के समान नहीं है। *तिमाही-दर-तिमाही, यहां तक कि अनुक्रमिक तिमाहियों में भी, कम विकास दर दर्ज की गई है (आलेख का चार्ट 12)। *‘क्या होगा अगर’ तर्क पूरी तरह से अटकलबाजी हैं: क्या होगा अगर 35,000 करोड़ रुपए का बड़ा हिस्सा घरेलू कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? और क्या होगा अगर अतिरिक्त आबंटन केंद्र द्वारा लगाई गई कठोर शर्तों को पूरा करने में असमर्थता के कारण राज्यों द्वारा खर्च नहीं किया जा सकता है (जैसा कि 2022-23 में हुआ था)? *‘भारत की विकास दर धीमी नहीं होगी’ केंद्रीय बैंकों के लिए एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी है, मानो भारत ने खुद को दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग कर लिया है।
हकीकत
मैं जीवन में विभिन्न क्षेत्रों के बहुत सारे लोगों से मिलता और उनसे बातचीत करता हूं। हाल के दिनों में मैंने लेखकों, वकीलों, एक नाई, ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों, एक पूर्व मेयर, एक तमिल विद्वान, साहित्यकारों, पार्टी कार्यकर्ताओं, एक मध्यम उद्यम के मालिक, पत्रकारों, एक प्रधानाध्यापक, एक एनजीओ प्रमुख, एक होटल व्यवसायी और कई युवा छात्रों से मिला। उनमें से किसी ने भी अर्थव्यवस्था को लेकर संतोष प्रकट नहीं किया। उनकी मुख्य चिंता महंगाई, बेरोजगारी, छंटनी, सुस्त मांग (विशेष रूप से निर्यात) और कम खपत को लेकर थी।
संकट के सामान्य बिंदुओं को परे रखते हुए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि निजी उपभोग की रफ्तार धीमी हो गई है और उसमें उदासी पसरी हुई है। जबकि सरकारी पूंजीगत व्यय में वृद्धि हो सकती है, सरकारी अंतिम खपत में गिरावट आई है। एक होटल व्यवसायी एक औद्योगिक शहर में इक्कीस कमरों का मामूली कीमत वाला होटल चलाता है।
उसके होटल में औसतन 9-10 कमरे या पचास फीसद से कम भर पाते है। एक छोटे और मंझोले उद्यम के मालिक वस्त्र निर्माता और निर्यातक फर्मों से मिले आर्डरों का आधा ही तैयार उत्पाद आपूर्ति कर पाते हैं। उनके पास साठ सीटों वाला कारखाना है, लेकिन उन्हें महीने में कुछ दिन उत्पादन बंद करना पड़ता है।
उन्होंने बताया कि कभी वे एक सफल व्यवसाय समूह हुआ करते थे, जो अंतरराष्ट्रीय ब्रांड मालिकों के लिए वस्त्र बनाते और आपूर्ति किया करते थे: उनके कारखाने हफ्ते में सातों दिन चलते थे, मगर अब सप्ताह में पांच दिन ही चलते हैं। उस औद्योगिक शहर में कई सौ करोड़ रुपए का वस्त्र भंडार है और वे विदेशी खरीदारों को छूट भी दे रहे हैं।
मगर जर्मनी ने साफ कर दिया है कि अगले साल तक किसी बड़े निर्यात आदेश की उम्मीद नहीं की जा सकती। माल के निर्यात और आयात दोनों में संकुचन आया है। कर्ज लेने की लागत अधिक है और यह बढ़ भी सकती है। शहरी क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित नहीं हो पा रहे हैं। अखिल भारतीय बेरोजगारी दर 7.4 फीसद (सीएमआइई) है। आप किस पर विश्वास करना चाहेंगे? अपने कानों, आंखों और पूर्वानुभवों पर या आरबीआइ की मासिक बुलेटिन के चक्करदार सांख्यिकीय और मौखिक दावों पर?