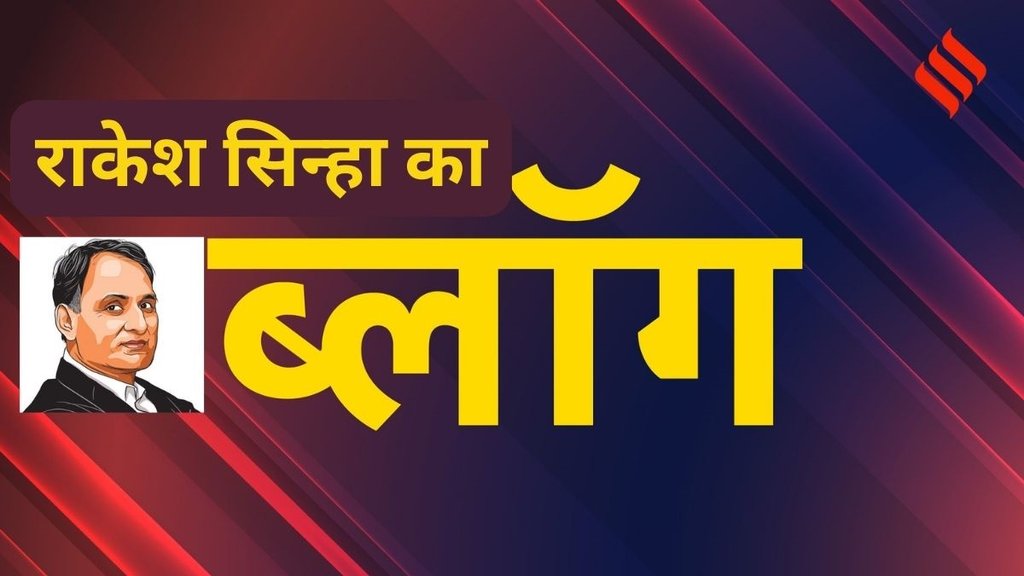वक्फ पर देश में अत्यंत ही सीमित चर्चा होती है। साधारण शब्दों में, परोपकार के उद्देश्य से दान में दी गई संपत्ति को वक्फ कहते हैं। दान, सेवा, परोपकार तो मानवीय वृत्ति है, जो हर युग और हर समाज में पाई जाती है। पर इसे भी धर्मों की श्रेणी में बांट दिया गया। स्वतंत्र भारत में 1954 में मुसलिम वक्फ कानून बना। दुर्भाग्य से 1954 में संसद की बहस के बाद इस पर बहस का दायरा 9.4 लाख एकड़ जमीन और आठ लाख से अधिक संपत्तियों के सिर्फ रखरखाव और इसके प्रबंधन के लोकतंत्रीकरण तक सिमट कर रह गया है।
साधारणतया लोग वक्फ जैसे विषय को धर्म-विशेष का मामला मानकर रुचि नहीं लेते हैं। ऐसी बातों को जानने और समझने को बोझ मानते हैं। इसी को अनभिज्ञता की विलासिता कहते हैं। फिर इस पर वैचारिक वर्चस्व हो जाता है। यह किसी भी समाज, जो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को साधन और साध्य, दोनों मानता है, के लिए घातक है।
सामान्य लोगों की इसी वैचारिक शिथिलता ने स्वतंत्रता के बाद नागरिक जीवन से जुड़े मामलों में औपनिवेशिक सामाजिक दृष्टिकोण, जो सांप्रदायिक संरचनाओं को प्रोत्साहित करता था, को ही आगे बढ़ाया। वह भी तब, जब कांग्रेस के भीतर बड़ा वर्ग इसके विरुद्ध मुखर था।
राज्यसभा में 1954 में वक्फ कानून पर बहस के दौरान कांग्रेस के ही राजगोपाल नायडू ने अपने नेतृत्व को कठघरे में खड़ा करते हुए सरकार पर पिछले दरवाजे से सांप्रदायिक कानून थोपने का आरोप लगाया। जो वक्फ कानून 1954 में बना, वह कांग्रेस के लोकसभा सदस्य सैयद मोहम्मद काजमी का ‘प्राइवेट मेंबर’ बिल था। सरकार का परोक्ष समर्थन इसी बात से जाहिर है कि इसे जब ‘सेलेक्ट कमिटी’ में विचारार्थ भेजा गया, तब स्वयं कानून और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री चारुचंद्र विश्वास उसके अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस के ही सदस्य हर प्रसाद सक्सेना ने 23 अप्रैल, 1954 को राज्यसभा में कहा कि ‘जहां तक इस विधेयक का मामला है, यह हमारे साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है। यह विधेयक सांप्रदायिक प्रकृति का है।’ इस तुष्टिकरण में अमंगल देखने वाले वे अकेले नहीं थे।
कांग्रेस के कैलाश बिहारी लाल ने राज्यसभा में बहस के दौरान चेताया था कि सांप्रदायिकता की कोई सीमा नहीं होती है और वक्फ कानून के बाद सभी धर्मों में अलग-अलग कानून की मांग बढ़ेगी। उन्होंने जो कहा, वह आज हकीकत है। लाल ने कहा कि ‘ऐसा कानून बनाकर हम केवल अपने राष्ट्र के बिखराव और (धर्मों को) सामाजिक जीवन में अलग अस्तित्व बनाए रखने की अनुमति दे रहे हैं। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 44 का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।’
विडंबना देखिए कि देश में तब धर्मनिरपेक्ष कानून विद्यमान था। मुबंई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट अधिनियम- 1950, सभी धर्मों के दान से प्राप्त संपत्तियों के लिए सफलतापूर्वक कार्यरत था। उच्च न्यायालय ने भी इसको मिली चुनौती को खारिज कर धर्मनिरपेक्षता के मिसाल के रूप में देखा था। पर हुआ उल्टा। सरकार ने इसे ही निरस्त कर मुसलिम वक्फ अधिनियम को थोप दिया। ऐसी संरचना के बनने से हमारे दृष्टिकोणों में उतरोत्तर भेदभाव और अलग-थलग रहने की प्रवृत्ति बढ़ती है। धर्मनिरपेक्षता के लिए अधिकतम परस्पर सहयोग, संवाद और दुख-सुख में सहभागिता आवश्यक होती है। पर छोटे-छोटे सामाजिक प्रश्नों पर सांप्रदायिक तुष्टीकरण के आधार पर कानून बनाया जाता रहा। इसी संदर्भ में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य पीवी काणे ने 1954 में बहस के दौरान सवाल किया था कि वक्फ की संपत्ति का उपयोग ‘मानवता के लिए होगा या सिर्फ मुसलमानों के लिए’। सरकार ने कांपती आवाज में अपाच्य तर्क दिया: ‘सबके लिए एक कानून बनाने की तैयारी में थी ही कि ‘प्राइवेट मेंबर’ बिल आ गया।’
भारतीय परंपरा में परोपकार, सेवा, दान का एक ही लक्ष्य मानवता है। यह सभी संकीर्णताओं को पराजित करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेट में अनाज और निर्बल की सहायता में धर्म-जाति की क्या भूमिका है? राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों में अनुच्छेद 44 सबसे महत्त्वपूर्ण प्रावधान है, जिसमें संविधान सभा की सामाजिक एकता और ‘एक जन’ का भाव निहित है। राजनीति ने उसी को बेमानी करने का काम किया। ऊंची आवाज में सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलने से इसका अंत न हुआ, न होगा। इसके उपजने का कारण ढूंढ़ना होता है। पर सत्तावादी बनकर यह कतई नहीं हो सकता है। स्वतंत्र भारत की राजनीति इसका जीता-जागता गवाह है। सांप्रदायिक मानसिकता उपार्जित करना आसान होता है, पर उस पर लगाम लगाना अत्यंत दुष्कर होता है।
कांग्रेस के हरि विनायक पातस्कर लोकसभा में 12 मार्च 1954 को वक्फ कानून को धर्मनिरपेक्षता की मूल भावना से भटकाव देख रहे थे, पर कांग्रेस नेतृत्व उन सबको अनसुना करता रहा। उन्होंने लोकसभा में कहा था- ‘संविधान में हमने अपना उद्देश्य रखा है। हम तत्काल उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। हिंदू, मुसलिम, ईसाई आदि के लिए तत्काल एक सिविल कानून बनाना संभव नहीं है। उस लक्ष्य तक पहुंचने में समय लग सकता है। लेकिन इस छोटे से मामले में एक प्रगतिशील राज्य (तत्कालीन बंबई) में एक कानून है, जो सब पर लागू होता है। फिर हम इस कानून (वक्फ) को क्यों पारित कर रहे हैं, जो भेदभाव पर आधारित है? इस कानून का परिणाम क्या होगा? यह बिखराव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।’
वक्फ को लेकर विवाद सतत चलता रहा है। निजी और राज्य के अधीन संपत्तियों पर भी वक्फ दावा करता रहा है। शाश्वत समिति (2011) ने इसकी संपत्ति से बारह हजार करोड़ रुपए वार्षिक आय का अनुमान लगाया था, जो 163 करोड़ तक रुक गया था। वक्फ संपत्ति का उपयोग और बोर्ड का गठन तात्कालिक पक्ष है। बड़ी तस्वीर दीर्घकालिक समाधान में निहित है। दान के लिए एक समान नागरिक कानून ही पंथनिरपेक्षता के अनुकूल होगा। ऐसा न करना संविधान की प्रस्तावना के चीरहरण की तरह है। आखिर कब तक हम मानवीय प्रश्नों को भी सांप्रदायिकता की काली कोठरी में छोड़कर ‘एक राष्ट्र एक जन’ की महत्त्वाकांक्षा को कुचलते रहेंगे? यह नहीं भूलना चाहिए कि सांप्रदायिकता का संक्रमण भस्मासुर पैदा करता है।