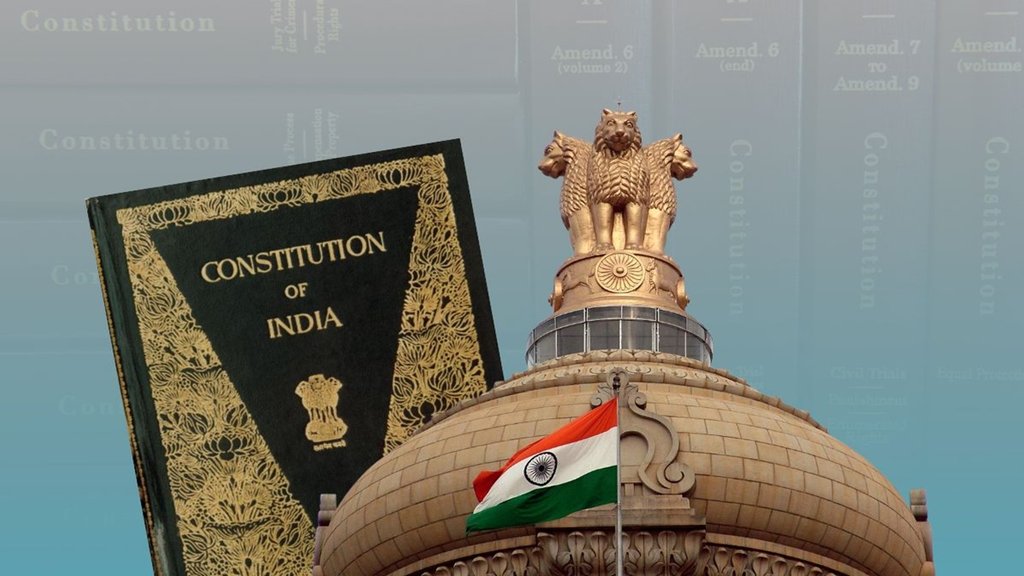बिपिनचंद्र पाल भारत के सुलझे चिंतकों में एक थे। उन्होंने समकालीन भारतीय मस्तिष्क पर एक टिप्पणी की थी। हम बीती बातों में इतने उलझ जाते हैं कि हमारी प्रकृति प्राचीन या पुरातत्त्ववादी बन जाती है। हालांकि वे स्वयं संस्कृति और सभ्यता की उपलब्धियों को अपने लेखन और भाषण में महत्त्व देते थे, पर वहीं ठहरते नहीं थे। वे भूत को निखारते हुए भविष्य को निहारते थे। विरासत हमारी ताकत है। पर उसकी परिक्रमा करते रहना कमजोर वर्तमान और भविष्य के प्रति लापरवाही है।
भारत के प्राचीन इतिहास को दबाकर रखा गया
चूंकि भारत के प्राचीन इतिहास को दबाकर रखा गया, इसके दर्शन की उपेक्षा की गई, विवेक, विद्वता और विवेचन से पूर्ण रचनाओं, वेद, उपनिषद, महाभारत आदि को अध्यात्म की श्रेणी में रखकर पीढ़ियों को उससे दूर रख दिया गया। इसलिए विरासत पर बल देने की जरूरत महसूस होना स्वाभाविक ही है। लेकिन यह बौद्धिक आलस्य का कारण भी बन गया। हमारी लेखनी और भाषणों में प्राचीन घटनाएं, साहित्य और नायक आसानी से उद्धृत होते हैं। पर यहीं विराम लग जाना बौद्धिक चोरी वैसे ही है जैसे परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी कुंजी से काम चलाता है।
विरासत के अध्ययन के लिए भी भारत में सबल ‘थिंक टैंक’ नहीं है
विरासत के अध्ययन के लिए भी भारत में सबल ‘थिंक टैंक’ नहीं है। और जो हैं भी, वहां समझ तो बहुत है, पर सोच का संकट है। सिर्फ पुरानी पुस्तकों, पांडुलिपियों, चित्रों के संग्रह से संतुष्ट रहते हैं। विडंबना है कि हम अपनी सभी पांडुलिपियों को नहीं जान पाए हैं, पढ़ना तो दूर। एक अनुमान के अनुसार देश में चार करोड़ पांडुलिपियां हैं, जो हमारे प्राचीन इतिहास की जीवंत गवाह हैं।
जब हम दर्शन, अध्ययन, विमर्श के क्षेत्र में शिखर पर थे, तब पश्चिमी दुनिया ताकत के तर्क में उलझी हुई थी। पर अब स्थिति भिन्न हो चुकी है। पश्चिम ने विचार की ताकत और महत्त्व, दोनों को समझा है। इसलिए पिछली तीन शताब्दियों से इसकी कोशिश रही है कि विचारों के सृजन और संवाद पर दुनिया में इसका एकाधिकार रहे। ब्रिटेन के आक्सफोर्ड और अमेरिका के हावर्ड विश्वविद्यालयों का लक्ष्य दुनिया भर के श्रेष्ठ चिंतकों को स्थान और हर सूक्ष्म विषयों पर भी शोध होता है। भारत के प्राचीन दर्शन और साहित्य पर भी उन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी में अध्ययन शुरू कर दिया था। उनके सृजन पर निर्भरता बढ़ती गई। मौलिकता का यह ह्रास भारत के स्वभाव के प्रतिकूल है।
पश्चिम के समाज ने राज्य को विचारों का एकाधिकारवादी बनने नहीं दिया
विचारों का सृजन तो व्यक्ति करता है, पर उसका परिष्कार और संस्थागत रूप समूहों में सत्संग से होता है। पश्चिम के समाज ने राज्य को विचारों का एकाधिकारवादी बनने नहीं दिया। जबकि नवस्वतंत्र देशों के राजनेताओं या राज्य ने अपने आपको विचारों का अंतिम सृष्टिकर्ता मान लिया। बौद्धिक वर्ग उसी का व्याख्याकार भर बन गया। करिअरवादी सबसे कमजोर तबका होता है। विचार का उनके हाथों में रहना उनके पतन के लिए पर्याप्त है। परिणामस्वरूप राज्य और जनता के बीच या राजनीतिक दलों में नेतृत्व एवं कार्यकर्ता के बीच जो विचार समूह होना चाहिए, वह सिर्फ साइनबोर्ड या भाषण तैयार करने की एजंसी के रूप में है।
आज विश्व में लगभग 6500 विचार समूह हैं, जिसमें अकेले अमेरिका में 1875 हैं। भारत 509 की संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है, पर गिने-चुने ही प्रभावी हैं। अधिकांश छोटी-मोटी रपट जारी कर या एक-दो सेमिनार कर अपना काम पूरा मान लेते हैं। न तो शोधकर्ता उनके पास हैं, न ही अपेक्षित संसाधन। उद्देश्य भी अस्पष्ट होता है।
अमेरिका में आप्रवासन की समस्या पर ‘सेंटर फार इमीग्रेशन स्टडीज’ और ‘फेडरेशन आफ इमीग्रेशन रिफार्म’ जैसी थिंक टैंक गंभीरता से अध्ययन करती है। भारत में विस्थापितों और घुसपैठियों की बड़ी संख्या है। उस पर कानून/ प्रस्ताव/ भाषण की प्रचुरता तो है, पर प्रामाणिक अध्ययन नहीं होता है। पश्चिम के ‘थिंक टैंक’ ने नीति विशेषज्ञों और नीतियों को जन्म दिया। कूटनीति में नाम कमाने वाले हेनरी किसिंजर हूवर इंस्टीट्यूट से जुड़े थे तो ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट ने ‘मार्शल प्लान’ बनाया था, जिसके तहत अमेरिका ने 13.3 खरब डालर की सहायता पश्चिमी यूरोप के देशों को की थी।
ब्रिटेन में 1884 से ‘फेबियन सोसाइटी’ चल रही है। इसके विचार से प्रतिकूल मत वाला एडम स्मिथ इंस्टीट्यूट है। लंदन में स्थित चैथम हाउस एक स्वतंत्र मंच है, जो 1920 से अनवरत सक्रिय है, जिसकी वैश्विक पहचान है। इसी चैथम हाउस में 20 अक्तूबर, 1931 को महात्मा गांधी का ‘भारत के भविष्य’ पर प्रसिद्ध भाषण हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अहिंसा के मार्ग पर चलने से ‘दुनिया का कोई देश अपनी इच्छानुसार भारत को झुका नहीं सकता है।’
गैर पश्चिमी देशों ने स्वतंत्र विचार समूहों को पनपने नहीं दिया। जो पनपे वे राजनीति के पालने में पहुंच गए। विचार समूह की प्रकृति शुद्ध वैचारिक होती है। यह विचारों के आईने में तथ्यों से तर्क गढ़ता है और इसी बौद्धिक मंथन नीति निर्माण से लेकर जनमत तैयार करने तक आलोचनात्मक भूमिका होती है।
भारत में हाल के वर्षों में सभी छोटे-बड़े औद्योगिक घरानों ने अपना-अपना ‘थिंक टैंक’ बना रखा है। इनकी रपट के कागज और उसकी छपाई सुंदर होती है, तथ्य अपचनीय होता है। वे सिर्फ बुद्धि विलास के ढाबे बनकर रह जाते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व गोखले, गांधी, तिलक, आंबेडकर जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने चिंतन-अध्ययन को अपने राजनीतिक कर्यकलापों के बीच मरने नहीं दिया। वे बौद्धिकों के अनौपचारिक समूह में रहते थे और सबके अपने-अपने अखबार थे। मिशन एक था, पर विचारों की धारा अनेक थी। आजाद भारत में वैचारिक मंथन में विपन्नता का साम्राज्य है। हम जरूरत से ज्यादा राजनीति के शिकार हैं। शास्त्रार्थ और कठोर स्वाध्याय भारतीय बौद्धिक जीवन का हिस्सा था। शंकराचार्य भी इससे बाहर नहीं थे और राजा जनश्रुति, ब्रह्मज्ञान के पिपासु थे। विरासत के महिमामंडन की अपनी उपयोगिता है। पर असली चुनौती उसकी विशेषताओं को संदर्भ के अनुकूल जीवित करने की है।