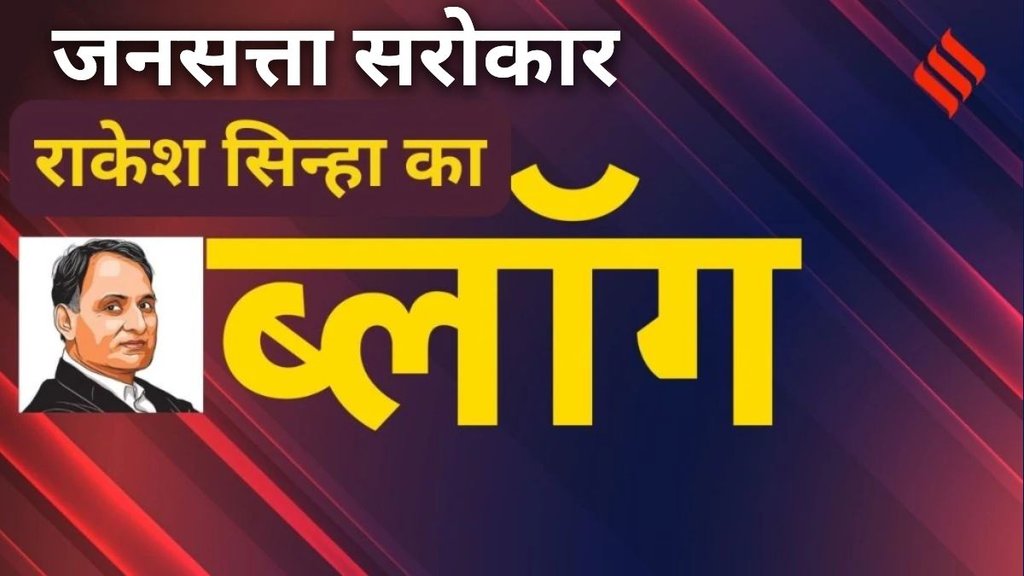वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में, और इससे पूर्व मुगल शासक औरंगजेब की कब्र के सवाल पर नागपुर में हिंसा हुई। विवाद का कारण तो समझा जा सकता है, पर जिसे हम समझना नहीं चाहते हैं, वह है हिंसा के पीछे की दलील और ताकत। इसे नजरअंदाज करना समाधान को दूर करना है। मगर हो यही रहा है। विडंबना यह है कि विभाजन के इतिहास से हमने शायद कुछ भी नहीं सीखा है। अगर सीखे होते तो संविधान सभा का ‘एक जन, एक राष्ट्र’ का संकल्प ख्वाब बनकर नहीं रह जाता। यह संकल्प संविधान की प्रस्तावना को सार रूप में अभिव्यक्त करता है। इसका तात्पर्य है पूजा पद्धतियों, जीवन मूल्यों और जातीय भिन्नताओं के बावजूद सामाजिक-सांस्कृतिक साझेदारी को बढ़ाना। यह तभी संभव है जब संवैधानिक पहचान को प्रबल करते हुए अन्य पहचानों की भूमिका सीमित अर्थों में देखने की प्रवृत्ति विकसित हो। पर हुआ उल्टा। सांप्रदायिक पहचान को अल्पसंख्यक अवधारणा की छतरी के नीचे पनपने के लिए स्थापित कर दिया गया। धार्मिक आधार पर बहुमत-अल्पमत होना अस्वाभाविक नहीं है, पर रोटी, रोजगार और राजनीति को उसके आधार पर बांट देना परस्पर सहयोग, सद्भाव और सहानुभूति की जगह प्रतिद्वंद्विता, कटुता और असहिष्णुता को जन्म देता है।
ब्रिटिश राज ने हिंदू-मुसलमान को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक प्रतिद्वंद्वी वर्गों में ‘बांटो और राज करो’ सिद्धांत के लिए खड़ा किया था। गवर्नर जनरल मेयो हिंसा से भयभीत थे। उन्होंने 1870 में प्रशासनिक अधिकारी विलियम विल्सन हंटर को मुसलमानों की राज्य के प्रति शिकायतों और उनके पिछड़ेपन का कारण ढूंढ़ने का निर्देश दिया। हंटर ने चतुराई से मुसलिम पिछड़ेपन के लिए साम्राज्यवाद और हिंदुओं, दोनों को समान रूप से कठघरे में खड़ा कर दिया। मुसलमानों की मांग मदरसा शिक्षा को प्रोत्साहन देने की थी। हंटर ने एक ओर यह सलाह दी कि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा से दूर रखा जाए, तो दूसरी ओर रोजगार और शिक्षा में उनके पिछड़ेपन का कारण हिंदुओं के अंग्रेजी शिक्षा लेने में तत्परता को बताया।
यही रपट ‘भारतीय मुसलमान’ के नाम से 1871 में प्रकाशित हुई। तबसे मुसलिम धार्मिक भावना को केंद्र में रखकर औपनिवेशिक नीतियां बनाई जाने लगीं। इसने आधुनिक मुसलिम मध्यवर्ग के विकास को रोक दिया। 1937 में जब प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी, तब ‘भारतीय मुसलमान’ की तर्ज पर मुसलिम लीग ने ‘पीरपुर रपट’, ‘कमल यार जंग’ और ‘शरीफ रपट’ प्रकाशित की। सभी का समान लक्ष्य था- कांग्रेस सरकार को ‘हिंदू राज’ साबित करना। लेकिन प्रश्न है कि आजादी के बाद आखिर हम समान भारतीयता का भाव विकसित करने का मार्ग क्यों नहीं ढूंढ़ पाए? कारण स्पष्ट है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक कृत्रिम विभाजन स्वतंत्र भारत की राजनीति के लिए उतना ही उपयोगी साबित हुआ, जितना यह मेयो-माउंटबेटन के लिए था।
हिंदू कोड बिल पर बहस के दौरान आचार्य जेबी कृपलानी ने भारतीय राज्य पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए पूछा था कि मुसलमानों पर सरकार कानून क्यों नहीं बना रही है? आगे 1954 का वक्फ कानून, 1960 का ‘रिलीजियस ट्रस्ट’ कानून से लेकर 1986 का शाहबानो प्रकरण आदि इसके उदाहरण हैं। 1957 में कांग्रेस ने एक अल्पसंख्यक उपसमिति बना कर उसे मुसलमानों की स्थिति जानने का काम सौंपा। यही सिलसिला सच्चर और रंगनाथ मिश्रा समितियों के निर्णय तक चलता रहा। इन सबने हिंदुओं के साथ मानसिक प्रतिद्वंद्विता भाव जगाकर रखा।
इस देश का सबसे छोटा समुदाय पारसी है, पर न उसे हिंदू बहुमत का खतरा महसूस हुआ, न ही उसे अल्पसंख्यक होने का कभी पछतावा हुआ। 1931 की जनगणना में पारसियों की जनसंख्या मात्र एक लाख नौ हजार थी। पर उनकी भागीदारी अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में सबसे अधिक रही। एक और रोचक तथ्य है। 1885 से 1890 के बीच कोई भी हिंदू कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा। 1886 और 1890 में क्रमश: दादा भाई नौरोजी और फिरोजशाह मेहता अध्यक्ष बने। दोनों पारसी थे। 1887 में बहरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने। वे मुसलिम थे। फिर भी कांग्रेस पर बहुमतवाद का आरोप लगता रहा।
इतना ही नहीं, 1885 में कांग्रेस के अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों में 59 हिंदू, दो मुसलिम, दो इसाई, और नौ पारसी थे। आगे के अधिवेशनों में भी यही क्रम चलता रहा। संविधान सभा में मुसलिम नेता बी पोकर और जेडएच लारी क्रमश: पृथक मतदाता संघ और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग करते रहे। यह अपरिवर्तित मानसिकता का प्रदर्शन था। मुसलिम मध्यवर्ग अन्य समुदायों के साथ सामाजिक-सांस्कृतिक साझेदारी बढ़ाने में असमर्थ साबित हुआ। इसका कारण था मुसलिम समुदाय में ऐसे लोगों की कमी, जो समुदाय की न्यूनताओं को सामने ला सके। जो थे, वे सभी दारा शिकोह की तरह वांछित रूप में देखे जाते थे। उसी की तरह वे अलग-थलग पड़ते चले गए। भेदभाव के आरोप पर हुमायूं कबीर ने कहा था कि संसाधनों और अवसरों के सीमित होने कारण ‘एक हिंदू दूसरे हिंदू पर, एक मुसलिम दूसरे मुसलिम पर, मुसलमान हिंदू पर, हिंदू मुसलमान पर आरोप लगाता है।’
पिछले दशकों में अल्पसंख्यकवाद इस हद तक संस्थागत हो रहा है कि कोई भी विवेकयुक्त तार्किक हस्तक्षेप भी समुदाय को उनकी हैसियत पर सवाल लगने लगता है। नागरिकता संशोधन कानून, तीन तलाक और वक्फ संशोधन इसके ताजा उदाहरण हैं। फिर एक जन-एक राष्ट्र की परिकल्पना यथार्थ से टकराकर शीशे की तरह चकनाचूर होता ही रहेगा।
हिंदू संगठन इसी साझेदारी के पक्षधर हैं। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने औरंगजेब की कब्र विवाद पर जो कहा, वह अत्यंत ही प्रासंगिक है- ‘कब्र का प्रश्न महत्त्वपूर्ण नहीं है। महत्त्व मानसिकता का है। औरंगजेब के अनुयायी हैं या दारा शिकोह के।’ दारा शिकोह इस्लाम के भारतीयकरण का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। जो ‘गंगा जमुनी’ संस्कृति का जनक था, आज वह विस्मृत किया जा रहा है। उसकी राह मुसलमानों का हिंदूकरण नहीं, भारतीयकरण की है। भारत के मुसलमानों से मेयो के सपने का मुसलमान नहीं, दारा शिकोह के सपने का मुसलमान बनने की अपेक्षा शुभ घड़ी का इंतजार कर रही है।