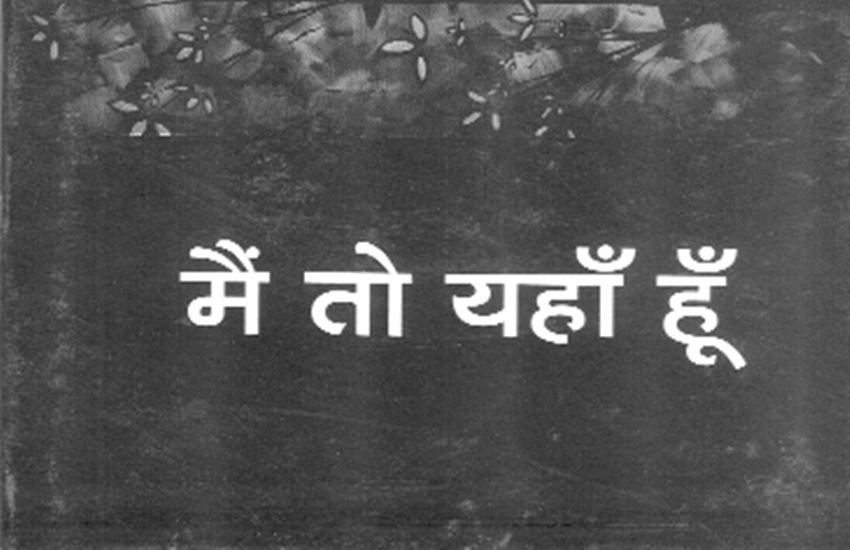जीवन और लेखन के लंबे पथ पर चलते हुए बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, जो अनवरत और अथक चलते हुए जीवन के हर अनुभव को शब्दबद्ध करने में संलग्न रहते हैं। रामदरश मिश्र ऐसे ही लेखकों में हैं, जिन्होंने लगभग छह दशक से ज्यादा का रचनात्मक समय जिया और कविता, आलोचना, कहानी, उपन्यास, यात्रावृत्त, संस्मरण, आत्मकथा और डायरी- लगभग हर विधा को गहराई से आत्मसात किया है। उनके लिए कविता रचना एक महोत्सव की तरह है।
रामदरश मिश्र का नया कविता संग्रह है- मैं तो यहां हूं। हमेशा बोलचाल के लहजे में कविताएं लिखने वाले इस कवि ने कविता के किसी प्रतिमान को अपने लिए रूढ़ नहीं बनने दिया, बल्कि वे अपनी सधी हुई लीक पर चलते रहे हैं। इस संग्रह की भूमिका में वे कहते हैं, ‘मैंने कई विधाओं में इस दुनिया को उतारा है। कथ्य को जो राह पसंद आई, उस राह वह हो लिया। वह राह छोटी भी थी और लंबी भी। अब लंबी राह चलने की शक्ति मुझमें नहीं रही। अत: छोटी-छोटी कविताओं या डायरी के माध्यम से रूप देता रहता हूं। ये कविताएं इसी तरह बनी हैं।’
रामदरश मिश्र की कविता ने जीवन का कोना-कोना खंगाला है। जीवन का कोई ऐसा भाव नहीं होगा, जो छूटा हो। शुरुआत गीतों से हुई। फिर कविताओं में उतरे। गजलें लिखीं। वे एक-एक कर हमारी विडंबनाओं पर प्रहार करते हैं। पहली ही कविता ‘ईश्वर’ हमारे बीच ईश्वर को लेकर तंगनजरी पर प्रहार करती है। यानी हम जिस तरह एक-दूसरे के ईश्वर से नफरत करते हैं, कवि उस विडंबना पर चोट करता है।
अपने परिवेश को रामदरशजी ने हमेशा अपने लेखन में उतारा है- चाहे उपन्यास हों, कहानियां या कविताएं। गांव से उनका जुड़ाव भी इसकी एक वजह है। इसीलिए उनकी कहानियों में आंचलिकता का पुट मिलता है, तो कविताओं में भी शहरी संवेदना के सूखते स्रोत दिखाई देते हैं। रामदरशजी वाणी विहार में रहते हैं, लिहाजा ‘वाणी विहार’ नामक कविता के बहाने घरों तक घुस आए बाजार पर चिंता जताते हैं। वे याद करते हैं कि कैसे यह वाणी पुत्रों की कॉलोनी वाणी विहार वणिक विहार में तब्दील हो चुकी है, जहां आज कवियों के भाव-स्वरों की लहरियां नहीं गूंजतीं, लेनदेन वाली बाजारू बोलियों की बजबजाहट सुनाई देती है।
उत्तर-वय की लेखकीय दुनिया ही कुछ अलग होती है।
लेखक अपने एकांत में लिखना भी चाहे तो लोग ऐसा नहीं करने देते। वे चाहते हैं कि वह लेखकों की पुस्तकों पर अनुशंसाएं लिखता रहे, गोष्ठियों की अध्यक्षता करता रहे। रोज-ब-रोज के तकाजे। इतनी मतलबी दुनिया, जो सर्जना की खिड़कियां खुली नहीं रहने देती, बल्कि लेखक को सनद बांटने का एक माध्यम बना देती है। इन दिनों कविता में उन्होंने जैसे हर बुजुर्ग लेखक की दुखती रग पर अंगुली रख दी है। कलाकार और कवि होना क्या आम मिस्त्री से कुछ अलग होता है। कवि कहता है कि घर बनाने वाले किस सुघरता और कला से घर का निर्माण करते हैं, पर वे कलाकार नहीं कहलाते, बल्कि कलाकार वह कहलाता है, जो ऐसे मकानों में बैठ कर कैनवस पर आकृतियां उकेरता है। चाहे वे किसी के काम की हों या न हों। मिस्त्री की सौंदर्यग्राही दृष्टि की शायद ही कोई उस तरह तारीफ करता हो जैसे कलाकार या कवि की। आज के समाज का यही ढर्रा बन गया है।
रामदरशजी ने कभी कविता के प्रतिमानों की परवाह नहीं की। वे लिखते हैं: ‘मेरी रचनाएं जैसी भी हैं, मेरी हैं, वे शुष्क सिद्धांत नहीं हैं, अंतर के छोटे-बड़े गान हैं; यानी आदमी के आदमी होने की पहचान हैं।’ वे चैनलों पर बाबाओं के बढ़ते प्रभुत्व की आलोचना करते हैं तो एक दल की दूसरे दल द्वारा की गई आलोचना भी उन्हें रास नहीं आती, जिससे आज के अखबार प्राय: आच्छादित रहते हैं। महानगर के अपने घर के खुले आंगन को निहार कर कवि-मन खुश होता है। आंगन में पहुंचते ही उसे लगता है कि वह अतीत के बाग बगीचों में पहुंच गया है। कवि समाज के जीते-जागते चरित्रों से ही नहीं, निर्जीव चीजों से भी बतियाता है। रामदरशजी ने ऐसा बहुतेरी कविताओं में किया है। ‘कुर्सी’, ‘चारपाई’, ‘आईना’, ‘अंगीठी’, ‘फाइल के साथ’, ‘चाबी’ ऐसी ही कविताएं हैं।
रामदरशजी ने जीवन के हर पहलू को बारीकी से टटोला है और बनावटी अभिव्यक्ति से बचते हुए जीवन से सूक्तियां चुनी हैं। धन क्या है, वे कहते हैं- जिसके पास अंतरात्मा का हीरा है वह अमीर है। जो मंदिर की देहरी पर दीप जलाने के बजाय अंधेरे में डूबे एक घर की देहरी पर चुपचाप एक दीया रख देता है, उसका त्योहार फलीभूत होता है। फर्श और वाटिका के संवाद के जरिए उन्होंने बताया है कि फर्श कितनी ही चिकनी हो और वाटिका कितनी ही मिट्टी और कीचड़ से भरी, पर जब वसंत आता है, फूलों से क्यारियां खिल उठती हैं, तो फर्श और वाटिका का फर्क पता चलता है। रामदरशजी ठहाके लगाने वाले इंसान हैं, इसलिए ठहाकों पर असभ्यता की मुहर दर्ज करने वालों को उनकी एक कविता जवाब देती है कि ‘मुझमें अब भी एक नादान बच्चा है, जो मुझे बूढ़ा नहीं होने देता।’
रामदरशजी हमेशा प्रकृति के बिंबों को कविता में चुनते-बीनते रहे हैं। बसंत के दिन उन्हें भाते हैं, तो दिसंबर-जनवरी की धूप उन्हें लुभाती है। बारिश के दिनों में कवि का मन मयूर आह्लादित हो उठता है, तो खिलखिलाते खेतों के बीच पहुंचते ही बोल उठता है- ‘मैं तो यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं।’ यही नहीं, वह अब भी यही मानता है कि तमाम तब्दीलियों के बावजूद गांव में गांव बचा हुआ है। यह कवि का ग्रामगंधी मन ही है, जो महानगर में रहते हुए भी गांव की ऊष्मा को अपने अवचेतन में बसाए हुए है। अकारण नहीं कि वे कविता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं: ‘आभारी हूं कविते/ तुमने इस तप्त समय में भी मुझे भिगो दिया भीतर तक/ और मैं/ गति-स्पंदित जीवन-राग की रचना के लिए अपने को तैयार कर रहा हूं।’ रामदरश मिश्र की कविताएं निस्संदेह जीवन-राग को स्पंदित और गतिशील बनाए रखने वाली कविताएं हैं।
ओम निश्चल
मैं तो यहां हूं: रामदरश मिश्र; इंद्रप्रस्थ प्रकाशन, के-71, कृष्णा नगर, दिल्ली; 200 रुपए।