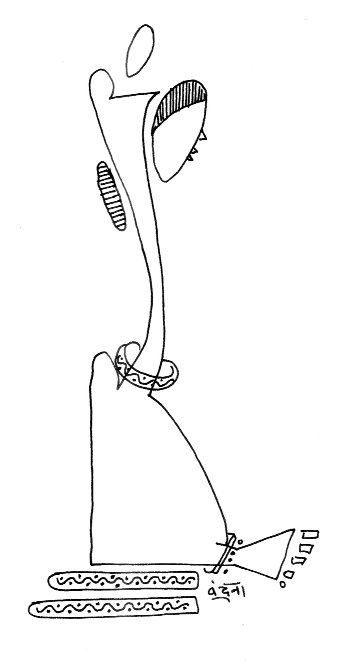मणींद्र नाथ ठाकुर
हम संक्रमण काल में जी रहे हैं? क्या जिन मान्यताओं, दर्शनों और संस्थाओं की शुरुआत आज से लगभग चार सौ साल पहले चिंतन में आए परिवर्तन से हुई थी, उनका अंत समय आ गया है? क्या हम उत्तर-मानवतावाद, उत्तर-पूंजीवाद और उत्तर-आधुनिकता से गुजरते हुए अब युग परिवर्तन की दिशा में बढ़ रहे हैं? इस नए समाज का स्वरूप क्या होगा? उसका नया दर्शन क्या होगा? ऐसे कई सवाल वर्तमान दर्शनिकों को बेचैन कर रहे हैं। समाज में परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। हर पल संसार, समाज, सब कुछ बदल रहा है। पर इन परिवर्तनों के दौरान कोई ऐसा समय आता है, जब परिवर्तन आमूल होता है और उसके बाद सोचना-समझना, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, संस्थाएं सब कुछ बदल जाती हैं। ऐसे आमूल परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं। अगर मार्क्स की मानें तो ऐसा आमूल परिवर्तन उत्पादन की पद्धति में आए परिवर्तनों के कारण होता है। हैबरमास इसका कारण संचार माध्यमों में आए परिवर्तन को मानता है। लेकिन हमारा समय इन सामान्य बातों से ऊपर है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि परिवर्तन का नया दौर चल रहा है और हम एक बार फिर आमूल परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तो दुनिया संचार क्रांति के कारण आए परिवर्तनों को ही ठीक से पुराने सिद्धांतों से समझ नहीं पा रही है। इसी बीच आनुवंशिकी में आई नई क्रांति से नए सवाल खड़े हो गए हैं। विज्ञान के इस क्षेत्र में हम जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं उससे ऐसा लगता है कि मनुष्य की मौलिक अवधारणा में परिवर्तन की जरूरत है। ‘जीन एडिटिंग’ एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे इस विधा के जानकार लोग किसी मनुष्य के जेनेटिक कोड को भी बदल सकते हैं। यानी आने वाले समय में सामान्य मनुष्य की जगह ऐसे लोग भी होंगे, जिनके जीन को सुधार कर उसमें असीम क्षमताएं विकसित की गई हों।
फ्रांस के एक उपन्यासकार हैं मीशेल हाऊलेबेक, जिनकी कुछ किताबें हाल में बहुचर्चित रही हैं। इनके उपन्यासों की खासियत है कि इनमें भविष्य के समाज की बात होती है, पर उस कल्पना का आधार यथार्थ रहता है, खासकर वैज्ञानिक खोजों का दूरगामी प्रभाव के इर्दगिर्द उनके पात्र रचे जाते हैं। एक उपन्यास का मुख्य पात्र आनुवंशिकी वैज्ञानिक है। उपन्यास में खासी चर्चा तो फ्रांस के व्यक्तिवादी समाज की है, जिसमें मनुष्य बहुत अकेला हो गया है। उसकी संबंधों की कल्पना ही सिकुड़ गई है। कामुकता की अनुभूति ही उनकी अस्मिता हो गई है। आदमी अपने वजूद का साक्ष्य ही अपनी काम भावनाओं से करता है। वह इतना व्यक्तिवादी हो गया है कि काम की भावना की अनुभूति के लिए पहले समलैंगिकता को अपनाता है और आखिर में किसी और मनुष्य पर निर्भर रहने के बदले अकेले प्रयास करना उचित समझता है। लेखक इसे सामाजिक यथार्थ के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन इस सबसे काम के प्रति उदासीन हो जाता है। काम और प्रेम को अलग करने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाता है। अंत में अपने शोध में यह खोज निकाला है कि मनुष्य के स्वभाव को जेनेटिक एडिटिंग के जरिए इच्छा अनुसार बनाया जा सकता है। और इससे समाज में एक नई क्रांति आ जाती है। खुद तो लेखक रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता है। उसकी गाड़ी समुद्र के किनारे खड़ी मिलती है। और कयास लगाया जाता है कि या तो उसने आत्महत्या कर ली है या फिर वह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए तिब्बत की ओर चला गया है। लेखक की इस खोज को लेकर शोध संस्था के लोग उसे बाजार में लाने का प्रयास शुरू कर देते हैं। इस उपन्यास से हमें बदलते समय का अंदाजा लग सकता है। अगर सचमुच यह संभव है, तो देखना केवल यही रहेगा कि इस तकनीकी का उपयोग बाजार किस तरह करता है और जिनोम से क्लोनिंग तक की यात्रा समाज कैसे तय करता है। लेखक बुद्ध की चर्चा कर शायद हमारा ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता है कि हमें सामाजिक मूल्यों पर फिर से सोचने की जरूरत है। मनुष्य की जगह संपूर्ण प्रकृति को ध्यान में रखने और काम को अपनी अस्मिता बनाने के खतरों को समझना जरूरी है।
इसी तरह रोबोटिक्स के बढ़ते कदम भी इस बात की तरफ इंगित कर रहा है कि हम एक नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं। जहां अन्य मशीनों की तरह आदमी जैसा एक मशीन भी हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होगा। कारखानों और कार्यालयों में तो बहुत जल्दी आप मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कामों को रोबोट करने लगेंगे। यह एक नई दुनिया होगी। पूंजीवाद में आए संकट से निकलने के प्रयास में उद्योग और व्यापार में लाभ की मात्रा बढ़ाने के लिय मनुष्य की जगह रोबोट लगाना लगभग तय-सा हो गया है। यानी हम आने वाले समय में एक नए तरह के मनुष्य से संवाद करेंगे। रोबोट की तरह का ही एक और मशीन हमारे जीन में प्रवेश के लिए झांक रहा है, जिसे ‘थ्री डी प्रिंटर’ कहते हैं। इस मशीन से हम हर कुछ बना सकते हैं। जिस सामान को हम बनाना चाहें उसका नक्शा कंप्यूटर में बना लें, फिर उसे प्रिंट कर लें। मसलन, अगर घर बनाना हो तो आवश्यक सामग्री को प्रिंटर में डाल दें और घर के नक्शे के अनुसार सब प्रिंट हो जाएगा। इस तकनीकी का उपयोग अभी चीन में सर्वाधिक हो रहा है। हजारों घर कुछ ही महीनों में बिना किसी मानव श्रम के बना लिए जा रहे हैं। यहां तक कि मनुष्य के अंगों को भी इस मशीन से बनाया जा सकता है। भौतिकी के प्रसिद्ध विद्वान मीशेल काकु की बात मानें तो संभव है कुछ दिनों में थ्री डी प्रिंटर से बने मनुष्य के अंग बाजार में दुकानों पर मिलने लगेंगे।
हाल के दिनों में विज्ञान और तकनीक ने मनुष्य के मस्तिष्क की ओर सोचना शुरू किया है। मस्तिष्क से संबंधित एक परियोजना के उद्घाटन में राष्ट्रपति ओबामा ने यह घोषणा की कि आने वाले समय की सबसे बड़ी क्रांति इसी क्षेत्र में होने वाली है और अमेरिका को किसी भी तरह इसमें महारत हासिल करना होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर अर्थ मुहैया किए जाने की बात की। इसका स्वरूप क्या होगा, अभी कहना कठिन है। पर इतना तो समझा जा सकता है मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमता में व्यापक विस्तार की संभावना है। शायद हमारे मस्तिष्क का जीवन हमारे शरीर पर निर्भर न करने लगे; ब्रेन ट्रांसप्लांट भी होने लगे।
अब आप कल्पना करें कि एक ऐसे समाज में हम रहेंगे, जिसमें मनुष्य भी कृत्रिम होंगे, जीन एडिटिंग से बने या क्लोन द्वारा एक व्यक्ति के कई प्रतिरूप होंगे, जिसमें अपने मन से सुधार कर सकेंगे; सोचने-समझने, प्यार प्रदर्शन करने वाले, घरों दुकानों और उद्योगों में काम करने वाले रोबोट होंगे; कान, नाक, किडनी और लिवर से लेकर घर और बंदूक बनाने वाली मशीनें हमारे घर में ही होंगीं; किसी के शरीर में किसी और का मस्तिष्क होगा। अब सोचें कि ऐसे में समाज, दर्शन, राजनीति, संस्थाएं सब कुछ क्या आज से अलग नहीं होंगे। न जाने ऐसी कितनी खोजें हो रही हैं आज, जिनके चलन में आ जाने से हमारी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। इसमें नई संस्कृति होगी, नए दर्शन होंगे, नया समाज होगा, नई राजनीति होगी। अब सवाल है कि क्या हम सोच के स्तर पर इसके लिए तैयार हो रहे हैं। या फिर हम पिछली सदी के लोग के नाम से जाने जाएंगे? क्या आदि मानव और आज के मानव में जो अंतर है, उससे भी ज्यादा अंतर हमारे और आने वाले समय के मनुष्यों के बीच होगा? क्या हम इस समय में रहते हुए इस बदलाव को समझ सकते हैं?