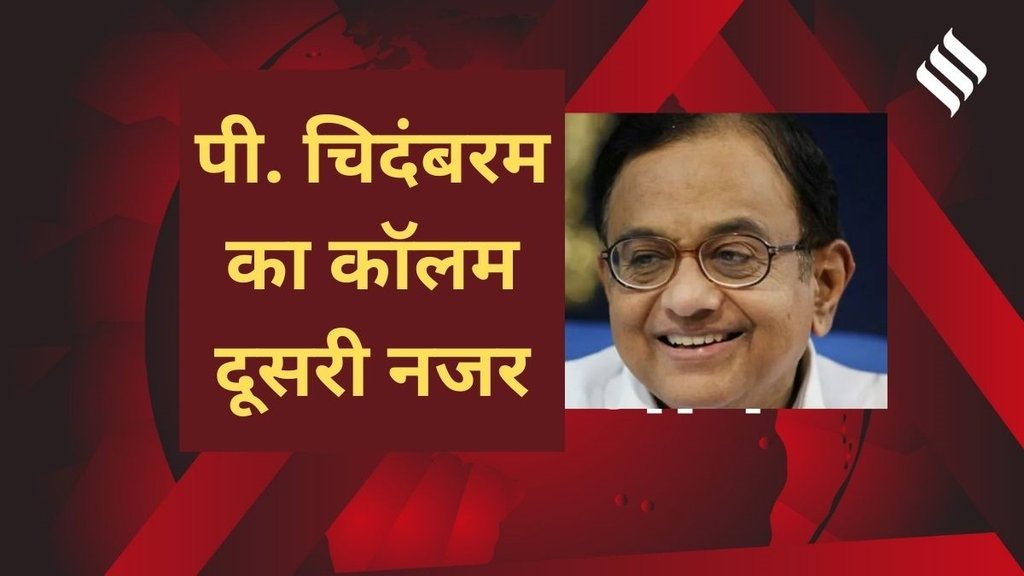बिना उकसावे के युद्ध किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि पक्षपातपूर्ण विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। भाजपा को बिना उकसावे के युद्ध शुरू करने का शौक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) इसके उदाहरण हैं। इन्हें किसी जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं बनाया गया था। सीएए और यूसीसी, दोनों को आरएसएस-भाजपा ने हिंदू और गैर-हिंदू समुदायों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए आगे बढ़ाया है।
केंद्र सरकार ने एक और बिना उकसावे के युद्ध का बिगुल फूंका है, इस बार भाषा पर। तथाकथित ‘त्रिभाषा फार्मूला’ (टीएलएफ) को सबसे पहले राधाकृष्णन समिति ने पेश किया था। यह फार्मूला आते ही धराशायी हो गया। किसी भी राज्य ने कभी टीएलएफ को लागू नहीं किया।
टीएलएफ प्राथमिकता नहीं
इसके कई कारण थे। पहली प्राथमिकता स्वाभाविक रूप से स्कूलों के निर्माण और शिक्षकों की नियुक्ति को दी गई। दूसरी प्राथमिकता, सार्वभौमिक नामांकन और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने की थी। अगला काम था शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, जिसमें न केवल भाषा, बल्कि गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और सामाजिक अध्ययन जैसे अन्य समान रूप से महत्त्वपूर्ण विषय भी शामिल थे। आजादी के 78 साल बाद भी ये काम अधूरे हैं।
भाषा ‘शिक्षा’ के कारण नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 343 के कारण विस्फोटक मुद्दा बन गई। घोषणा की गई कि हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी, लेकिन अंग्रेजी का उपयोग पंद्रह साल की अवधि के लिए जारी रहेगा। पंद्रह साल 1965 में समाप्त हो गए। एक अविवेकपूर्ण तरीके से तत्कालीन सरकार ने घोषणा की कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी एकमात्र आधिकारिक भाषा होगी। प्रतिक्रिया तत्काल और स्वत: स्फूर्त थी। तमिलनाडु में राजनीति ने करवट ली और एक द्रविड़ पार्टी सत्ता में आई। जवाहरलाल नेहरू ने वादा किया था कि जब तक गैर-हिंदी भाषी लोग चाहेंगे, तब तक अंग्रेजी सह-आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रहेगी। 1965 के संकट के चरम पर होने पर भी अकेले इंदिरा गांधी में ही उग्रपंथियों का विरोध करने और वादे को दोहराने का साहस और बुद्धिमानी थी।
मगर प्रशासन की अनिवार्यताओं के कारण केंद्र सरकार को द्विभाषी होना पड़ा। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भी विज्ञान, कानून, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग, विदेशी व्यापार, विदेशी संबंध, अंतरराष्ट्रीय निकायों आदि की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से बहुमुखी नहीं थी। राज्य सरकारें भी द्विभाषी हैं और कानून पारित करने व प्रशासन के कई पहलुओं के लिए अंग्रेजी पर निर्भर हैं।
इस बीच, दूरगामी परिणामों वाले तीन घटनाक्रम हुए हैं। पहला, 1975 में ‘शिक्षा’ को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे स्कूली शिक्षा के मामले में राज्यों की स्वायत्तता खत्म हो गई। दूसरा, भारत ने 1991 में उदारीकरण व भूमंडलीकरण को और इस तरह अनिवार्य रूप से अंग्रेजी को अपनाया। तीसरा, अभिभावकों की ओर से अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की मांग थी और अब यह बढ़ती जा रही है।
तीसरी भाषा कौन सी?
वर्तमान विवाद नई शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के विभिन्न पहलुओं और विशेष रूप से टीएलएफ पर है। क्षेत्रीय या राज्य भाषा स्कूलों में ‘पहली’ भाषा है, जबकि अंग्रेजी ‘दूसरी’ भाषा है। लेकिन ‘तीसरी’ भाषा कौन-सी है?
केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पास एक आसान-सा तर्क है। एनईपी एक राष्ट्रीय नीति है और हर राज्य संवैधानिक रूप से इस नीति को अपनाने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, एनईपी तीसरी भाषा के शिक्षण को अनिवार्य बनाती है, मगर वह यह निर्धारित नहीं करती है कि तीसरी भाषा हिंदी होनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मासूमियत का दिखावा करते हुए पूछा कि तमिलनाडु सरकार एनईपी और तीसरी भाषा के शिक्षण का विरोध क्यों कर रही है?
उत्तर आसान हैं: पहला, एनईपी वर्तमान केंद्र सरकार की नीति है और संविधान द्वारा अनिवार्य नहीं है। दूसरा, तमिलनाडु में सरकारों की आधिकारिक नीति रही है कि सरकारी स्कूलों में तीन नहीं, बल्कि दो भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। तमिलनाडु सरकार ने निजी स्कूलों में हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ाने में कोई बाधा नहीं डाली है। तमिलनाडु में केंद्रीय विद्यालय और सीबीएसई (642), आइसीएसई (77) और आइबी से संबद्ध (8) स्कूल हिंदी पढ़ाते हैं और हजारों बच्चे हिंदी सीखते हैं। सरकार भी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा या इसी तरह के संगठनों के माध्यम से हिंदी सीखने वाले लाखों बच्चों के रास्ते में बाधा नहीं डालती है।
कई राज्यों में एक भाषा
जहां तक एनईपी का सवाल है, इसमें अच्छी और अस्वीकार्य, दोनों विशेषताएं हैं। विवादास्पद पहलुओं में से एक है टीएलएफ। टीएलएफ को हिंदी भाषी राज्यों में लागू नहीं किया गया है, लेकिन गैर-हिंदी भाषी राज्यों में इसे लागू करने की मांग की गई है। यह रेकार्ड में है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के सरकारी स्कूल प्रभावी रूप से केवल हिंदी की एक-भाषा नीति का पालन करते हैं। इन राज्यों के सरकारी स्कूलों में नामांकित अधिकतर बच्चे कोई अन्य भाषा नहीं सीखते हैं, क्योंकि वहां अंग्रेजी के शिक्षक बहुत कम हैं और शायद ही किसी अन्य भाषा के शिक्षक हों। निजी स्कूल सरकारी स्कूलों का अनुसरण करके और हिंदी पढ़ा कर खुश हैं; कई स्कूल अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, लेकिन तीसरी भाषा नहीं। जिन कुछ स्कूलों में तीसरी भाषा पढ़ाई जाती है, वहां हमेशा संस्कृत ही होती है। पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तीसरी भाषा हिंदी है, लेकिन यह सर्वविदित है कि पंजाबी, गुजराती और मराठी का हिंदी से गहरा संबंध है।
इसके अलावा पढ़ाई जाने वाली अंग्रेजी की गुणवत्ता बहुत खराब है। जिन सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, वहां पढ़ने वाले बच्चे अंग्रेजी कक्षा के बाहर शायद ही अंग्रेजी बोल पाते हैं। यह तमिलनाडु सहित सभी राज्यों के लिए सच है। इससे पहले कि शिक्षा मंत्री तमिलनाडु को टीएलएफ- यानी वास्तव में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी- स्वीकार करने के लिए मजबूर करें, उन्हें पूरे भारत में दो भाषाओं (क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी) को पढ़ाने में सफलता हासिल करनी चाहिए। बोली जाने वाली अंग्रेजी अपर्याप्त है; अच्छी बोली जाने वाली अंग्रेजी दुर्लभ है।
सरकार स्वीकृत दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाने में विफल रही है; ऐसे में सरकार को तीसरी भाषा पढ़ाने में सफल होने की महत्त्वाकांक्षा क्यों है?