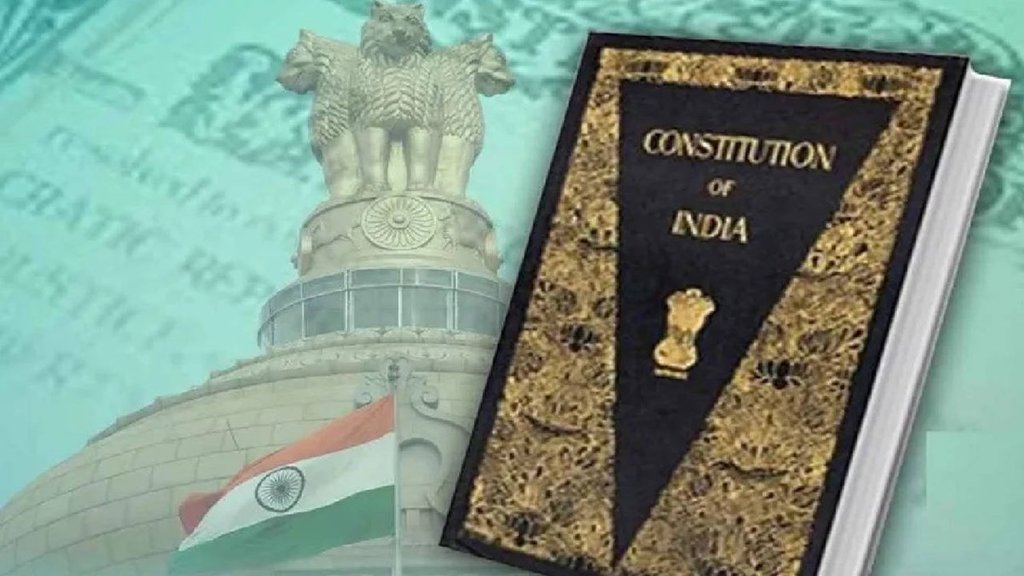देश में 25 जून, 1975 को आपातकाल लगाया गया था। इसने संविधान को निरस्त कर दिया था। इस दिन को ‘संविधान हत्या दिवस’ मनाने के निर्णय से एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि उनचास साल बाद इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आपातकाल एक घटना मात्र होने से कहीं अधिक एक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो लोकतंत्र के बीच ही विद्यमान रहती है। उसके प्रति अज्ञानता को बनाए रखना स्वयं के प्रति छल है। समय चाहे जितना बीत जाए, सत्य कभी बासी नहीं होता है, न ही इसके प्रति आकर्षण कम होता है। यही इसकी संजीवनी है।
आपातकाल का अर्थ बीजेपी-कांग्रेस के बीच टकराव बन गया है
जिस देश में संविधान पर इतना बड़ा वज्रपात हुआ हो, उस देश की पीढ़ियों को अपनी ही व्यवस्था के प्रति उदासीन तथा अज्ञानी बनाकर रखना ऐतिहासिक अपराध से कम नहीं माना जाएगा। आज विचित्र परिस्थिति है। आपातकाल का अर्थ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच टकराव बनकर रह गया है। राजनीति में परस्पर संघर्ष तो रहता ही है, पर उसके कारण इतिहास के प्रवाह को रुकने नहीं देना चाहिए। यह प्रवाह राष्ट्र के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों प्रकार की घटनाओं को सम्मिलित करने से बनता है।
एक जनतांत्रिक समाज में स्वयं की त्रुटियों या न्यूनताओं को स्वीकार करने की ताकत विकसित होती है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो इसका अभिप्राय जनतंत्र में परिपक्वता की अल्पता है। भारत के संदर्भ में यह सच है। तभी तो आपातकाल के नाम पर राजनीति और बौद्धिकता दो खेमों में बंट जाती है। ‘संविधान हत्या दिवस’ सिर्फ एक दिन का जलसा न होकर भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में उतार-चढ़ाव को रेखांकित करने वाला सिद्ध होगा। यह कार्य अब तक क्यों नहीं हुआ? उत्तर हमें समकालीन बौद्धिकता की न्यूनता या कमजोरियों तक ले जाता है। अमेरिकी न्यायाधीश फेलिक्स फ्रैंकफर्टर, जिन्होंने स्वतंत्रता के पक्ष को मजबूत करने की लंबी लड़ाई लड़ी थी, ने सच को वस्तुनिष्ठ बताया था।
आपातकाल के प्रति जानकारियों में वस्तुनिष्ठता का सख्त अभाव है। जब तक यह बना रहेगा, नई पीढ़ी को विध्वंसात्मक ताकतों के प्रति जागरूक करना कठिन होगा। आपातकाल की जानकारी कितने लोग जेल गए और कितना अत्याचार हुआ, इसे जानने तक सीमित नहीं है। यह संविधान की जनपक्षधरता पर जीवंत बहस है। हमारा संविधान सामान्य लोगों को केंद्र में रखकर बनाया गया है, इसलिए इसकी रक्षा भी उन्हीं लोगों द्वारा सुनिश्चित हो सकती है। समकालीन राजनीति में संविधान को परस्पर आरोप-प्रत्यारोप का उपकरण बना दिया गया है। यह संविधान सभा की मूल भावना के विपरीत और विरोधी है।
संविधान सभा में सभी रंगों और दृष्टिकोणों के लोग थे। एक तरफ घोर समाजवादी केटी शाह थे तो दूसरी तरफ दक्षिणपंथ के प्रतिनिधि मीनू मसानी थे, लेकिन विरोधी और विपरीत विचारधारा के प्रतिनिधि शालीनता से बोलते भी थे और दूसरों को धैर्य से सुनते भी थे। असहमति शत्रुता का कारण नहीं बनती थी। मतांतर ने मर्यादा को कभी मरने नहीं दिया। इसका कारण था कि संविधान सभा के सदस्य पीढ़ियों के लिए सोचते और बोलते थे। यह भाव और भावना, दोनों ही स्वतंत्र भारत में राजनीति से लुप्त होती गई। इसीलिए आपातकाल के दौरान जुल्म और जबर्दस्ती के ऊपर भी राजनीतिक विभाजन होना एक इसके क्षरण का उदाहरण है।
लोकतंत्र कभी करिअरवादी बुद्धिजीवियों से न समृद्ध होता है, न ही सुरक्षित रहता है। ऐसे लोग सभी व्यवस्थाओं में स्वघोषित नवरत्न बनकर सोचते, बोलते और लिखते हैं। इतिहास लेखन को कुलीनता और करिअरवाद, दोनों जंजाल से मुक्त करना ही उसे सहज स्वरूप देना होगा। यह विडंबना ही है कि लोकतंत्र पर बोलते या लिखते वक्त हम एथेंस की तरफ देखते हैं। हम स्वयं के इतिहास से विस्मृत हैं। लिच्छवी का गणतंत्र प्राचीनतम लोकतंत्र है। अगर यह यूरोप से जुड़ा होता, तो हम बारीकियों में वैसे ही पढ़ते, जैसे प्लेटो या अरस्तु को पढ़ते हैं।
एक जीवंत समाज अपने इतिहास को सदैव टटोलता रहता है। यह वर्तमान को ताकत देने का काम करता है। आपातकाल का विस्तृत अध्ययन और उसकी जानकारी भारतीय समाज की प्रचंड सजगता का भी उदाहरण है। प्रजातंत्र के पक्ष की एक घटना दर्जनों नकारात्मकता को पछाड़ती है। इंदिरा गांधी का रायबरेली से चुनाव रद्द किया जाना सिर्फ निर्णय नहीं है, बल्कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल का कानून के राज के प्रति व्यावहारिक समर्पण का उदाहरण है। वैसे ही दूसरी घटना है जो दर्शाती है कि लोकतंत्र की सुरक्षा तटस्थता में नहीं होती है।
नानी पालकीवाला जाने-माने वकील थे। उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय को चुनौती देने वाले मामले में वकील बनने की सहमति दी थी। पर जैसे ही इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने की घोषणा की, उन्होंने विरोध में इंदिरा गांधी के पक्ष से अपने आपको अलग कर लिया। इसलिए आपातकाल पर बहस का फलक राजनीतिक सरगर्मी की उपज नहीं होनी चाहिए।
पूरी दुनिया में आपातकाल जैसी प्रकृति से खतरा है, इसीलिए लोकतंत्र की गुणात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश इतिहासकार जार्ज ग्रोट ने ग्रीस का इतिहास लिखते हुए संवैधानिक नैतिकता की बात की थी। जो लोग आपातकाल का इतिहास लिखे और बताए जाने का विरोध करते हैं, वे संवैधानिक नैतिकता से दूर भाग रहे हैं।