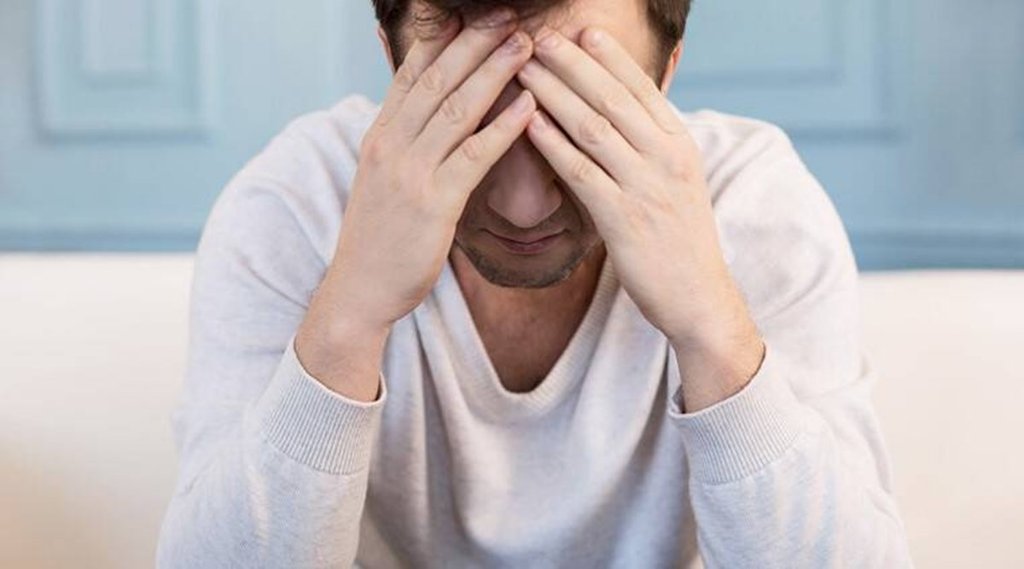सोनम लववंशी
वर्तमान दौर की अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती किसी राष्ट्र के सामने है, तो वह है मानसिक तनाव की। इस बीमारी से आजकल हर आयु वर्ग के लोग पीड़ित हैं, लेकिन भारत में इसे सामान्य विकार मान कर टाल दिया जाता है। गौरतलब है कि ‘द स्टेट आफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन-2021 आन माय माइंड’ रिपोर्ट के अनुसार भारत में पंद्रह से चौबीस वर्ष के इकतालीस फीसद बच्चों और किशोरों ने मानसिक बीमारी के लिए मदद लेने की बात कही है।
यह रिपोर्ट इक्कीस देशों के करीब बीस हजार बच्चों पर हुए सर्वेक्षण से निकल कर आई है। इसमें करीब तिरासी फीसद बच्चे इस बात को लेकर जागरूक दिखे कि मानसिक परेशानियों के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। वहीं भारत के संदर्भ में भी इस विषय को लेकर गंभीरता देखने को मिली, लेकिन अब भी स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा उतनी बेहतर नहीं है, जितनी कि होनी चाहिए।
पल-पल बढ़ता तनाव न केवल मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए भी संकट पैदा कर रहा है। आए दिन लाखों लोग मानसिक अवसाद के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं, पर अफसोस कि इस गंभीर बीमारी के प्रति हम सजग नहीं हो पा रहे हैं। समाज में सबसे अधिक मानसिक अवसाद का शिकार महिलाएं हैं। इसकी वजह है, उनका भावनात्मक रूप से शोषण।
पितृसत्तात्मक समाज आज भी महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करता है। आज भी समाज में पुरुष वर्ग महिलाओं के जीवन पर स्वामित्व हासिल करने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, आज भी महिलाओं को पुरुषों के समान न तो अधिकार मिल पाए हैं और न ही स्वतंत्रता। उनके साथ लैंगिक भेदभाव उनके जन्म के पूर्व से ही प्रारंभ हो जाता है और आगे चल कर यही उनके मानसिक तनाव का कारण बनता है।
समाज में ऐसा कोई वर्ग नहीं, जहां महिलाएं प्रताड़ित न हो रही हों। बचपन से ही दुर्भावना का शिकार होती महिलाएं मानसिक अवसाद के दलदल में फंसती चली जाती हैं। हमारे देश की युवा पीढ़ी तक इस अवसाद से ग्रसित है। हर दिन मानसिक अवसाद के कारण युवा खुदकुशी तक कर लेते हैं, लेकिन अफसोस कि इस बीमारी के प्रति न हमारी सरकार गंभीर है और न ही हमारा समाज। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक लगभग सभी उम्र के अट्ठाईस करोड़ से भी अधिक लोग मानसिक अवसाद का शिकार हैं।
विश्व बैंक का मानना है कि आने वाले दस सालों में मानसिक अवसाद अन्य बीमारियों की अपेक्षा राष्ट्र पर अधिक असर डालेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ‘मेंटल हेल्थ एटलस’ नाम से प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि ‘भारत में प्रति एक लाख व्यक्तियों के लिए सिर्फ 0.29 मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं और मनोवैज्ञानिकों की संख्या तो इससे भी निम्नतम स्तर पर है। मनोवैज्ञानिकों की संख्या प्रति एक लाख व्यक्तियों पर 0.15 है। वहीं कुल मिलाकर 1.93 मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रति एक लाख जनसंख्या के लिए उपलब्ध हैं।
इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि एक विश्व शक्ति बनने को लालायित देश की स्थिति मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कितनी खोखली है। जहां एक लाख की आबादी पर एक मनोचिकित्सक भी उपलब्ध नहीं है, वह देश कैसे विकास के नए आयाम स्थापित कर पाएगा? ‘मेंटल हेल्थ एटलस’ के मुताबिक ही 2017 तक पूरे देश में केवल उनचास बाल मनोवैज्ञानिक थे। अब सोचिए, बाल मन कैसा होता और कैसे एकाएक विचलित हो जाता। ऐसे में पढ़ाई और सामाजिक दबाव के आगे वह अगर झुक गया, तो उसे बाहर कौन निकाल पाएगा? वैसे कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और अगर यही भविष्य मानसिक अवसाद में पड़ गया फिर देश का वर्तमान क्या होगा? यह बहस का विषय होना चाहिए।
मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च का अनुमान लगाने के लिए नीति निर्माताओं को आधारभूत संरचना और मानव संसाधनों के वांछित विस्तार की स्पष्ट जानकारी की आवश्यकता है। पर 2019 में एक संसदीय प्रश्नावली से पता चला था कि संपूर्ण भारत में केवल इक्कीस राज्यों में कुल तैंतालीस सरकारी मानसिक चिकित्सालय हैं। उसके बाद शायद ही मानसिक रोगों को लेकर कहीं कोई अस्पताल खुला हो।
वैसे एक आंकड़े के मुताबिक विकसित देश भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उतना जागरूक नहीं हैं, जितना होना चाहिए। फिर भी उनकी स्थिति भारत से लाख गुना बेहतर है। विकसित देशों में प्रति एक लाख व्यक्तियों पर तकरीबन तीन मनोचिकित्सक हैं। इस संख्या के आधार पर, भारत को 2029 तक इस कमी को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष लगभग सताईस सौ नए मनोचिकित्सकों की आवश्यकता पड़ेगी। पर प्रतिवर्ष इतनी बड़ी संख्या में मनोचिकित्सक निकल कर सामने कैसे आएंगे, यह भी एक यक्ष प्रश्न है।
वैसे तो हम उस देश के नागरिक हैं, जहां ‘चिंता को चिता समान’ माना गया है। फिर भी आज तक मानसिक अवसाद को लेकर कोई गंभीरता किसी भी तरफ से देखने को नहीं मिलती है। समय समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा जारी रपटें भी यह बताने के लिए काफी हैं कि इस गंभीर बीमारी के प्रति हम अब भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। हमारा देश मानसिक अवसाद के मरीजों की श्रेणी में अग्रणी देशों में शामिल है।
पर हम इस गंभीर विषय को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। अवसाद को हम आम मानसिक विकार की तरह देखते हैं। यही वजह है कि देश में साढ़े चार करोड़ से अधिक लोग इसका शिकार हैं। सामाजिक जनसांख्यकीय सूचकांक (एसडीआई) राज्य समूह में तमिलनाडु, केरल, गोवा और तेलंगाना अवसादग्रस्त राज्यों में अग्रणी हैं। यही वे राज्य हैं जो कहीं न कहीं शिक्षा के मामले में देश में बेहतर हैं। यानी शिक्षित होना भी इससे अछूता होने का आधार नहीं। वहीं पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 3.9 प्रतिशत अधिक अवसाद की संभावना रहती है।
हालांकि हमारे यहां मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 है, जो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधारों की वकालत करता है। यह अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 को रद्द करके बनाया गया था। इस अधिनियम की विफलता की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह मानसिक रोगियों के अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करने में असमर्थ था। पर नया अधिनियम आने के बाद भी स्थिति प्रतिकूल ही है। इसके अलावा कोविड महामारी में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या कई गुना बढ़ गई है। इसके बावजूद हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में मानसिक अवसाद को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 तो निर्बाध जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदहाली जीवन जीने के अधिकार को बाधित कर रही है।
स्वास्थ्य के प्रति सरकार की बढ़ती बेरुखी यह बताने के लिए काफी है कि हम स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकता को किस हद तक नजरअंदाज कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत एक बीमारू देश बनता जा रहा है। इससे निपटने के लिए हमें सबसे पहले मानसिक अवसाद से निपटना होगा। यह कैसे संभव हो पाएगा, इसकी रूपरेखा अभी न सरकार के पास है और न आम नागरिक इसको लेकर सचेत हैं। ऐसे में स्थिति विकट ही मालूम पड़ती है।