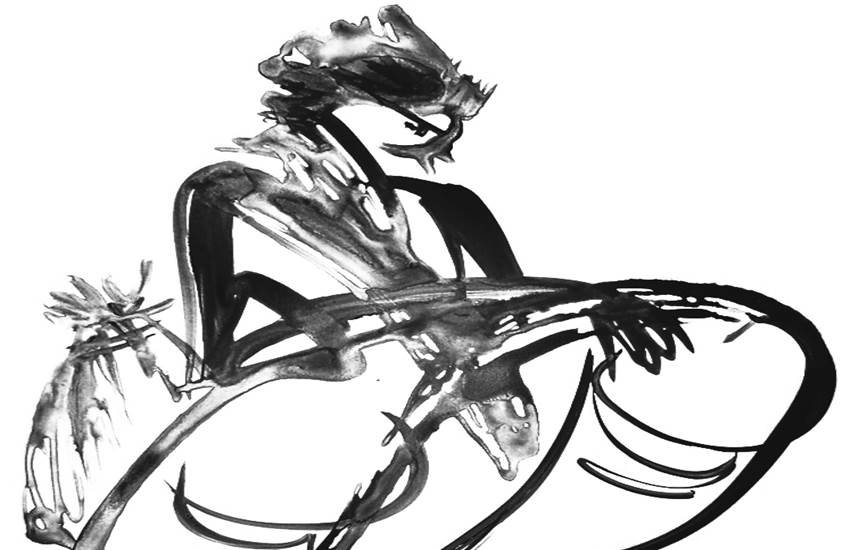मीडिया और नागरिक समाज के लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि विज्ञापन में बेची जा रही चीज के खरीददार से धोखा नहीं होना चाहिए। लेकिन छल तो विज्ञापन की प्रकृति में है। वह छल नहीं करेगा तो बेचेगा कैसे? बड़ी चीज यह है कि छल की मात्रा कितनी हो! विज्ञापन के लिए बनी आचार संहिताएं और निषेध कानून के निर्माण में ही यह बात निहित है कि किन चीजों में विज्ञापनदाता जनता को छल सकता है और किन चीजों में नहीं।
व्यावसायिक विज्ञापनों की खूबी है कि वे शुद्ध मुनाफे पर निगाह रखते हुए प्रसारित किए जाते हैं। उनमें सबसे ज्यादा पैसा और कुशल पेशेवर लोगों का परिश्रम लगा होता है। वे तभी सफल होते हैं जब जन-जन की जबान पर चढ़ जाएं और बाजार में उनका असर दिखाई दे। लेकिन पूंजीवाद के इस उत्तरवर्ती दौर में जब हर चीज का बाजारीकरण हो रहा है, कृत्रिमता और कुशलता का अटूट रिश्ता बनता जा रहा है। उपभोक्ता केंद्रित विज्ञापन की खूबी है कि वह उपभोक्ता को व्यक्तिगत तौर पर अपील करने की कोशिश करता है। यह दो गैर-बराबर समूहों के बीच संप्रेषण है, जिसमें एक तरफ अपरिपक्व खरीददार है तो दूसरी तरफ हर तरह की चालाकी से भरा विज्ञापनदाता, जो वस्तु का मालिक भी होता है।
विज्ञापन में महत्त्वपूर्ण चीज है ‘पर्सुएशन’ यानी कायल करना। एकमात्र वर्गीकृत विज्ञापन में ‘पर्सुएशन’ का तत्त्व कम होता है, क्योंकि वहां उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार केवल विशिष्ट सूचना चाहता है। जैसे नौकरी, भाड़े का घर, खरीद-बिक्री, वर-वधू के वर्गीकृत विज्ञापनों में, जो ज्यादातर निजी तौर पर दिए और ग्रहण किए जाते हैं, पर्सुएशन का तत्त्व कम रहता है। लेकिन बड़े विज्ञापनों में स्थिति एकदम भिन्न होती है। ऐसे विज्ञापन बड़ी-बड़ी कंपनियां देती हैं और इनमें विज्ञापन एजेंसियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। इन्हें अखबारों में प्रमुख जगहों पर छापा जाता है।
टेलीविजन के मुख्य हिस्से में विज्ञापन का आना आम बात है। यानी मीडिया के किसी भी माध्यम के लोकप्रिय कार्यक्रम में सबसे ज्यादा विज्ञापन का होना मामूली स्थिति है। इन ललचाने वाले विज्ञापनों का माध्यम केवल मीडिया के प्रचलित और नए रूप नहीं, बल्कि परिवहन के तमाम साधन भी हैं। दिल्ली और अन्य शहरों में मेट्रो के सारे डिब्बे विज्ञापनों से सजे दिखाई देते हैं। ऑटो और रिक्शा की पीठ तो पोस्टर, हैंडबिल की नुमाइश के लिए हैं ही। इसके अलावा बड़े-बड़े कटआउट्स, बिल बोर्ड, नेट पर छाए अनचाहे विज्ञापनों ने वास्तविक और संभावित उपभोक्ता को बिल्कुल गले से पकड़ रखा है।
अगर इन विज्ञापनदाता कंपनियों को विश्वास हो कि उनके सामान या बनाए गए घरों की बाजार में जरूरत है, उसकी मांग है, उनका माल गुणवत्ता के लिहाज से अच्छा है और ग्राहक की जरूरतों को पूरा करता है तो उसे भरोसा विज्ञापन से ज्यादा अपने माल पर होगा। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मालूम है कि बाजार में मंदी का दौर है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, वे बाजार जाने से बच रहे हैं। रीयल एस्टेट की हालत और खराब है। खरीददार नहीं हैं। बैंकों में जमा पैसों पर ब्याज घटाए जाने के बावजूद उपभोक्ता अपना पैसा बजार में लगाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। सरकार और राष्ट्रीय बैंक जनता का पैसा बाजार में भेज कर जोखिम उठा रहे हैं।
ऐसे में विज्ञापन, खासकर ‘पर्सुएसिव’ विज्ञापनों का समाज में होना दो बातों से तय होता है। पहला कि समाज में अतिरिक्त उत्पादन हो और दूसरा, समाज में क्रय शक्ति हो। भारत में शहरी मध्यवर्ग की क्रय शक्ति घटी है। अगर बैंक इस वर्ग को निजी जरूरतों के लिए कर्ज देना बंद कर दें तो यह वर्ग जी नहीं सकता। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन उपभोक्ता माल का उत्पादन हो रहा है। बाजार उपभोक्ता सामान से अटे पड़े हैं, लेकिन खरीददार नहीं हैं। सुंदर घर के सपनों पर उपभोक्ता आसानी से जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं, बल्कि इस तरह के किसी बड़े खर्चे को उसने भविष्य की इच्छा के रूप में संचित कर लिया है।
इसलिए रीयल एस्टेट के बड़े खिलाड़ियों की मुश्किल है कि वे ग्राहक का भरोसा कैसे हासिल करें। वे ग्राहक को इस बात के लिए कैसे मनाएं कि वह अपनी गाढ़ी कमाई उनके झूठे वादों पर निछावर कर दे। विज्ञापन को अगर संभावित उपभोक्ता न मिले तो उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता। जब किसी घाटे की चीज को नफे की वस्तु बता कर बेचना हो तो विज्ञापन करना पड़ता है। इसी अर्थ में विज्ञापन केवल सूचना नहीं, विचार और व्यवहार भी होता है। आज कोई मध्यवित्त वाला व्यक्ति साठ से अस्सी लाख रुपए का घर खरीदता है, तो वह लगभग अड़तालीस से बासठ हजार रुपए बैंकों को बीस से तीस वर्ष की अवधि तक चुकाता है। यानी व्यक्ति की औसत उम्र ऋण चुकाने में ही समाप्त हो जाती है। इससे कहीं कम में भाड़े का घर बढ़िया से बढ़िया मध्यवर्गीय इलाकों में आसानी से उपलब्ध हो सकता है। लेकिन घर के साथ इतने तरह के सामाजिक मूल्य और निजी भावनाएं जोड़ कर उसे विराट बनाया जाता है कि वह अनिवार्य निवेश लगता है, जिसके लिए व्यक्ति को कोई भी जोखिम उठा लेना चाहिए।
अब डरपोक मध्यवर्गीय मन को भरमाने के लिए इन कंपनियों को काम करना होता है। तो हाजिर होते हैं हमारे ‘सेलिब्रेटी’ यानी चमकीले चेहरे। ये घर और विलास की अन्य वस्तुओं की तारीफ करते हैं। ये जितनी चीजों की तारीफ करते हैं, विज्ञापन में उन सबकी सत्यता और विश्वसनीयता पर ठप्पा लगाने की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ये वस्तुओं के खुद उपयोग का दावा भी करते हैं। विज्ञापन में छोटे-बड़े, पठनीय-अपठनीय, आरंभ-अंत-मध्य कहीं नहीं लिखा या बताया जाता है कि सेलिब्रेटी की सामाजिक साख का विज्ञापन की सत्यता या विश्वसनीयता से कोई संबंध नहीं है। या सेलिब्रेटी केवल वस्तु के विज्ञापन और प्रचार का एक उपकरण है, जिसे भाड़े पर लिया गया है। या जिसकी सेवाओं को उस वस्तु विशेष के लिए सीमित या पूर्ण अवधि के लिए खरीदा गया है। न ही ये सेलिब्रेटी किसी साक्षात्कार, सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक मेलजोल की जगहों पर जनता से कभी यह कहते हैं कि वे जिन वस्तुओं का विज्ञापन कर रहे हैं, वह केवल प्रचार मात्र है, उस पर भरोसा न करें। बल्कि इनका और विज्ञापनदाता कंपनियों का सारा जोर इस बात पर रहता है कि हर हाल में भरोसा किया जाए।
जिस बात को आज शाहरुख खान और महेंद्र सिंह धोनी ट्वीट करके कह रहे हैं कि सेलिब्रेटी हर चीज का जानकार नहीं होता कि वह जान सके कि विज्ञापन में जो बात कही जा रही है वह ठीक है या नहीं, वह ठीक है। लेकिन यह चीज विज्ञापनदाता कंपनियां विज्ञापन में किसी भी रूप में बताने या लिखने को क्यों नहीं बाध्य हैं? वे इन चमकते साख वाले सितारों के साथ जब करारनामा करती हैं तो एक बिंदु क्यों नहीं नकार या स्वीकार का होना चाहिए, जिसमें यह बताया गया हो कि विज्ञापित वस्तु की विश्वसनीयता और सत्यता का सेलिब्रेटी से कोई लेना-देना नहीं है। या यह स्वीकार हो कि विज्ञापनदाता कंपनी सेलिब्रेटी द्वारा जो चीज विज्ञापन में कहलवा या करवा रही है उसकी विश्वसनीयता और सत्यता भरोसे के लायक है!
इस तरह गुमराह करने वाले विज्ञापनों की जवाबदेही, जिस पर सब कुछ लुटा कर उपभोक्ता निरीह बनता है, कहीं तो सेलिब्रेटी के स्तर पर भी तय होनी चाहिए। उन्हें भी पक्ष बनाना चाहिए। मीडिया का स्वनियंत्रण और एएससीआइ के तमाम नियम धनलोलुपों के पक्ष में कैसे तब्दील हो जाते हैं!