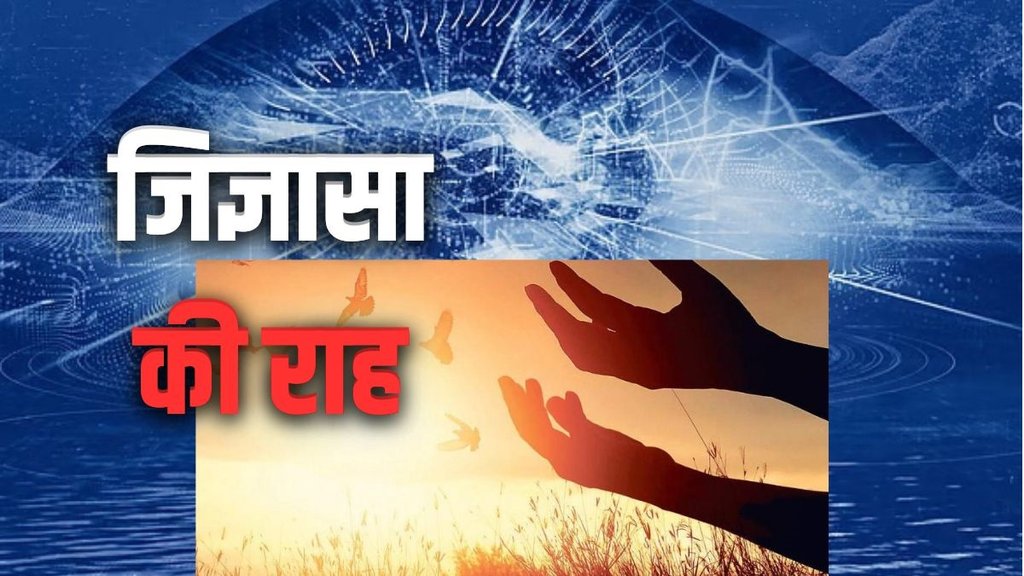दार्शनिक और धार्मिक परंपराओं के इतिहास में एक स्थायी विरोधाभास बार-बार मुखर हुआ है। एक ओर वह मूल, सरल और सर्वसुलभ साधना, जो सहज नियमों, संयम और स्वाध्याय पर आधारित है। तो दूसरी ओर वे मार्ग, जो अपने को ‘विशेष’ और ‘गुह्य’ कहकर प्रस्तुत करते हैं और जिनका आकर्षण उनकी जटिलता, नाटकीयता तथा वर्जना-भंग में निहित होता है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक विचार पर गौर किया जा सकता है, जिसमें वे कहते हैं- ‘कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो,‘गुह्य’ और ‘रहस्य’ के प्रवेश से वह विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है’। इसी सिरे से क्रिया-प्रतिक्रिया के सिद्धांत को केंद्र में रख कर एक बड़े फलक पर भी विचार की संभावना बनती है।
इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति शिखर को लक्ष्य करके पहाड़ की ओर जाती पगडंडी पकड़े चला जा रहा था, मगर उसे मार्ग नहीं पता था। थोड़ी देर चलकर उसे एक और व्यक्ति मिला, उसे भी रास्ता नहीं पता था। दोनों साथ चलने लगे। वे दोनों एक-दूसरे को नहीं जानते थे, पर उनका लक्ष्य एक था। फिर उन दो लोगों को एक और व्यक्ति मिला, जिससे रास्ता पूछने पर उसने उसी ऊसर वाले रास्ते पर सीधा चलते जाने को कहा। वे दोनों फिर चलने लगे। एक आदमी रेशम के कपड़े पहने चला आ रहा था।
शब्दों की गूंज और मौन की ताकत, चुप रहकर हम कैसे पाते हैं अंदर की शांति और जीवन का असली आनंद
उन्हें देखकर उसके भीतर कुछ जिज्ञासा हुई और तत्काल वह जिज्ञासा मुंह पर आ गई। उसने उनसे मंजिल पूछी। जानने पर उसने उन्हें उल्टी दिशा की ओर जाती पगडंडी दिखाई, पगडंडी से लगती बस्ती-बाजार का फायदा गिनाया, फिर आती गाड़ी में बैठ कर चला गया। वे दो लोग उसी पगडंडी की ओर निकल पड़े। हाट की तस्वीर से एक को समोसों की और दूजे को जलेबी की याद आ गई। साथ में दोनों को चाय की तलब हुई। चाय की दुकान पर गजलें बजाते रेडियो से चाय का पूरा पैसा वसूल हो गया। और सफर यहीं पूरा हो गया।
संदेश स्पष्ट है कि शरीर और मन का संतुलन, आहार-विहार की मर्यादा, कर्म का अनुशासन आदि। यही योग की आधारभूमि है। यह सरल प्रतीत होता है, पर यही कठिन है, क्योंकि इसमें कोई बाहरी चमत्कार नहीं, कोई रहस्यमयी अनुष्ठान नहीं, कोई मंचित विस्मय नहीं। मगर जनमानस का मन विचित्र है। वह अक्सर उस ओर आकृष्ट होता है, जो असामान्य हो, जो मंच पर खेल-सा प्रतीत हो, जहां प्रतीक, गूढ़ भाषा और इंद्रिय-उत्तेजक प्रयोग किसी ‘उच्चतर अनुभूति’ का आभास दे। ऐसे मार्ग, जो आरंभ में आत्म के विस्तार का वचन देते हैं, अक्सर अंत में आत्म की विस्मृति की ओर ले जाते हैं। इतिहास के अनेक उदाहरण इस सत्य के प्रमाण हैं, जहां आरंभिक करुणा और तप की धारा बाद में रस, राग और रहस्य के चक्रव्यूह में उलझकर अपना मूल स्वर खो बैठी।
क्या सपने पूरे करने के लिए सिर्फ संघर्ष ही जरूरी है, या आसान रास्ते से भी सुकून मिल सकता है?
वास्तविक साधना में कोई प्रवेश शुल्क नहीं, न उसे हर बार केवल कोई दूरस्थ स्थान या कोई विशिष्ट स्वीकृति चाहिए। वह तो हमारे घर के एकांत में, हमारे भीतर के मौन में, श्वास की लय और आचरण की मर्यादा में निहित है। मगर शायद इसी कारण वह भीड़ की आंखों में फीकी पड़ जाती है। भीड़ के लिए आध्यात्मिकता अक्सर एक तमाशा होती है, जिसे वे देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं और जिसके माध्यम से वे यह अनुभव कर सकें कि वे किसी असाधारण शक्ति के साक्षी बन रहे हैं। यह तमाशा चाहे चमत्कारिक उपचार हो या किसी परंपरा-विरुद्ध आचरण का सार्वजनिक प्रदर्शन, उसमें नाटकीयता का तत्त्व ही उसका मुख्य आकर्षण बन जाता है।
यही कारण है कि इतिहास में अत्यधिक भव्य और वर्जना-भंग करने वाले आंदोलनों की लोकप्रियता साधारण, लेकिन गहन मार्गों की अपेक्षा कहीं अधिक रही है। यह प्रवृत्ति केवल धर्म में ही नहीं, बल्कि साहित्य, राजनीति और कला में भी दिखाई देती है। जहां गंभीर और संयत विचार धीमी गति से फैलते हैं, वहीं उग्र और असामान्य विचार, भीतर की अपेक्षा बाहर अधिक शोर करते हैं और इसी कारण तेजी से भीड़ को आकर्षित करते हैं। मनुष्य का मन अद्भुत विरोधाभासों से भरा है। वह शांति चाहता है, पर शांति की ओर जाने वाले मार्ग पर चलने के लिए अक्सर उसका धैर्य और संयम नहीं टिकता।
कुछ छोड़ें, कुछ माफ करें और रिश्तों को मजबूत बनाएं – सच्चा सुकून चाहिए तो टेंशन से बाहर निकलें
दुनिया भर के महान ग्रंथों ने बार-बार यह संदेश दिया है कि धर्म का सार त्याग, आत्मसंयम और सत्य में निहित है। फिर भी, ‘गुप्त रहस्य’ और ‘विशेष योग’ का प्रलोभन लोगों को इस विश्वास की ओर खींचता है कि साधारण मार्ग पर्याप्त नहीं, उन्हें कुछ असाधारण चाहिए। यही वह बिंदु है, जहां साधना साधक के लिए साध्य न रहकर दृश्य-प्रदर्शन में बदल जाती है। इस विषय पर एक और गहन प्रश्न उठता है कि क्या यह प्रवृत्ति मात्र अज्ञान का परिणाम है, या इसमें सामाजिक-मानसिक संरचनाओं की भी भूमिका है!
संभव है, समाज में ‘असाधारण’ से प्रभावित होने की यह प्रवृत्ति मानव इतिहास के पुराने दौर से जुड़ी हो, जब समूह-नेतृत्व के लिए किसी विशेष या ‘दैवी’ शक्ति का प्रदर्शन अनिवार्य माना जाता था। उस काल के ‘चमत्कार’ आज के मंचीय आयोजनों में परिवर्तित हो गए हैं, पर मूल मनोवृत्ति वैसी की वैसी है। अगर हम इस मानसिक प्रवृत्ति को पहचान लें और समझ लें तो शायद हम अपने समय के अनेक अनावश्यक भ्रमों और पाखंडों से बच सकते हैं।