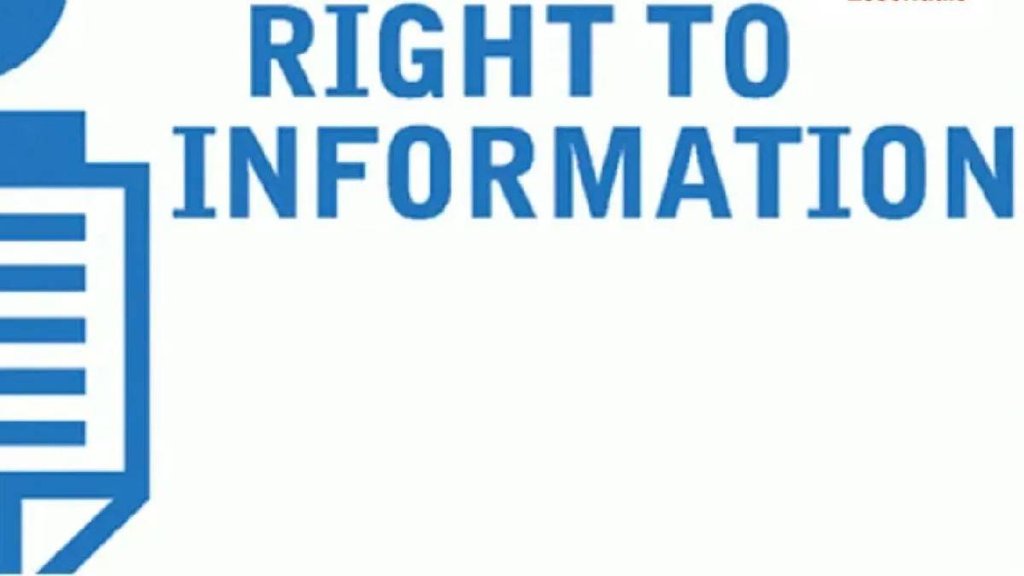सूचना का अधिकार कानून (आरटीआइ) लागू होने के बीस वर्ष पूरे हो गए हैं। जब यह कानून अस्तित्व में आया था, तब भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की एक नई उम्मीद जगी थी। यह वह दौर था, जब जनता शासन-प्रशासन से सवाल पूछने के अधिकार से लगभग वंचित थी। भ्रष्टाचार, कुशासन और मनमानी के खिलाफ कोई ठोस औजार नागरिकों के पास नहीं था। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जब मजदूरी और विकास कार्यों में गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए ‘सूचना’ को हथियार बनाया, तब एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरूआत हुई। अरुणा राय और निखिल डे जैसे कार्यकर्ताओं ने यह दिखाया कि जानकारी ही सशक्तीकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। इसी संघर्ष ने आगे चल कर पूरे देश में सूचना के अधिकार कानून का रास्ता खोला।
वर्ष 2005 में जब यह कानून संसद से पारित हुआ, तो लगा कि एक नई सुबह हुई है। अब नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय, विभाग या संस्था से यह पूछ सकता था कि उसके नाम पर पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ। यह अधिकार केवल दस्तावेज देखने तक सीमित नहीं था, बल्कि सरकार को उत्तरदायी बनाने का औजार था। यह लोकतंत्र में जनता की भागीदारी का सशक्त प्रतीक बन गया। मगर दो दशक बाद जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं, तो तस्वीर मिश्रित नजर आती है। एक ओर यह कानून कई ऐतिहासिक खुलासों का जरिया बना और लोगों को हक दिलाने में मददगार साबित हुआ, तो दूसरी ओर कई मायनों में जमीनी हालत आज भी चिंता का विषय है।
मुख्यमंत्री को देना पड़ा था इस्तीफा
इसमें दोराय नहीं कि सूचना का अधिकार कानून ने आम नागरिकों को सशक्त किया। मुंबई में आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले का खुलासा इसी कानून से हुआ था। यह वह इमारत थी, जो करगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों के लिए बनाई जानी थी, लेकिन बाद में उसमें नेताओं, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों को सस्ते दामों पर आवास दे दिए गए। परिणामस्वरूप महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह, कई बड़े घोटाले सार्वजनिक दायरे में बहस का मुद्दा बने तो इसका कारण सूचना का अधिकार कानून के तहत हासिल की गई जानकारी थी। इसके बाद पूरे देश में पारदर्शिता को लेकर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा छिड़ गई।
हमारे भीतर छिपा है सबसे बड़ा दुश्मन, उसे पहचानें; डीएनए पर हो रहे अदृश्य हमले से कैसे बचें?
राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में हुए कथित भ्रष्टाचार, मनरेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताओं और हाल के वर्षों में चुनावी बांड से जुड़ी गोपनीयता जैसे मुद्दों में भी सूचना का अधिकार एक प्रभावी साधन साबित हुआ। गांवों में लोगों ने राशन, पेंशन और मजदूरी के बकाए के लिए इसी कानून का सहारा लिया। इस कानून ने लोकतंत्र को केवल संसदीय दायरे में नहीं रखा, बल्कि उसे लोगों के रोजमर्रा के जीवन तक पहुंचाया।
कई आरटीआई कार्यकर्ताओं की हो चुकी है हत्या
मगर इस सफलता के बरक्स एक गहरी निराशा भी है। सतर्क नागरिक संगठन की रपट बताती है कि देश के उनतीस सूचना आयोगों में से कई आयोग लगभग निष्क्रिय हैं। झारखंड, त्रिपुरा और तेलंगाना में आयोग वर्षों से काम नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में भी अधिकांश पद खाली हैं। इसका सीधा असर यह हुआ है कि लाखों की संख्या में अपील और शिकायतें वर्षों से लंबित हैं। कई राज्यों में तो एक मामले का निपटारा होने में कई वर्ष बीत जाते हैं। यह उस कानून के लिए बेहद विडंबनापूर्ण स्थिति है, जो समयबद्ध सूचना देने की गारंटी देता है। वर्ष 2023-24 में केंद्रीय सूचना आयोग में पिछले दस वर्षों की तुलना में दोगुने से अधिक आवेदन दायर किए गए, लेकिन साथ ही रेकार्ड संख्या में आवेदन अस्वीकार भी हुए। बढ़ती मांग और घटती पारदर्शिता के बीच यह असंतुलन लोकतंत्र की गहराती खामोशी का संकेत है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि जिन अधिकारियों ने जानबूझ कर सूचना देने में देरी की या उसे रोका, उनमें से लगभग अट्ठानवे फीसद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह स्थिति बताती है कि जवाबदेही की भावना धीरे-धीरे खत्म हो रही है।
सियासत का सच- अब राज नहीं, पूंजी का खेल चला रहा है दुनिया, सत्ता और धर्म बने बाजार के मोहरे
जमीनी स्तर पर भी हालात चिंताजनक हैं। वर्ष 2005 से अब तक कई आरटीआइ कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। सैकड़ों को धमकियां मिली हैं।इन कार्यकर्ताओं पर हमलों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओड़ीशा और राजस्थान सबसे आगे हैं। कई कार्यकर्ताओं की हत्या से यह स्पष्ट हो गया कि सूचना मांगना अब कितना खतरनाक काम बन गया है। एक रपट के मुताबिक, अधिकतर मामलों में दोषियों को सजा नहीं मिली और सरकारों ने इन हत्याओं का कोई दस्तावेज भी नहीं रखा। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि राज्य अब सूचना मांगने वालों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। फिर भी इस कानून ने नागरिकों की सोच और शासन की शैली में गहरा बदलाव किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय, राजनीतिक दलों और भारतीय रिजर्व बैंक जैसी संस्थाओं को भी जवाबदेह बनाने की प्रक्रिया इसी कानून से संभव हुई। मगर विडंबना यह है कि वही शासन तंत्र जो कभी पारदर्शिता की शपथ लेता था, आज सूचना के अधिकार को धीरे-धीरे कमजोर कर रहा है।
अब अधिकारी इस कानून से नहीं डरते
आज स्थिति यह है कि बेरोजगारी, कोविड से हुई मौतों, अपराध के आंकड़ों या आर्थिक नीतियों के प्रभाव जैसे विषयों पर जानकारी मांगने पर ‘डेटा उपलब्ध नहीं’ कह कर जवाब दिया जाता है। सूचना कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब अधिकारी इस कानून से नहीं डरते। जहां पहले लोग उम्मीद के साथ आवेदन करते थे, अब वे निराशा के साथ लौटते हैं। यह स्थिति बताती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम न तो पूरी तरह विफल हुआ है और न पूरी तरह सफल। यह एक अधूरी यात्रा है। उसने नागरिकों को आवाज दी, लेकिन उस आवाज को सुनने वाला तंत्र अब मौन हो गया है। संस्थाओं को अब सीधे खत्म नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें अंदर से कमजोर किया जाता है। वे अस्तित्व में तो रहती हैं, लेकिन निष्प्रभावी हो जाती हैं। यही आज आरटीआइ के साथ हो रहा है।
यदि इस कानून को पुनर्जीवित करना है, तो कुछ बुनियादी कदम उठाने जरूरी हैं। बीस वर्ष पहले जब यह कानून आया था, तब यह जनता के हाथ में मशाल की तरह था जिसने अंधेरे में रोशनी फैलाई। आज वह मशाल मद्धिम जरूर हुई है, लेकिन बुझी नहीं है। यह अब भी नागरिक जागरूकता और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का सबसे बड़ा प्रतीक है। सूचना का अधिकार कानून हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल वोट डालने का अधिकार नहीं, बल्कि सत्ता से जवाब मांगने का अधिकार भी है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि उस मशाल को फिर से प्रज्वलित करें या उसे अंधेरे में खो जाने दें।
यदि नागरिक समाज, मीडिया, न्यायपालिका और ईमानदार नौकरशाही मिल कर पारदर्शिता की इस भावना को फिर से जीवित कर दें, तो यह कानून एक बार फिर अपनी मूल भावना को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा, आने वाले वर्षों में यह सिर्फ एक प्रतीक बन कर रह जाएगा, जिसका जिक्र इतिहास में तो होगा, लेकिन उसका प्रभाव खत्म हो चुका होगा। लोकतंत्र केवल कानूनों से नहीं चलता, वह नागरिकों की सतर्कता और राज्य की जवाबदेही से जीवित रहता है। यह मद्धिम होती मशाल फिर भी उम्मीद देती है कि जब तक लोग सवाल पूछते रहेंगे, तब तक रोशनी पूरी तरह बुझ नहीं सकती।