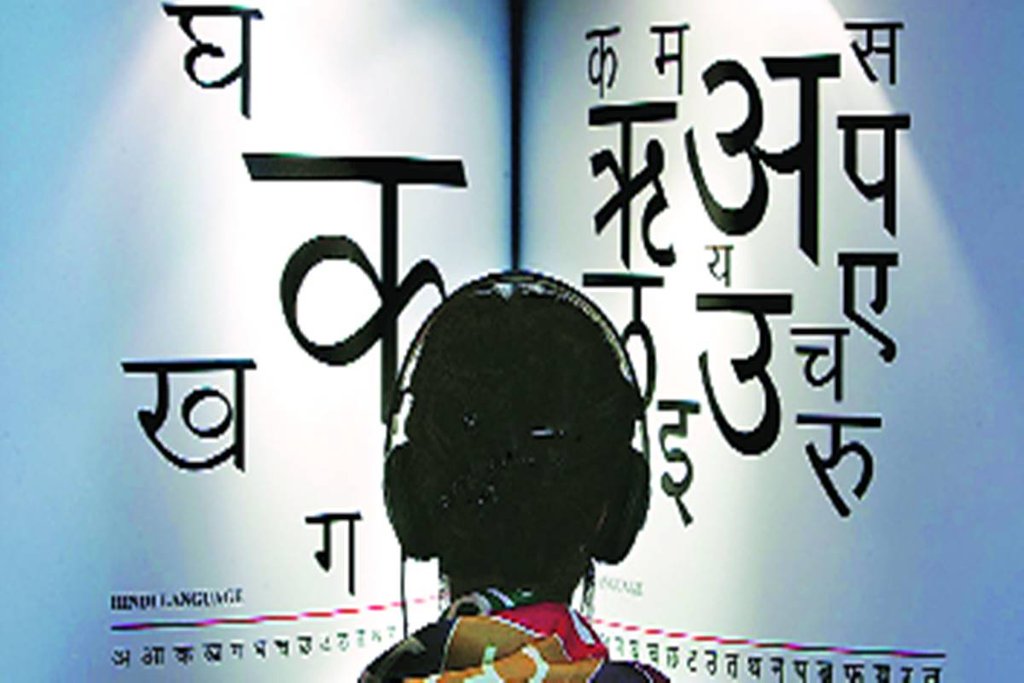हिंदी का क्या होगा? जब साहित्य की दुनिया के दिग्गज किसी अखबार और पत्रिका में हिंदी की चिंता पर लिखे अपने लेख को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे थे तो उसी समय फेसबुक पर न्यू मीडिया और नए समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समझ रखने वाले पत्रकार जे सुशील (सुशील कुमार झा) अपने इस प्रस्ताव के साथ लोगों के सामने थे कि वे अपने लेखों को भुगतान के आधार पर लाना चाहते हैं। सुशील के मुताबिक ‘पेड सब्सक्रिप्शन’ साल भर का होगा और उसमें 52 पोस्ट होंगी। यानी हर हफ्ते एक पोस्ट होगी और लंबी होगी। सब्सक्रिप्शन का लिंक लगाने के सात मिनट के अंदर ही तीन लोग उनके ग्राहक बन गए।
सुशील फिलहाल अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने कहा कि उनकी पेड पोस्ट में किताबें, सिनेमा, डॉक्युमेंटरी, अमेरिकी जीवन, कभी-कभार भारतीय राजनीति, आर्ट से जुड़े कुछ पोस्ट, किताबें कैसे पढ़ी जाएं या फिर कुछ वाययीव पोस्ट मसलन फैक्ट और वैल्यू से जुड़ी मोटी बहसें होंगी। अपने भुगतान वाले लेखों में उन्होंने आइआइआटी दिल्ली के युवा प्रोफेसर को जोड़ने की भी बात कही।
सुशील अपनी पोस्ट में लिखते हैं, ‘आप सब लोग पेड सब्सक्रिप्शन लेकर एक नई किस्म की शुरुआत करेंगे फेसबुक पर। मुझे नहीं पता कि भारत में कोई ऐसा कर रहा है या नहीं।’ रोचक तथ्य यह है कि बहुत से लोगों ने उन कई विद्यार्थियों के लिए वजीफे के तौर पर पोस्ट का भुगतान किया जो सुशील को पढ़ना चाहते थे। हालांकि संपर्क करने पर सुशील ने कहा कि मेरे पेड पोस्ट हिंदी या किसी भाषा का मसला नहीं है। मसला यह है कि लोग खराब कंटेंट से दुखी हैं और पैसे देकर भी अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं।
दरअसल, पिछले दो दशक में इंटरनेट ने पूरी दुनिया के लोगों को नया मंच दिया तो हिंदी बोलने वाले भी इस मंच पर आए और साबित किया कि हिंदी नए समय के दरकारों को कामयाबी के साथ पूरा कर सकती है। इसका एक पूरा ढांचा खड़ा होने लगा तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट यूनिकोड लेकर आए। गूगल की भाषाई समझ में ‘बिहारी’ तक स्वतंत्र भाषा है।
वहां ‘लटपटा गए हैं’ भी स्वीकार्य है। यहां जो बात समझने की है, वह यह कि तकनीक का बड़ा से बड़ा जोर भी बोली और भाषा की ताकत की न तो अवहेलना कर सकता है और न ही इसका किसी भी तौर पर कोई विकल्प रच सकता है। बात अकेले सूचना तकनीक की करें तो इसने भाषाई संभावनाओं के कई ऐसे प्रयोग आजमाए, जिसमें हम अपनी ही भाषा से सर्वथा नए सिरे से परिचित हुए।
आलम यह कि दो-तीन दशक पहले जो विद्वान बड़े-बड़े अखबरों-जर्नलों में अपने लेखों के जरिए यह दावा कर रहे थे कि तकनीक का नया संजाल अभिव्यक्ति और भाषा के स्वायत्त चरित्र को समाप्त कर देगा, वे आज इन्हीं माध्यमों के जरिए देश-दुनिया का लोकतंत्र बचाने से लेकर नस्लवाद के कारगर विरोध और जेंडर संघर्ष के लिए तार्किक विमर्श रच रहे हैंं।
मिस्र, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के कई देशों और अमेरिका की सड़कों पर हजारों-लाखों की संख्या में उतरे लोगों की हाथों में जो तख्तियां हैं, वो दरअसल नए समय में बदलाव की नई इबारतें हैं। यही नहीं, उनके हाथों में जो कंदीलें जल रही हैं, उनकी रोशनी इस भरोसे का हामी है कि मनुष्य और उसके सरोकार किसी परिस्थिति विशेष में नजरअंदाज तो हो सकते हैं, पर खारिज हरगिज नहीं।