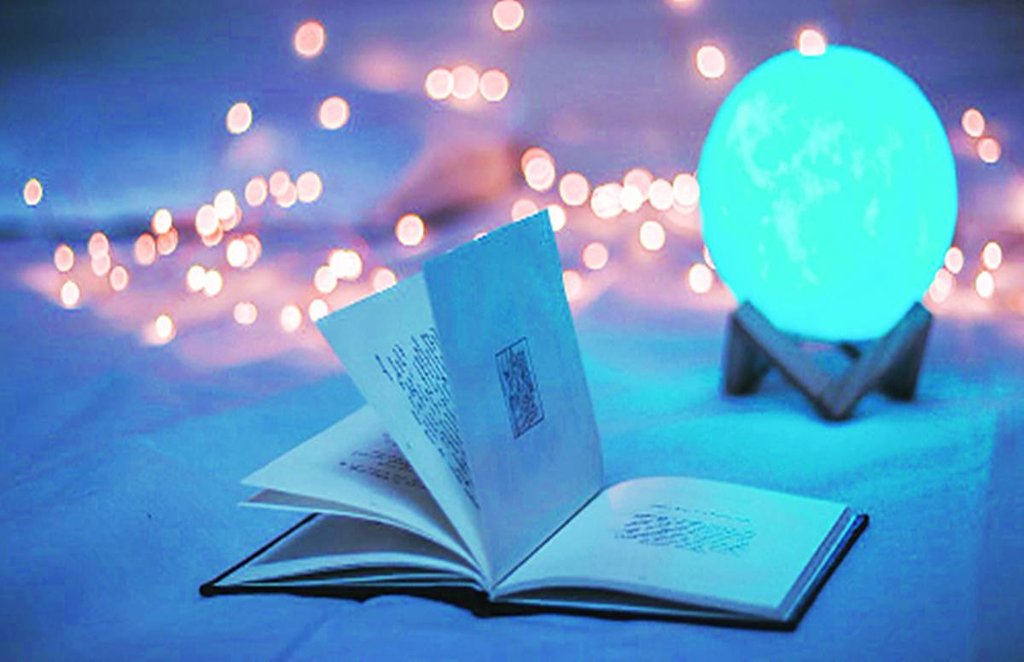भोपाल में उत्कृष्टता संस्थान के प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह वेबिनार की परंपरा को नई संभावना के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि अभी यह नई पद्धति है, इसलिए लोगों को इससे तादात्म्य बिठाने में कुछ कठिनाई आ रही है, मगर बहुत जल्दी लोग इसके अभ्यस्त हो जाएंगे और बेहतर नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। वेबिनार के कारण कई तरह की आसानी हुई है।
धन और समय की बचत तो हो ही रही है, संपर्क का दायरा बढ़ा है। अब देश-दुनिया के सभी कोनों के विद्वान आपस में जुड़ कर किसी विषय पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। पहले ऐसी सुविधा न होने से शोध-पत्रों की पहुंच भी बहुत सीमित दायरे में हो पाती थी। इसलिए उनमें गुणवत्ता विकास की संभावना सीमित होती थी, पर जब इसका क्षेत्र विस्तृत होगा, तो शोध-पत्रों की गुणवत्ता भी निखरेगी।
मगर आंबेडकर विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत वेबिनार को शोध के लिहाज से उचित माध्यम नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि वेबिनार कभी सेमिनार का विकल्प नहीं हो सकता। शोध की प्रक्रिया अक्सर सेमिनार के बाद शुरू होती है और वहां से उसके वास्तविक आयाम खुलते हैं। साहित्यिक गोष्ठियों, रचना-पाठ वगैरह के लिए तो वेबिनार एक माध्यम अवश्य हो सकता है, पर शोध कार्यों में इससे गुणवत्ता प्रभावित होगी। जब भी स्थितियां सामान्य होंगी, सेमिनार की परंपरा को चलाए रखना होगा।
हालांकि साहित्यिक गतिविधियों में गरमी बनाए रखने के मकसद से जूम, गूगल मीट और फेसबुक लाइव जैसे मंचों पर इस बीच खूब सक्रियता रही, मगर कुल मिला कर उनमें नई पीढ़ी के रचनाकारों की सक्रियता ही अधिक दिखाई दी। पुरानी पीढ़ी के, तकनीकी संसाधनों से सहज महसूस न कर पाने वाली पीढ़ी के रचनाकार न तो इनमें ठीक से शिरकत कर पाए और न उन पर चल रही गतिविधियों से रूबरू हो पाए। इसलिए चहल-पहल तो खूब दिखाई दी, मगर जैसी ऊष्मा सांस्थानिक मंचों से पैदा हुआ करती थी, वह महसूस नहीं हो पाई।
एक तो यह भी वजह समझी जा सकती है कि तकनीक कुछ सुविधा जरूर उपलब्ध करा देती है, मगर उसमें एक तरह का नीरसपन और ऊब पैदा करने वाला तत्त्व भी होता है। सेमिनारों के समागम में जीवंतता होती है। परस्पर मेलजोल से जो रचनात्मक ऊर्जा और ऊष्मा पैदा होती है, वह वेबिनार के मंचों पर शायद उपलब्ध होने से रह जाता है। खुली वैचारिक बहसों से प्राप्त होने वाला अनुभव और आनंद वेबिनार देता नजर नहीं आता।