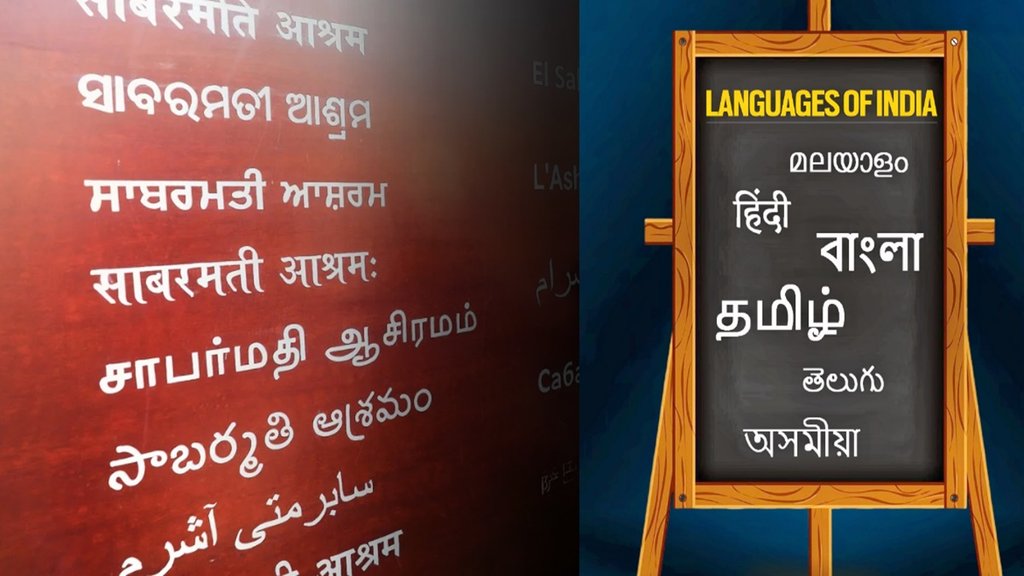मातृभाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती। उससे व्यक्ति के जीवन की शुरुआत के संस्कार जुड़े होते हैं, इसलिए वह अपने उपयोगकर्ताओं के लिए आत्मिक और मानसिक संबल भी होती है। शायद इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बार कहा था- ‘निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल।’ यानी अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का आधार है।
आजादी के पहले जब अंग्रेजों ने भारत में लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति लागू की थी, तो उसका भी उद्देश्य यही था कि भारतीयों से उनका सांस्कृतिक और भाषाई गौरव छीन लिया जाए, ताकि ब्रिटिश शासन को उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पढ़े-लिखे सेवक मिल सकें। कहना नहीं होगा कि अंग्रेज अपनी इस नीति में बहुत हद तक सफल भी रहे थे।
आजादी के बाद भी समाज में ऐसा वर्ग आज भी अभिजात्य होने के गर्व में जीता है, जो अंग्रेजी और अंग्रेजियत को ही सार्थक जीवन का सोपान समझता है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि ऐसी कई भारतीय भाषाएं हैं जो सीधे तौर पर रोजगार से नहीं जुड़ी होने के कारण धीरे-धीरे चलन से बाहर हो गई हैं और आज उनका उपयोग करने वाले लोग कम ही बचे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जरवां, शोम्पेन, वहीं मणिपुर की एमोल, कोइरेन, तराओ; हिमाचल प्रदेश की बधाती, हंदुरी, पंगवाली, ओड़ीशा की मंडा, परजी, पेंगो; कर्नाटक की कोरोगा, कुरूबा और इसी तरह असम की तेई नोरा एवं तेई तेई रोंग ऐसी ही भाषाएं हैं। यूनेस्को की सूची में ऐसी 197 भारतीय भाषाएं हैं जो या तो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं।
आधुनिक समाज के सम्मुख प्राचीन भाषाओं के साथ उनकी लिपियों को बचाने का भी संकट है। संकटग्रस्त भाषाएं श्रुति परंपरा के कारण किसी तरह से कुछ और समय तक अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सफल होती भी हैं, तो प्रचलन से बाहर होने के कारण उनकी लिपि को पढ़ने और समझने वाले नहीं मिलते।
राजस्थानी भाषा के उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है। इस भाषा को बोलने वालों की संख्या आज भी करोड़ों में है, लेकिन प्राचीन राजस्थानी लिपि मुंडिया को पढ़ने और समझने वाले लोग आज गिनती के हैं।
दरअसल, आजादी के बाद तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए देश की एकता बचाए रखने के लिए सेठ गोविंद वल्लभ पंत ने राजस्थानी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखने का आग्रह किया। राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने के लिए राजस्थानियों ने इस भावनात्मक आग्रह को स्वीकार कर लिया।
परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे मुंडिया लिपि चलन से बाहर हो गई और उससे परिचित लोग घटते चले गए। आज जब राजस्थानी भाषा के समर्थक अपनी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग करते हैं, तब विरोधियों द्वारा एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इस भाषा की पृथक लिपि ही नहीं है।
भाषा के सवाल को राजनीतिक सवाल के तौर पर भी बार-बार इस्तेमाल किया गया है। भाषा से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव क्या रूप ले सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण है। वर्ष 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, तो उन्होंने गंगा और सिंधु की धरती को बांट दिया। तब ढाका की तरफ वाले हिस्से यानी पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान में शामिल होना बेहतर लगा। मगर धीरे-धीरे पूर्वी बंगाल के लोगों का मोह टूटने लगा। इस क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया। मगर जब वहां की भाषा को विस्थापित करने की कोशिश की गई, तो जनता के सब्र का बांध टूट गया। फिर हिंसा फैली और भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा। परिणामस्वरूप एक नए राष्ट्र का उदय हुआ।
भारत में भाषाएं बार-बार संघर्ष का मुद्दा बनती हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रवासी बांग्लाभाषियों के हितों की रक्षा के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसे बांग्ला भाषा अभियान नाम दिया गया है।
कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी की सुगबुगाहट हुई थी। दक्षिण भारत में तो हिंदी विरोध के कई आंदोलन हुए। उत्तर और पूर्वी भारत में भाषा के नाम पर राज्यों के पुनर्गठन किए गए हैं। भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था जो तत्कालीन मद्रास राज्य के तेलुगू भाषी क्षेत्रों से बना।
दरअसल, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किए जाने की बात जब संविधान सभा में बार-बार उठी, तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1948 में इलाहबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इस पर जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की सदस्यता वाली एक समिति बनाई गई। इस समिति ने भी अपनी सिफारिशों में आयोग की बात का समर्थन किया।
इसके बाद तेलुगू भाषियों ने आंदोलन कर दिया। अक्तूबर 1952 में पोट्टी श्रीरामालू ने तेलुगू भाषी आंदोलन के तहत अपनी मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन के 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया और अंतत: सरकार को झुकना पड़ा। आजाद भारत में ही बंबई राज्य का विभाजन मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर किया गया। वर्ष 1966 में असम से नगालैंड, वर्ष 1966 में ही पंजाब से हरियाणा बनने जैसी घटनाओं के पीछे भी भाषा ही आधार रही।
आज भी मैथिली, भोजपुरी, मुंडारी, अंगिका और राजस्थानी बोलने वाले लोग अपनी-अपनी भाषाओं के संरक्षण के लिए चिंतित हैं और उन्हें संवैधानिक मान्यता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इन भाषाओं के समर्थकों का कहना है कि उनकी भाषा को संवैधानिक संरक्षण या मान्यता नहीं मिली, तो नई पीढ़ी अपनी भाषा से दूर होती जाएगी।
इस तरह उनकी भाषा के अस्तित्व पर संकट बढ़ता चला जाएगा। मगर यूनेस्को द्वारा संकटग्रस्त घोषित 197 भाषाओं की सूची में शामिल भूमिज भाषा के समर्थकों ने अपने अनूठे संकल्प से यह साबित कर दिया कि भाषा के सबसे बड़े संरक्षक उसके अपने समर्थक होते हैं। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के जंगल महल क्षेत्र यानी झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिमी मेदिनीपुर जिलों में भूमिज समुदाय की एक बड़ी आबादी रहती है। इस समाज के कुछ जागरूक लोगों ने वर्ष 2018 में अपनी भाषा को बचाने के लिए कुछ करने की ठानी और क्षेत्र में ऐसे स्कूल खोले, जहां लोगों को अपनी भाषा का शिक्षण दिया।
नई पीढ़ी को अपनी भाषा से जोड़ने के लिए पढ़ाया भी। परिणाम यह हुआ कि जिस भाषा के अस्तित्व पर संकट मंडराता दिखता था, उसे पचास हजार से अधिक लोगों ने सीख लिया। अब इन पचास हजार लोगों को यह दायित्व दिया गया है कि वे कम से कम एक व्यक्ति को भूमिज भाषा सिखाएंगे।
रूस के महान उपन्यासकार फ्योदोर दोस्तोएव्स्की ने एक स्थान पर लिखा है- ‘यदि तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारा सम्मान करें, तो इसकी सबसे पहली और सबसे महत्त्वपूर्ण जरूरत यह है कि तुम स्वयं अपने आप का सम्मान करो।’ भूमिज समुदाय के लोगों ने अपने संकल्प से यह साबित किया है कि अपनी मातृभाषा के संरक्षण के लिए किसी का मुंह ताकने से अच्छा है कि हम स्वयं अपने संकल्पों को हौसलों का आसमान दें।