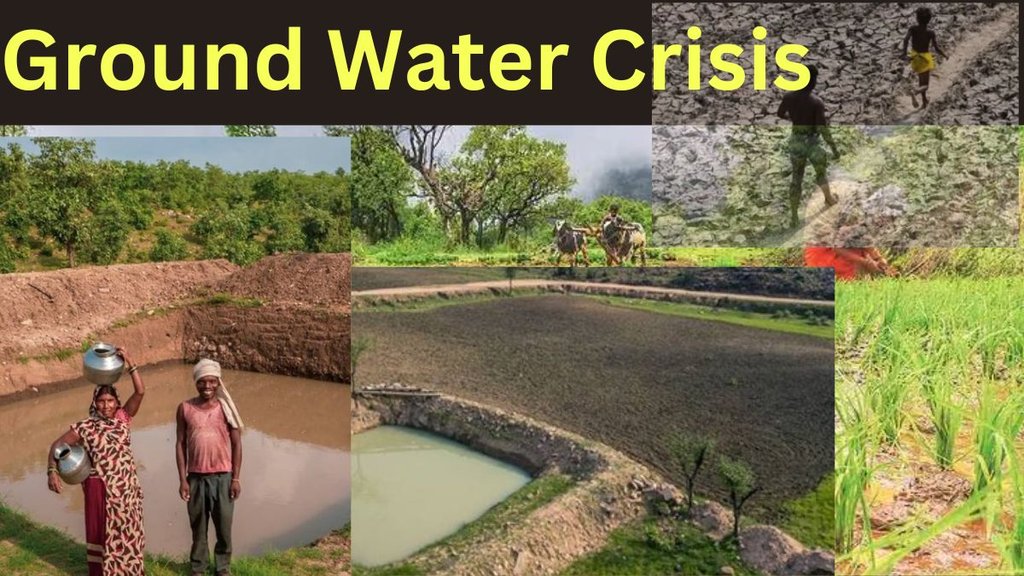एम. दिनेश कुमार और कामना झा
Water Crisis in India and Solutions: हाल ही में दिनेश कुमार और चेतन पंडित ने एक लेख में भारत के जल प्रबंधन पर चर्चा की है, जिसमें उन्होंने जल प्रबंधन के क्षेत्र में विपरीत विचारों के बारे में लिखा है। उनका कहना है कि ये विपरीत विचार आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सही उपयोग में रुकावट डालते हैं। वे बताते हैं कि मौजूदा हालात को अतीत से अलग करने वाली एक बड़ी बात सिविल सोसायटी की पैरवी करने वालों का उदय है। ये लोग जल, ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित तमाम नीतियों के समर्थन या विरोध में जोरदार अभियान चलाते हैं, जो देश के सामाजिक ताने-बाने और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डालता है।
विपरीत विचारों का बड़ा संकट
कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि सिविल सोसायटी की पैरवी करने वालों का असली मकसद आर्थिक एजेंडों को प्रभावित करना है, और जल, ऊर्जा और पर्यावरण नीतियां इस उद्देश्य को साधन के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं। चाहे जैसा भी हो, यह साफ है कि ये सिविल सोसायटी समूह राजनीतिक गतिविधियों में लगा है और सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।
नागरिक समाज का प्रभाव
सिविल सोसायटी और जल प्रबंधन के बीच एक जटिल संबंध है, जिसे जल क्षेत्र के पेशेवरों को समझना चाहिए। भारत में विद्वानों और व्यवसायियों के बीच जल प्रबंधन पर चल रही बहस में दिखता है कि इस वर्ग के कुछ विचारों में एक नकारात्मक पूर्वाग्रह है। यह पूर्वाग्रह अक्सर ‘आक्रामक’ रूप में सामने आता है, लेकिन दिलचस्प यह है कि ऐसे विचारक आधुनिक सरकारों द्वारा अपनाए गए विकास के ‘विनाशकारी रूपों’ के प्रति अपनी चिंता ज़ाहिर करते हैं। जब हम यह देखते हैं कि ये विचारक महत्वपूर्ण नीति दस्तावेजों की मसौदा समितियों पर भी प्रभाव डालते हैं, तो उनकी चिंताएं और भी गंभीर हो जाती हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दिल्ली में बाढ़ से हुए नुकसान को कुछ लोग अतीत में ऐसे मुद्दों की अनदेखी का परिणाम मानते हैं।
जल प्रबंधन में नकारात्मक पूर्वाग्रह
जैसा कि कुमार और पंडित ने अपने लेख में बताया है, सिविल सोसायटी समूह उन लोगों के लिए ‘घरेलू नलों के माध्यम से आपूर्ति किए गए आयातित पानी’ के विरोध में खड़े हैं, जो जल की कमी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। वे पारंपरिक जल निकायों को पानी के स्रोत के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं और बड़े बांधों का विरोध कर रहे हैं, यह कहते हुए कि वे ‘नकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव’ पैदा करते हैं। इन समूहों का समर्थन विकेंद्रीकृत जल संचयन के लिए है, लेकिन वे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी जल अवसंरचना के विकास के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हैं।
बड़े बांधों का विरोध और जल संरक्षण
वे आधुनिक सिंचाई प्रणालियों, जलाशयों और बड़ी परिवहन प्रणालियों का विरोध करते हैं, और केवल पारंपरिक तालाबों और टैंकों को ही टिकाऊ मानते हैं। इनमें से अधिकतर लोग सिंचाई का विरोध करते हैं और वर्षा आधारित फसलों को बढ़ावा देने का तर्क देते हैं, यह कहते हुए कि इसे करने से पानी की खपत कम होती है। इसके अलावा, वे जल विद्युत बांधों के खिलाफ हैं, जो ‘खराब बिजली’ पैदा करते हैं, और केवल सौर एवं पवन ऊर्जा को ‘स्वच्छ ऊर्जा’ मानते हैं।
सिंचित जल और फसलें
भारत में जल प्रबंधन के संदर्भ में नागरिक समाज संगठनों (सिविल सोसायटी आर्गनाइजेशन) द्वारा प्रस्तुत कुछ विकल्पों में “पौधरोपण” एक प्रमुख समाधान के रूप में उभरा है। यह विचार कि पौधरोपण नदियों को पुनर्जीवित कर सकता है और भूजल पुनर्भरण में सहायता कर सकता है, ने जन सामान्य का ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि, यह जानना महत्वपूर्ण है कि पेड़ों की भूमिका जैविक पंप के रूप में कार्य करती है, जिससे मिट्टी की सतह और उथले भूजल से पानी का भारी नुकसान हो सकता है। इस तथ्य पर आमतौर पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
इसके अलावा, जबकि वर्षा जल के रिसाव में पेड़ों की भूमिका को बढ़िया बताया गया है, कई अध्ययनों से पता चलता है कि घास का आवरण वर्षा जल के रिसाव को सुधारने में कहीं अधिक प्रभावी है। यह महत्वपूर्ण है कि जल संरक्षण के उपायों का मूल्यांकन तथ्यों के आधार पर किया जाए, न कि केवल प्रचारित दावे के आधार पर।
विकल्प और नीतियों का मूल्यांकन
दूसरी ओर, भूजल में कमी को रोकने के लिए एक आम तौर पर सुझाया जाने वाला उपाय, खास तौर पर पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार को बदलना है। उदाहरण के लिए, अक्सर धान की जगह ऐसी फसलें उगाने की सलाह दी जाती है, जो बहुत ज़्यादा पानी की खपत करती हैं, और ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो कम पानी का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि यह सच है कि धान, गेहूं, ज्वार और बाजरा को काफी मात्रा में सिंचाई की ज़रूरत होती है। तमाम कारकों के आधार पर लगभग 1,000 से 1,500 मिमी तक पानी की जरूरत होती है, लेकिन कई नीति निर्माता और विशेषज्ञ धान की सिंचाई में शामिल पानी की गतिशीलता को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। इसलिए, जल प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों को सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत है, ताकि ये वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण का पालन करें और वास्तविक मुद्दों का समाधान प्रदान करें।
सिंचित जल का उपयोग और समाधान
जल प्रबंधन से संबंधित मुद्दे और समाधानों के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि सिंचित जल का उपयोग और इसके प्रभावों के बारे में गहरी समझ की जरूरत है। पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा (भारत) तथा दक्षिण कोरिया जैसे क्षेत्रों में तमाम अध्ययन यह दर्शाते हैं कि धान के खेतों में सिंचित जल से उथले भूजल में पानी का रिसाव होता है। इसे केवल खपत के रूप में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि यह वास्तव में भूमि और जलवायु पर निर्भर करता है। विशेष रूप से एशिया के कई हिस्सों में धान मुख्य रूप से मानसून के दौरान उगाया जाता है, और धान के खेत वर्षा जल को रिसने के लिए फैलाने वाले बेसिन के रूप में कार्य करके भूजल संतुलन को सुधारने में मदद करते हैं। इस दृष्टिकोण से पंजाब में भूजल की कमी का संभावित समाधान फसल की तीव्रता को कम करने में है, जिससे कुल वाष्पोत्सर्जन मांग में कमी आएगी।
हालांकि, वास्तविक चिंता इस बारे में नहीं है कि जल समस्याओं का समाधान खोजने में देरी हो रही है, बल्कि यह है कि कई समाधानों को लागू करने में सावधानी नहीं रखी जाती है। केंद्र सरकार की जल प्रबंधन के लिए एक लंबी अवधि का विजन है, लेकिन हम ऐसे उपायों को लागू कर रहे हैं जो उस दृष्टि का हिस्सा नहीं होते और जिनकी प्रभावशीलता का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
टेक्नोक्रेट्स की भूमिका
इस स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि टेक्नोक्रेट्स को शामिल किया जाए जब हम जल प्रबंधन के समाधानों की योजना बनाते और उन्हें लागू करते हैं। आधे-अधूरे समाधानों का परिणाम अक्सर उम्मीद से अधिक महंगा होता है। उदाहरण के लिए, एक सटीक मामला यह है कि जलाशयों के ऊपरी जलग्रहण (Upper Catchments) क्षेत्रों में बनाए गए चेकडैम वाष्पीकरण के कारण जलवायु संघर्ष को बढ़ा रहे हैं, जिससे उनके द्वारा संचित पानी की मात्रा वास्तव में घट रही है। इसलिए, जल प्रबंधन के लिए सतत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है ताकि दीर्घकालिक योजनाओं को वास्तविकता में बदलने का प्रयास सफल हो सके और जल संसाधनों का संरक्षण हो सके।
भारत में जल संकट की समस्या काफी गंभीर और तेजी से बढ़ती जा रही है। मध्य, प्रायद्वीपीय और पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों में लोग पहले से ही इस गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। भविष्य में भी पानी की कमी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस संकट का सामना करने के लिए ठोस कदम उठाएं।
जैसा कि कुमार और पंडित ने उल्लेख किया है, जब भविष्य के इतिहासकार भारत की जल समस्याओं का लेखा-जोखा लेंगे, तो संभवतः यह निष्कर्ष निकालेंगे कि भारत ने पानी की भयंकर कमी का सामना इसलिए नहीं किया कि टेक्नोक्रेट समुदाय ने गलत निर्णय लिए, बल्कि इसलिए कि सिविल सोसायटी ने उन्हें अंतहीन चर्चाओं और न्यायिक लड़ाइयों में उलझाकर रखा। इसके चलते, टेक्नोक्रेट समुदाय को जरूरी और प्रभावी निर्णय लेने से रोका गया, जिससे जल संकट के समाधान में देरी हुई।
इसलिए, यह आवश्यक है कि हमें संवाद, सहयोग और स्वायत्तता के साथ काम करना चाहिए। जल प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट और दीर्घकालिक रणनीति विकसित करना आवश्यक है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों –सरकार, टेक्नोक्रेट, और नागरिक समाज–की अंतर्दृष्टि को शामिल किया जाए। केवल तभी हम इस जल संकट का प्रभावी और सतत समाधान खोजने में सफल हो सकेंगे। जल संसाधनों का संरक्षण और कुशलता से उपयोग करना, न केवल वर्तमान पीढ़ियों के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी आवश्यक है।