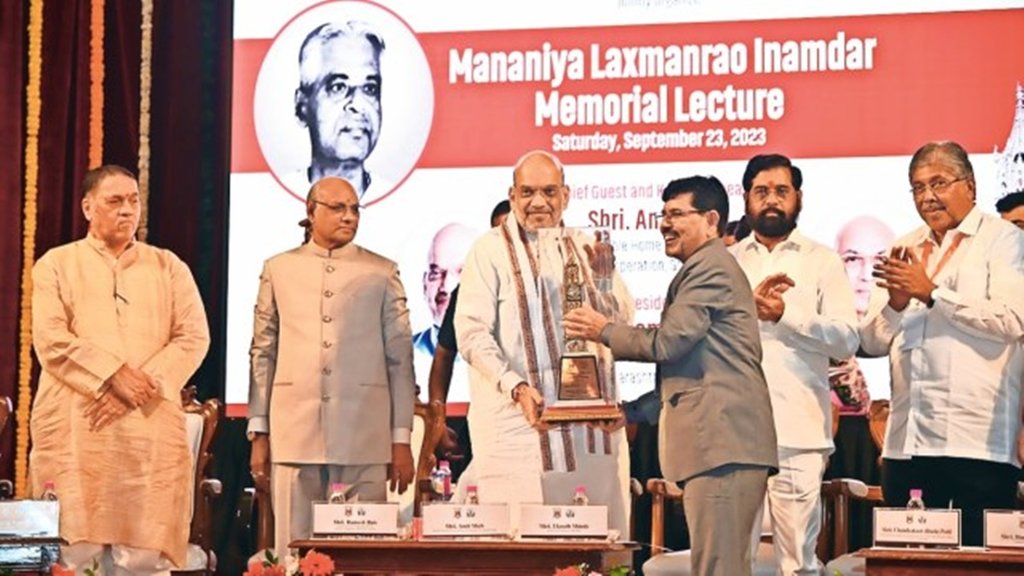दुनिया भर में वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है- सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता वर्ष के लिए जो विषय लिया, वह भारत सरकार के ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है। भारत में सहकारी समितियों की अच्छी-खासी संख्या है। ग्यारह दिसंबर, 2024 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सहकारिता मंत्री ने बताया था कि देश में कुल 6,21,514 सहकारी समितियां हैं। समितियों का यह तंत्र भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में सहकारिता की महत्त्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करता है। सबसे अधिक कार्यरत सहकारी समितियों वाला राज्य महाराष्ट्र है, सहकारी आंकड़ों के अनुसार यहां सहकारी संस्थाएं दो लाख से अधिक हैं। इन समितियों से जुड़े 7,96,65,337 लोगों के साथ इसका सदस्यता आधार भी सबसे बड़ा है। महाराष्ट्र में इतनी कार्यरत समितियां सहकारी आंदोलनों विशेष रूप से कृषि, डेयरी और ग्रामीण बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में मजबूत संगठनात्मक ढांचे को दर्शाती हैं।
अमूल डेयरी उद्योग में नए मानक स्थापित किए हैं
गुजरात की सहकारी संस्था ‘अमूल’ अपनी सफलता की कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। उसने डेयरी उद्योग में नए मानक स्थापित किए हैं। राज्य की सहकारी पहलों ने किसानों, लघु उत्पादकों और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में अहम योगदान दिया है। कर्नाटक 38,828 सहकारी समितियों और 2,36,76,736 लोगों की सदस्यता के साथ समितियों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। कर्नाटक में सहकारी क्षेत्र विविध है, जिसमें ऋण समितियां, कृषि विपणन और कृषि उपज का प्रसंस्करण शामिल है। इसने राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करने में भी सहायता की है।
इसी तरह केरल में 7,076 कार्यशील सहकारी समितियां हैं और 2,94,72,329 व्यक्तियों की सदस्यता है। यह आंकड़ा राज्य में सहकारी समितियों की दक्षता और व्यापक पहुंच को दर्शाता है। केरल का सहकारिता माडल समावेशी विकास पर केंद्रित है और यह क्रेडिट यूनियनों, उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा आवास समितियों के जरिए कल्याणकारी गतिविधियों को संचालित करता है। उत्तर प्रदेश में भी सहकारी संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण उपस्थिति है, जहां 19,587 समितियों के साथ 1,86,72,654 सदस्य जुड़े हुए हैं। ये समितियां इस घनी आबादी वाले राज्य में ग्रामीण और कृषि विकास के लिए संसाधन जुटाने में अहम भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। बिहार में 16,475 समितियां 1,53,81,807 सदस्यों के साथ सहकारी उपक्रमों में ग्रामीण आबादी की सक्रिय भागीदारी दर्शाती हैं।
सहकारिता का भारतीय कृषि में अहम योगदान, मंत्रालय से अलग होने पर किसानों को जगी उम्मीद
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप जैसे छोटे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सहकारी समितियों की संख्या कम है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1,210 कार्यरत सहकारी समितियां हैं, जिनके 73,182 सदस्य हैं। जबकि लक्षद्वीप में 30 समितियां हैं, जिनके 79,091 सदस्य हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद ये सहकारी समितियां इन क्षेत्रों की विशिष्ट आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से ऋण तक पहुंच प्रदान करने और स्थानीय आजीविका को सहारा देने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही हैं।
कुल मिला कर भारत में सहकारी क्षेत्र अपनी पहुंच और प्रभाव में विविधता प्रदर्शित करता है। देश भर में सहकारी समितियों का यह व्यापक संजाल समुदायों को सशक्त बनाने, आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। सहकारी समितियां जन-केंद्रित उद्यम हैं, जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन उनके सदस्यों द्वारा उनकी साझा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए किया जाता है।
हालांकि, देश भर में फैली सहकारी समितियां सरकार के ‘सहकार से समृद्धि’ के लक्ष्य को पूरा करने की दृष्टि से उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, जितना अपेक्षित है। इसका कारण उनके सामने कई चुनौतियां हैं। अधिकांश सहकारी समितियां अपनी पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की कमी की चुनौतियों से जूझ रही हैं। कार्य संचालन में सदस्यों की सीमित भागीदारी, हाशिये पर पड़े समुदायों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा कुछ व्यक्तियों के पास सत्ता का केंद्रीयकरण सहकारी समितियों की समावेशी प्रकृति को कमजोर करता है।
कौन हैं त्रिभुवनदास पटेल जिन्हें माना जाता है सहकारिता आंदोलन का जनक, अमूल से क्या है कनेक्शन?
हाशिये पर पड़े समुदायों की सेवा करने वाली समितियों को वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में कई कठिनाइयों का सामना पड़ता है। उनके पास अक्सर पारंपरिक वित्तीय संस्थानों द्वारा अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं और दस्तावेजों की कमी रहती है, जिससे उनके लिए ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इनके लिए आधारभूत संरचना की कमी भी उनकी दक्षता तथा प्रभावशीलता को प्रभावित करती है, जिससे उनकी पहुंच सीमित हो जाती है।
वित्तीय सेवाएं देने वाले सहकारी बैंक और सहकारी समितियों के लेन-देन में भ्रष्टाचार और उनके संचालन संबंधी दिक्कतों के कारण आम जमाकर्ता का पैसा या तो डूब जाता है या अटक जाता है। इस कारण जमाकर्ताओं का बैंकिंग कार्य करने वाली सहकारी समितियों से लोगों का विश्वास खत्म होने लगता है। इससे भी सहकारी समितियों की साख पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो सहकारी संस्थाएं निर्माण कार्य में लगी हुई हैं, वे बड़ी कंपनियों द्वारा उत्पादित माल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पातीं, क्योंकि उनके उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बड़ी कंपनियों के उत्पादों या सेवाओं की तुलना में कमजोर रह जाती हैं। इस कारण भी ये सहकारी संस्थाएं पिछड़ जाती हैं।
बड़ी कंपनियों के लुभावने विज्ञापन और विपणन अभियान के कारण भी सहकारी संस्थाएं पीछे रह जाती हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में कार्यरत समितियों के उत्पाद को विक्रय स्थल तक लाने-ले जाने के लिए परिवहन की कमी का भी सामना करना पड़ता है। कुछ सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों का भ्रष्टाचार इन संस्थाओं के विकास और उनकी जन सहभागिता को प्रभावित करता है।
सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के अनुरूप सहकारिता को लागू करने के लिए सहकारी समितियों का नियमित आडिट होना और सहकारी संस्थाओं में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना जरूरी है। हाशिये पर छूट गए समुदायों की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से उनकी सहभागिता भी आवश्यक है। सहकारी समितियों को अन्य नए तरीके से वित्तपोषण के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सदस्यों को शिक्षित करने और उनको आकर्षित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं तथा चुनौतियों का समाधान करने में सहायक हों।
ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और अधिक सरकारी निवेश, सहकारी समितियों के लिए संचार व्यवस्था और बाजारों तक पहुंच के लिए संसाधनों का विकास किया जाना आवश्यक है। सहकारी संस्थाओं के सदस्यों और प्रबंधकों के लिए कौशल निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाना चाहिए। संभावित सदस्यों को सहकारी समितियों के लाभों और सिद्धांतों के बारे में शिक्षित करने के लिए स्थानीय भाषाओं में जागरूकता अभियान की जरूरत है। अगर केंद्र और राज्य सरकारें तथा सभी संबंधित पक्षकार मिल-जुल कर प्रयास करें, तो सहकारिता को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था में उसका योगदान भी बढ़ेगा।