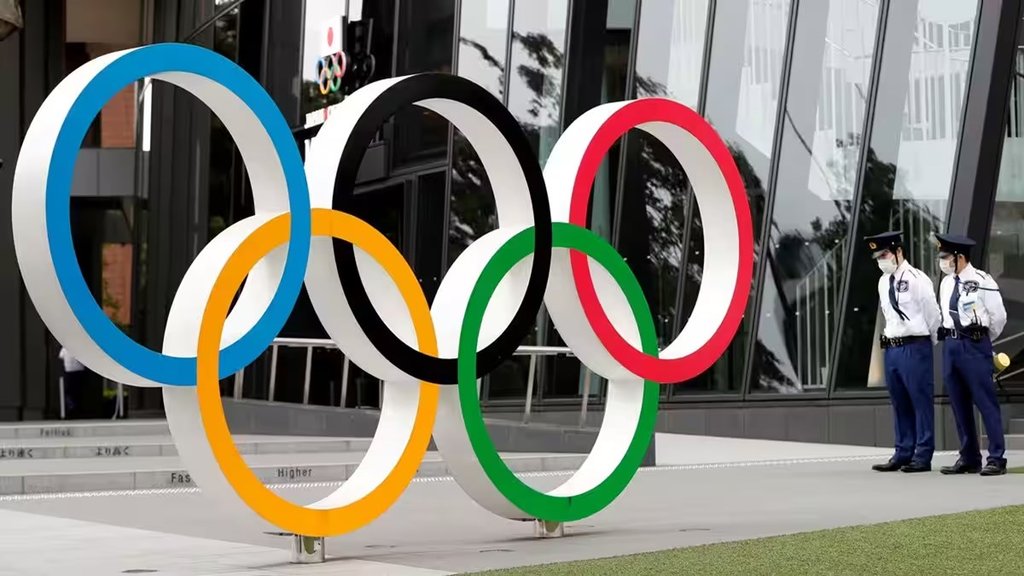लगता है वे दिन लद गए, जब कोई भी देश एक पैर पर खड़ा होकर बड़े खेल आयोजनों का मेजबानी पाने के लिए पूरा जोर लगा देता था। वह चाहे ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल खेल हो या विश्वकप फुटबाल। विभिन्न देशों के बीच कठिन प्रतिस्पर्धा होती थी मेजबानी पाने की, क्योंकि इससे देश का नाम पूरे विश्व में विख्यात तो होता ही था, साथ में उस देश की आर्थिक क्षमता का भी पता चलता था।
दरअसल, खेल के आयोजन में अरबों डालर खर्च करने पड़ते हैं। आधारभूत संरचनाएं तैयार करनी पड़ती है। हजारों की संख्या में मेहमानों का स्वागत करना पड़ता है। उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया करानी पड़ती हैं। दर्जनों नए स्टेडियमों का निर्माण कराना पड़ता है। पानी बिजली की अतिरिक्त खपत के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है।
शायद इन्हीं सब परेशानियों के कारण अब कई देश बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी करने से पीछे हट रहे हैं। जैसे आस्ट्रेलिया में विक्टोरिया ने 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने से पीछे हटने की बात कही है, क्योंकि उस आयोजन में सात अरब डालर से भी ज्यादा का खर्च आ रहा था। आस्ट्रेलिया शायद अतिरिक्त आर्थिक बोझ को उठाने में सक्षम नहीं लग रहा है।
इसी तरह, 2015 में दक्षिण अफ्रीकी शहर डरबन को वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन की जिम्मेदारी दी गई थी। मगर दक्षिण अफ्रीका ने उस आयोजन के लिए न तो ‘हां’ कहा, न ही ‘ना’ कहा। उसके इस उदासीन रुख को देखते हुए राष्ट्रमंडल खेल संघ ने 2017 में डरबन का मेजबानी खत्म करके इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम को जिम्मेदारी सौंप दी थी। अब देखना है कि 2026 का आयोजन किस देश को मिलता है। कोई लेने को तैयार भी होता है या नहीं, यह देखना अभी बाकी है।
जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर।
परीक्षा का स्वरूप
स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी-यूजी) की परिकल्पना दो साल पहले भारतीय उच्च शिक्षा में अत्यधिक कटआफ की समस्या के एक नए समाधान के रूप में की गई थी, जो विभिन्न राज्य और केंद्रीय बोर्डों में पंजीकरण कराने वाले विद्यार्थियों की बाढ़ से उत्पन्न हुई थी। कुल 1.1 मिलियन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी।
सौ प्रतिशत अंक की अधिकतम संख्या अंग्रेजी में थी, उसके बाद जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र और व्यवसाय अध्ययन थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब कालेज प्रवेश में अधिक तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेगी। विशेष रूप से कुछ विशिष्ट संस्थानों में जो अंतर-पीढ़ीगत गतिशीलता में सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए सबसे बड़ी मांग है।
उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के बीच सीटों के लिए होड़ दो परस्पर जुड़े कारकों का एक कार्य है- एक अपरिष्कृत परीक्षा प्रणाली और कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों तक सीमित गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा विकल्पों की कमी। इस बंधन को तोड़ने के लिए सीयूईटी एक मजबूत पहला कदम था, लेकिन इसके पूछताछ और अंकन स्वरूप को और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता हो सकती है।
हालांकि समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक कि भारत न केवल अपने महानगरों में, बल्कि पूरे देश में उच्च शिक्षा और बीज गुणवत्ता वाले संस्थानों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।
टीकेआर नूरी, मुंबई।
सफाई के पंछी
चंबल के रेतीले टापुओं पर भारतीय स्कीमर पक्षी के अंडों में विगत वर्षों की तुलना में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होने की खबर आई। भारतीय स्कीमर की विशेषता यह है कि ये ऐसी मछलियों का शिकार करते हैं जो पानी मे गंदगी बढ़ाती हैं। पानी को स्वच्छ रखने वाले पक्षी का संरक्षण करना आवश्यक है। देखा जाए तो वर्षों पहले गंगा नदी के जल को स्वच्छ करने के लिए डाल्फिन मछलियां छोड़ी गई थीं।
मलेरिया की रोकथाम के लिए पानी में गबुसिया मछली छोड़ी जाती है, ताकि मच्छर के लार्वा को पानी मे ये मछलियां चट कर सकें। जल स्वच्छता अभियान में भारतीय स्कीमर पक्षी की संख्या बढ़ाने से अस्वच्छ जल को स्वच्छ कर बीमारियों से निजात दिलाने में मदद मिल सकेगी।
संजय वर्मा ‘दृष्टि’, धार, मप्र।
कुदरत का हिसाब
कहा जाता है कि ‘प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति की पूजा ही ईश्वर की पूजा है!’ लेकिन आजकल के इस भौतिक व चकाचौंध से भरे युग में प्रकृति के प्रति दिखावा ही अधिक होता है। भले ही हम समय-समय पर प्रकृति के नाम पर व्रत, उपवास, पूजन करते हैं, मगर उस प्रकृति के प्रति कितने वफादार हैं, यह जगजाहिर है।
उजड़ते हुए वन, प्रदूषित होती नदियां, सिमटते हुए वन्यजीव-जंतु, बढ़ता प्रदूषण इस बात का द्योतक है कि हम केवल अपने स्वार्थ में केंद्रित हैं। देश में कोई पहली बार भयावह बारिश नहीं हो रही है। पहले भी हो रही थी। लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ का ही दुष्परिणाम है कि हम अब जानमाल से हाथ धो रहे हैं। जीने के लिए संघर्ष के साथ-साथ प्रकृति के प्रति पूरी वफादारी भी बहुत जरूरी है।
हम चाहें तो अपना भौतिक विकास कर लें या फिर सुरक्षित जीवन के लिए प्रकृति की कद्र करना सीख लें। अन्यथा प्रकृति अपने हिसाब किताब से हमको दंड देगी। फिर रोने से कुछ नहीं होगा।
हेमा हरि उपाध्याय ‘अक्षत’, उज्जैन।
जिम्मेदारी की जरूरत
‘हैवानियत की हद’ (संपादकीय, 21 जुलाई) पढ़ कर रूह कांप गई। प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक अरस्तू की उक्ति ‘मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है’ कई बार गलत लगने लगती है। चंद्र, मंगल मिशन फख्र की बात न रहे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कैसे गौरवान्वित महसूस करें। जहां चुनी हुर्इं सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था के बावजूद वीभत्स कृत्य होते रहते हैं। उस मत का क्या महत्त्व रहा, जिससे सत्ता का अधिकार मिला।
दो-ढाई महीने से चल रही अमानवीय कृत्यों की जांच चल रही है, यह कहना कब तक जारी रहेगा। आजादी हासिल करने के लंबे अंतराल के बाद भी हम मजहबी और जातिगत वैमनस्यता को समाप्त नहीं कर पाए। बड़ा दुखद लगता है कि डरा-सहमा अंतिम व्यक्ति अगर किसी तरह जिंदा है तो यह विचार करने का वक्त है। महिलाओं के प्रति अत्याचार समाज और राज के गैरजिम्मेदाराना रुख को रेखांकित करते हैं और इसमें तत्काल सुधार किए जाने की जरूरत है।
हुकुम सिंह पंवार, इंदौर।