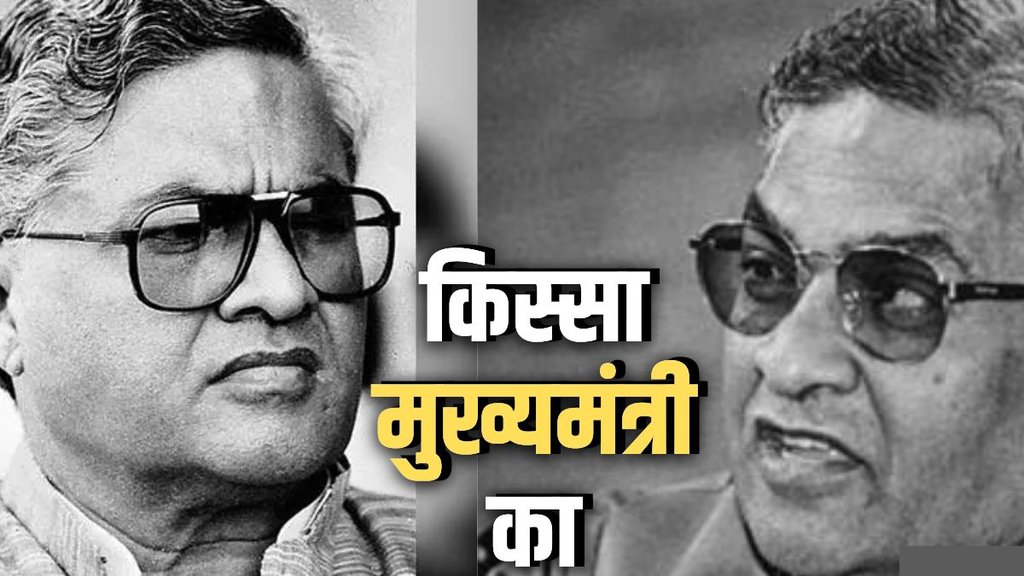जब दिल्ली की राजनीति में इंदिरा गांधी का रुतबा अपने चरम पर था और बिहार की गलियों में जेपी आंदोलन की गूंज फैल चुकी थी, तब राज्य की राजनीति किसी ज्वालामुखी की तरह उबल रही थी। इसी दौर में एक ऐसा चेहरा उभरा, जो न आंदोलन का नायक था, न सड़कों का योद्धा – पर केंद्र की नजर में भरोसेमंद, शांत और आज्ञाकारी था। यह चेहरा था जगन्नाथ मिश्रा का, जिन्होंने अगले दो दशकों में बिहार की राजनीति को कई उतार-चढ़ावों से गुजारा। उनका उदय, उत्थान और पतन – तीनों ही इंदिरा युग की सत्ता शैली, कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी और बिहार की सामाजिक उथल-पुथल की कहानी कहता है।
1972 के विधानसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी। जनता को उम्मीद थी कि वर्षों की राजनीतिक अस्थिरता और राष्ट्रपति शासन के बाद अब स्थिर सरकार मिलेगी। पर सत्ता संभालते ही कांग्रेस में गुटों की खींचतान शुरू हो गई। नतीजा यह हुआ कि तीन साल में बिहार ने तीन मुख्यमंत्री देख लिए।
2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हुए बम विस्फोट में कांग्रेस के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या ने राजनीति को हिला दिया। वही मिश्रा, जिन्होंने केदार पांडे और अब्दुल गफूर दोनों को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था, अचानक इस खेल से बाहर हो गए। बिहार दिशाहीन हो गया, और केंद्र को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी, जो सत्ता को नियंत्रित रख सके।
पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे एक बार फिर वापसी की कोशिश कर रहे थे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष हरिनाथ मिश्रा और बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी भी दावेदारी में थे। लेकिन दिल्ली को चाहिए था कोई ऐसा चेहरा जो न बहुत महत्वाकांक्षी हो, न विवादास्पद। 6 अप्रैल 1975 को कांग्रेस विधायक दल ने जगन्नाथ मिश्रा को अपना नेता चुना, और पांच दिन बाद, 11 अप्रैल को वे मुख्यमंत्री बने। महज 38 साल की उम्र में वे बिहार के इतिहास में दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बने—सतीश प्रसाद सिंह के बाद।
मिश्रा मूलतः शिक्षक थे। मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाते-पढ़ाते वे राजनीति में आए। 1968 में विधान परिषद के सदस्य बने और 1972 में झंझारपुर से विधायक चुने गए। उनका मुख्यमंत्री बनना, एक तरफ पारिवारिक विरासत का विस्तार था, तो दूसरी ओर उस दौर के “दिल्ली मॉडल” का उदाहरण – जहां केंद्र ऐसे मुख्यमंत्रियों को पसंद करता था, जो सवाल न करें, बस आदेशों का पालन करें।
लेकिन उनका पहला कार्यकाल ठीक उस समय शुरू हुआ जब देश की राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल आया – आपातकाल। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गईं, प्रेस पर सेंसरशिप लग गई। बिहार, जो पहले ही जेपी आंदोलन का केंद्र था, अब दमन की प्रयोगशाला बन गया। जबरन नसबंदी, विपक्षी नेताओं की गिरफ़्तारी और राजनीतिक डर का माहौल – इन सबके बीच मिश्रा ने इंदिरा गांधी के आदेशों का ईमानदारी से पालन किया, पर कांग्रेस को जनता के गुस्से से नहीं बचा सके।
1977 के आम चुनावों में उत्तर भारत से कांग्रेस का नामोनिशान मिट गया। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सत्ता में आई और 30 अप्रैल 1977 को नौ राज्यों की कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया—मिश्रा सरकार भी चली गई।
जून 1977 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस केवल 57 सीटों पर सिमटी। जनता पार्टी 214 सीटों के साथ सत्ता में आई। मिश्रा विपक्ष के नेता बने और पार्टी को फिर से खड़ा करने में जुटे। तीन वर्षों में उन्होंने संगठन में नई ऊर्जा भरी।
1980 में इंदिरा गांधी की नाटकीय वापसी हुई। केंद्र में कांग्रेस फिर से सत्ता में आई, और बिहार की जनता ने भी इंदिरा पर भरोसा दिखाया। कांग्रेस ने 324 में से 169 सीटें जीत लीं और 8 जून 1980 को मिश्रा दोबारा मुख्यमंत्री बने।
इस बार उन्होंने गुटबाज़ी पर नियंत्रण पाने और प्रशासन को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की। उन्होंने पार्टी की राज्य इकाई और कांग्रेस विधायक दल दोनों पर पकड़ मजबूत की। लेकिन दिल्ली की राजनीति का मिजाज बदल चुका था। आलाकमान राज्यों के मुख्यमंत्रियों को “स्थायी” नहीं रहने देना चाहता था।
इसी बीच मिश्रा का सबसे विवादास्पद कदम सामने आया – 31 जुलाई 1982 को बिहार प्रेस विधेयक। सरकार का तर्क था कि यह अशोभनीय और ब्लैकमेलिंग वाली खबरों पर रोक लगाने के लिए है, लेकिन देशभर के पत्रकारों ने इसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया। बिहार से दिल्ली तक विरोध हुआ। एक साल तक चले इस विवाद के बाद, आखिरकार 1983 में सरकार को यह विधेयक वापस लेना पड़ा।
इसी दौरान मिश्रा और दिल्ली के रिश्ते बिगड़ गए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से केंद्र की खनन नीतियों पर सवाल उठाए, जिससे आलाकमान नाराज हो गया। अब उन्हें “काबू में न आने वाला” मुख्यमंत्री माना जाने लगा। 11 अगस्त 1983 को उन्हें अचानक नई दिल्ली बुलाया गया। वहां तत्कालीन कांग्रेस महासचिव राजीव गांधी ने खुद उनके इस्तीफे की घोषणा कर दी और कहा कि जल्द ही नया नेता चुना जाएगा। तीन दिन बाद, 14 अगस्त को चंद्रशेखर सिंह ने मुख्यमंत्री पद संभाला।
लेकिन मिश्रा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो कांग्रेस ने 1985 में बिहार में 196 सीटें जीत लीं। पर पार्टी के भीतर अस्थिरता जारी रही। तीन मुख्यमंत्री बदले गए—बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद और सत्येंद्र नारायण सिन्हा—पर कोई भी स्थिर शासन नहीं दे सका।
1989 के आते-आते देश में कांग्रेस विरोधी लहर उठी। वी. पी. सिंह ने बोफोर्स घोटाले को मुद्दा बनाकर जनता दल को एकजुट किया और भाजपा व समाजवादियों के साथ गठबंधन किया। बिहार में लालू प्रसाद यादव पिछड़ों की राजनीति का प्रतीक बन चुके थे।
ऐसे माहौल में, कांग्रेस आलाकमान ने दिसंबर 1989 में एक बार फिर जगन्नाथ मिश्रा पर भरोसा जताया और उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया।
लेकिन यह कार्यकाल पहले से भी कठिन था। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को साधने की भरपूर कोशिश की, जिससे विपक्ष ने उन्हें व्यंग्य से “मौलाना मिश्रा” कहना शुरू कर दिया। कल्याणकारी योजनाएं और तुष्टिकरण की राजनीति भी जनता के रुख को नहीं बदल सकीं। 10 मार्च 1990 को जनता दल ने निर्णायक जीत हासिल की और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। यह दिन बिहार में कांग्रेस शासन का आखिरी दिन साबित हुआ।
मिश्रा झंझारपुर से फिर विधायक बने और विपक्ष के नेता रहे। बाद में राज्यसभा पहुंचे और पी. वी. नरसिम्हा राव की सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री बने। वे ज्योतिष और तंत्र-मंत्र में गहरा विश्वास रखते थे, और राजनीतिक संकटों में तांत्रिकों से सलाह लेते थे—उनकी यह आदत आलोचकों के लिए हंसी का विषय बन गई थी।
पर उनके जीवन का अंतिम अध्याय बेहद निराशाजनक रहा। अरबों रुपये के चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें जेल की सजा हुई। सेहत बिगड़ने पर उन्हें जमानत मिली और नवंबर 2019 में 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया।
उनकी राजनीतिक विरासत अब उनके बेटे नीतीश मिश्रा आगे बढ़ा रहे हैं। झंझारपुर से तीन बार जद(यू) के टिकट पर विधायक रह चुके नीतीश मिश्रा 2024 में भाजपा में शामिल हुए और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री बने। अब वे 2025 का चुनाव उसी सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं।