अर्जुन सेनगुप्ता
कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी टिप्पणियों की ऐतिहासिकता या उसकी कमी के लिए आलोचना होने के बाद, कंगना ने अपने दावे के सबूत के रूप में 1943 में बोस द्वारा स्थापित निर्वासित सरकार का हवाला देते हुए अपनी बात दोहराई।
आइए जानते हैं वह असल में किस बारे में बात कर रही है:
आज़ाद हिन्द सरकार
सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर, 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद की निर्वासित सरकार के गठन की घोषणा की थी। उस निर्वासित सरकार के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री खुद सुभाष चंद्र बोस थे, उनके पास विदेशी मामलों का विभाग और युद्ध विभाग था। एसी चटर्जी वित्त के प्रभारी थे, एसए अय्यर प्रचार और प्रचार मंत्री थे, और लक्ष्मी स्वामीनाथन को महिला मामलों का मंत्रालय दिया गया था। बोस की आज़ाद हिंद फ़ौज के कई अधिकारियों को भी कैबिनेट में शामिल किया गया था।
आज़ाद हिंद सरकार ने ब्रिटेन के दक्षिण पूर्व एशियाई उपनिवेशों (मुख्य रूप से बर्मा, सिंगापुर और मलाया) में सभी भारतीय नागरिकों और सैन्य कर्मियों पर अधिकार का दावा किया था।
जैसे चार्ल्स डी गॉल ने स्वतंत्र फ्रांस के लिए अटलांटिक में कुछ द्वीपों पर संप्रभुता की घोषणा की थी, ठीक वैसे ही बोस ने अपनी सरकार को वैधता देने के लिए अंडमान को चुना था। सरकार ने दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीयों को भी नागरिकता प्रदान की अकेले मलाया में 30,000 प्रवासियों ने आजाद हिंद सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त की थी।
कूटनीतिक रूप से बोस की सरकार को जर्मनी, जापान और इटली, साथ ही क्रोएशिया, चीन, थाईलैंड, बर्मा, मंचूरिया और फिलीपींस में नाजी और जापानी कठपुतली सरकारों द्वारा मान्यता दी गई थी। अपने गठन के तुरंत बाद आज़ाद हिंद सरकार ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी।
सुभाष चंद्र बोस से पहले भी बनाई गई थी निर्वासित सरकार
आज़ाद हिंद सरकार के अस्तित्व में आने से 28 साल पहले काबुल में भारतीय स्वतंत्रता समिति (आईआईसी) नामक एक समूह द्वारा भारत की निर्वासित सरकार का गठन किया गया था।
जिस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ने के लिए बोस ने जर्मनी और जापान जैसे देशों के साथ गठबंधन किया था। उसी तरह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों (ज्यादातर जर्मनी और अमेरिका में) ने भारत के क्रांतिकारियों और पैन-इस्लामवादियों के साथ मिलकर भारत को आजाद कराने की कोशिश की थी।
आईआईसी ने ओटोमन खलीफा और जर्मनों की मदद से भारत में विद्रोह भड़काने की कोशिश की, मुख्य रूप से कश्मीर में मुस्लिम जनजातियों और ब्रिटिश भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा के बीच।
इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आईआईसी ने काबुल में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता और मौलाना बरकतुल्लाह के प्रधानमंत्रित्व काल में एक निर्वासित सरकार की स्थापना की। बरकतुल्लाह क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश में भारत के बाहर दशकों बिताए थे।
बरकतुल्लाह भी ग़दर आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे, जो 1913 में कैलिफोर्निया में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था।
हालांकि युद्ध के अंत तक भारत में आंदोलन को कुचल दिया गया था, लेकिन गदर आंदोलन ने भारतीयों और अंग्रेजों पर एक मजबूत और स्थायी प्रभाव छोड़ा। काबुल की निर्वासित सरकार ग़दरवादी क्रांतिकारियों द्वारा चलाए गए कई कदमों में से एक थी।
क्यों बोस और बरकतुल्लाह की सरकार को नहीं मान सकते असली सरकार?
निर्वासित सरकारों की स्थापना करना लंबे समय से आंदोलनों के लिए राजनीतिक वैधता हासिल करने का एक तरीका रहा है। उदाहरण के लिए धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) को लें। इस निर्वासित सरकार का उद्देश्य ही तिब्बत पर चीनी कब्जे की वैधता को चुनौती देना है। तिब्बती लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली एक समानांतर सरकार चलाकर, सीटीए प्रतिरोध की लौ जलाए रखता है, तब भी जब तिब्बत में सरकार के दमन और सत्ता द्वारा प्रायोजित हान प्रवासन ने चीजों को कठिन बना दिया है।
इसी तरह 1915 और 1943 की दोनों अस्थायी सरकारें, कुछ और नहीं बल्कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अवज्ञा की प्रतीकात्मक पहल थीं, जो कुछ राजनीतिक विचारों को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं।
बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने सशस्त्र संघर्ष को वैध बनाने के लिए आजाद हिंद सरकार की घोषणा की। एक अस्थायी सरकार की घोषणा करके, उन्होंने अपनी सेना को अंतरराष्ट्रीय कानून की नजर में वैधता प्रदान की – वे सिर्फ विद्रोही या क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक विधिवत गठित सरकार के सैनिक थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों द्वारा ली गई नागरिकता की शपथ को उनके कार्यों की वैधता के सबूत के रूप में 1945-46 के लाल किले परीक्षणों के दौरान पेश किया गया था।
दूसरी ओर काबुल की निर्वासित सरकार को आईआईसी के इरादों की गंभीरता को स्थापित करने के लिए घोषित किया गया था। 1917 में यह सोवियत तक भी पहुंच गया और भारत की सीमाओं पर निर्वासित सरकार के अधिकार के रूप में, ब्रिटिशों के लिए एक बड़ा ख़तरा बन गया।
ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों में से किसी को भी, किसी भी तरह से, भारत सरकार नहीं कहा जा सकता है। ऐसा दो मुख्य कारणों से है- पहला, ये दोनों सरकारें व्यापक अंतरराष्ट्रीय मान्यता हासिल करने में विफल रहीं। हालांकि कुछ देशों ने उन्हें मान्यता दी और उनका समर्थन किया, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्यों के लिए ऐसा किया। विश्व युद्धों (जिसमें अंग्रेज विजयी हुए) के बाद यह समर्थन तेजी से खत्म हो गया।
दूसरा, इन दोनों सरकारों ने कभी भी भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं किया। बोस ने आधिकारिक तौर पर अंडमान पर कब्ज़ा कर लिया था लेकिन प्रभावी रूप से, द्वीप जापानी कब्जे में थे। काबुल सरकार ने कभी भी भारतीय धरती पर कदम नहीं रखा, और 1919 में इसके विघटन तक यह केवल कागजों पर ही रहा।
जापान के अंडमान पहुंचने के इतिहास को विस्तार से पढ़ने के लिए फोटो पर क्लिक करें:
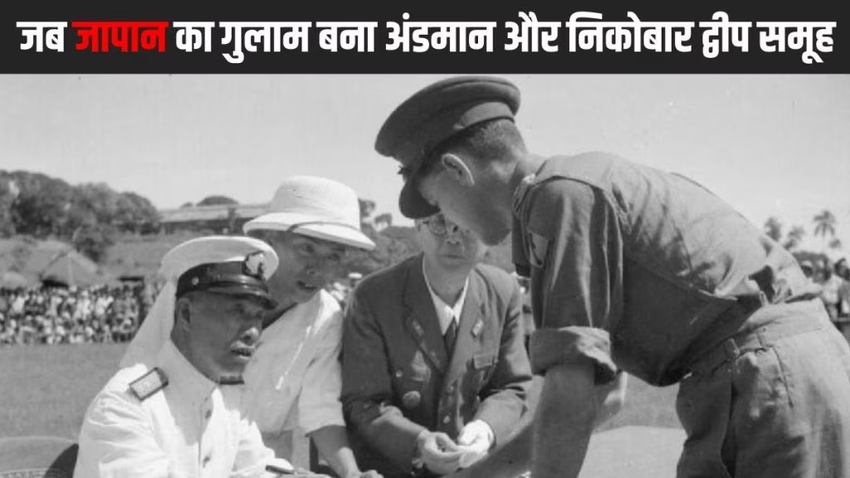
ये भी पढ़ें- जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सुभाष चंद्र बोस ने दी थी चेतावनी
विस्तार से पढ़ने के लिए फोटो पर क्लिक करें:
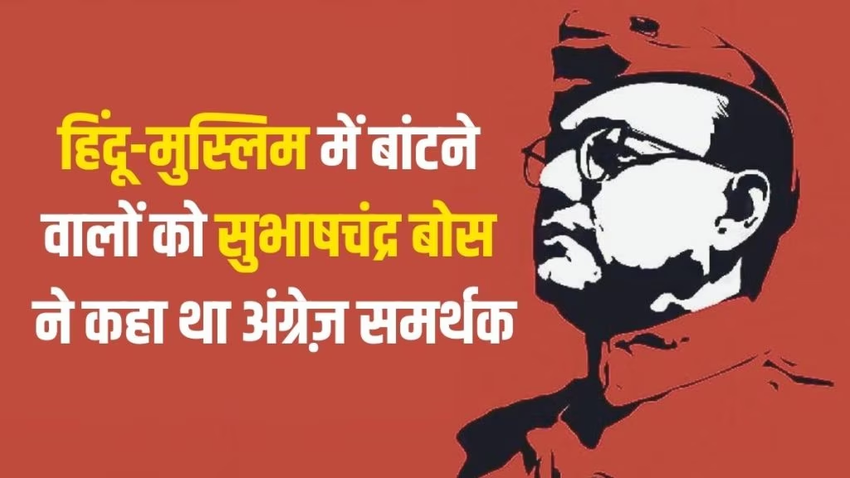
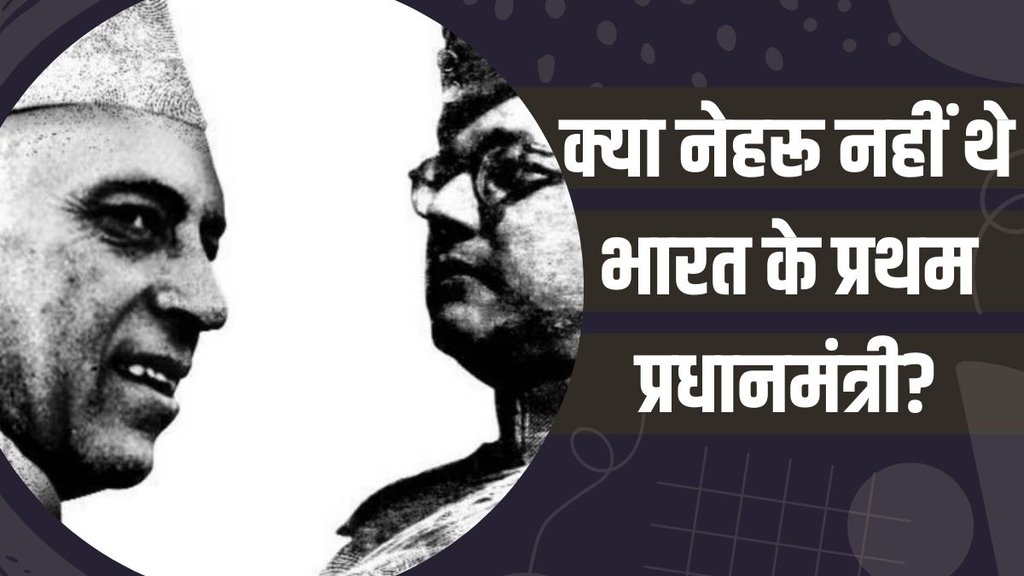
 — Kangana Ranaut (Modi Ka Parivar) (@KanganaTeam)
— Kangana Ranaut (Modi Ka Parivar) (@KanganaTeam)