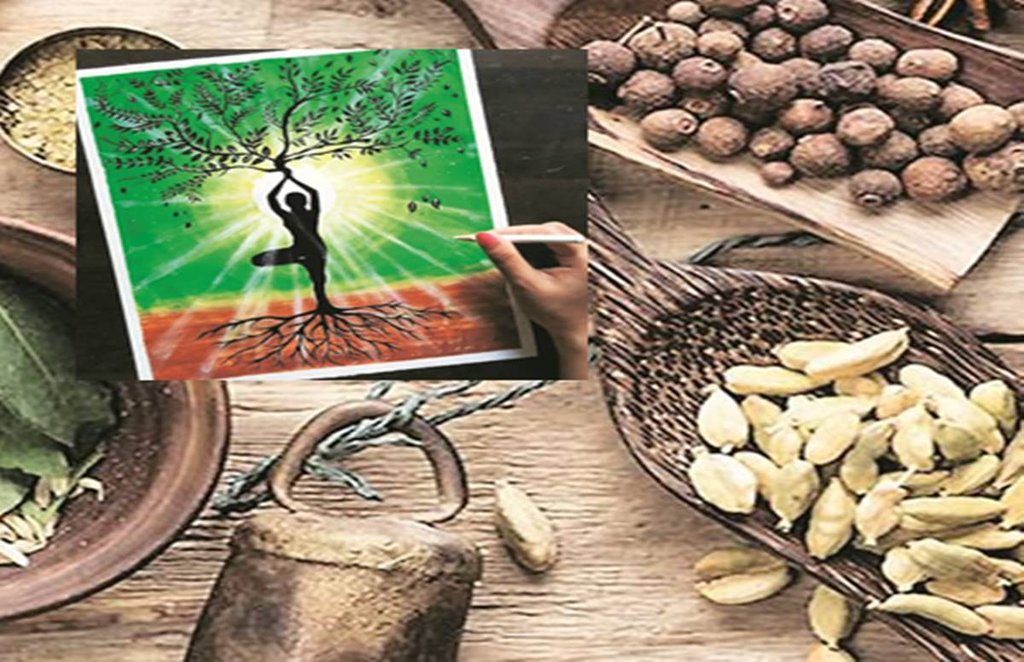सेहत न तो आज महज निजी चिंता का विषय है और न ही ऐसा क्षेत्र जिसकी जिम्मेदारी अकेले सरकार के ऊपर है। बीते तीन दशकों में बाजार ने इस चिंता को इस तरह हथिया लिया है कि वही इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नियामक बन बैठा है। आलम यह है कि एक तरफ जहां स्वास्थ्य से जुड़ी बेहतरीन तकनीक और सेवाएं आज हमारी पहुंच में हैं, वहीं मर्ज को चामत्कारिक तरीके से ठीक करने के झांसे टीवी और मोबाइल फोन के जरिए हमारे घर, हमारे दिमाग तक पहुंच बना चुके हैं। सेहत के नाम पर ठगी और लूट के इस धंधे का पसारा इतना बड़ा है कि यह आज खुद में एक फलता-फूलता उद्योग बन चुका है। सेहत से खिलवाड़ पर उतारू इस खतरनाक उद्यम से जुड़े तमाम संदर्भों की चर्चा कर रही हैं मृणाल वल्लरी।
लोगों की भीड़ में से एक महिला उठती है और सामने बैठे किसी योगगुरु या कथित आयुर्वेदाचार्य से बहुत भावुक होकर कहती है कि उसे सालों का गठिया था लेकिन आपके इलाज से वो अब सामान्य और अच्छा महसूस कर रही है। मंच पर बैठे बाबाजी उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि अब तुम एकदम स्वस्थ जीवन जिओगी। उसी भीड़ से सिर पर पल्लू लिए एक अधेड़ महिला उठती है और कहती है कि वह बरसों से नि:संतान थी लेकिन बाबाजी के इलाज की वजह से वह जुड़वां बच्चों की मां बन गई है। गौरतलब है कि जुड़वां पर जोर था। बाबाजी उसे भी आशीर्वाद देते हैं।
सुबह-सुबह यह दृश्य ज्यादातर टीवी चैनलों पर चल रहा होता है। ज्यादातर दर्शकों को पता नहीं होता कि यह कोई खबर नहीं बल्कि उस बाबा का विज्ञापन है जो वो टीवी चैनल पैसे लेकर दिखाता है। बाबाओं के इस तरह के सेहत मेले सुबह-सुबह चैनलों पर दिखाए जाते हैं।
उस वक्त विज्ञापनों की दर कम होती है तो ऐसे कार्यक्रम एक घंटे तक के भी होते हैं और कई दर्शकों को ये सब बिलकुल असली लगता है। अचानक से कोई ‘मरीज’ उठ कर इस तरह से अपनी बीमारी का वर्णन करता है कि अपनी बैठक में टीवी देख रहे लोगों का हाथ अपने घुटने पर चला जाता है और वे भी उस बाबाजी के पास जाने की सोचने लगते हैं।
विवेक का स्थगन
पारंपरिक रूप से विज्ञापन के बजाए इस तरह मेला लगा कर उसे असल कहानी का रूप देने का असर यह होता है कि दर्शक सबसे पहले इस विवेक को खोते हैं कि एक ही आदमी गठिया से लेकर नि:संतानता तक का इलाज कैसे कर देता है। विज्ञान कहता है कि हर इंसान का डीएनए अलग होता है।
यानी एक इंसान, दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। किसी भी रोग का इलाज कोई भेड़चाल नहीं होती कि अगर एक को इस इलाज से फायदा होगा तो दूसरे को भी इस इलाज का फायदा होगा। लेकिन टीवी वाले बाबा रूपी डॉक्टर सारे मरीजों को एक नजर से देखते हैं और ‘कृपा’ बरसा देते हैं।
उन्हें मरीज के इलाज में अपनी दूरदृष्टि से कभी पपीता दिखता है तो कभी समोसा दिखता है और उसी के अनुसार मरीजों का इलाज भी बता देता है। उन मरीजों की सत्यता के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं लेकिन उसे एक ‘सत्य कथा’ के रूप में दिखा कर बाबा के प्रति भरोसा पैदा किया जाता है और इस खेल का सम्मोहन ऐसा कि देखते-देखते अपने घरों में बैठे लोग टीवी स्क्रीन पर दिया नंबर नोट करने लगते हैं।
पूर्वी दिल्ली में रहने वाली आराधना की उम्र 45 साल थी। उसे अपने स्तनों में गांठ महसूस हो रही थी और उसे कैंसर का डर सता रहा था। वो रोज अपने मोहल्ले के पार्क में जाती थी। उसने वहां महिलाओं के समूह से इस पर चर्चा की। टीवी देख कर पार्क में चल रहे सेहत मेला का असर था कि उसे समझया गया कि बेकार में डॉक्टर के चक्कर में न पड़ो, वो चीड़-फाड़ करके तुम्हें मौत के मुंह में धकेल देंगे।
आराधना को भी लगा कि खास तरह के योग और बाबाओं के बताए तरीके से उसकी गांठ कैंसर में तब्दील नहीं होगी। इन सब के चक्कर में जब वह असह्य पीड़ा के साथ डॉक्टरों के पास पहुंची तो उसके कैंसर को अंतिम चरण का घोषित किया गया और उसके पास मौत के इंतजार के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। आराधना ने जब अपनी बीमारी को योग और बाबाओं के सहारे छोड़ दिया तो उसके परिजनों ने भी इस बात को लेकर तवज्जो नहीं दी। भारतीय समाज में आम मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं की सेहत को प्रसव और उससे जुड़े मामलों तक ही तवज्जो दी जाती है।
इसके अलावा महिलाएं भी कम से कम डॉक्टरों के चक्कर में पड़ना चाहती हैं ताकि उनकी सेहत के कारण घर का बजट न बिगड़े। हां, पैंतालीस साल के बाद बच्चों के बड़े और आत्मनिर्भर हो जाने के बाद वो खुद पर थोड़ा ध्यान देना शुरू करती हैं और पार्क में घूमने जाती हैं। जहां उन्हें मिलते हैं नाखून घिसने और लौकी का जूस पीने के नुस्खे। आमतौर पर बाबाओं के चक्कर में ज्यादातर महिलाएं और बुजुर्ग ही पड़ते हैं, जो या तो आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हैं या जिनकी कमाई का जरिया खत्म हो चुका है। उन्हें लगता है कि इसी तरह से आराम मिल जाए तो क्या बुरा है।
दावों का झांसा
हरिद्वार में रहने वाली विनीता बताती हैं कि वैसे तो दुनियाभर के डॉक्टर कैंसर का सटीक इलाज नहीं खोज पाए हैं लेकिन हमारे फैमिली वाट्सऐप ग्रुप में रोज कैंसर के इलाज के नए-नए तरीके फॉरवर्ड होते रहते हैं। क्या खाने से कैंसर होता है और क्या न खाने से नहीं होता की लंबी सूची होती। हमारे घरों में इसके पालन का दबाव बनने लगता है।
विनीता कहती है कि इसी तरह के एक वाट्सऐप संदेश में कच्ची हल्दी को कैंसर का रामबाण बताया गया था। मेरी सास हर चीज में भरपूर मात्रा में कच्ची हल्दी डलवाने लगी और घर में एक-दो दिन के अंतर से कच्ची हल्दी की सब्जी भी बनने लगी। लेकिन मुझे पेट में दर्द होने लगा और डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ गई। डॉक्टर ने कहा कि मुझे कच्ची हल्दी की ज्यादा खुराक परेशान कर रही है।
विनीता बताती हैं कि मैंने कैंसर का रामबाण (कच्ची हल्दी) लेना बंद किया तो मेरे पेट में दर्द के बाण भी छूटने खत्म हो गए। वो कहती हैं कि वाट्सऐप के अस्पताल में अलग तरह की डॉक्टरी चल रही है। इसने घरेलू नुस्खे और डॉक्टरों से दूर रहने के नाम पर कितना नुकसान पहुंचाया है असली डॉक्टरों को तो इस पर शोध करना चाहिए।
विज्ञापन का आखेट
विज्ञापन का अर्थ होता है अपने उत्पाद के प्रति लोगों को आकर्षित करना। पहले इसके लिए अतिरेक का सहारा लिया जाता था। टायर के विज्ञापन में बिकनी पहनी लड़की पर सवाल उठने शुरू हो चुके थे। इसमें दिखाया गया कि युवक बनियान पहन कर दस गुंडों को मार देता है और देह को परोसती हुई लड़की उसके साथ चल देती है। लेकिन नब्बे के दशक के बाद विज्ञापनों को यथार्थवादी रूप दिया जाने लगा। टूथपेस्ट से लेकर साबुन तक के उत्पादों में इसका चलन बढ़ा। उजला कोट पहने और आला लटकाए डॉक्टर सलाह देते कि फलां पेस्ट किस तरह से कीटाणु को मारता है।
फिनाइल का प्रचार डॉक्टर का कोट पहने महिला करती है और कहती कि वो डॉक्टर से पहले एक मां है। वो अपने बच्चे की सेहत के लिए फलां फिनाइल पर भरोसा करती है। शिशु खाद्य उत्पादों से लेकर डायपर तक की गुणवत्ता का प्रमाण डॉक्टर देते हैं। साथ ही डॉक्टरों की किसी संस्था का प्रमाणपत्र भी नत्थी कर दिया जाता है।
इसके साथ ही असल जीवन के नायकों के साथ उसके सफल होने का प्रमाण दिया जाने लगा। सचिन तेंदुलकर से लेकर कई सफल खिलाड़ियों के प्रमाणपत्र से ही भारत में ‘हेल्थ ड्रिंक’ का कारोबार फला-फूला। मैंने ये किया तो ये हो गया। जब असल जिंदगी के नायकों ने ये बोल दिया तो उस उत्पाद पर लोगों का भरपूर भरोसा हो चला।
सवाल और दरकार
विश्वास का मतलब तभी है जब कि वो यथार्थ होने का, सच होने का दावा करे। ठंडा मतलब कोकाकोला में आडंबर दिखता है। लेकिन जब उसे वास्तविकता के जामे में चित्रित किया जाता है तो वो महज विज्ञापन नहीं रह जाता है। हमारे यहां सेंसर बोर्ड फिल्मों पर बैठता है। इन दिनों किसी न किसी फिल्म पर भावना आहत होने के आरोप के बाद ‘तांडव’ मच जाता है। लेकिन विज्ञापन को चालाक सच में बदलने की प्रवृत्ति लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, उस पर हर तरफ चुप्पी है।
विज्ञापन का मकसद उत्पादों के प्रति आकर्षित करना भर होना चाहिए।
यानी दर्शक उत्पाद के बारे में जानें और उसे आजमाने की सोचें। एक तरफ तो विज्ञापन जिज्ञासा भरते हैं। लेकिन उसे यथार्थ का जामा पहना कर उसकी जरूरत पैदा की जाती है। जिन्हें उसकी जरूरत नहीं उनके लिए भी वह जरूरी करार दिया जाता है, असल जिंदगी के डॉक्टरों और खिलाड़ियों का सहारा लेकर। पिछले कुछ समय से चुनाव में इसी तरह का काम अखबारों-टीवी चैनलों के जरिए हो रहा है।
राजनीतिक दल विज्ञापित खबरों को चलवाते हैं। उनके विज्ञापनों को यथार्थवादी खबरों के रूप में परोसा जाता है। लोगों को यह न लगे कि प्रचार है बल्कि वे उसे खबर के रूप में लें। यह जोर आज पत्रकारिता के मूल स्वभाव को बदलने पर तुला है। खबर के रूप में चुनावी विज्ञापनों का संज्ञान चुनाव आयोग ने भी लिया और विभिन्न मंचों पर इसे लेकर चिंता जताई गई। खबर रूपी चुनावी विज्ञापनों को लेकर कई दिशानिर्देश बने कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
लेकिन भारत जैसे देश में जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत चिंताजनक है वहां सेहत के भ्रामक विज्ञापनों को सच बता कर पेश करने पर चुप्पी क्यों है! हर सुबह देश के लाखों घरों में टीवी और संचार के अन्य साधनों के जरिए अवैज्ञानिक और अंधविश्वासी इलाज को विज्ञान का सच बता कर पेश किया जा रहा है। इसके खिलाफ सरकार और अन्य संस्थाएं कब जागेंगी। जिस तरह पेड या फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये ‘विज्ञापन बाबा’ भी पूरे देश के सेहततंत्र को अवैज्ञानिकता के खतरे में धकेल चुके हैं।
कोरोना और हम
कोरोनाकाल में भारत में अवैज्ञानिकता की जो महागाथा लिखी गई है वो भी चिंताजनक है। बाजार के कारखानों से इम्युनिटी का उत्पादन शुरू हुआ और हर चीज रातोंरात इम्युनिटी बूस्टर हो गई। आपदा में अवसर तो बाजार की प्रवृत्ति रही है लेकिन सबसे चिंताजनक रही कोरोना की दवा को लेकर राजनीति। जिस पर सिर्फ चिकित्सकों, अनुसंधानकर्ताओं और सेहत के नुमाइंदों को बोलना था उस पर अफवाहों का बाजार गर्म था। समर्थन से लेकर विरोध तक में घनघोर अवैज्ञानिकता दिखी। कोरोना टीके को लेकर अवैज्ञानिक राजनीति खतरे की घंटी है कि हमें वैज्ञानिकता की ओर लौटना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम एक बड़ी त्रासदी के मुहाने पर खड़े मिलेंगे।