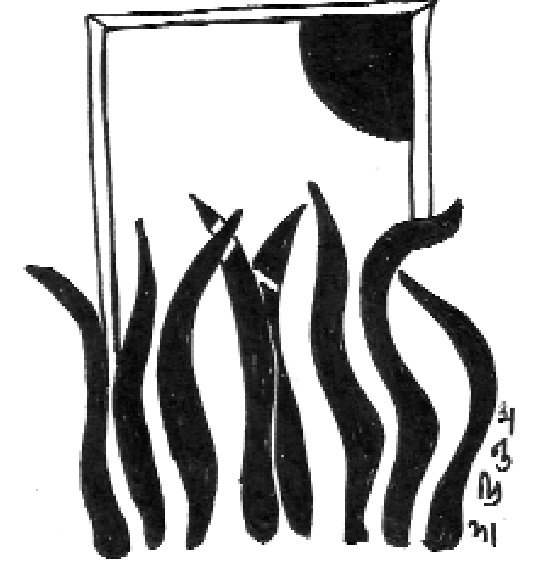राजेंद्र कुमार
बहुतों के मुंह से अक्सर यह सुनने को मिलता है कि यह समय कविता का समय नहीं है। देखने में यह आ रहा है कि इस समय अन्य विधाओं की तुलना में जिस विधा में सबसे ज्यादा लिखा जा रहा है, वह कविता ही है। यह तो पहले भी होता रहा कि जो लेखक विशेषत: अन्य-अन्य विधाओं में प्रतिष्ठित हुए, उन्होंने भी लिखने की शुरुआत कविता से की थी। पर इधर यह भी देखने में आने लगा है कि कई लेखक, जिन्हें अन्य-अन्य विधाओं के लेखक के रूप में पहचाना जाता रहा, जब अपनी-अपनी विधाओं में कुछ खास नहीं कर पाते या चुक जाते हैं और अपना लेखन समेट रहे होते हैं तो वे भी अंत में कविता लिखने लगते हैं। बहरहाल, इस सारे परिदृश्य की वास्तविकता यह है कि कविता जितनी लिखी जा रही है, उतनी पढ़ी नहीं जा रही। लिखे जाने और पढ़े जाने के बीच के इस उलटे अनुपात को किस रूप में लिया जाए?
असल में, आज कविता हमारे समय में तो है, पर हमारे अपने समाज में नहीं है। वैसे तो, बात घूम फिर कर बार-बार यहां पहुंचती है कि कविता को समाज का होना चाहिए। कविता का, समाज का होना मानो आज कविता की समकालीनता की शर्त बन गई है। पर कविता खुद का भी तो एक समाज रचती है। समाज की कविता जैसा मुहावरा तो आम हो चलता है, पर कविता का समाज-जैसा प्रत्यय हमारी चेतना में नदारद है।
कहते हैं कि कालजयी रचना वह होती है, जो अपने समय में भी हो और फिर अपने समय का अतिक्रमण भी करे। क्या इसी तरह एक शर्त यह भी नहीं होनी चाहिए कि कविता समाज की हो, लेकिन फिर समाज की होकर समाज का अतिक्रमण भी करे। अपनी आकांक्षा का समाज रचने की आकुलता भी उसमें हो। इस सूत्र के आखिर वाले सिरे से उलटे चल कर, शुरू वाले सिरे तक पहुंचें तो एक सचाई यह भी नजर आएगी कि जो कविता अपने समय में रहकर समय का अतिक्रमण कर पाती है और अपने समाज में रहकर समाज का अतिक्रमण कर पाने का सामर्थ्य रखती है, सच्चे अर्थ में वही कविता अपने समय की होती है और अपने समाज का प्रतिनिधित्व करती है।
आज हमारी कविता पर तात्कालिकता का दबाव बहुत ज्यादा है। हमारा पूरा समाज जिन स्थितियों की गिरफ्त में है, उनके दबाव से हर व्यक्ति की मानसिकता यही बनती जा रही है कि अपने समय और श्रम को वही-वही काम करने में लगाया जाए, जिससे तत्काल कुछ मिलने वाला हो। यह अधैर्य कविता की अपनी प्रकृति के प्रतिकूल है। कविता से तत्काल क्या मिलेगा? सच्ची कविता तो तत्काल, अपना कोई अर्थ तक देने को अक्सर राजी नहीं होती।
आज हर क्षेत्र में तत्काल कुछ पा लेने को सार्थकता की शर्त इस हद तक मान लिया गया है कि हमारे कविगण भी झट से कुछ पा लेना चाहते हैं-पुरस्कार या सम्मान या कुछ भी। जिन्हें यह सब मिलता जाता है, पाठक भी थोड़े-बहुत उन्हें मिल जाते हैं। प्रकाशक तो खैर आसानी से मिल ही जाते हैं।
न सिर्फ यह कि इन स्थितियों में कविता का कोई अपना समाज नहीं बन पाता, बल्कि यह भी कि यश:प्रार्थी कवियों की संख्या बढ़ती जाती है, पर इन कवियों का भी कोई अपना समाज नहीं बन पाता। यानी, न कविता का समाज, न कवियों का समाज।
कवियों का अपना समाज बनने की शर्त है कि उनकी अपनी-अपनी रचनात्मक बेचैनी कोई ऐसा रूप ले, जिससे उनके बीच परस्पर आत्मीयता का रिश्ता बने। यानी उनकी रचनात्मक बेचैनी उनको आपस में जोड़ने वाली हो। आपसी स्पर्धा या ईर्ष्या में उन्हें न ढकेले। रचनात्मक प्रयासों में कविगण अपनी-अपनी विशिष्टता तो अर्जित करें, लेकिन एक-दूसरे की विशिष्टता के प्रति सम्मान-भाव भी रखें। रचनात्मक सक्रियताओं में कवियों का सहभाव/साझा ऐसा हो कि किसी को किसी से ईर्ष्या न हो। माना कि सबकी रचनाशीलता न तो समान स्तर की हो सकती है, न समान स्वीकृति की। लेकिन इस वास्तविकता का बोध अलग-अलग कवियों में इस तरह हो कि किसी को ग्रंथिग्रस्त न कर सके।
आज के कविगण प्राय:, पुरस्कार, वगैरह के रूप में तात्कालिक उपलब्धियों को ही अपनी व्यापक मान्यता का प्रमाण-पत्र जैसा कुछ मानते नजर आते हैं। जिन्हें यह सब नहीं मिल पाता, उन्हें हीनता-बोध का अहसास होने लगता है या अहसास कराया जाने लगता है। इसकी परिणति होती है परस्पर ईर्ष्या में, कुंठाओं में। ऐसे में कवियों का कोई अपना समाज कैसे बन सकता है?
कविता का और कवियों का कोई अपना समाज ही न बन पा रहा हो, तो कवि उस समाज का भी अपना कैसे हो सकता है, जिसने अपनी भाषा में कवि को रचनात्मक हस्ताक्षेप करने का अधिकार दिया होता है। कवि की कविता का समाज, कवि की भाषा के समाज से इतना अलग हो जाए कि दोनों में संवाद ही न हो सके, तो उसका हश्र तो यही होना है, जो आज है। किसी भी भाषा का, और उस भाषा के समाज का गौरव तभी बढ़ता है, जब उस भाषा-विशेष को कोई कवि अपनी कविता का रचा एक नया समाज सौंपकर समृद्ध करता है।
अपने समाज की दी हुई भाषा के लिए कविता एक इशारा भी होती है कि भाषा को किधर जाना चाहिए।
यह तो लगभग हर काल का सत्य है किसी समाज में जो शक्तियां होती हैं, उनकी भूमिका किसी एक ही दिशा वाली नहीं होती। उनकी अपनी-अपनी भूमिकागत भिन्नता के चलते उन्हें अपनी भाषा में यह विवेक अर्जित करना होता है कि किस शब्द को वे कितना महत्त्व देंगे। लेकिन हमारे समय की विडंबना यह है कि कोई शब्द अपने अर्थ में किस पक्ष में है, इसकी पहचान ही संभव नहीं रह गई है। मनुष्य अपनी भाषा में किस शब्द को कितना अर्थवान् मानता है, पहले इसी से उसकी प्रकृति और उसकी सामाजिकता की पहचान हम कर लेते थे। पर अब ऐसा कहां संभव है? किसी शब्द को अब किसी से भी यह पूछने का अधिकार नहीं है कि वह उसका प्रयोग सच को अभिव्यक्त करने के लिए कर रहा है या सच को छिपाने के लिए। हर शक्ति अपनी-अपनी भूमिका में एक-दूसरे के प्रतिकूल होने के बावजूद, किसी भी शब्द का प्रयोग आज समान रूप से कर सकती है। वही शब्द इधर भी हैं, वही शब्द उधर भी। कोई भी शब्द अपना पक्ष चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है। निराला ने कविता की मुक्ति का सवाल उठाया था। पर अब उससे भी बड़ा प्रश्न शब्द की मुक्ति का है। कविता क्या है? का सबसे सार्थक जवाब मेरे ख्याल से आज यह हो सकता कि कविता शब्द को शब्द के सही पक्ष में आने देने की आजादी है।
कविता क्या है? इस प्रश्न से हमारे आचार्यगण न जाने कबसे जूझते आ रहे हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र से लेकर रामचंद्र शुक्ल तक। रामचंद्र शुक्ल से लेकर नामवर सिंह तक। आगे भी यह सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि प्रश्न वही हो तो भी, हर काल में उसका उत्तर वही नहीं रहता। पर मुझे लगता है, ‘कविता क्या है’-यह प्रश्न आज निरा अकादमिक बन कर रह गया है। ‘अकादमिक जड़ता से उबरने के लिए क्या आज यह जरूरी नहीं है कि हम प्रश्न को थोड़ा भिन्न तरह से अपनी चेतना में लाएं-‘कविता कर क्या सकती है?’
हमारे समय के किसी बड़े कवि ने (शायद शमशेर ने) कहा कि कविता हमेशा एक आशीर्वाद की तरह मनुष्य के साथ रहती है। लेकिन मुझे लगता है, कविता के लिए जरूरी है कि वह बद्दुआ या एक शाप की तरह भी हो। बद्दुआ या शाप उन लोगों के लिए, जो मनुष्य होकर भी मनुष्य होने का मर्म नहीं पहचानते और मनुष्यता की ऐसी-तैसी करने पर उतारू रहते हैं या ऐसा करने वालों का साथ देने में अपना हित देखते हैं। आखिर शाप ही तो श्लोक बन गया था हमारे आदि कवि के यहां-मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम: शाश्वती: समा:…।
कविता ऐसे ही जन्म लेती है। हर काल में। संवेदनहीनता को शाप देती हुई, मनुष्य की संवेदनशीलता को असीसती हुई। शाप और आशीष के बीच, अपने सही पक्ष में जब मानव-हृदय धड़कता है, उसकी धड़कन कविता बन जाती है। ०