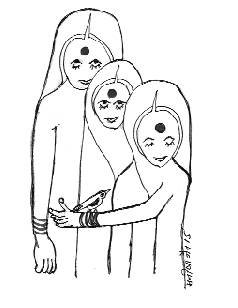जयकुमार जलज
हमारे देश के लोकजीवन में व्यवहार के अनेक दूरअंदेशी सूत्र हैं। उन्हीं में एक महत्वपूर्ण सूत्र है-‘जिस रास्ते नहीं चलना, उसके पेड़ क्या गिनना?’ लेकिन आज का आदमी उन तमाम रास्तों के पेड़ों को गिन रहा है जिन पर उसे शायद ही कभी चलना पड़े। मेरे एक मित्र ने वर्षों से ट्रेन में कदम नहीं रखा, न भविष्य में कभी रखने की संभावना है। पर, वे हर बार रेलवे की नई समय सारिणी खरीदते हैं, अपनी कमजोर आंखों से उसके छोटे हरूफों को पढ़ते रहते हैं। एक व्यस्त सज्जन सात-आठ अखबारों में समाचारों को पढ़ते हैं। फिर समाचारों को सुनते है, समाचारों को देखते भी हैं। बहुत से स्टेशन हैं, चैनल हैं। समाचार की भूख उनके लिए नशा बन गया है।
यों तो आदमी फितरतन जिज्ञासु है। उसकी असीम रचनात्मक जिज्ञासा के कारण ही संसार भौतिक उन्नति के शिखर तक पहुंचा है। लेकिन आज का आदमी अधिकतर दिशाहीन जिज्ञासा से परिचालित है। पुराने जमाने में जिज्ञासा के लिए क्षितिज बहुत सीमित था। जैसे आदमी रूखा सूखा खाकर सो जाता था वैसे ही दो चार सूचनाओं से उसका पेट भर जाता था। आज तो तमाम एजेंसियां दुनिया को ही नहीं आकाश-पाताल को भी उसकी थाली में परोसने में लगी हैं और वह बदहजमी के बावजूद खाए चला जा रहा है। इसलिए इस जिज्ञासा की कोई रचनात्मक उपलब्धि नहीं है। दूसरे आदमी की सोच कितना ही सामंतवादी हो, लेकिन अगर वह अतिसूति है तो उसे स्मार्ट, आधुनिक और विद्वान तक कहने वालों की कमी नहीं रहती। सूचनाएं ज्ञान या बोध नहीं हैं। पर हम उन्हें ज्ञान या बोध की कुर्सी पर बिठाने में लगे हुए हैं। जब यह बता देने पर कि अमुक देश की मुद्रा क्या है, अमुक वस्तु का आविष्कार किसने किया था, व्यक्ति ज्ञानी कहलाने लगता है तो भला दिमाग में सूचनाओं के ढेर को ऊंचा करते जाने में कौन पीछे रहना चाहेगा ?
सूचना ग्रहण करने में दिमाग खर्च नहीं होता। थका हुआ दिमाग अखबार पढ़कर ताजा हो जाता है। अखबार का संपादकीय पृष्ठ क्यों और कैसे का उत्तर भी देता है। उसकी विश्लेषणपरकता में पाठक का दिमाग खर्च होता है। इसलिए ज्यादातर पाठक उसे नहीं पढ़ते। सूचनाओं की अधिकता हमारे साहस को कमजोर करती है। कई बार जिसे जानकार लोग नहीं कर पाते उसे गैरजानकार लोग कर गुजरते हैं। अधिक छानबीन अधिक खोजखबर, अधिक पूर्वानुमान और अधिक विश्लेषण जैसी चीजें सक्रियता-विरोधी है। वे यात्रा को शुरू ही नहीं होने देतीं।
सूचनाओं के चौतरफा विस्फोट और उनका एक पूरा बाजार तैयार हो जाने के बावजूद सूचनातंत्र की जरा सी गफलत तबाही ला सकती है। ऐसी ही एक गलत सूचना से रूस और अमेरीका एक बार आणविक युद्ध के कगार पर जा पहुंचे थे। दूरसंचार तकनालॉजी और कंप्यूटर के मेल से जन्मा इंटरनेट, दूरसंवेदी उपग्रह आदि दिनरात उपभोक्ताओं की सेवा में मुस्तैद हैं। लेकिन इस सेवा का मूल्य चुकाना सबके बस की बात नहीं है। हमारे अपने दूरसंवेदी उपग्रह आसमान में लगभग आठ सौ किलोमीटर की ऊंचाई से रोज हमारे ऊपर से गुजरते हैं। वे खास किस्म के इन्फ्रारेड कैमरों से चप्पे-चप्पे की तस्वीर खींचते हैं। उन्हें मानो दिव्यदृष्टि प्राप्त है, लेकिन उनसे मिली इतनी सारी सूचनाओं का अपनी खेती, समुद्र, गांव-शहर, जलसंसाधन र्इंधन, खनिज संपदा आदि किसी भी क्षेत्र में फिलहाल हम कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सकल पदार्थों की दुनिया में सूचनाएं भी महंगा पदार्थ हैं। भाग्यवान नर ही उन्हें पा सकते हैं। लेकिन उनके उपयोग के लिए उन्हें और बड़े भाग्य की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
सूचनाओं के घटाटोप से भाषा को हो रहे नुकसान के बारे में कथाकार ज्ञानरंजन की टिप्पणी बेहद सटीक है। वे कहते हैं- ‘हमारे सिर पर सूचनाएं हर पल कचरे और धूल की तरह गिर रही हैं। कंप्यूटर के तूफानी आगमन ने हमारी भाषा पर असर डाला है और उसको न केवल तोड़ा है बल्कि बिल्कुल फीका भी कर दिया है।’ अपनी कविता में जार्ज कोनार्ड कहते हैं- यह एक खतरनाक समय है। शब्द की गरिमा नष्ट हो रही है। वास्तव में सूचनाओं की भरमार हमारी भाषा के चेहरे को सपाट बना रही है। वह उसे
तार की भाषा या फौजी भाषा में बदल रही है। भाषा का वह स्वरूप जो अर्थ की बहुविधि छवियों और उसके विविध स्तरों का उद्घाटन करता है, प्रचलन से हट रहा है। समर्थ भाषा के अभाव में हमारी संवेदनाएं भी भोथरी होती जा रही हैं।
सूचना संपन्नता आधुनिकता का प्रमाण नहीं है। कंप्यूटर से सजा और सॉफटवेयर, फ्लॉपी, डाटाबेस, इनपुट, नेटवर्क, पैन ड्राइव, फैक्स, पेजर जैसे शब्दों से गुंजायमान दफ्तर निहायत दकियानूस और सामंतवादी भी हो सकता है। कुछ साल पहले संसार के आधुनिकतम देश संयुक्त राज्य अमेरिका में उनतालीस व्यक्तियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए सामूहिक आत्महत्या की थी। वे सब कंप्यूटर प्रोग्रामर थे और कंप्यूटरस और इंटरनेट से परिपूर्ण अपने घर को मंदिर कहते थे। आधुनिकता तो विचार की बेटी है। आज के तमाम सूचना संपन्न चमकदार व्यक्तियों की तुलना में महात्मा गांधी ज्यादा आधुनिक थे। सूचना बहुलता से व्यवस्था में पारदर्शिता आ ही जाए, यह जरूरी नहीं है। बड़ा सरअंजाम हमेंं बड़े छल और बड़ी हेराफेरी की दिशा में भी ले जा सकता है।
इन दिनों सूचना के अधिकार की भी चर्चा है। यह गोपनीयता, एकाधिकार और शासन-प्रशासन में कार्यों के लंबित रहने के विरुद्ध शुरू हुई सुगबुगाहट है। पर, यह जान लेने से कि दरख्वास्त किस पायदान पर है, हमें क्या सुख मिलने वाला है? ऐसी सूचना से क्षोभ और उत्तेजना तो मिलेगी, तृप्ति नहीं। मूल सवाल नीयत का है। अगर दफ्तर की नीयत ठीक हो तो दरख्वास्तकर्ता को घड़ी-घड़ी सूचना पाते रहने की जरूरत ही क्या है ?
सूचना पाने का अधिकार किसी दिन वैयक्तिक रिश्तों और परिवारिकता के दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। वहां इससे कई नुकसान हो सकते हैं। एक तो कभी कभी सूचना न देना ज्यादा प्रभावी होता है। पिता आर्थिक संकट को झेलता हुआ पुत्र को पढ़ाई का खर्च देता रहे और इस बारे में कभी चर्चा न करे तो पुत्र के कृतज्ञतापूर्वक सही दिशा में चलते रहने की अधिक संभावना है, क्योंकि सूचना के अभाव में पुत्र की देखने, समझने, कल्पना करने और महसूस करने की शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाएंगी। अगर, सूचना समय के पूर्व प्राप्त हुई तो यह नदी पर पहुंचने के पूर्व ही उसे तैर कर पार करने जैसा होगा। इसमें हाथ पैर छिल सकते हैं तीसरे, ज्यादा सूचना परीक्षण रिश्तों में जहर घोल सकता है। संसार में सभी मनुष्य आधे अधूरे हैं। हमें इन्हीं में से यात्रा के साथी चुनने होंगे। परिपूर्ण मनुष्य की तलाश में बैठा व्यक्ति कभी यात्रा पर निकल ही नहीं पाएगा। साथी के बारे में ज्यादा खोजबीन करते रहेंगे तो साथी से ही हाथ धो बैठेंगे। किसी कवि की पंक्तियां हैं- मेरी इतनी कठिन परीक्षा तो मत लो प्रिय/ खो दोगे यदि मुझे तुम्हीं तो पछताओगे।
सूचनाओं ने अचानक हमला करके आरंभिक लाभ ले लिया है। सूचनाओं से व्यावसायिकता को और व्यावसायिकता से सूचनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। मनुष्य के स्वभाव में व्यावसायिकता का प्रवेश हो गया है। लेकिन सूचनाएं अपने आप में कोई मूल्य नहीं हैं। उन्हें प्राप्त हुई प्रतिष्ठा क्षणिक और तात्कालिक है। इसलिए उनके संजाल में घिरे होने, कंप्यूटर के सामने बैठे रहने, वाट्स अप और इंटरनेट से जुड़ने और अखबारों को ओढ़ने-बिछाने के बावजूद हमें सूचनाओं को उनकी औकात बताते रहना चाहिए। हम उनके लिए नहीं, वे हमारे लिए हैं। ०