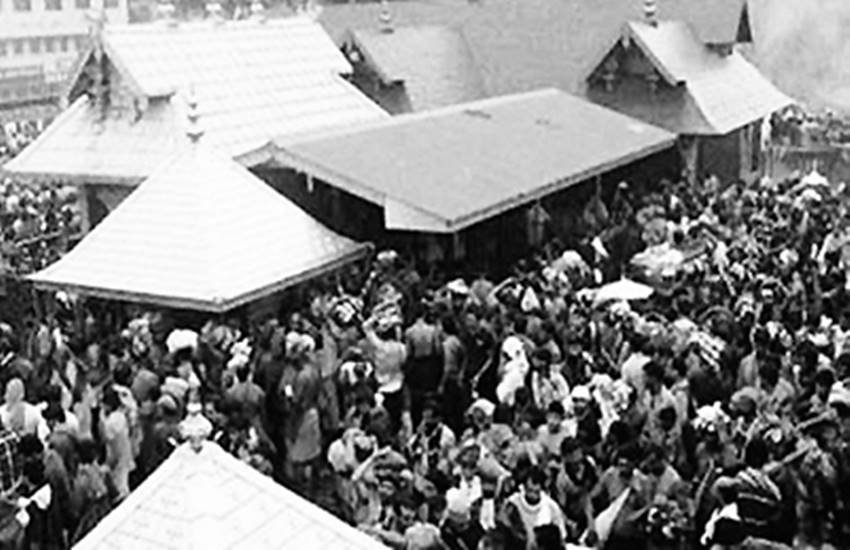ब्रह्मदीप अलूने
विकास के उच्च प्रतिमान स्थापित करने की होड़ में आगे बढ़ता समाज इस समय गहरी निराशा, हताशा और वैचारिक संकीर्णता से जूझ रहा है। इसका प्रमुख कारण विभिन्न देशों में उभरती राजनीतिक सत्ताएं हैं जो अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मध्ययुगीन जातीय, राजनीतिक, नस्लीय और धार्मिक वैचारिक द्वंद्व को पुन: स्थापित करने को प्रतिबद्ध नजर आ रही हैं। इसका प्रभाव पिछड़े, विकासशील राष्ट्रों से लेकर विकसित दुनिया में भी देखा जा सकता है। यूरोप से जुड़ा मुसलिम बहुल देश तुर्की विकास और खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है। हाल ही में वहां के राष्ट्रपति ने महज स्थानीय चुनावों में फायदा लेने के लिए न्यूजीलैंड के उन कथित वीडियो का सहारा लेने तक से गुरेज नहीं किया जिनमें एक दक्षिणपंथी मस्जिद में घुस कर मुसलिम धर्मावलंबियों को निशाना बनाते हुए दिख रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रैचेप तैयब अर्दोआन का अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूत करने के लिए देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को ही निशाना बनाने के इन प्रयासों का न्यूजीलैंड ने भी विरोध किया और इसे समूचे क्षेत्र के लिए खतरनाक बताया। माना यह जा रहा है कि दक्षिणपंथी अर्दोआन ने यह वीडियो दिखा कर चुनाव को मुसलिम बनाम ईसाई का रंग देने की कोशिश की।
दरअसल, फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में उदारवादी विचारधारा पनपी और यहीं से राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों का बेहतर समन्वय भी हुआ। उदारवाद अठारहवीं सदी के बौद्धिक आंदोलन से प्रेरित था, जिसने असमानता और निरंकुशता का विरोध करते हुए संसदीय शासन और विधि के नियम को सर्वोपरि मान कर इसका समर्थन किया। इसके दूरगामी परिणाम विश्वभर की राजसत्ताओं पर पड़े और स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के विचारों को मजबूती मिली। सभ्यता जब चरम पर पहुंच जाती है तो उसका पतन भी शुरू हो जाता है। अमेरिका सहित यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई देशों में बीते कुछ सालों से सत्ता का संक्रमण काल चल रहा है। मध्ययुगीन पुरातनवादी राजसत्ता अब राजनीतिक सत्ता के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ऐसे में विश्व समुदाय के सामने ऐसा संकट बढ़ता जा रहा है जिसके अनुसार सत्ता की संकीर्णता राष्ट्रवाद की आड़ लेकर समाज के सार्वभौमिक वैचारिक ढांचे को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। इसका व्यापक असर समूची दुनिया पर पड़ सकता है और कई देशों में सांप्रदायिक तनाव की तीव्रता बढ़ कर उन्हें गृहयुद्ध की कगार पर ढकेल सकती है।
द्वितीय विश्व युद्ध में सभ्यता और संस्कृतियों के द्वंद्व के बाद परिवर्तनशील बौद्धिक क्रांति ने परंपरावादी, दक्षिणपंथी और धर्मांध समाज को मध्यमार्गीय उदारता से जोड़ने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र जैसे अभिकरण मानवता की रक्षा करने की दिशा में कामयाबी से आगे बढ़ते रहे। महाशक्तियों की आपसी कड़ी प्रतिद्वंद्विता में भी मध्यपूर्व के इराक जैसे इस्लामिक देश की राजनीतिक सत्ता में ईसाइयों का प्रभुत्व राष्ट्रवाद का संतुलन धर्मनिरपेक्षता के आदर्श से स्थापित करता हुआ प्रतीत होता था। तुर्की की पहचान भी धर्मनिरपेक्ष और उदार देश की रही है। लेकिन अब वहां दक्षिणपंथी राजनीति के उभार से सार्वभौमिकता पर संकट गहराने लगा है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दुनिया को विभाजनकारी राष्ट्रवाद के खतरे से आगाह किया था। उन्होंने 2016 में अपने कार्यकाल के अंतिम विदेशी दौरे पर यूनान में ट्रंप की नीतियों पर निशाना साधा था। ओबामा ने दुनिया में साथ रहने की जरूरत पर बल देते हुए कहा था कि इस दुनिया का भविष्य इससे तय होगा कि हममें क्या समानताएं हैं, न कि उन बातों से जो हमें अलग करती हैं या संघर्ष की ओर ले जाती हैं। अमेरिका में दक्षिणपंथी ट्रंप के उभार को वैश्विक संकट के रूप में देखा गया। ट्रंप की जीत के बाद उनकी जातीय और धार्मिक भेदभाव की नीति को लेकर ओबामा खुद आशंकित थे और उसे अमेरिका के वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों से जोड़ कर देख रहे थे। अब ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं और उनके नस्लवादी और मजहबी विचारों का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता दिखाई दे रहा है। अट्ठाईस साल के जिस आॅस्ट्रेलियाई नागरिक ब्रेंटन टैरंट ने न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर की दो मस्जिदों में गोलियां दागी थीं, वह भी अपने को ट्रंप का प्रशंसक बता रहा था।
यह भी बेहद दिलचस्प है कि धर्मांधता और असमानता में विश्वास करने वाला बेहद पढ़ा लिखा वर्ग तो है ही, इसके साथ ही ग्रामीण इलाके भी इस विचारधारा को पोषित कर रहे हैं। ट्रंप को पसंद करने वालों में पैंतालीस साल से लेकर वरिष्ठ नागरिकों का बाहुल्य है जो बेहद परंपरावादी होकर नस्लीय भेदभाव में विश्वास रखते हैं। अपनी विभेदकारी स्पष्ट नीतियों को लेकर ट्रंप अमेरिका की बुजुर्ग आबादी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बेहद परंपरावादी समाज की एकमात्र पसंद के तौर पर उभरे हैं जिसे क्रुद्ध श्वेत भी कहा जाता है। ये लोग दुनिया भर के लोगों को अमेरिका में रहते देखना नहीं चाहते और अपने बच्चों के रोजगार के लिए भी विदेशियों को खतरा समझते हैं। न्यूजीलैंड में मस्जिद पर हमला करने वाले आॅस्ट्रेलियाई नागरिक ब्रेंटन टैरंट को भी क्रुद्ध श्वेत माना गया। उसने भी यूरोप के लिए प्रवासियों को खतरा ही माना है। जाहिर है, इन अति दक्षिणपंथी ताकतों को ट्रंप जैसे लोग मजबूत कर रहे हैं, वहीं कथित धार्मिक और जातीय समूह इसे धर्मयुद्ध के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। इस विकासवादी युग में सभ्यता और संस्कृति की आपसी प्रतिद्वंद्विता बढ़ रही है, वहीं दक्षिणपंथी और उग्र-राष्ट्रवादी सत्ताओं का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी बढ़ा है।
बदलते दौर में दक्षिणपंथी ताकतों ने न केवल वैधानिक सत्ता के जरिए व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया है, बल्कि वे जातीय और धार्मिक समूहों के पैरोकार भी बन गए हैं। पाकिस्तान जैसे मजहबी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा इसीलिए चुनौती बन गई है क्योंकि प्रभावी धार्मिक समूहों के सामने सत्ता कड़े कदम उठाने से बचती रही है। इन्हीं कारणों से कट्टरता आगे बढ़ कर आतंकवाद को बढ़ावा देने लगती है। ब्रिटेन की धुर दक्षिणपंथी ब्रिटिश नेशनल पार्टी के पूर्व सदस्यों ने 2011 में ‘ब्रिटेन फर्स्ट’ नामक संगठन की स्थापना कर नस्लीय दूरियां पैदा करने कोशिशें शुरू की थीं। ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरेजा मे ने भी स्वीकार किया कि ब्रिटेन फर्स्ट नफरत फैलाने वाली बातें करता है जो झूठी होती हैं और तनाव पैदा करती हैं। यूरोप के सबसे बड़े मुसलिम बहुल राष्ट्र फ्रांस में साल 2017 के चुनावों में कोई दक्षिणपंथी सत्ता में न आ जाए, इसे लेकर अल्पसंख्यक गुट दहशत में नजर आए। इस प्रकार मैक्रों के दल को कई गुटों से समर्थन मिला। पेरिस की मस्जिदों ने मुसलमानों को मैक्रों को वोट देने के लिए आग्रह किया था।
ब्राजील के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। इस समय वहां के राष्ट्रपति धुर दक्षिणपंथी जेयर बोल्सोनारो हैं। उन्होंने खुद को एक विभाजनकारी के रूप में साबित किया और नस्लवादी, समलैंगिक विरोधी और महिला विरोधी सोच को समाज के सामने रख कर चुनाव बड़े अंतर से जीता। उनकी विभाजनकारी नीतियां न केवल इस देश के लिए बल्कि पूरे महाद्वीप के लिए खतरा बन गई हैं। आधुनिक प्रगतिशील युग में कई देशों में धुर दक्षिणपंथी राजनेता अपनी विभाजनकारी नीतियों के बल पर बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं और उनके दल सत्ता पर काबिज भी हो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा संकट अल्पसंख्यक धार्मिक, नस्लीय और जातीय समूहों के सामने उठ खड़ा हुआ है। यदि दुनिया भर में स्थापित वैधानिक व्यवस्थाएं समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखा सकीं तो इसके नतीजे बेहद घातक हो सकते हैं।