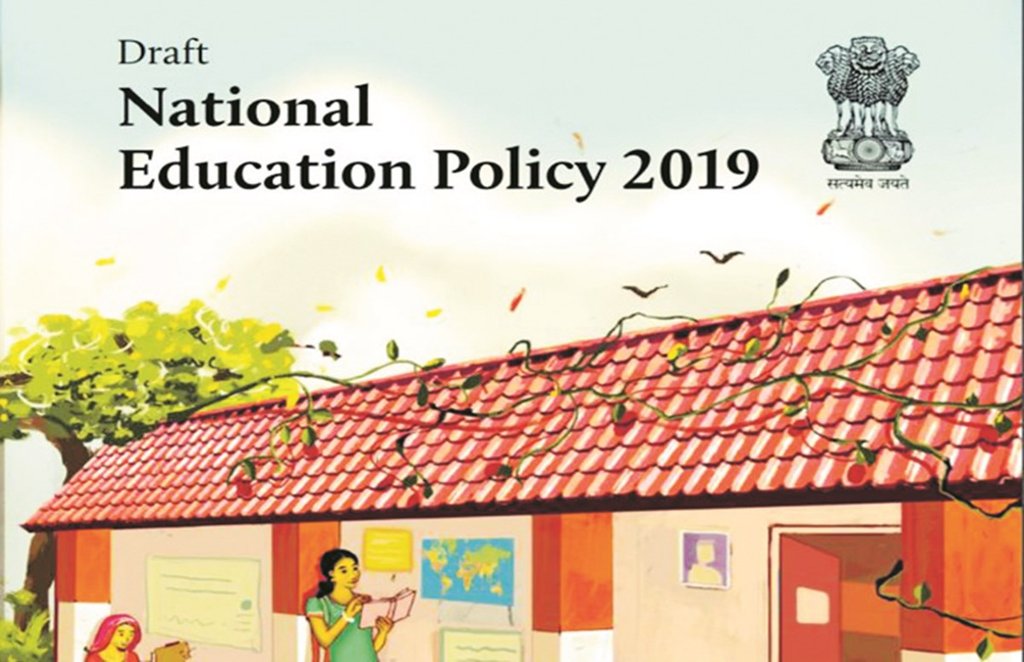नई शिक्षा नीति घोषित होने के बाद अब स्वाभाविक ही पीछे से चली आ रही कमियों के बरक्स इसे नापा-तोला जा रहा है। विश्वविद्यालयों में शोध से पहले एमफिल की अनिवार्यता की समीक्षा भी उसी का नतीजा है। नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। इस पर कुछ पूर्व कुलपतियों और शिक्षाविदों का कहना है कि यह फैसला उचित है, इससे विद्यार्थियों का नाहक वक्त बर्बाद होता था। मगर कुछ विद्यार्थी समूह और शिक्षाविद इसे हटाए जाने के खिलाफ हैं। दरअसल, लंबे समय से मांग की जा रही थी कि शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाए, ताकि बारहवीं तक की पढ़ाई के बाद जो बच्चे जिस रोजगार में जाना चाहते हैं, जा सकें। जिन्हें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, शोध, अनुसंधान वगैरह करना है, उनके लिए लंबी अवधि की शिक्षा रखी जा सकती है। बहुत सारे देशों में यही व्यवस्था है।
बच्चे स्कूल से निकलने के बाद ही अपना रोजगार चुन लेते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में विभिन्न पाठ्यक्रमों की अवधि तय की गई है। स्नातक और परास्नातक स्तर पर बच्चों की सुविधा और कौशल विकास के मद्देनजर पढ़ाई-लिखाई को डिप्लोमा और डिग्री के रूप में विभाजित कर दिया गया है। उसी क्रम में एमफिल की अनिवार्यता भी हटाई गई है।
दरअसल, एमफिल पाठ्यक्रम लागू करने के पीछे मकसद था कि विद्यार्थियों को पहले शोध की सही प्रविधि सिखाई जाए। इससे उनमें वैज्ञानिक तरीके से शोध करने का कौशल विकसित होगा। इस पाठ्यक्रम की अवधि दो साल रखी गई थी। उसके बाद तीन साल शोध के लिए। हालांकि कुछ साल पहले तक सभी विश्वविद्यालय एमफिल पाठ्यक्रम नहीं चलाते थे। पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे अनिवार्य करने को कहा, तो लगभग सभी जगह यह लागू हो गया। एमफिल में विद्यार्थी को शोध प्रविधि की पढ़ाई करने के बाद एक लघु शोध प्रबंध जमा करना होता है।
माना जाता है कि इससे विद्यार्थी में शोध का अभ्यास बनता है। चूंकि शोध करने वाले ज्यादातर विद्यार्थी आगे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या फिर शोध संस्थानों में जाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें शोध की वैज्ञानिक पद्धति सिखाना अनिवार्य माना गया था। पर विश्वविद्यालयों में शोध की जैसी स्थिति हो चली है, चालू ढंग से शोधपत्र लिख कर जमा कर देना आम बात है। इससे एमफिल का मकसद कहीं पूरा होता नहीं दिख रहा था। इसलिए कई शिक्षाशास्त्री इसे समय की बर्बादी मानते थे।
निस्संदेह एमफिल पाठ्यक्रम समाप्त होने से विद्यार्थियों का दो साल का वक्त बचेगा। जहां तक शोध प्रविधि की बात है, वह उन्हें शोध निर्देशक सिखा-बता सकते हैं। मगर इस फैसले से शोध और अनुसंधान की गुणवत्ता कितनी बेहतर होगी, यह सवाल शायद अनुत्तरित ही रहने वाला है। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई के स्तर का सालाना मूल्यांकन बताता है कि शोध और अनुसंधान के मामले में भारत लगभग फिसड्डी है। ऐसे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विज्ञान, समाज विज्ञान आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने वाले संस्थानों की तरफ से खर्च होने वाले धन पर सवाल उठते रहे हैं। शोध प्रबंधों में चोरी और नकल की प्रवृत्ति आम है।
जरूरत है अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने की। वह कैसे आएगी, यह भी सोचने का विषय है। एमफिल समाप्त कर देने भर से इसकी गारंटी नहीं मिल जाती। आज इसे फिजूल माना जा रहा है, पर जब इतने सालों से अनेक कुलपति इसे हटाने की मांग कर रहे थे, तब उनकी बातों पर कान क्यों नहीं दिया गया!