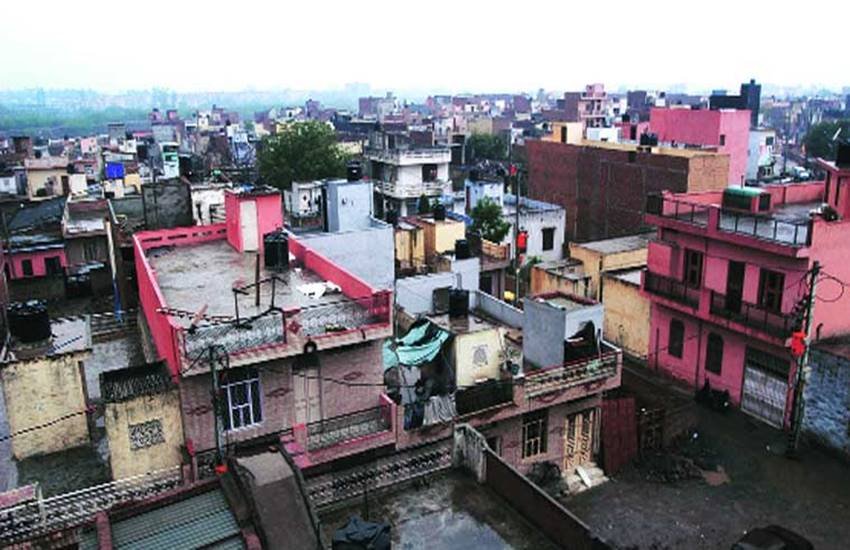शहरी जिंदगी में कॉलोनियों-सोसाइटियों की दीवारें कुछ हद तक सुरक्षा का अहसास तो देती हैं, लेकिन उसी अनुपात में दुनिया की जीवंतता से भी दूर करती हैं। हाल में जब एक दिन अपनी नौकरी और घर की एक जड़ दिनचर्या और महानगरीय ‘दड़बे’ से निकलने का मौका मिला तो इस पहलू पर थोड़ा ज्यादा गौर कर सकी। यों दिल्ली अपने आप में विविधताओं के केंद्र के रूप में ही निखरती है। लेकिन यहां के एकाध ठिकाने इसी विविधता को कलात्मक शक्ल देते हैं। ऐसी ही खुशनुमा और गुलजार जगहों में से एक है दिल्ली हाट, जहां न सिर्फ स्थानीय लोगों, बल्कि देशी-विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा हर वक्त लगा रहता है। भारत के लगभग हर राज्य की हस्तकला की सुंदर चीजें और सुस्वादु भोजन के साथ-साथ जो एक चीज दिल्ली हाट को ज्यादा खास बनाती है, वह है दूरदराज के इलाकों के गांव-कस्बों के किसानों और कुटीर उद्यमियों को अपने उत्पादों के लिए एक बाजार की सुविधा।
हालांकि दिल्ली हाट मेरे घर से कार्यालय जाने के रास्ते में ही पड़ता है। लेकिन शहरी जीवन के कृत्रिम अभावों के बीच वहां जाना खास था। वहां एक दुकान पर कुछ खाने के बाद मैं स्टॉलों पर यों ही घूमने लगी। मणिपुर के स्टॉल पर दो ग्रामीण महिलाएं दिखीं जो अपनी कुशल कारीगरी से बने सामान और वस्त्र बेचने में तल्लीन थी। वहीं एक मणिपुरी छात्रा भी साथ में खड़ी थी जो सामान खरीदने आए लोगों से मोल-भाव करने के साथ-साथ हर सामान की विशेषता भी हिंदी या अंग्रेजी में बता रही थी। मैं भी वहां रुकी और वहां रखे एक हैंडलूम शॉल की कीमत के बजाय उसके बारे में पूछा कि ये कहां और कैसे बनाई जाती है। जवाब में मुझे जो कहा गया, वह मेरे लिए अचरज भरा था।
दरअसल, ये शॉल और सामान मणिपुर की उन ग्रामीण महिलाओं ने बनाए हैं जो अपने पति की असामयिक मृत्यु या घरेलू हिंसा के कारण अकेले जीवन-यापन कर रही हैं। ये महिलाएं अलग-अलग गांव या कबीले की रहने वाली हैं और इनमें से अधिकतर किसी न किसी जनजाति से संबंधित हैं। हर कबीले की हस्तकला, चाहे वह कपड़े बुनने की हो या डलियां-बर्तन बनाने की, दूसरे कबीले या जनजाति से अलग और अनोखी होती है। ये महिलाएं अपने स्थानीय बाजारों में तो सामान बेचती ही हैं, साल में एक बार ‘मदर्स हाट’ के नाम से दिल्ली हाट में भी अपना स्टॉल लगाती हैं। इससे होने वाली आय से ये अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करती हैं।
परिवार चलाने और बच्चों को पढ़ाने-लिखाने का पूरा दायित्व इन महिलाओं पर है। इन सबके पीछे दुखद अतीत है और आगे चुनौतीपूर्ण भविष्य, इसके बावजूद जो खुशी इनके मुंह पर दिखती है, उससे इन ‘वूमेन सरवाइवर्स’ यानी किसी तरह जिंदा बची रही इन महिलाओं के लिए सम्मान भाव मन में सहज ही उमड़ पड़ता है। उस छात्रा की मदद से मैं जो भी बातें उन दोनों महिलाओं से कर पाई, उससे यह बिल्कुल साफ समझ में आया कि सुदूर उत्तर-पूर्व की महिलाओं के जीवन में न जाने कितनी परेशानियां हैं। घर-परिवार, समाज और प्रशासन से मिलने वाली चुनौतियों और लगने वाले अंकुश का जवाब ये महिलाएं अपनी कुशल कारीगरी से देती हैं।
कई कबीलों में आपस में कलह होता रहता है, जिसे ‘एथनिक वार’ या जातिगत संघर्ष कहा जाता है। सैन्य प्रशासन और स्थानीय उग्रवादी गुटों में भी निरंतर संघर्ष होता रहता है। एक दशक से ज्यादा वक्त से इरोम शर्मिला के अनशन के बावजूद मणिपुर की त्रासदी के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले आफ्सपा कानून को हटाने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। जबकि सब जानते हैं कि लंबे समय से वहां लागू आफ्सपा के चलते मणिपुर के समाज को किस त्रासदी से गुजरना पड़ रहा है। ऐसी लड़ाइयों में अपने पति या बेटे को खो चुकी महिलाओं की तादाद अकेले इंफल में ही पांच हजार से ज्यादा है। मणिपुर के बाकी इलाकों में भी इनकी संख्या हजारों में है।
ऐसी स्थिति में स्वरोजगार या लघु उद्योग के माध्यम से ये महिलाएं अपना परिवार तो चला ही रही हैं, स्त्री सशक्तीकरण के आधुनिक पाठ को भी रच रही हैं। इनकी जिजीविषा और आर्थिक आत्मनिर्भता से भारत के अन्य हिस्सों की महिलाओं को भी प्रेरणा मिलती है। दरअसल, स्त्री जीवन की हर समस्या और समाज द्वारा खींची गई सीमाओं का अंत उसी वक्त हो जाता है, जब वह अपने घर के बाहर कदम रखती है। फिर चाहे वह कदम किसी स्कूल की तरफ हो या ‘मदर्स हाट’ की तरफ।
ज्योति ठाकुर