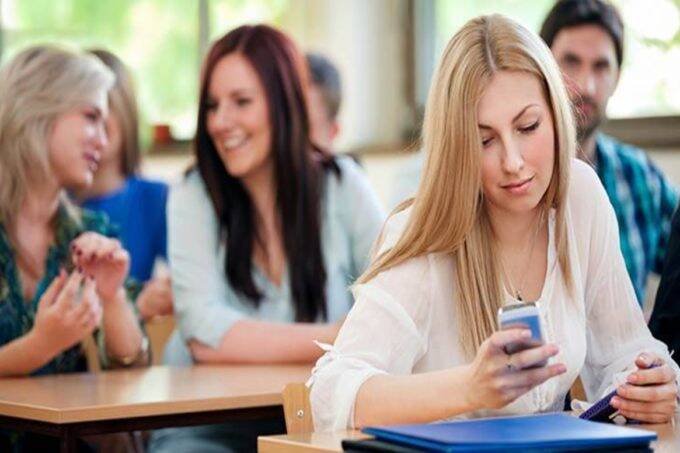मोनिका भाम्भू कलाना
समाज संवाद से जिंदा रहता है। लेकिन क्या अब इस समाज को संवाद की जरूरत महसूस हो पा रही है? उम्र के आखिरी दशक में मेरी दादी को दिखना बंद हो गया था। उन्हें इस बात का मलाल अंत तक रहा कि पता नहीं क्या-क्या उनके देखे बगैर रह गया है। लेकिन अपने जीवट को उन्होंने उसी अनुपात में श्रवण पर केंद्रित कर लिया था। किसी से भी बतियाने की, कुछ पूछने की अजीब-सी आकांक्षा उनमें आखिरी सांस तक रही। वे ढेर सारी बातें कर लेती थीं, किसी अजनबी से भी। वे किसी न किसी का मुंह खुलवाने में कामयाब हो जातीं। हर रोज वही बातें उतनी ही दिलचस्पी से किसी के भी साथ बांटने की जो सामर्थ्य उनमें थी, वह विरले लोगों के पास होती है।
मगर आजकल संवाद का सिरा पूरी तरह गड़बड़ाया हुआ है। एक तो फालतू की व्यस्तता है, ऊपर से यह भी कि बताने से आखिर होना भी क्या है! ऐसा नहीं है कि कोई किसी से बोलना नहीं चाहता या किसी के पास साझा करने के लिए कुछ न हो, मगर हमारे दिमाग में इतना कचरा है कि उसे अवशोषित करने में हमारा वास्तविक माहौल उतना सक्षम नहीं है। फिर जहां हम रहते हैं, वहां अपनी कमजोरियां जाहिर करना भी बड़ा जोखिम वाला काम है। एक तरह के डर से हमेशा घिरे रहना पड़ता है। किसी को कुछ न कह पाने की बेचैनी से ज्यादा मुश्किल है किसी को कुछ बता कर किस्तों में उनकी प्रतिक्रियाओं को झेलने की विवशता। अब न संवाद उतने सरल हैं, न समझ। हर कोई खुद से ही इतना भरा हुआ था कि किसी ‘दूसरे’ के लिए जगह बच ही नहीं जाती। और बचती है तो अपने अनुकूल न होने की शिकायत।
इसके उलट सोशल मीडिया के मंच हैं। वहां किसी तरह का कोई दायरा नहीं है। हम कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं और खुद ही समझदार होने का भ्रम भी पालते रह सकते हैं। गुस्सा, तनाव, परेशानी, कुंठा- सभी से निजात मिलेगी, बिल्कुल मुफ्त में। समस्या एक और भी है। गैरजिम्मेदारी से किया गया कोई भी कार्य सही परिणाम कब तक दे सकता है? यहां लगाव नहीं है। किसी को समझने की फुर्सत नहीं है। बस खाली होने की जल्दी है। अपने दुख को बयान करने की जो तत्परता इससे पैदा हुई है, उससे हम लेंस लगा कर केवल अपने दुख के ही बारे में सोचने के आदी हो गए हैं। दूसरों की ओर देखने की, अपना गम जज्ब करने की जो संस्कृति हमारे यहां थी, वह इस पीढ़ी में लुप्त होती जा रही है।
परिवारों में अंदरूनी जुड़ाव के जो मसले थे कम होते जा रहे हैं। हर कोई जरूरत भर के लिए बोलता है या यों कहें कि स्वार्थ के लिए ही। कोई आ भी जाए तो सबको यही जल्दी रहती है कि यहां से उठ कर फोन चलाया जाए। कुछ लोग चौबीस घंटे स्मार्टफोन से जुड़े रहने की अनिवार्यता में अपनी जागरूकता समझते हैं, भले ही उन्हें मालूम न हो कि उनके बच्चे ने पिछले साल भर में कुछ नया सीखा है या नहीं।
संवाद के सूत्र इस कदर टूट क्यों रहे हैं? पहले की बैठकें, हथाई, गुरबत तो अब रही नहीं। तो क्या दो-चार बातें साझा समस्याओं पर भी नहीं? लेकिन क्रांति तो सारी काल्पनिक दुनिया में कर चुके होते हैं! फिर वास्तव में वे छोटे-छोटे कार्यों के लिए अपने बड़े दिमाग और पवित्र शरीर का इस्तेमाल क्यों करें। दो युवा व्यक्ति इकट्ठा होते ही वैश्विक नागरिक होने का दायित्व निभाते हुए देश-दुनिया की राजनीतिक समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते देखे जाते हैं, जबकि वे जिस जमीन पर खड़े होते हैं, वहां फैले कीचड़ को उनकी साफ आंखे नहीं देख पातीं। यह विरोधाभास है या अपनी समस्याओं से भागने की मजबूरी या कातर असहायता?
आज घरों में बहुत सारी दादियां हैं जो कई-कई दिन घर में किसी से बतियाने को तरसती हैं। लेकिन जुबान सुनती है तो आखिर चुप रहने की ही। वहीं इस अनबोले जमात में धीरे-धीरे घर के सभी सदस्य शामिल होते जा रहे हैं। संवादहीनता की इस स्थिति में व्यक्ति तब्दील होता जा रहा है खुद एक ‘स्थिति’ में और घर बदलते जा रहे हैं घरों के समूह में। घरों में अब परिवार नहीं, हर व्यक्ति ही अलग घर है। कितने ऐसे लोग हैं, जिनके पास न कोई बतियाने को है और जिनकी पहुंच किसी तरह के सामाजिक मंचों तक भी नहीं है। ऐसे लोग क्या करें? वे किनसे बतियाएं, किस तरफ जाएं? आत्महत्या करें या घुटते-घुटते संवेदनहीन होने को मजबूर हों?
स्थितियां दरअसल उतनी साफ और सरल नहीं होती जितनी अक्सर दिखती हैं। उनकी तह में जाने पर उनके अतिरिक्त जिन शाखाओं से हमें रूबरू होना पड़ता है, वहीं से ही किसी समाधान की संभावना बन सकती है। ‘संबंधों के दरकने’ की यह समस्या न तो किसी एक स्तर पर है और न ही किसी एक वजह से। हजारों छोटी-छोटी चीजें जो इसके बनने-बिगड़ने में अपनी भूमिका निभाती है, उनको नियंत्रित करके ही समस्या बनने वाले मुद्दों को सुधारा जा सकता हैं।