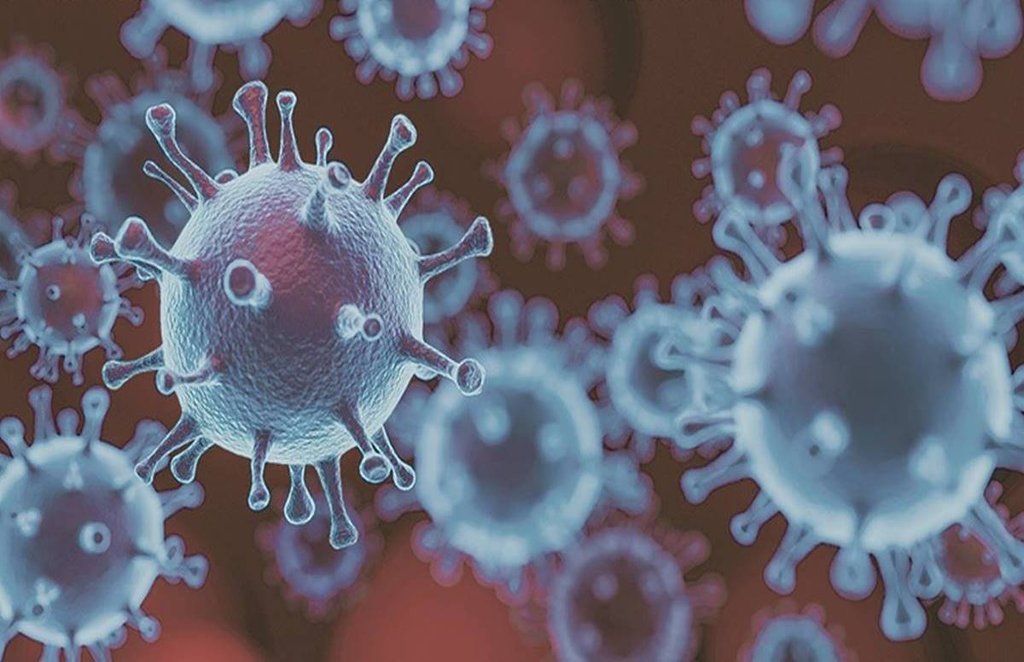कोरोना के चलते भौतिक समृद्धि का दंभ कोसों दूर जा चुका होगा। निश्चित ही हम चाहे आसमान की उड़ान भरें, लेकिन धरातल को कभी विस्मृत नहीं कर पाएंगे। भौतिक उन्नति ही प्रगति का पर्याय नहीं है। सुरक्षित जीवन आज के दौर की प्रथम आवश्यकता है। यकीनन हमारी महत्त्वाकांक्षाओं पर कोरोना ने काफी हद तक विराम लगा दिया है। आने वाले दौर में प्रगति के मायने बदलते जाएंगे। दुनिया भर की चकाचौंध सर्वथा निरर्थक होगी। भरपूर जीवन जी लिए, यह एक बड़ी उपलब्धि होगी।
इन संदर्भों में हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत की ओर लौटने का मार्ग प्रशस्त होता है। शहरों की तुलना में ग्रामीण परिवेश वर्तमान परिवर्तित दौर में अधिक सुरक्षित दिखाई देता है। निश्चित रूप से जहां आधुनिकता ने पैर नहीं पसारे हैं, वहां नई परंपरा को आसानी से स्थापित होते हुए देखा जा सकेगा।
शहरी क्षेत्रों में पुरानी पीढ़ी के लोगों ने चूंकि पुराना दौर देखा और भोगा है, इसलिए उनकी वापसी बहुत आसान होगी। जहां तक नई पीढ़ी की बात है, उन्हें समझौता करने को विवश होना होगा। कुल मिला कर परिवर्तन के इस दौर में विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा अपने देश के नागरिकों में बदलाव की प्रक्रिया बहुत ही आसानी के साथ संभव सिद्ध हो सकेगी। वैसे भी सादा जीवन उच्च विचार हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है।
पूर्णबंदी के दौर में हमारे अपने वैचारिक दृष्टिकोण में आए हुए सकारात्मक परिवर्तनों को हमें चिह्नित करना होगा। यकीन मानिए जीवन इतना सहज-सरल हो जाएगा कि दुनिया भर के तमाम आडंबर हमारे लिए व्यर्थ सिद्ध होंगे। यों भी जीवन भर के प्रबल क्षमताओं से हमने जो कुछ अर्जित किया है, वह सब कुछ यहीं से लिया और यहीं का दिया है।
यह समय भौतिक समृद्धि पर अभिमान करने का नहीं, बल्कि जीवन को निरापद बनाने का है। दुनिया की कहानी का चक्र प्रारंभ, विकास, चरमोत्कर्ष और अंत के रूप में आदि-अनादिकाल से फलित होता रहा है। दुनिया की तमाम सभ्यताओं में यह समय के दस्तावेजों में दर्ज होता रहा है।
’राजेंद्र बज, हाटपीपल्या, देवास, मप्र
भ्रष्टाचार की घुन
पिछले दिनों भ्रष्टाचार पर जो रिपोर्ट आई, उससे ये बातें स्पष्ट झलकती हैं कि गणतांत्रिक देश में भी आमजन की पहुंच उन अधिकारियों तक नहीं है, जिनसे उनका वास्ता पड़ता है। यह हाल एक बड़े तबके का है। हम सब पुराना गणतंत्र होने की दुहाई देते हैं और वास्तव में हैं भी।
पर समझ में नहीं आता कि स्वाधीनता के इतने बरस के दौरान तमाम पार्टियों की सरकारें आर्इं और गर्इं, लेकिन क्यों हालात नहीं बदले। भला कौन ऐसी पार्टी होगी जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध नरम रवैया अपनाने की बात करेगी। लेकिन यह है कि बदस्तूर जारी है। इसका मतलब यही लगता है कि सरकारों के बदलने से इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब तक इसकी जड़ों पर प्रहार करने की कोशिश क्यों नहीं की गई?
सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों का व्यवहार लोकतांत्रिक देश की तरह क्यों नहीं बदला? उनकी आमजन से दूरी क्यों बनी रही? जबकि इसी का नतीजा है कि बिचौलिए की तरह का या एक अलग तबका निचले स्तर पर पनप चुका है, जो जांच के नाम पर अलग किस्म का भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है।
इससे लालफीताशाही बढ़ने के साथ-साथ तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं।
इसके आश्चर्यजनक पहलू भी हैं कि पहले भ्रष्टाचार की जांच देश हित में होते थे। यह देखे जाते थे कि राज्य के राजस्व का नुकसान नहीं हो। लेकिन हमारे यहां लंबे समय से ऐसी जांचें विरोधियों को निपटाने के लिहाज से हो रही हैं। इसकी सूक्ष्मता पर गौर किया जा सकता है
यह भी अपने आप में भ्रष्टाचार ही है। ऐसा भी नहीं है कि यह केवल ऊपरी स्तर पर है, बल्कि गांव पंचायत स्तर पर भी ऐसी तमाम जांच करवाई जाती है। काम लटके पड़े रहते हैं। रिपोर्ट जब आती है तो नतीजा ढाक के तीन पात। ऐसी व्यवस्था हो कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत की ही प्रारंभिक जांच पहले हो, ताकि विकास में बाधा उत्पन्न न हो। ईमानदारों को हतोत्साहित न किया जाए।
’मुकेश कुमार मनन, पटना, बिहार
शिक्षा में नैतिकता
‘सार्थक शिक्षा तभी है, जब उसमें नैतिकता का समावेश हो।’ किसी विद्वान द्वारा कही गई यह बात भारतीय शिक्षा व्यवस्था और समाज में नैतिकता की आवश्यकता को स्पष्ट करती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर चौहत्तर फीसद है, वहीं शहरी साक्षरता पचासी फीसद और ग्रामीण साक्षरता उनहत्तर फीसद है।
लेकिन वर्तमान समस्याओं, जैसे बलात्कार, हत्या, आतंकवाद, प्रदूषण आदि शहरों में ही क्यों अधिक देखने को मिलते हैं? क्या कारण है कि शहर इन समस्याओं से निरंतर पीड़ित रहते हैं? जवाब है नैतिकता का अभाव। गांधीजी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। गांव ही वास्तविकता में वर्तमान भारतीय संस्कृति के परिचायक हैं। वहीं शहर निरंतर भौतिकतावादी मानसिकता से ग्रस्त होते जा रहे हैं।
गांव में जो नैतिकता बच्चे खेल-खेल में सीख जाते हैं, वह शहरी बच्चे बंद कमरे एवं प्रौद्योगिकी सहारे के कारण नहीं सीख पाते हैं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अधिक अंक लाने वाले विद्यर्थियों को श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन वास्तव में वह श्रेष्ठ है जिसकी शिक्षा में नैतिकता का समावेश हो। वही सच्चे अर्थों में शिक्षित है।
’शुभम मेश्राम, भोपाल, मप्र
समाधान की राह
सरकार द्वारा पारित किए गए तीन कृषि विधानों के विरुद्ध तीन महीने से चल रहे आंदोलन के कारण राष्ट्रीय स्तर पर भारी चर्चा का दौर जारी है। पक्ष-विपक्ष का प्रपंच चल रहा है। कुछ किसानों के संगठनों के द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी अर्जी की जा चुकी है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा त्वरित सुनवाई करते हुए सरकार को अपना पक्ष रखने का एक कठोर निर्देश दिया गया है। यह त्वरित निर्णय यह दर्शाता है कि सरकार के साथ-साध देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी देश के अन्नदाताओं की कितनी चिंता है।
हमारे देश के इस शीर्षस्थ न्यायालय के द्वारा देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए काफी कुछ किया गया है। यहां इस न्याय के मंदिर में महत्त्वपूर्ण न्याय निर्णयों का इतिहास रहा है। इस कारण यह भी अपेक्षा की जाती है कि जनमानस के हितों में सर्वोच्च न्यायालय शीघ्र निर्णय देगा।
’अशोक, पटना, बिहार