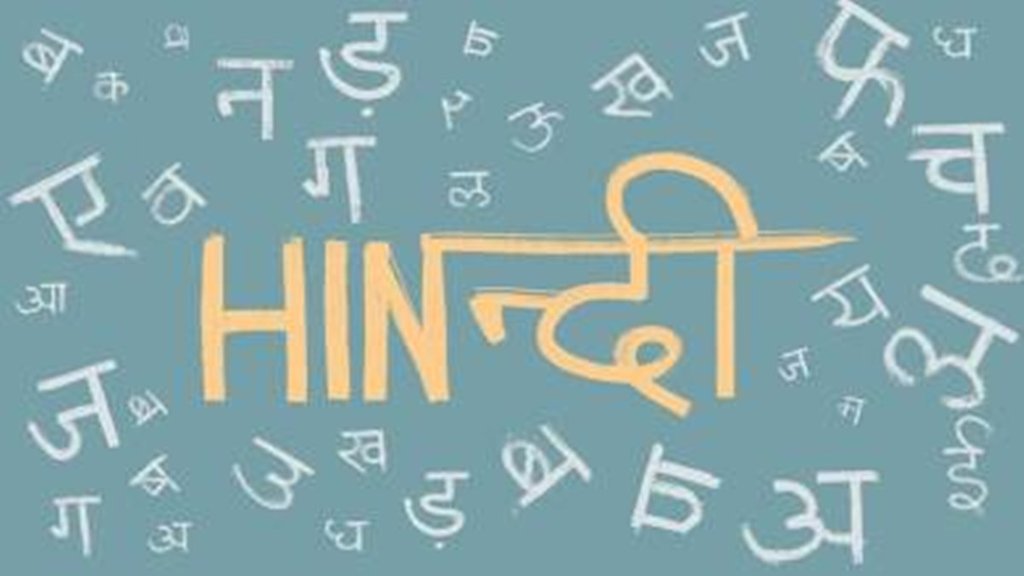फिर भी कोई एक भाषा है जो जनसमूह के अधिकतम हिस्से के द्वारा बोली जाती है तो वह हिंदी है। देश की अधिकांश आबादी की मातृभाषा हिंदी है, पर हिंदी इस देश की भाषा होकर भी दोयम दर्जे पर कायम है।
अंग्रेजों ने जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की तो उन्होंने भारत में शासन के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया, क्योंकि वे भारतीय साहित्य को यूरोपीय साहित्य से निकृष्ट मानते थे और साथ ही अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को पूरा करना चाहते थे। पर आजादी के बाद भी हमारे देश में अंग्रेजी का प्रभुत्व बरकारार है। जबकि गांधीजी ने भी कहा था कि भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य एकमात्र हिंदी भाषा ही कर सकती है। लेकिन हिंदी सिर्फ राजभाषा ही बनकर रह गई।
आज भी भारत सरकार के लगभग सभी अधिकारिक कार्य मूल रूप से अंग्रेजी में ही होते हैं। हमारी न्यायपालिका में अंग्रेजी का प्रभुत्व स्थापित है। सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। उच्च शिक्षा और रोजगार में भी अंग्रेजी का दबदबा है, जबकि हिंदी काफी पिछड़ी हुई स्थिति में है। साथ ही हमारे देश में अंग्रेजी बोलने वाले को विद्वान समझा जाता है, जबकि हिंदी बोलने वाले को निम्न।
जबकि अंग्रेजी मात्र एक भाषा है, ज्ञान का मानक नहीं। यहां बात अंग्रेजी का विरोध करने की नहीं, बल्कि हिंदी को प्रोत्साहन देने की है, क्योंकि यह हमारी मातृभाषा है। हालांकि पिछले कुछ समय से हिंदी को शिक्षा और रोजगार की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, जिसमे नई शिक्षा नीति के प्रावधान प्रमुख हैं। इसमें बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा/हिंदी में दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा उच्च शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग में भी हिंदी में पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।
शैक्षणिक मनोविज्ञान के शोध और यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार मातृभाषा में सीखना और समझना आसान होता है। जबकि इतर भाषाओं में बच्चे को रटना पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान आदि विकसित देशों में स्कूली और उच्च शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही कराई जाती है। इसलिए वास्तविक तरक्की के लिए हिंदी और स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हिंदी में ज्ञान विज्ञान विषयक लेखन होना चाहिए और शोध कार्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तभी हिंदी रोजगार से जुड़ेगी और अपना सही हक पा सकेगी।
आशू सैनी, शोध छात्र, मुरादाबाद
मनमानी के मंच
आजकल सोशल मीडिया का उपयोग कुछ लोग दुर्भावनाओं को फैलाने के लिए तेजी से कर रहे हैं। आए दिन होने वाली ये बातें जनमानस के मानस पटल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। जानकारियों को तोड़-मरोड़ कर और भ्रामक रूप से फैलाने के कारण लोग इनके उपयोग करने से हिचकने और इस पर संशय करने लगे हैं।
जानकारियों का स्वरूप बदल कर, फोटो-वीडियो का संपादन करके उसे बिगाड़ कर उन्हें भड़काने वाला बनाने का चलन भी बढ़ गया है। इनके कारण देश भर में आए दिन अनेक विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। साइबर अपराध की दिनोंदिन बढ़ती संख्या ने आधुनिक संचार सुविधाओं को संदेह के घेरे की गिरफ्त लेना शुरू कर दिया है।
सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों का उपयोग सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के साथ व्यक्ति, संस्था, समूह और देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध करने मे किया जाए, तब इनकी सार्थकता अधिक नजर आती है। वरना आज यह, आपसी वैमनस्यता और भेदभाव को बढ़ाने में ही ज्यादा सहायक सिद्ध हो रहे हैं।
नरेश कानूनगो, देवास, मप्र
मुद्दे पर पर्दा
हमारे देश की अस्सी फीसदी जनसंख्या मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग से आती है। इसमें करीब आधी जनसंख्या के परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलती है, जहां एक दिन की कमाई उसी दिन राशन-दाल में खर्च हो जाती है और उसमें भी यह मुमकिन या जरूरी नहीं कि हर किसी का पेट भरे। ऐसे में महंगाई का लगातार बढ़ते ही रहना उन मजदूरों और उनके परिवारों के पेट पर सीधा लात मारने जैसा है।
चाहे कितना भी बेमानी मुद्दों का पर्दा डाला जाए, सच यह है कि हमारे देश में खत्म होती आय और बढ़ती महंगाई ही सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। कोई भी पार्टी या नेता महंगाई कम करने के हजारों वादें करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर महंगाई लगातार बढ़ती ही चली आ रही है। महंगाई के संदर्भ में सरकारी या गैर-सरकारी, हर वस्तु और सुविधा के दाम पिछले कुछ वर्षों में बेलगाम बढ़ते जा रहे हैं।
इस साल दूध के दाम पांच बार बढ़ चुके हैं। गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल, राशन-दाल सबके दामों में बढ़ोतरी महसूस की जा सकती है। इसकी वजह से गरीब और गरीब होता जा रहा है और नेता यह साबित नहीं कर पा रहे हैं कि किस आधार पर उनकी संपत्ति में उछाल आ रहा है। नेताओं को यह समझना होगा कि जनता के हित से ही किसी भी देश का कल्याण हो सकता है। देश की जनता के हित के लिए महंगाई पर जल्द से जल्द लगाम लगाना होगा। वरना इसके नतीजों के लिए आखिरकार जिम्मेदार उन्हें ही माना जाएगा।
रोहित पांडेय, नई दिल्ली।
उलटी दिशा
‘तालिबान के राज में’ (संपादकीय, 29 दिसंबर) पढ़ा। हाल ही में तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं को कालेज और विश्वविद्यालय में जाने से रोक दिया था। वहां उच्च शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सारे कालेज और विश्वविद्यालय सरकार के इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करें। अब तालिबान ने महिलाओं को स्वयंसेवी संगठनों और विदेशी सहायता संगठनों में काम करने से रोक दिया।
यह सवाल है कि अगर महिलाओं के प्रति तालिबान का यही रवैया रहा तो अफगानिस्तान का भविष्य कैसा होगा और क्या-क्या मुसीबतें आ सकती हैं। आज अफगानिस्तान की सबसे बड़ी समस्या भुखमरी, कुपोषण और स्वास्थ्य को लेकर है। करीब तीन करोड़ आबादी के पास खाने को नहीं है। विदेशी संगठनों की मदद से खाना और दवाइयां मुहैया करा करवाई जा रही हैं। ऐसे में तालिबान ने महिलाओं के काम पर जाने को लेकर जो पाबंदी लगाई है, उसके भयानक असर देखने को मिलेगा।
सिमरन चौबे, दिल्ली।