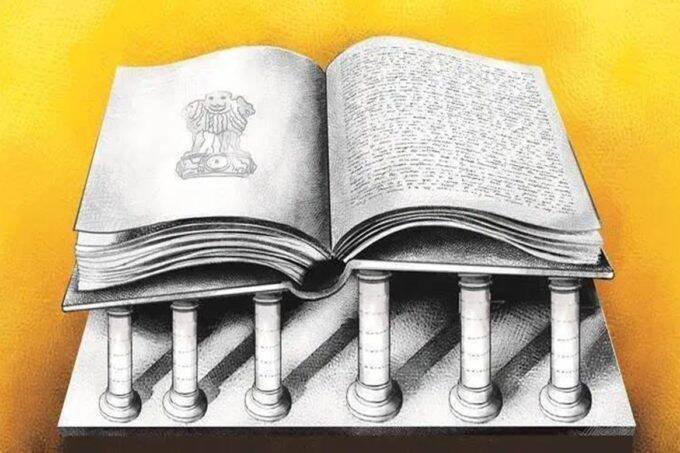राजनीतिक नेतृत्व द्वारा आधारभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति को ही विकास का नाम देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली जाती है। जबकि बदलते दौर में विकास की अवधारणाएं कुछ और ही अर्थ रखती हैं। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय संदर्भों के साथ विकास की अवधारणा को मूर्त रूप दिए जाने की आवश्यकता है। इन संदर्भों में आवश्यकता इस बात की है कि आम नागरिकों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत उन्हें प्राप्त अधिकारों की निर्णायक शक्ति के प्रति जागृत किया जाए। मतदाताओं की परंपरागत दल विशेष के प्रति प्रतिबद्धता जितनी परिवर्तित की जा सकेगी, उतना ही लोकतंत्र परिपक्व हो सकेगा। स्थिर सरकार की जितनी जरूरत है, उतनी ही जरूरत राजनीति में सशक्त विकल्प को लेकर महसूस की जानी चाहिए।
ऐसा होने पर ही राजनीतिकों की निरंकुश मनोवृत्ति पर अंकुश लग सकेगा और राजनीतिक दलों को नीति और नीयत के प्रति जवाबदेह भी बनाया जा सकेगा। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह विचित्र लग सकता है, लेकिन जन-जन के सपनों को साकार करने की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक दल नीति और सिद्धांतों के अनुरूप अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। इसके साथ-साथ प्रतिपक्ष भी सत्तापक्ष से बेहतर कुछ कर गुजरने की तीव्र आतुरता लिए मतदाता के बीच रहेगा। प्रतिस्पर्धा होगी, तीव्र से तीव्रतम होगी और इसके सकारात्मक रूप से आश्चर्यजनक परिणाम सामने आएंगे। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के बीच यह बड़ा विचित्र लगता है। लेकिन एक प्रकार से समान उद्देश्य को लेकर जनहित के प्रति समर्पित राजनीति का सपना संजोए राष्ट्रभक्तों के लिए यह मनमाफिक मुराद को पाने के समकक्ष ही तो होगा। यह सब कुछ संभव है, बशर्ते कि हम राजनीतिक चश्मे को छोड़ कर देश-प्रदेश के हित की ही सोचें। आम नागरिकों के मन में राजनीति के प्रति अविश्वसनीय भाव लोकतंत्र की सार्थकता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
ऐसे में सुधारवादी प्रक्रिया को क्रियान्वित किए जाने की नितांत आवश्यकता है। राजनीतिक दलों को अपने चिंतन में गहराई लानी होगी और ऊंचाई भी। आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति को तिलांजलि देकर स्वस्थ राजनीतिक परंपराओं का सूत्रपात किया जाना चाहिए। नीतियों में पारदर्शिता, आचरण एवं व्यवहार में शुचिता और पवित्रता और सकारात्मक सोच के साथ जनहित के प्रति समर्पित नीतियों की राजनीति को आगे लाना होगा। दरअसल राजनीति के तौर तरीकों में आमूलचूल परिवर्तन समय की मांग है। हमें समय की नब्ज को पहचानना होगा और उसके अनुरूप स्वयं को ढालना होगा। इसके साथ साथ बदलते दौर में परिवर्तित तौर-तरीकों के साथ सकारात्मक राजनीति को प्रतिष्ठापित भी करना होगा।
’राजेंद्र बज, हाटपीपल्या, देवास, मप्र
अनाथ बच्चे
‘एक लाख से ज्यादा भारतीय बच्चे हुए अनाथ’ (समाचार, 22 जुलाई) पढ़ा। इसमें नेशनल इंस्टिट्यूट आॅन ड्रग एब्यूज और नेशनल इंस्टिट्यूट आॅफ हेल्थ के अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी में अपने माता-पिता या अभिभावक को खोने वाले यतीम बच्चों की संख्या भारत में एक लाख से अधिक और अन्य देशों में पंद्रह लाख से अधिक दर्शाया गया है। यह जानकारी महज एक आकड़ा नहीं, बल्कि सरकार तथा अन्य सभी लोगों के लिए एक महत्त्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है, क्योंकि वर्तमान परिवेश अधिक तीव्रता के साथ अपना रंग रूप बदल रहा है और इसमें माता-पिता के अलावा कोई भी ऐसे सगे-संबंधी नहीं होते हैं जो किसी अनाथ बच्चे को अपने पास रख कर उसका पालन पोषण कर सकने में सक्षम हों। खासतौर पर वर्तमान समय में, जब लोग बढ़ती महंगाई में अपना ही भरण-पोषण नहीं कर पा रहे हैं।
ऐसी स्थिति में अनाथ हुए उन लाखों बच्चों के मन-मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने का डर बना हुआ है, क्योंकि माता-पिता के खोने के बाद उन बच्चों की पढ़ाई और उनकी छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है की कई बच्चे अपना भरण-पोषण करने के लिए गलत राह न चुनने को मजबूर हो जाएं। ऐसी परिस्थिति में आवश्यक है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल कर उन यतीम हुए बच्चों की देखभाल और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके लिए सरकार की सर्वप्रथम पहल होनी चाहिए कि वे अनाथ हुए बच्चों की पहचान और विवरण दर्ज करें, बाल संरक्षण योजना के तहत बाल देखभाल केंद्रों के माध्यम से तत्काल बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करें और कई संस्थानों के माध्यम से सहायता के रूप में शिक्षा, चिकित्सा और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। साथ ही आवश्यक है कि उन सभी बच्चों के आसपास का माहौल खुशनुमा रहे, ताकि वे अपने परिवार के सदस्य को खोने के सदमे से जल्द से जल्द उबर सकें और अपना सुनहरा भविष्य बना सकें।
’सिमरन कुमारी, पूर्णिया, बिहार</p>
खोती मासूमियत
इन दिनों बन रहे समाज में बच्चों की स्कूल जाने की उम्र घटती जा रही है। दो-तीन वर्ष के बच्चों पर शिक्षा का बोझ लादा जा रहा है। यह बचपन पर बोझ है, लेकिन आमतौर पर लोग इसकी अनदेखी करते हैं। जबकि इसका प्रमाण इससे अधिक और क्या हो सकता है कि अस्पतालों में आधी से अधिक भीड़ बच्चों की होती है। छोटी-सी उम्र में बच्चो की आखों पर मोटे-मोटे चश्मे लग जाते हैं। विकास और आधुनिकता के नाम पर हमारे चारों ओर जो घेरा बन गया है, वह अभिमन्यु के चक्र की तरह हो गया है, जिसमें प्रवेश तो आसानी से कर सकते हैं, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता हैं।
यहां मुद्दा हमारी बाल पीढ़ी का है, जो खेलने-कूदने की उम्र में भविष्य को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि मानसिक तनाव का शिकार होने लगे हैं। बचपन में ही मासूमियत खो रही है। अब तक तो युवा या वृद्ध होने के बाद ही हम अपने बचपन को याद करते थे। बचपन बहुत अनमोल समय होता है, लेकिन आज के मशीनीकृत जीवन ने इसे क्षतिग्रस्त कर दिया है। बचपन है तो भविष्य है, बालमन की इस बोझिल पढ़ाई से मुक्ति से मुहिम जरूरी है, ताकि हमारी बाल पीढ़ी मुस्कराने से महरूम न हो जाए।
’कल्पना झा, फरीदाबाद, हरियाणा