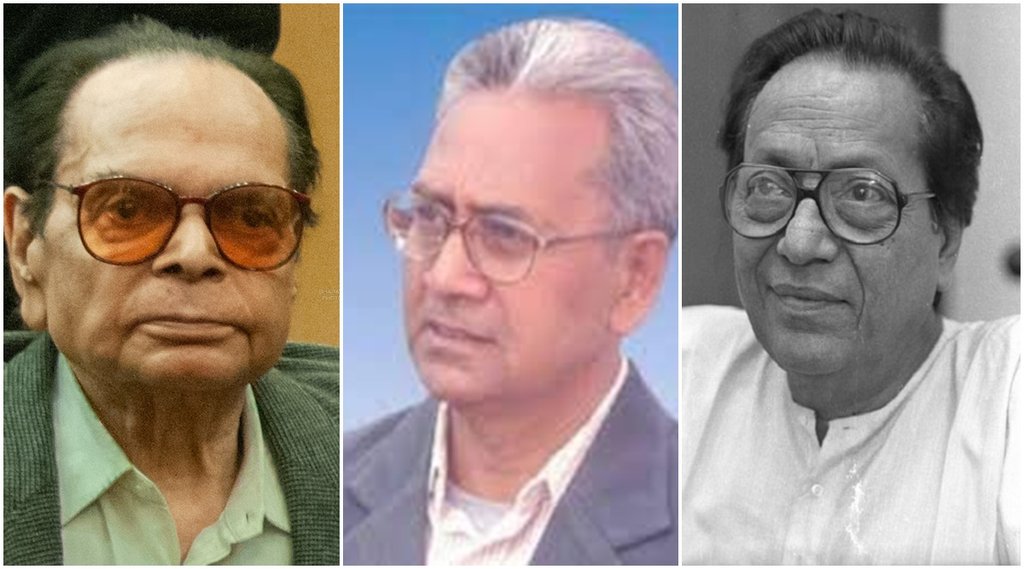राम जन्म पाठक
Literature and Empathy: दलित साहित्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कलावाद, प्रयोगवाद और साहित्य के पुराने मानकों से निपटने की। कलावादियों के अलावा, जनवादी-मार्क्सवादी लेखक और विचारक भी दलित साहित्य के किसी धारा को तब तक अंगीकार करने से इनकार करते रहे, जब तक कि उसने अपनी स्वायत्तता और प्रक्रिया ( प्रोसेस) को खुलकर सामने नहीं रखा। दलित साहित्य के समक्ष बड़ी चुनौती थी अपने साहित्यिक मानदंडों को सुपरिभाषित करने की। ऐसे में मराठी भाषा के लेखक शरण कुमार लिंबाले की मराठी आत्मकथा ” अक्करमाशी” ने जैसे राजमार्ग खोल दिया। यही तो वह नाभि में छिपी कस्तूरी थी, जिसकी तलाश में हिंदी पट्टी के दलित विचारक थे।
राजेंद्र यादव ने विधिवत घोषणा की कि ‘आत्मकथाएं’ ही दलित साहित्य की रीढ़ हैं। ‘अक्करमाशी’ मराठी में पर्याप्त आलोचना झेल चुकी थी। इसकी भाषा को लेकर, इ्सके शीर्षक को लेकर प्रश्न उठाए गए थे। अक्करमाशी का शाब्दिक अर्थ तो होता है ग्यारह माशे का। सोने के एक तोले में बारहमाशा होता है यानी तोले से एक माशा कम। यानी ऐसी चीज, जिसमें कुछ खोट रह गई है। इसका भावात्मक अर्थ ज्यादा नुकीला था। इससे भद्रसाहित्य को चोट पहुंची। ऐसी संतान, जो विवाहित पति-पत्नी से न पैदा हुआ। यह वही महाभारत का सूतपुत्र, जारज संतान था, जिसे इस्लाम में ज्यादा नंगे ढंग से ‘हराम की औलाद’ माना गया। यही वह मानुष था, जो ‘दलित’ था। लिंबाले ने दुखते रग पर हाथ रख दिया था। इसके बाद हिंदी में भी जूठन, अछूत, तिरस्कृत, अपने-अपने पिंजरे, दोहरा अभिशाप प्रभृत आत्मकथाएं सामने आईं।
ये ऐसी (सं)रचनाएं (constructions) थीं, जिससे साहित्य की मुख्यधारा की भृकुटि में तनाव आ गया। लेकिन, बाद में उसने माना कि दलित चिंतन कोई स्वतंत्र धारा तो नहीं, हां एक धारा अवश्य है। दलित साहित्य को हिंदी में अवकाश मिल गय, जो कि अबाध जारी है। दलित साहित्य ने पारंपरिक साहित्य के तत्कालीन विभिन्न स्वरूपों, मसलन, यथार्थवाद, जादुई यथार्थवाद, कलावाद वगैरह को भीषण चुनौती दे दी, फिर भी वह अभी उस बीजरूप को, पुंजीभूत आकुलता को व्यक्त करने की छटपटाहट में था। तभी किसी ‘उदयाचल’ पर वह स्वर्ण-रश्मि चमकी। सुकोमल प्रभात में उन्हें एक शब्द मिला ” स्वानुभूति या स्वानुभूत”। स्वयं महसूसा हुआ या भुगता हुआ यथार्थ या भोगा हुआ यथार्थ।
भुगतने और भोगने में भी अंतर है। इसलिए, कायदे से भुगता हुआ यथार्थ ही लिखना चाहिए। दलित साहित्यिकों ने अपने इस ‘पारस पत्थर’ को उठाया और पारंपरिक साहित्य के शीशे पर दे मारा। इसकी टेक थी –जो भोगेगा, वही लिखेगा, लिख सकेगा। क्योंकि वही प्रामाणिक है। इसने ‘हाई-टावर’ पर चढ़कर यह भी घोषणा कि तुम्हारा साहित्य ‘सहानुभूति’ भर है, कि सहानुभूति से कभी सत्य का निदर्शन संभव नहीं।
यह द्वंद्व हिंदी साहित्य में अब भी जारी है। समय-समय पर रणभेरी बजती रहती है। विश्वविद्यालयों में यह भिड़ंत आचार्यों के बीच विनोदेन या विवादेन चलती रहती है। लेकिन, इस लेखक को इतने लंबे प्रस्तावना की जरूरत इसलिए हुई कि इस प्रश्न से टकराए बगैर आज का लेखक बच ही नहीं सकता।ज्यादा बखेड़ा गाने से अच्छा है कि वह घटना ही आपके सम्मुख रख दूं, जिसे कहने के लिए मैं उतावला हो रहा हूं।
हो सकता है कि उस सहानूभूति बनाम स्वानुभूति के मुकदमे का भी कोई तोड़ निकल आए। स्वानुभूति के तर्क को जो विगलित करना चाहते हैं, वे अक्सर यह प्रश्न करते हैं कि तो क्या वेश्या पर कहानी या कविता लिखने के लिए उन्हें वेश्यागमन करना पड़ेगा। एक आलोचक ने तो यहां तक कह दिया कि क्या आमलेट बनाने के लिए उन्हें मुर्गी बन कर अंडा देना पड़ेगा। इस तरह के तर्क को तर्कशास्त्र में उभयतःपाश कहते हैं। दोनों तरफ से घेराबंदी। ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया ही नहीं जा सकता। सिर्फ नजीर पेश की जा सकती है। मैं जिसे पिछड़े इलाके से आता हूं, वहां आग्नेयास्त्रों की बड़ी महत्ता है। ऐसे शस्त्र लिए तो जाते हैं आत्मरक्षार्थ, लेकिन वे ज्यादातर किसी के भक्षार्थ होते हैं।
तो जब मैं बीसवीं सदी के आखिरी दशक में मुरादाबाद पहुंचा तो जाने कहां से इलाकाई पिछड़ेपन की बंदूक खरीदने की सुषुप्त लालसा जाग्रत हो उठी। मैंने अपने संपादकीय प्रभारी से कहा कि मुझे कंपनी से दस हजार का ऋण दिला दें। उन्होंने पूछा कि क्या करोगे ? मैंने कहा- बंदूक खरीदूंगा। वे हंसे कि अजीब आदमी है यह। उन्होंने कंपनी के निदेशक से बात की और मुझे दस हजार मिल गए। समस्या थी लाइसेंस की। उन दिनों एक अपरजिलाधिकारी थे, जो अक्सर मुझसे कहते थे कि सब कोई न कोई काम लेकर आते हैं, तुम आते हो और चले जाते हो। मैंने कहा कि मुझे कोई जरूरत ही नहीं महसूस होती। भोजन-भजन चल रहा है।
उनके प्रश्नों से आजिज आकर एक दिन मैंने कहा कि गन का लाइसेंस दिला दीजिए। वे बेतहाशा हंसे। क्योंकि, ऐसी उम्मीद तो उन्हें भी नहीं रही होगी। उन्होंने दो-तीन महीने में इधर-उधर से रिपोर्ट मंगाकर, अर्जी भराकर, बिना कोई धनराशि जमा कराए मुझे लाइसेंस दिला दिया। मुझे तो लाइसेंस मिल गया था, लेकिन इस दौरान मैंने उस सरकारी प्रक्रिया की जो दीर्घउत्तरीय प्रश्नमाला देखी, जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा प्रशासन का देखा, जो समाज में ‘स्थापित’ लोगों की दबंगई देखी, जो पस्तहाल आम आदमी देखा, उसे मिलाजुला कर एक कहानी रची– ‘बंदूक’। साहित्य में उसकी जगह कहां है, यह समय तय करेगा।
‘बंदूक’ में बंदूक की कहानी है ही नहीं। वह एक दलित स्त्री की कहानी है, जो समाज के निम्नतम से भी निम्नतम पायदान पर खड़ी है और उसका पति भी उसी तल पर है। दोनों सामाजिक और प्रशासनिक या व्यवस्था की अचल क्रूरता और दमन के मारे हैं। मेरा प्रश्न है कि अगर मैंने बंदूक नहीं खरीदी होती तो क्या ‘बंदूक” लिख सकता था। इसका उत्तर दोनों तरफ से दिया जा सकता है। और नहीं भी।
अगर आपमें पर्याप्त संवेदना है और नजर खुली है तो आप बिना भोगे भी इतना बेहतर लिख सकते हैं, जो भोगनेवाला भी नहीं लिख सकता। वाल्मीकि में वह पर्याप्त संवेदना थी, जो क्रौंच-वध को अनुभव कर सकती थी। वर्ना, तबसे अरबों-खरबों बहेलियों ने न जाने कितने ‘क्रौंचों’ का वध किया होगा, लेकिन उसके बाद फिर कोई वाल्मीकि पैदा नहीं हुआ।
इसके लिए हमारे कवियों ने एक शब्द खोजा है–‘परदुखकातरता।’ अगर आपमें परदुखकातरता है, तो आप एक महान रचयिता होंगे। लेकिन, अगर आप परदुखकातर भी हैं और आपका भोगा हुआ यथार्थ भी है तो शायद बात सोने में सोहागे वाली हो जाएगी। इसी को मणि-कांचन योग कहा गया है। और, अगर, वह नहीं है तो भोग कर भी क्या होगा। फूलहिं-फलहिं न बेंत, जदपि सुधा बरसें जलद। इसे इस तरह से सूत्रबद्ध कर सकते हैं कि सहानुभूति के बिना स्वानुभूति वंध्या है, जबकि स्वानुभूति, सहानुभूति की ‘तीसरी आंख’ है। प्रथमदृष्टया, दोनों विरोधाभासी लगते हैं, मगर हैं जुड़वां।