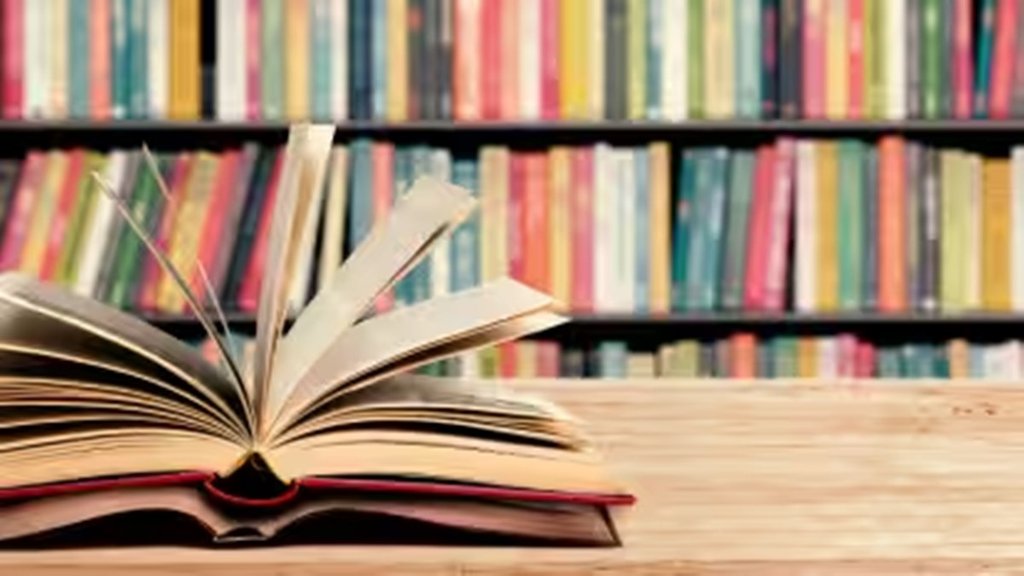शोभा जैन
अपने आसपास हम आजकल कई बार जिस तरह की भाषा से गुजरते हैं, उसे देख कर ऐसा लगता है कि लोगों के भीतर इस मामले में नाहक आक्रामकता बढ़ती दिख रही है। क्या इसे समय के बदलाव के साथ लोकतंत्र में भी भाषा के जायके बदलने के तौर पर देखा जा सकता है? हम जिस समय में जी रहे हैं, वह विश्व बाजारवाद का समय है।
इसमें समय मनुष्य का न होकर मशीनों का है, उपकरणों का है और नई-नई अवधारणाओं का है। हम सूचना के विस्फोट के ऐसे समय में हैं, जहां प्रचार के बड़े माध्यमों का भाषा पर दबदबा है, जिसके चलते आज वह जड़ विहीन और तात्कालिक होती जा रही है। इसे इस रूप में देख सकते हैं कि ‘बोलो और भूल जाओ’! सवाल है कि इस बढ़ती प्रवृत्ति का हासिल क्या होना है, क्या इसका अंदाजा लगाया जा पा रहा है?
भाषा अब कलात्मकता के साथ बनाई जाती है। भवन, भूषा, भोजन सब बदल चुके हैं। पिज्जा आज का भोजन हो गया है तो बर्गर नाश्ता। भाषा के माध्यम से बाजार को विकसित करने की धारणा ने भाषा की शुद्धता और सृजनशीलता को थोड़ा असुरक्षित कर दिया है। भाषा में प्रयोग और नवाचार भाषा को समृद्ध बनाते हैं, लेकिन आज बाजार की सुविधा के लिए गढ़े जाने वाले शब्द जन्म ले रहे हैं। इसे भाषा की अशुद्धि कहें या खिचड़ी, इसमें वंचित जनता की मार्मिक स्थितियों की छवि नहीं दिखाई पड़ती। उनके जीवन के तनाव को नहीं देखा जा सकता।
भाषा की ऐसी गति बुद्धिजीवियों को कैसे शांत रख सकती है? यह स्वाभाविक भी है। सृजन की हर साहित्यिक विधा भाषा की कसौटी पर ही कसी जाती है। अभी तक दुनिया के जितने देश महाशक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, वे अपनी राष्ट्रीय भाषा में बड़े काम करते देखे जा सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और जापान जैसी महाशक्तियां अपनी भाषा अंग्रेजी, फ्रेच या जापानी में ही चिंतन, खोज और काम करते हुए समृद्ध हुए हैं। सिर्फ भारत में कल्पना की जाती है कि यह देश भारतीय भाषाओं और खास कर हिंदी को किनारे रख कर महाशक्ति बन जाएगा। ऐसा लगता है कि भारत में औपनिवेशिक ‘हैंगओवर’ छाया हुआ है।
इसकी एक वजह शायद सांस्कृतिक रूप से आत्मविश्वास की कमी भी है। दूसरी कसर टेलीविजन पूरी कर देता है, जिसमें ऐसी लोकप्रियतावादी चीजें ज्यादा दिखाई जाती हैं, जिनके विज्ञापन से बाजार विकसित हो सके। फिर उसकी भाषा चाहे जो भी हो। केवल माल बेचने और गांव-कस्बों में नए बाजार बनाने के लिए हिंदी का जिस सुविधा के साथ प्रयोग हो रहा है, वह एक तदर्थ और व्यावहारिक उद्देश्य के लिए है, किसी व्यापार आदर्श, राष्ट्र निर्माण या मूलगामी परिवर्तन के लिए नहीं। कारोबार में भी किसी उच्च प्रशासनिक बैठक का वार्तालाप हिंदी में नहीं होता। विज्ञापन एजेंसियों में सारे विज्ञापन पहले अंग्रेजी में बनते हैं, बाद में जैसे-तैसे उनका कामचलाऊ हिंदी में अनुवाद कर दिया जाता है।
भाषा की यह हालत केवल बाजार में नहीं, राजनीति में भी है। जबकि लोकतंत्र में शपथ की भाषा अनुशासन है। अब स्थिति यह है कि भाषा के साम्राज्य में शब्दों की सीमा और अक्षरों की आचार संहिता ने वर्तनी में इन दिनों नए शब्द सर्वमान्य प्रचलित परंपरा बनकर आ गए। या यों भी कहा जा सकता है कि हिंदी के घर में अंग्रेजी के आगत अतिथि के रूप जमात लगाकर बैठे हैं।
इन शाब्दिक अतिथियों को घर से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए आए दिन हिंदी दिवस पर लंबे-लंबे भाषण दिए जाते रहे हैं। देश भर के लगभग सभी महत्त्वपूर्ण संवाद मंचों में ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो’ की तरह ‘अंग्रेजी घर छोड़ो’ के संवादात्मक असफल निवेदन किए जाते रहे हैं। अंग्रेजी के शब्द हिंदी के घर में जिस तरह गैरजरूरी तरीके से भी प्रयोग किए जा रहे हैं, उनके भी अन्य भाषाओं के संपर्क में आकर समृद्ध होने की जगह किसी नकारात्मक और नुकसानदायक संक्रमण का शिकार होने की पूरी आशंका हैं या फिर हिंदी के ही कुछ शब्द ‘भीड़ तंत्र’ का शिकार न हो जाएं।
ऐसा जब हो रहा होता है, तब पता नहीं चलता है। बल्कि कई बार उसे सकारात्मक प्रभाव वाला बता कर पेश किया जाता है। लेकिन बाद में जब उसका असर जमीन पर उतरने लगता है कि और वास्तविक हकदारों को वंचित करने लगता है, तब उसकी हकीकत और चाल का अंदाजा लगता है। भारत की विशाल अल्पशिक्षित और साधनहीन जनता, विशेषकर भावी पीढ़ी अपनी जरूरतों के साधनों की पूर्ति के साथ अपनी दिनचर्या मौज-मस्ती और उपभोग को टेलीविजन पर बाजारीकरण की भाषा के माध्यम से देख रही है। यह वैश्विक बाजार में हिंदी भाषा की कुल भूमिका है। इस पर भाषा वैज्ञानिकों सुभचिंतकों, हिंदी सेवियों के साथ नीति निर्धारकों को भी गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।