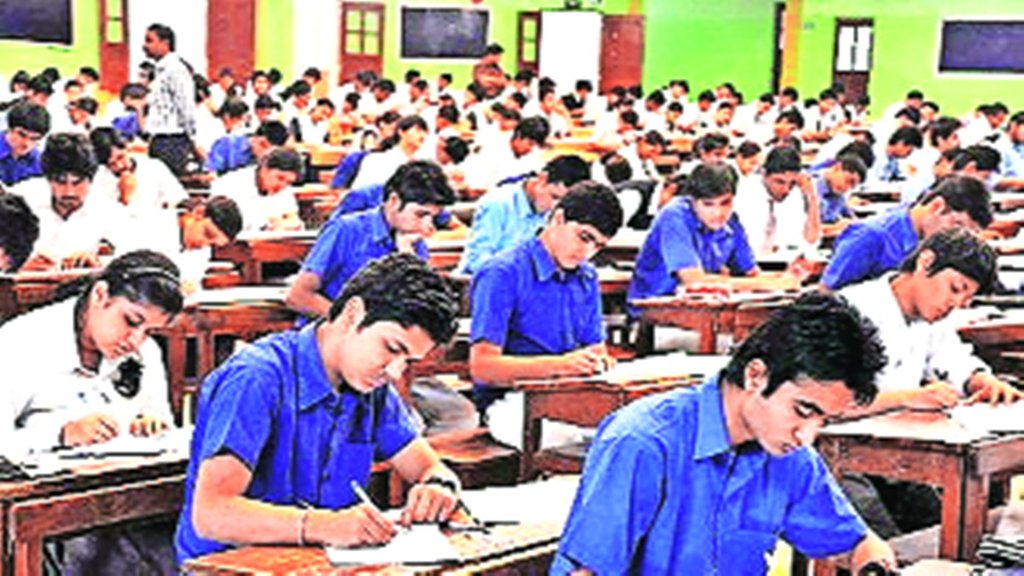इस वर्ष एक बार फिर बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे सुर्खियों में रहे। इसमें अच्छी और सुहानी लगने वाली बातों के समांतर अंकों और ‘रैंक’ को ही जीवन का सब कुछ समझने वाली आज की पीढ़ी के बीच से परीक्षा में असफलता के भय होने, ग्रेड या रैंक कम आने, अपने आपको माता-पिता और शिक्षकों की आशा के अनुरूप खरा साबित न होने पर आत्महत्या किए जाने की खबरें भी आईं। यह निश्चित ही बेहद चिंता का विषय है। परीक्षाओं के नतीजे आने के बाद बच्चों के बीच से आत्महत्या की घटनाएं आमतौर पर हर वर्ष देखने में आती हैं, पर इसका कुछ समाधान अभिभावक, शिक्षक और प्रशासन निकाल नहीं पाते हैं और न ही ऐसी स्थिति बनाई जाती है कि आज के बच्चे इस पर विचार करें कि कामयाबी अगर अच्छा है तो कम अंक या नाकामी खुद को बेहतर करने और अगली कामयाबी का रास्ता है।
बच्चों को यह क्यों नहीं समझाया जा सकता है कि क्या जीवन का लक्ष्य केवल परीक्षा ही पास करना है! अगर अंक कम आ गए या नतीजे खराब रहे तो जीवन तो खत्म नहीं हो जाता। जीवन के मुकाम कुछ और करके भी हासिल किए जा सकते हैं। मगर भविष्य मानो स्कूली परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंकों के दायरे में ही कैद कर दिया जाता है और अभिभावक से लेकर विद्यार्थी तक इसी चक्र में अपना सोचना-समझना केंद्रित कर लेते हैं। इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो सामने आने ही हैं।
देखा जाए तो आज के स्कूली शिक्षा के समूचे ढांचे में पढ़ाई से लेकर परीक्षा और नतीजे के बीच दिखावे की संस्कृति में बच्चों के अभिभावक ही ज्यादा जिम्मेदार नजर आते हैं, जो अपनी अधूरी महत्त्वाकांक्षाओं की भूख की वजह से बच्चों पर दबाव बनाते हैं कि वे नब्बे या सौ फीसद अंक नहीं लाएं। सबसे अव्वल आएं। वहीं स्कूलों में भी बच्चों पर दबाब बनाया जाता है।
ऐसे में स्कूल की कक्षाओं के अलावा ट्यूशन, कोचिंग, परीक्षा के तनाव और बोझ के साथ इंटरनेट, टीवी के चक्रव्यूह में फंसे बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं। जबकि पढ़ाई के बाद बेहतर भविष्य बनाने के लिहाज से देखें तो उसमें अंकों के निर्धारण का कोई आकलन नहीं होता है। बढ़ती महत्त्वाकांक्षा के चलते बच्चे तीन घंटे की परीक्षा में पूरे साल की पढ़ाई का, अपनी योग्यता का सही प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं।
इस स्थिति की जटिलता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कहां एक समूचा व्यक्तित्व बनने के लिए बच्चे अपना जीवन-सफर शुरू करते हैं और फंस जाते हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने और अव्वल लाने की होड़ में। इस होड़ का हासिल यह है कि जिन बच्चों को पढ़ना, खेलना-कूदना और आनंद उठाना था, उनमें से कई पढ़ाई से उपजे तनाव और हताशा के चलते आत्महत्या करने से भी नहीं चूक रहे।
दिखावे के अंको का छलावा बाल मन को लगातार आकर्षित कर रहा हैं। बच्चे बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को ही अपने जीवन की आधारशिला, अंतिम सच, करियर का सब कुछ मान बैठे हैं। जबकि यही अंतिम सच नहीं है। सच यह है कि अंकों का जीवन में कोई मूल्य नहीं हैं, क्योंकि अंकों या डिग्री से किसी की भी योग्यता का सही मूल्याकंन नहीं किया जा सकता।
कितने ही आइएएस, कलेक्टर, खिलाड़ी, अभिनेता, गायक, कारोबारी, कलाकार, लेखक, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि में बेहद साधारण किस्म के विद्यार्थी रहे। वे पढ़ाई में कक्षा में अव्वल दर्जे में नहीं आए, फेल भी हुए, स्नातक, स्नातकोत्तर की डिग्री भी नहीं ली, फिर भी आगे जाकर वे अपने-अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं।
उनसे आज की पीढ़ी सीख ले तो वह भी अंकों से जीवन की हार-जीत को भूल कर करिअर को बनाने में अपनी प्रतिभा, योग्यता और रुचि के अनुसार पढ़ाई के अलावा खेल, गीत-संगीत, पेंटिग, व्यवसाय, अभिनय, किसी दूसरे क्षेत्र में मुकाम हासिल कर सकती है। बच्चों को चाहिए कि वे असफलताओं से भी सीख लें। एक अच्छा और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें।
यह ध्यान रखने की जरूरत है कि लगातार मेहनत, धैर्य, आत्मविश्वास और संकल्प से सफलता हासिल की जा सकती हैं। अगर सफलता न भी मिले तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। दुबारा प्रयास करना चाहिए। बच्चे हंसें, खिलखिलाएं और अर्जुन की तरह लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें, तो कभी न कभी सफलता जरूर हाथ लगेगी। ऐसे तमाम आंकड़े दर्शाते हैं कि आज के बच्चे किस तरह की महत्त्वाकांक्षा के शिकार हो गए हैं।
उनके सपने बड़े हैं और उनके पूरे न होने पर वे मौत को गले लगाने में भी नहीं चूकते! सवाल है कि उनको समाज या स्कूल के स्तर पर इस तरह की सोच को गले लगाने की ‘सीख’ कहां से मिलती है? उनकी समय पर काउसिलिंग कराई जाए, सलाह दी जाए, शिक्षक, परिवार वाले उन्हें कुछ समझाएं तो बच्चे आत्महत्या करने के फैसले तक शायद नहीं पहुंचें।
वहीं संयुक्त परिवारों के विघटन, कामकाजी माता-पिता के व्यस्त जीवन की दिनचर्या से बालमन एकाकी और उपेक्षित होता जा रहा हैं। प्रतिस्पर्धा के दौर में आगे बढ़ने की चाहत में आज अंकों और रैंक का खेल जीवन का खेल बन चुका हैं। इन आत्महत्याओं के बढ़ते ग्राफ का आखिर जिम्मेदार कौन है? आज की शिक्षा प्रणाली, प्रशासन, माता-पिता, सामाजिक परिवेश या आधुनिक संस्कृति। इस पर हमें निश्चित ही गंभीर चिंतन-मनन करना होगा।