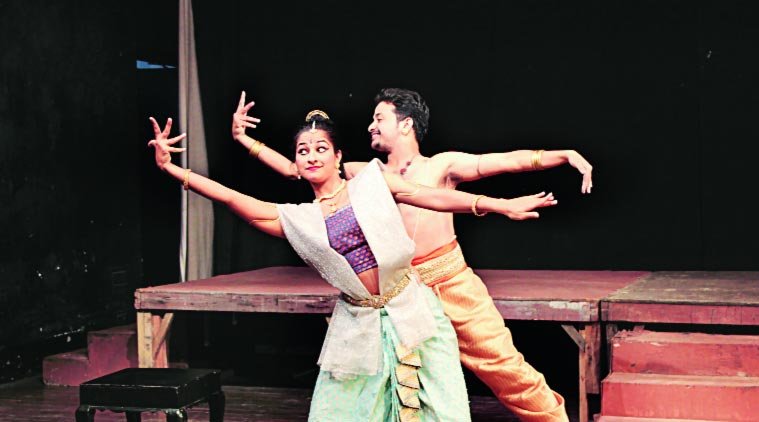पिछले सात-आठ साल से लगातार नाटक देखने या प्रदर्शन वाले परिसरों में जाते रहने के पीछे वजह यह कभी नहीं रही कि मुझे किसी रूप में रंगमंच से जुड़ना था। यह भी नहीं कि मुझे नाटक विधा की महत्ता जैसे किसी विषय पर लेख लिखना था या पीएचडी करनी थी। तब तो मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि ‘नाटक’ को किसी किताब के जरिए पढ़ा भी जाता है। हां, ‘अभिनय एक कला है, जिसे सीखा जाता है’, यह जरूर पता था। बस इतनी-सी वजह है कि मुझे नाटक देखना अच्छा लगता है! यह वजह पर्याप्त होती थी सत्रह-अठारह की उम्र में आज के कुछ सुपर स्टारों की फिल्में देखने के बाद भी उस भीड़ से निकल कर एनएसडी यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तो कभी श्रीराम सेंटर के बाहर लाइन लगाने के लिए। नाटक मेरे लिए एक समांतर दुनिया है। मगर फिल्मों के लिए दोस्तों का झुंड भले मिल जाता हो, पर नाटक के लिए कभी कोई इक्का-दुक्का ही तैयार होता था। मैंने दस में आठ दफे खुद को अकेला पाया। शिकायत बिल्कुल नहीं। अकेले घूमने से मैंने यों भी कभी परहेज नहीं किया। इस मामले में मैं कहीं ज्यादा भावुक हूं। लगातार देखने का फायदा यह हुआ कि नाटक की समझ पैदा हुई। यह समझ मुझे किसी पाठ्य-पुस्तक से नहीं मिली। अब भी वजह वही थी- ‘नाटक देखना अच्छा लगता है।’
नाटक के बाहर की दुनिया में नाटककर्मी फिल्मी सितारों की तरह नहीं हुआ करते। बल्कि नाटक तो उन्हें जीवन बीमा करवाने जितना भी मुहैया नहीं करवाता। यह सच परेशान करता रहा। कई बार सोचती कि कोई सुपर स्टार एक बार शूटिंग करता है, फिल्म बन जाने के बाद उसे दोहराना नहीं पड़ता। वह अभिनय फिर उसकी सारी जिंदगी की कमाई का हिस्सा बन जाता है। रंगकर्मी को कितना कम मिलता है, यह सोच कर तकलीफ होती। जबकि वह एक-एक नाटक को कई-कई बार दुहराता है। नाट्य-विश्लेषण की किताबों में इसे नाट्य विधा की विशेषताओं में शामिल किया जाता है। उसे जीवंत बनाने वाले कर्मियों की जिंदगी अक्सर अभाव और गुमनामी में ही खो जाती है, बशर्ते कि किस्मत उन्हें लंबी रेस में हारने और मरने से रोक ले। नाटक से जुड़ा हर दूसरा नाम नसीरुद्दीन शाह या ओमपुरी नहीं होता।
महिलाओं के बारे में बात की जाए तो दस नाम गिनवाने में ही स्मृति जवाब दे जाती है। सुरेखा सीकरी जैसे नाम गिनवा कर मुक्त हो जाना बहुत आसान है। ऐसे में मेरे नाटक देखने की वजह में ‘अच्छा’ लगने के साथ एक ‘दायित्वबोध’ भी जुड़ गया। इसे मैंने अपने सुखद अनुभवों में गिना है। पिछले साल जब एनएसडी में एक ही दिन में तीन बार दाखिल होते समय तीन बार हाजिरी लगा कर अंदर जाने की वजह दरवाजे पर खड़े गार्ड को बतानी पड़ी, तब लगा कि कुछ बदल रहा है। फिर लगा कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया जा रहा है। एनएसडी इतने सालों से असुरक्षित तो नहीं था! मगर अब शायद फिजां बदल रही है।
इस साल की शुरुआत में चोट की वजह से कुछ नाटक नहीं देख सकी। प्लास्टर उतरने के बाद मैंने एनएसडी की राह ली। अब यहां सब कुछ अलग है। दरवाजे पर ही ‘कहां जाना है, क्यों जाना है, किससे मिलना है’ जैसे कई सवाल पूछे गए। सोचा रजिस्टर पर दस्तखत करके शायद अंदर जाना नसीब होगा, लेकिन बदले में एक मुस्तैद सवाल ने चौंका दिया- ‘क्या आप यहां के स्टूडेंट हैं? आई-कार्ड दिखाएं!’ मैंने कहा- ‘मैं तो कभी यहां की स्टूडेंट नहीं थी! तो क्या अब सिर्फ अंदर वहां के विद्यार्थी ही जा पाएंगे!’ जब उनसे सारे नाटकों और उनकी समय-सारणी के बारे में कुछ जानना चाहा तो जवाब मिला कि ‘बाहर सड़क किनारे बैनर लगा है वहां से देख लो!’ आखिर तक अंदर जाना नसीब नहीं हुआ। बल्कि यह सवाल मिला कि ‘क्या मिल जाएगा अंदर जाकर! फिजूल जिद है!’ इस जवाब ने मेरे उत्साह को मार दिया। एनएसडी के परिसर में वाकई कभी कुछ नहीं था। लेकिन अच्छा लगता था!
मेरे जैसे बहुत हैं जो बिना किसी शर्त अपने जेबखर्च और वक्त का एक हिस्सा यों ही नाटकों की दुनिया पर खर्च करना पसंद करते रहे हैं। अब कितना कर पाएंगे, यह नहीं पता! मैं तो अब भी देख लूंगी, पर नाटक देखना सिर्फ बंद कमरे में एक या दो घंटे का ‘लाइव परफार्मेंस’ देखना भर नहीं होता, बल्कि एक पूरा माहौल होता है, जहां नाटक देखने से पहले किसी एक तस्वीर को देख कर आप रुक जाते हैं। नाटक खत्म होने के बाद बीच सड़क पर ट्रैफिक की आवाज सुनना नाटक देखना नहीं है। बाहर निकल कर किसी कोने में बैठ कर खुद भूल जाना भी नाटक का हिस्सा है। अब सिर्फ कोरे नाटक होंगे! सवाल है कि आने वाले कुछ सालों में अगर दिल्ली में नाटक के चाहने वालों की संख्या में थोड़ी-बहुत भी कमी आए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा!