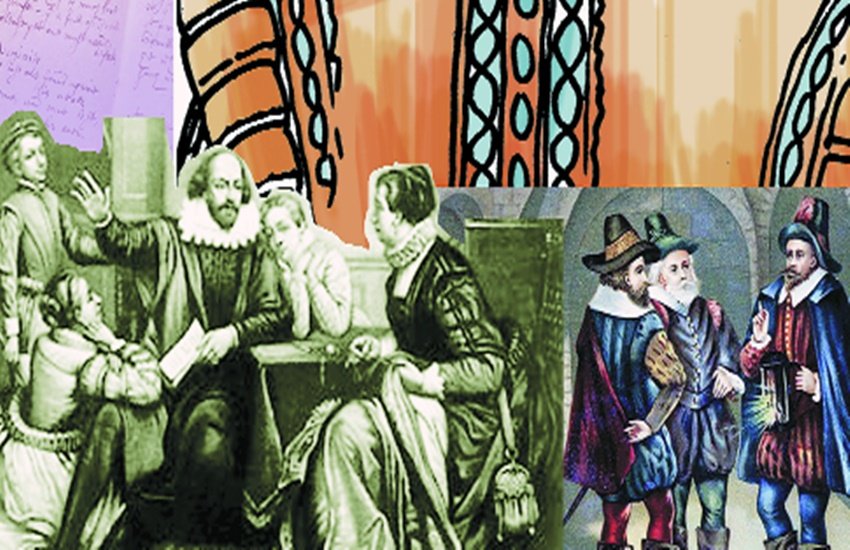शेक्सपियर भले ही अंग्रेजी भाषा के लेखक रहे हों, लेकिन उनकी गणना विश्व के अमर साहित्यकारों में की जाती है। उनके नाटक अपने देश, काल और परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हैं। उनकी रचनाओं में करुणा, पछतावा, आत्मग्लानि, प्रतिशोध आदि प्रवृत्तियां मुखर हैं। उनकी चार सौवीं पुण्यतिथि के अवसर उन्हें याद कर रही हैं अनामिका।
इंग्लैंड में एवन नदी के किनारे बसे जिस छोटे से गांव, स्ट्रैटफोर्ड में शेक्सपियर 26 अप्रैल, 1564 के दिन जनमे थे, वह आज विश्वपर्यटकों का साहित्यिक तीर्थ है! आप सबने बचपन में ‘स्टैचू’ नाम का खेल खेला ही होगा। दौड़ते-भागते कोई अचानक कहे – ‘स्टैचू’ तो आपको उसी तरह मूर्तिवत ‘फ्रीज’ कर जाना होता था – हाथ खड़े हैं तो खड़े ही रहें, एक पांव उठा है तो वहीं उठा-उठा जम जाए! जब आप स्ट्रैटफोर्ड जाएंगे तो आपको लगेगा कि शेक्सपियर के प्रेमियों ने काल-देवता के संग ‘स्टैचू’ खेला है! जम गया है शेक्सपियर का समय! जस का तस! जहां का तहां।
शिकार खेलने के, मुर्गा और बतख जिबह करके टांगने के, सूद के पैसे देने, लौटाने, सौदा-सुलफ करने, गिरजाघर के मोड़ पर ठहरकर रोजमर्रा के दुख-सुख बतियाने और जीवन की विडंबनाएं दर्शाते नाटक खेलने के हजार दृश्य वहां चारों तरफ बोलते हुए से पुतलों में मूर्तिमान हैं।
आज के समय में जो लोकप्रियता दूरदर्शन धारावाहिकों की है, शेक्सपियर के वक्त नाटकों की थी! लोग झुंड बांधकर नाटक देखने जाते थे और नाटकों की प्रिय रेसिपी थी -मृत्यु और विनाश, चुटकुले और भोंडे मजाक, डायनपंथी, राजा और गुंडे-मवाली, नफरत और दिल की जलन, मारपीट-खूनखराबा!
शेक्सपियर के नाटकों में ये सारे मसाले हैं, उनके कथानक भी होलिंशेड क्रॉनिकल आदि लोकप्रिय स्रोतों से आयातित हैं, फिर आखिर क्या है शेक्सपियर में कि पूरी धरती आज शेक्सपियर का गांव है और जहां देखो वहीं शेक्सपियर के पात्र टिमटिमा जाते हैं! किसी दुविधाग्रस्त, संवेदनशील युवक में आपको ‘हैमलेट’ नजर आता है, टांय-टांय फिस्स हुए जाते किसी रोबीले बूढे में ‘किंगलियर’, लगातार व्यर्थ की भर्त्सनाएं सहते-सहते चिड़चिड़े हो चले अल्पसंख्यक में शाइलॉक, समाज के शोषित तबके से श्रमपूर्वक ऊपर उठे हर शंकालु पे्रमी में आॅथेलो, वाक्पटु हर सुंदरी में पोर्शिया, रोजेलिन, बिएट्रिस; वक्तृत्वकला के दम पर झट से पांसा पलट लेने वाले हर वक्ता में मार्क ऐंटनी दिखाई दे जाता है। ऐसा भला क्या विशिष्ट है शेक्सपियर में मुख्यत: दो तत्त्व हैं जो उन्हें महान बनाते हैं : संवादों की चुस्त-चपल, बिंब बहुल भाषा और हर तरह के चरित्रों की मानसिक उथल-पुथल की गहरी पहचान।
‘नेट-सेट’, ‘कैट-मैट’ संघीय लोकसेवा आयोगादि की परीक्षाओं की तैयारी का स्वप्न आंखों में धारे हर साल बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तर-पूर्व से हजारों की तादाद में लड़के-लड़कियां दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते हैं और कहीं-न-कहीं पाठ्यक्रम में शेक्सपियर से उनकी आंखें चार होकर रहती हैं। पर अब यह पुराने जमाने का ‘आंखें चार होना’ नहीं रह गया। एक बार आंखें उठार्इं और झप से गिरा लीं, गिरा क्या लीं, चुरा ही लीं, चुरा क्या लीं, फेर ही लीं! फेरकर कहां टिकार्इं तो कुंजियों पर, ऐसी कुंजियों पर जिनसे कि कोई भी ताला नहीं खुलता। आभास-भर हो जाता है कि यह कथाक्रम है, ये मुख्य चरित्र हैं, ये उनके मुख से उचारी गई पंक्तियों का सार-संक्षेप है।
ऐसा नहीं है कि द्वितीयक स्रोतों या अनुवादों के माध्यम से शेक्सपियर या कालिदास तक आने की तैयारी कोई गर्हित बात है। युद्ध और पे्रम की तरह पठन-पाठन में भी सब जायज है। सब रास्ते जायज हैं पर आधे रास्ते लौट आने से बात नहीं बनती। भाष्य या शब्दार्थ तक ही ठहर जाना दरवाजे पर खड़े रह जाना है। पाठ के अवचेतन में प्रवेश के बिना तो जीवन में वह अंतर्दृष्टि विकसित ही नहीं हो सकती जो पाठ का उद्देश्य होता है और पाठ के अवचेतन में प्रवेश का एक ही माध्यम है हर पात्र, चरित्र की दृष्टि से समग्र पाठ का अंतरंग पारायण- वह भी कई-कई बार और नाटक-कविता आदि के प्रसंग में तो सामूहिक और सस्वर पाठ भी जैसा कि मंचन के दौरान होता है।
बार-बार के घर्षण से काठ की आत्मा में दबी अग्नि भी फूट पड़ती है (स्फुर्लिंग के रूप में) और फिर प्राणवायु देकर उस स्फुर्लिंग को सतत लौ में तब्दील करना होता है। ठीक इसी तरह शेक्सपियरादि के परतदार पाठों के सस्वर सामूहिक पारायण के बिना अर्थाग्नि पूरी समग्रता में कभी जग ही नहीं सकती। जैसे किसी वाद्ययंत्र में कई तरह के राग कीलित होते हैं, किसी कालजयी रचना में कई तरह के अर्थ! आपके मतलब या आपके अपने जीवन-प्रसंग के लिए उपयोगी अर्थ आपके पारायण से ही संभव होगा! अपने विशिष्ट अनुभवों के आलोक में आप शेक्सपियर के संवादों और उसके विशिष्ट पात्रों में सो विशिष्टार्थ जब जगाते हैं तो ही आप उसके पाठ के सह-प्रस्तोता हो सकते हैं। उस पाठ में आपका अपना ‘इनपुट’, उसमें सोई आग सुलगाने वाली आपकी अपनी प्राणवायु वही होगी- जब तक हम यह बात समझ नहीं लेते, शेक्सपियर मध्यकालीन ‘असंभवा’ (इंपॉसिबल शी) की तरह हमें दूर से लुभाते रहेंगे, आत्मा में एवन नदी की तरह रुनझुन बजते हुए बहेंगे नहीं।
फिर भी भला हो अनुवादकों, भाष्यकारों, फिल्मकारों और नाट्य-निर्देशकों का, जिन्होंने शेक्सपियर का आंशिक अवतरण भी जनमानस में संभव किया! ‘शेक्सपियर वाला’ से ‘शेक्सपियर इन लव’ और ‘आेंकारा’ तक शेक्सपियर अलग-अलग अर्थछवियों में आज भी हमारे हैं- एनी बेसेंट और मदर टेरेसा जितने अपने! इनका फिरंगीपन हमें कभी ‘कैलिबन’ वाली दहशत में नहीं डालता। महानता का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि यह अलग-अलग ढंग से ‘अपनी’ लगती है- करीब-करीब मां जितनी अपनी! मां के साथ छेड़छाड़ आम बात है, इसी तर्क से शेक्सपियर के पात्रों, प्रसंगों, संवादों और एकालापों के साथ भारत ही नहीं, दुनिया के अलग-अलग देशों में कई तरह की छेड़छाड़ होती रही। जिस पाठ से अंतर्पाठीय गपशप हो ही नहीं पाए – राजशेखर ने उसे ‘अयोनि’ पाठ कहकर उचित ही धिक्कारा है!
एक उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगी। ‘वेनिस के व्यापारी’ नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ‘मर्चेंट आॅफ वेनिस’ का अनुवाद शुरू किया था। बाद में ‘दुर्लभ बंधु’ नाम से उसका अनुवाद एक दुर्लभ बंधु ने कैसे किया और अनुवाद में ली गई छूटें प्रतीक-रूप में एक अलग स्तर पर समानांतर स्वतंत्रता आंदोलन कैसे रेखांकित करती रहीं, आगे की चर्चा इसी पर।
नस्ली पूर्वग्रह का प्रश्न औपनिवेशिक भारत में भी चर्चा का प्रमुख विषय था। आश्चर्य की बात यह है कि भावानुवाद में भारतेंदु ने यहूदी को जैन बना दिया है। बेचारे जैनी जो जीवाणुओं की भी हत्या नहीं करना चाहते – मानुष-हृदय का एक पौवा लेने की बात कैसे करेंगे! तत्कालीन समाज में वणिकों की प्रमुख स्पर्द्धा जैनियों से थी। वे अधिक सफल व्यापारी सिद्ध हो रहे थे। भारतेंदु व्यापार नहीं करते थे फिर भी बाप-दादाओं का जैन-विद्वेष यहां रंग दिखाता जान पड़ता है। तुर्क या मुसलमान भी बनाया जा सकता था शाइलॉक यानी शैलाक्ष! शैलाक्ष न सही वह शाहनवाज होता, पर इससे हिंदू-मुसलिम विद्वेष को हवा मिलती, हवा मिलती ‘डिवाइड एंड रूल’ को! जैनी अधिक सहिष्णु थे सो तलवार उनके ही गले पड़ी।
मर्चेंट आॅफ वेनिस’ शेक्सपियर के उन दुर्लभ नाटकों में है जहां शेक्सपियर भौगोलिक मानचित्र से एक वास्तविक भूखंड उठाकर अपना नाटक मंचित करते हैं। एलीजाबीदनों के लिए आर्थिक वैभव और सांस्कृतिक रंग-रुतबे का प्रतीक था वेनिस – और वहां सिर चढ़कर बोलता था नस्ली पूर्वग्रह। अंगे्रज भी सौदागर ही थे, वेनिस के नहीं, लंदन के सौदागर ही सही, कॉस्मोपॉलिटन उन्हें भी होना चाहिए था पर वे नाम के ही कॉस्मोपॉलिटन थे, ऐंटोनियो की तरह! यह भी औपनिवेशिक भारत में इसकी लोकप्रियता का एक कारण हो सकता है।
‘पैसा’ इस नाटक का केंद्रीय रूपक है। पे्रम भी आर्थिक लोभ-लिप्सा से मुक्त नहीं! शेक्सपियर अपने नस्ली पूर्वग्रह के बावजूद शेक्सपियर ही थे, खूब खबर ली है उन्होंने उन प्रेमियों की जिनकी एक निगाह पे्रमी-पे्रमिका के मुखकमल पर रहती है तो दूसरी निगाह पैसे पर। जेसिका पे्रमी के पास भागती है तो बाप के पैसों के साथ और शाइलॉक उसके लिए विलाप करता है तो उसकी एक आह उठती है बेटी के लिए, दूसरी अपने पैसों के लिए : दोनों आहें मनोरंजक ढंग से शेक्सपियर नत्थी करते हैं:
‘‘ओ मॉय डॉटर! ओ मॉय ड्वेट्स ! ओ मॉय डॉटर ’’
मूल नाटक में सलानियो सलारिनो से बताता है शाइलॉक का हाल। अनुवाद में इनके नामों में ध्वनिसाम्य कायम रखा गया है: सलारन सलोने से कहता है –
‘ मैंने तो आज तक घबराहट और झुंझलाहट के ऐसे बेजोड़ और विचित्र वाक्य सुने न थे, जैसे वह जैनी कुत्ता सड़क पर बक रहा था :
‘मेरी बेटी। हाय! मेरी अशर्फियां! हाय, मेरी बेटी! हाय! एक आर्य के साथ भाग गई! हाय मेरी आर्य अशर्फियां! न्याय, कानून!’ ‘आर्य’ शब्द का प्रयोग कितना व्यंजक है और कुत्ता जैनी कैसे हो गया, जैनी बेचारे तो शाकाहारी होते हैं इस पर विचारते हुए ‘आवहु सब मिलि रोवहुं भारतवासी’ की इच्छा तीव्रतर होती है।
इसी तरह अंक एक, दृश्य एक में बोसेनियो (अनुवाद का सरल) ओंटोनियो (अनंता) से पोर्शिया के रूप-वैभव का वर्णन कंचन के आलोक में करता है :
‘ हर सनी लॉक्स
हैंग आॅन हर टेंपल्स लाइक ए गोल्डन फ्लीस’
यहां प्रसंगगर्भत्व थोड़ा था – सांस्कृतिक पर्याय जुटाए बिना बात नहीं बन सकती थी, पर ‘सनीलॉक्स’ और ‘गोल्डन फ्लीस’ के बीच जैसा विटी संयोजन अनुवाद में फिर भी हो सकता था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसका एक कारण तो शायद ये ही हमारे यहां कुंतल काले होते हैं, धूप यानी सोने के रंग से कैसे होंगे बिल्वमठ की पुरश्री के केश! वेनिस (बिल्वमठ हो जाता है अनुवाद में, पोर्शिया पुरश्री हो जाती है ध्वनि साम्य फिर से सामने आता है, और विट का विस्तार ‘पुर’ के विस्तार में नियोजित हो जाता है।)
‘उनका नाम पुरश्री है… पुरश्री क्या वह सारे संसार की श्री है! रूप में श्री और गुण में सरस्वती है…’ पोर्शिया बुद्धिमती है किंतु शेक्सपियर का पाठ कहीं उसे मिनर्वा यानी सरस्वती नहीं बताता। यह गुणारोप भारतेंदु की अपनी अपेक्षा है भारतीय ललनाओं से कि वे लक्ष्मी और सरस्वती का शुभमेल धारित करें।
अ ब नस्ली विद्वेष के प्रश्न पर फिर से आते हैं। ऐंटोनियो शाइलॉक से नफरत करता है क्योंकि वह सच्चा क्रिश्चियन है, पैसे को ‘यूजरी’ का साधन वह नहीं बनाता, उसे कहता है अ बीड आॅफ बैरेन मेटल। शाइलॉक को यह उदारता ग्राह्य नहीं है और उसे लगातार याद रहती है यहूदियों की अपमान शृंखला!
यह तो व्यावहारिक कारण हुआ कि आंटोनियो रेट बिगाड़ता है विदेशी मुद्रा से, लेकिन असल कारण नस्ली विद्वेष है, उसके अनुवाद पर थोड़ी चर्चा करती हुई मैं औपनिवेशक अनुवाद के सिद्धांत पर आती हूं।
‘विल बॉय विद् यू, सेल विद् यू, टॉक विद् यू, वॉक विद् यू एंड सो फालोइंग, बट आई नाट ईट विद् यू, विद् यू, नार प्रे विद् यू।’
अपनी विशिष्ट शैली और प्रखर भाषा में वह आगे कहता है :
‘ फेयर सर, यू स्पेट आॅन मी आॅन वेडनेस डे लास्ट, ‘ यू कॉल्ड मी डॉग, एंड फॉर दीज कर्टजीज, आइ विल लेंड यू दिस मच मनी ?’
शेक्सपियर अंत में इसे दरिद्र कर देते हैं, लेकिन भाषाई वैभव शाइलॉक का अंत तक नहीं छिनता, नायक की भाषा से कहीं समृद्ध और चुटीली है खलनायक की भाषा। काव्योचित न्याय का यह भी एक प्रखर पक्ष है।
‘टेल मी वेयर इज फैंसी बे्रड
इन द हार्ट आॅर इन द हेड
हाउ बिगॉट, हाउ नॉरिशड?
रिप्लाई, रिप्लाई
इट इज एनजेंडर्ड इन द आइज
विद गेजिंग फेड; ऐंड फैंसी डाइज,
इन द क्रेडल वेन इट लाइज
लेट अस आॅल रिंग फैंसीज नेल
लेट्स विगिन इट-डिंग डॉंग बेल!’
इसका अनुवाद भारतेंदु ने ब्रजभाषा में किया है क्योंकि उनके अनुसार गान की भाषा खड़ी बोली हो ही नहीं सकती थी और अंग्रेजी का छोटा-सा गीत ब्रजभाषा का विरह गान बन जाता है! कथ्य का पट-परिवर्तन हो जाता है, एक अलग ही तरह का हस्तक्षेप बन जाता है, अनुवाद नहीं रह जाता! अंगे्रजी की सफेद चमड़ी पर ब्रज की पिचकारी एक अलग तरह की भाषिक होली खेलती है। होली खेलना अपने रंग में रंग लेने की एक ठिठोली-भरी रणनीति भी माना जा सकता है। इस तरह की भाषिक होली कई भारतीय अनुवादों ने बेरंग अंगे्रजी पात्रों से खेली। यह एक अलग तरह का सांस्कृतिक प्रतिकार था – अपने रंग ले लेने का, अपने शीशे में उतार लेने का: अब जैसे शाइलॉक प्रसंग का ही अनुवाद देखें तो वह मूल से अधिक विस्तृत और रंगीला है।
‘क्या जैनी की आंख, नाक, हाथ, पांव और दूसरे अंग आर्यों की तरह नहीं होते? क्या उसकी सुधि, सुख और दुख, प्रीति और क्रोध आर्यों की भांति नहीं होता? क्या वह वही अन्न नहीं खाता, उन्हीं शस्त्रों से घायल नहीं होता, वही रोग नहीं झेलता, उन्हीं औषधियों से अच्छा नहीं होता, उसी गर्मी और जाड़े से सुख और कष्ट नहीं उठाता जैसा कि कोई आर्य? क्या तुम चुटकी काटो तो हम लोगों के रुधिर नहीं निकलता? क्या तुम गुदगुदाओ तो हम लोगों को हंसी नहीं आती? क्या यदि तुम विष दो तो हम लोग मर नहीं जाते? तो फिर जो तुम हम पर अत्याचार करोगे तो क्या हम बदला न लेंगे? यदि हम लोग और बातों में तुम्हारे सदृश हैं तो इस बात में भी तुम्हारे तुल्य होंगे। यदि कोई जैनी किसी आर्य को दुख दे तो वह किस भांति अपनी नम्रता प्रकट कर सकता है? बदला लेकर, तो यदि कोई कार्य किसी जैन को क्लेश पहुंचावे तो इसे उसके उदाहरण के अनुसार किस प्रकार से सहन करना चाहिए। अवश्य बदला लेकर। जो पाजीपन तुम लोग मुझे अपने उदाहरण से सिखलाते हो, उसे मैं कर दिखलाऊंगा और कितनी ही कठिनता क्यों न पड़े, मैं बदला लेने में अवश्य तुम से बढ़कर रहूंगा।’
ये और इस तरह के हजार अंत:पाठीय संवाद प्रमाण हैं इस आधारभूत तथ्य का कि भूमंडीकरण सच्चे अर्थों में ‘भूमंडलीकरण’ तभी बन पाएगा जो अनुवादों के रास्ते सांस्कृतिक आदान-प्रदान बराबर के हो और दुनिया के सारे देश वृहत्तर विश्व की कालजयी कृतियों का स्पंदन आत्मा में दर्ज करने को लालायित हो जाएं! तभी एक सार्थक संवाद शुरू होगा पूरब और पश्चिम, गंवई और शहराती, लोक और शास्त्र के बीच! एक अधिक न्यायसम्मत, सरस और सुंदर दुनिया की नींव यही संवाद संभव करेंगे। ये ही उठाएंगे हमें सारी क्षुद्रताओं, कुंठाओं, संकीर्णताओं के ऊपर!
(अनामिका)