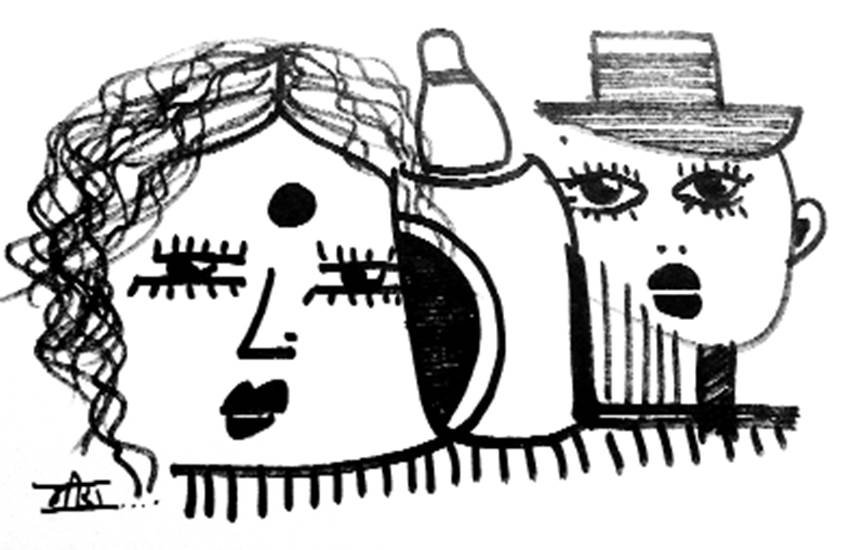सम्मानजनक तरीके से आजीविका कमाने का हक ही ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ सकता है। इसी बात को बल देने वाली एक पहल मुंबई में हुई है। मुंबई विंग्स रेनबो नाम से एक एलजीबीटी (लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर) रेडियो कैब की शुरूआत की गई है। कुछ समय से एलजीबीटी समुदाय को जो कानूनी और सामाजिक अधिकार दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसे उसी की एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। इस कार्यक्रम के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के पांच लोगों को रेडियो कैब चलाना सिखाया जाएगा।
ट्रांसजेंडरों के मानवीय अधिकारों को लेकर भारत ही नहीं दुनिया में लंबे समय से बहस जारी है। भारत में इन दिनों कई उदाहरण सामने आए हैं, जो बताते हैं कि ट्रांसजेंडर समाज की मुख्यधारा में सम्मान और अधिकार हासिल करने के लिए अपने बलबूते अपनी पहचान बना रहे हैं। थर्ड जेंडर को कानून से जो बराबरी का हक मिला है उसे अब सामाजिक स्वीकार्यता भी मिल रही है। चैन्नई की वीके पृथिका जल्द ही देश की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस सब-इंस्पेक्टर बनेंगी। मद्रास हाईकोर्ट ने पृथिका को योग्य उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिससे तमिलनाडु सरकार को उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। पहले पृथिका का आवेदन खारिज कर दिया गया था, क्योंकि पुलिस भर्ती बोर्ड के पास न तो तीसरे लिंग के लिए कोई श्रेणी थी और न ही ट्रांसजेंडरों को लिखित, शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार में किसी तरह का कोई आरक्षण या छूट दी जाती है। अदालत ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश भी दिया है कि वह भर्ती के नियमों में बदलाव करे। ऐसी एक और खबर ने ध्यान खींचा है। ‘द सिक्स पैक बैंड’ संगीत टोली में छह ट्रांसजेंडर गायक हैं। जाने-माने गायक सोनू निगम ने इस बैंड के एक गाने के लिए अपनी आवाज दी है।
दरअसल 2014 में ही उच्चतम न्यायालय ने तीसरे लिंग श्रेणी की मान्यता दी थी। इस फैसले के बाद भारत भी दुनिया के ऐसे इक्के-दुक्के देशों में शामिल हो गया, जहां ट्रांसजेंडरों को यह दर्जा मिला। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकारों से भी वंचित इस तबके लिए यह निर्णय यकीनन मानवीय गरिमा को बहाल करने वाला था।
उच्चत्तम न्यायालय ने ट्रांसजेंडरों को शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में आरक्षण देने की भी बात कही थी। इस फैसले के बाद उन्हें शिक्षा, सामाजिक समानता और काम पाने का पूरा अधिकार है। ऐसे में पृथिका को लेकर दिया गया न्यायालय का यह आदेश भी बहुत मायने रखता है। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश ने सिद्ध किया है कि समाज में हर मनुष्य को अपने जीवन को पूरा-पूरा जीने का अधिकार है। चाहे वह महिला हो, पुरुष हो या थर्ड जेंडर।
2009 में चुनाव आयोग ने ‘अन्य’ की श्रेणी में उन्हें मतदाता पहचान पत्र देना शुरू कर दिया था। भारत में तकरीबन अठाईस हजार मतदाता इस रूप में पंजीकृत हैं। 2011 की जनगणना में इस समुदाय के लोगों की गिनती ‘अन्य’ में की गई थी, जिसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। लेकिन गैरसरकारी संगठनों की माने तो ट्रांसजेंडरों की आबादी पांच लाख तक होने का अनुमान है।
देश में संविधान में कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। लेकिन समाज में हमेशा से हाशिये पर रहे ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक स्वीकार्यता को लेकर आमजन की मानसिकता में आज भी बड़ा बदलाव नहीं आया है। अपनी काबिलियत के बल पर इस समुदाय के लोगों ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसीलिए भेदभाव भरी सोच और नियम उनके आड़े नहीं आने चाहिए। हैदराबाद की शबनम देश की पहली ट्रांसजेंडर एमएलए बनकर एक मिसाल कायम कर चुकी हैं। छत्तीसगढ़ की मधु महापौर बन चुकी हैं। हाल में, पद्मिनी प्रकाश ने अपनी प्रतिभा के बल पर न्यूज एंकर की नौकरी हासिल की। थर्ड जेंडर समुदाय के लिए काम करने वाली कार्यकर्ता पद्मशाली भी कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड से सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर बनीं। तमिलनाडु के मदुरै में जिला पुलिस ने होमगार्ड में भी ट्रांसजेंडरों की भर्तियां की है। तमाम बाधाओं और असमानताओं के बावजूद थर्ड जेंडर के लोगों का यों आगे आना वाकई सराहनीय है।
आत्मगलानि में जी रहे थर्ड जेंडर के लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाना ही उनको सबसे अधिक पीड़ा देता है। इसीलिए कानूनी फैसलों और आदेशों के साथ ही समग्र रूप से पूरे समाज की सोच में बदलाव आना भी जरूरी है। केवल न्यायिक निर्णय इन्हें समाज और कार्यस्थल पर मान और मेहनत का अधिकार नहीं दिला सकते। ऐसे फैसलों से इस समुदाय को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। प्रशासनिक सक्रियता और सामाजिक व्यवहार ट्रांसजेंडरों का सम्मान और हक दोनों बनाए रख सकता है। जिस हिम्मत के साथ इस समुदाय से कई चेहरे आगे आ रहे हैं उनके मनोबल को बनाए रखना समाज की नैतिक जिम्मेदारी भी है।