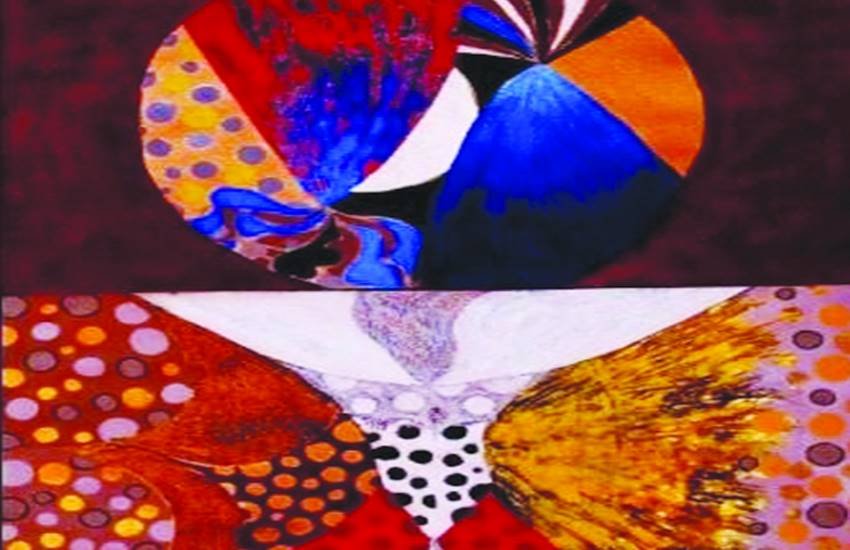रचना का क्या कोई एक परिसर है? अवश्य ही इसका उत्तर ‘नहीं’ में दिया जाएगा। रचना जीवन के वैविध्य, विस्तार और गहराई की अमूर्तता को मूर्त रूप देने की रचनात्मक मानवीय कोशिश है! दुनिया के साहित्य में इसी कारण वैविध्य का विस्तार है। हर बड़ा रचनाकार पिछले रचनाकार के रचना-परिसर का विस्तार करता है। इसी के साथ वह नया परिसर उद्घाटित करने की कोशिश भी करता है। जब न तो जीवन का कोई एक रूप परिभाषित किया जा सका है और न रचना का, तब आलोचना को ही किसी परिभाषा में बांधने की कोशिश क्यों की जाए? उसे किसी एक परिभाषित परिसर तक सीमित क्यों किया जाए। रचना की तरह उसके भी क्या कई परिसर नहीं होने चाहिए। जब ‘दुनिया रोज बनती’ है तब रचना भी रोज बनती है और आलोचना भी। रोज-रोज बनने का यह जो सिलसिला है, वह किसी भी जड़ता और यथास्थिति के विरुद्ध सृजनात्मक पहल से ही संभव होता है।
पिछली सदी का बहुत बड़ा हिस्सा शीतयुद्ध की छाया और उसकी वैचारिक परिणतियों से आक्रांत रहा है। दो शिविरों में बंटी हुई भौगोलिक और वैचारिक दुनिया के आग्रह-दुराग्रह से बने साहित्य और सौंदर्य संबंधी प्रतिमानों की सीमाएं अब उजागर हो चुकी हैं। यथार्थवाद समेत पिछले सभी साहित्यिक प्रतिमानों की सीमाएं जब साफ-साफ नजर आने लगीं, तभी अश्वेत, दलित, अल्पसंख्यक आदि समूहों ने अपने साहित्य के नए परिसर उद्घाटित किए। ऐसे में मूल्यांकन और सौंदर्य के दूसरे आधार और परिसर विकसित हुए। पूंजीवाद और गैरबराबरी के विरुद्ध संघर्ष का एकमात्र आधार जो पहले मार्क्सवाद हुआ करता था, उसके समांतर दूसरे वैचारिक आधार भी अस्तित्व में आए। अपने देश में ही गांधी, आंबेडकर, लोहिया आदि की वैचारिकी ने समाज और साहित्य में प्रतिरोध के नए तौर-तरीके विकसित किए। निश्चित रूप से उनकी आलोचना की दृष्टियां भी नए-नए रूपों में आर्इं। पिछले वर्षों में साहित्य और समाज पर विचार करते हुए जो आलोचना लिखी गई उस पर इनका असर है।
पुराने साहित्यशास्त्र में भी अनेक संप्रदाय रहे हैं, जो बताते हैं कि तब भी साहित्य चिंतन का कोई एक ही परिसर नहीं था, लेकिन उस अनेक में एक आग्रह जो सृजनात्मकता का था, वही प्रमुख था। लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था के अस्तित्व में आने के बाद जन-आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के अनेक-अनेक रूप सामने आए, उनके पीछे सक्रिय दृष्टियां भिन्न थीं। मानव-मुक्ति का सपना सिर्फ जनक्रांति तक न सीमित रह कर भिन्न-भिन्न आंदोलनों-संघर्षों के जरिए प्रकट होने लगा। स्त्री, दलित, आदिवासी, किसान, जल-जंगल, पर्यावरण आदि से जुड़ा कोई भी रेडिकल आंदोलन किसी अब एक ही वैचारिकी से प्रेरित-पोषित नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हुई हैं, उसमें जन भागीदारी बढ़ी है। लोकतंत्र का नियंत्रण अब कुछ समूह या जातियों के हाथ तक सीमित नहीं है। लेकिन इसी के साथ वंचित और सुविधा संपन्न तबके का अंतर भी तेजी से बढ़ा है। इस अंतर को पाटने के लिए जैसा जन-प्रतिरोध होना चाहिए, वैसा नहीं दिखता है। सामूहिक संघर्ष की जगह छोटे-छोटे संघर्ष का यह समय है। देश और दुनिया के विभिन्न अंचलों में चलने वाले छोटे-छोटे आंदोलनों के जरिए प्रतिरोध की नई जमीन और भाषा अस्तित्व में आई है। इसका असर रचना-आलोचना पर पड़ा है। नई रचना-आलोचना की अपनी समस्याएं और चुनौतियां हैं और इन्हीं के बीच से आलोचना के नए-नए औजार भी विकसित हुए हैं।
यों तो साहित्य मात्र लोकतांत्रिक समाज में प्रतिपक्ष की भूमिका में है। अनेक रूपों में वह लोकतंत्र की आलोचना करते हुए उसे समृद्ध करने का काम करता है। लेकिन साहित्य-रूपों में यह काम आलोचना सबसे मूर्त और मुखर रूप में करती है। इस अर्थ में आलोचना लोकतांत्रिक समाज में साहित्य का सतत किंतु रचनात्मक प्रतिपक्ष है। जिस समाज में आलोचना की जगह जितनी अधिक होगी, लोकतंत्र की जड़ें उस समाज में उतनी गहरी होंगी। ठीक इसी तरह जो साहित्य-समाज किसी भी तरह के वैचारिक कठमुल्लेपन और जड़ता से जितना मुक्त होगा, उसमें आलोचना-दृष्टि का विस्तार और विकास उतना अधिक होगा। आलोचना सिर्फ किसी एक परिसर तक सीमित न रह कर समाज के व्यापक दायरे तक जाती है और समाज और साहित्य में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती है। पिछले वर्षों में इन्हीं अर्थों में हिंदी आलोचना नए-नए अर्थ ग्रहण करती हुई विकसित हुई है। आलोचना का एक काम समाज और साहित्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गति देना है।
हमारे युवाकाल का बहुत बड़ा हिस्सा जन-आंदोलनों और जन-संघर्षों के बीच बीता है। उन राजनीतिक झंझावातों के बीच साहित्य के नए अर्थ बनते-खुलते हमने देखे हैं। हमने देखा है कि आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हिंदी कविता की कैसी आंदोलनधर्मी व्याख्या करते थे। वे व्याख्याएं साहित्य के पंडितों की व्याख्याओं से भिन्न और नई होती थीं। एक बार बिहार आंदोलन के दौरान जनता की विशाल भीड़ को देखते हुए वे भाव विह्वल हो गए। उस भाव विह्वल क्षण में उनके मुंह से स्वत: बच्चन की एक काव्य पंक्ति फूट पड़ी- ‘तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण’। इसके आगे वे इसकी व्याख्या करने लगे- ‘ये जन सैलाब, ये लहरें मुझे निमंत्रित कर रही हैं। लोग कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, बीमार हूं, मैं इस आंदोलन का नेतृत्त्व नहीं कर सकता।…’ यह हमारे लिए बच्चन की कविता की नई जनधर्मी व्याख्या थी। बच्चन को हम अब तक हालावाद के कवि के रूप में जानते थे, साहित्य के आलोचक उन्हें ‘शराब’ और ‘कबाब’ का कवि मानते थे। साहित्य के एक आचार्य ने उन्हें ‘आह और वाह’ का कवि कहा था। लेकिन जेपी ने बच्चन की कविता की ऐसी जनधर्मी व्याख्या की, जिससे हम चमत्कृत हो गए। 25 जून, 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक रैली हुई थी, उसका नारा था- ‘सिंहासन खाली करो कि जनता आती है’। यह दिनकर की काव्य पंक्ति थी। उस रैली के लिए जेपी ने स्वयं उस काव्य पंक्ति का चुनाव किया था। इस दौरान हमने यह भी जाना कि जनधर्मिता किसी एक विचारधारा और संगठन तक सीमित नहीं है। उसके अनेक रूप-रंग हैं। इन कारणों से बेहतर भविष्य के लिए देखे गए किसी एक सपने तक सीमित न रह कर दूसरे सपनों की संभावनाओं पर भी एक आलोचक की नजर रहनी चाहिए। और उसे जनधर्मिता के इन रूपों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
बनारसीदास चतुर्वेदी ने पांडेय बेचन शर्मा ‘उग्र’ की एक रचना को अश्लील मान कर उनके विरुद्ध ‘घासलेटी साहित्य’ का अभियान चलाया और गांधीजी से भी अपने अभियान के लिए समर्थन मांगा। गांधीजी ने कुछ महीनों बाद वह रचना पढ़ी और जो पत्र लिखा वह बनारसीदास की धारणा के विपरीत था। गांधी ने उग्र की उस रचना को समाज सुधार के संदर्भ में देखा था। बनारसीदास ने गांधी के उस पत्र को सार्वजनिक नहीं किया। किया होता तो उग्र को जीवनी शक्ति मिली होती। गांधी का वह पत्र बनारसीदास जी के निधन के बाद ही प्रकाशित हो पाया। यहां साहित्य के एक आचार्य और एक जननेता की साहित्य संबंधी समझ का फर्क नजर आता है। सूरदास संबंधी साहित्य-आलोचकों की व्याख्याएं अपनी जगह हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के बाद सूर की नई व्याख्या तो राममनोहर लोहिया के कृष्ण संबंधी लेखों में ही मिलती है, रासलीला का स्त्री-स्वातंत्र्य की दृष्टि से जो नया अर्थ खुलता है, वह साहित्य-आचार्यों की व्याख्या से अलग और नया है। समाजवादी नेता मधुलिमये ने विजयदेव नारायण साही के वैचारिक लेखों के संकलन ‘लोकतंत्र की कसौटियां’ की भूमिका में ‘नेता और प्रणेता’ का सवाल उठाया है। इसका अर्थ यह है कि एक नेता में प्रणेता यानी प्रणयन करने वाले रचनाकार का योग होना चाहिए और एक प्रणेता यानी रचनाकार में एक नेता की सामाजिकता होनी चाहिए। हमारे कई लेखकों में सामाजिक सक्रियता और साहित्यिक रचना का अद्भुत मेल रहा है। रामवृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वरनाथ ‘रेणु’, विजयदेव नारायण साही आदि लेखकों का साहित्य जन-आंदोलनों में उनकी भागीदारी और उससे पैदा हुई चेतना से निर्मित साहित्य है। लेकिन इन लेखकों की जनधर्मिता की हिंदी आलोचना में प्राय: अनदेखी हुई है। राहुल सांकृत्यायन और नागार्जुन को जनधर्मी लेखक के रूप में याद किया जाता है, जो सही है। लेकिन उक्त लेखकों को भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यह साहित्य में जनधर्मी दृष्टि का विस्तार होगा।
मार्क्सवाद या गांधीवाद जैसी बड़ी विचारधाराएं दुनिया की नई व्याख्या प्रस्तुत तो करती ही हैं, उसे बदलने का नया स्वप्न भी देती हैं। उनसे प्रभावित जो जीवन-दृष्टि है वह साहित्य रचना और उसके मूल्यांकन का बड़ा आधार रही है। आधुनिक काल में भारत की साहित्यिक रचनाशीलता पर उनके स्पष्ट प्रभाव देखे जा सकते हैं। लेकिन स्त्री, दलित, आदिवासी, पर्यावरण आदि के संदर्भ में इन वैचारिकियों की सीमाएं पिछले वर्षों में स्पष्ट हुई हैं। स्त्री मुक्ति संबंधी विमर्श के कारण आज मीरां, महादेवी, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि का महत्त्व नए सिरे से उद्घाटित हुआ है। साहित्य के पुराने इतिहास ग्रंथों से भिन्न इनके महत्त्व का शिखर अलग से दिखने लगा है। सुमन राजे जब ‘हिंदी साहित्य का आधा इतिहास’ लिखती हैं, तो यह नई इतिहास-दृष्टि और आलोचना-दृष्टि भी प्रस्तावित करती हैं। साहित्य में जब दलित चेतना का विकास होता है तो रैदास का वही सामाजिक और साहित्यिक अर्थ नहीं रह जाता, जो शुक्ल, द्विवेदी और रामविलास जी के समय में था। अश्वेत साहित्य के कारण साहित्य में सौंदर्य संबंधी नए प्रतिमान बनते हैं और नई सौंदर्य-दृष्टि का विकास होता है। पर्यावरण संबंधी आंदोलनों ने विकास की वर्तमान रफ्तार को चुनौती दी है। उन आंदोलनों से प्रसूत जो साहित्य और आलोचना-दृष्टि है उससे हमारे समय की नई रचनाशीलता और उसे देखने वाली आलोचना-दृष्टि में परिवर्तन आया है। वीरेंद्र जैन के ‘डूब’ जैसे उपन्यास को अगर प्रसंशा मिली है तो यह हमारे भिन्न आलोचना-परिसर का ही प्रमाण है।
तेजी से बदलते समय में जो साहित्य लिखा जा रहा है उसके अर्थ और मूल्य की खोज आलोचना के किसी पुराने परिसर तक सीमित रह कर नहीं की जा सकती। किसी रचना में रचनाकार के मूल आशय की खोज और उसके परे जाकर उसकी समीक्षा के जरिए एक नई रचना को उपलब्ध करना आलोचना का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इस क्रम में रचना के सामाजिक अर्थ और साहित्य-सौंदर्य का जो झिलमिल-सा पर्दा है उसको थोड़ा सरका कर, ओट में चुपचाप खड़ा जो सच एवं कला है, उसे थोड़ी मुखरता देने के लिए आलोचना के नए और भिन्न परिसर की दरकार होती है। यह सुखद है कि इस दृष्टि से हिंदी आलोचना के नए परिसर उद्घाटित हो रहे हैं।