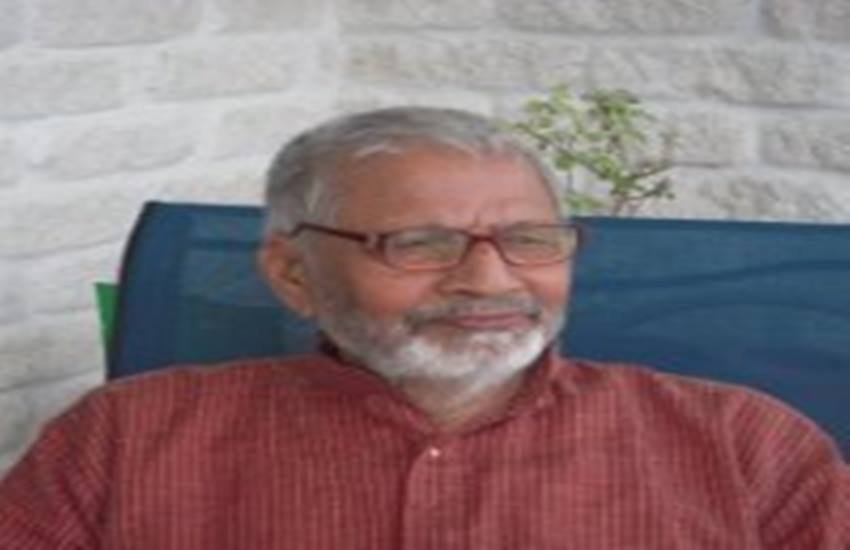अवनिजेश अवस्थी
अ पने-अपने राम’ जैसे उपन्यास से ख्यात भगवान सिंह की ‘किताबघर’ से नई किताब ‘इतिहास का वर्तमान’ आई है। वे मार्क्सवाद से प्रभावित रहे हैं- लेकिन मार्क्सवाद और मार्क्सवादियों से अपने मोहभंग को भी छिपाते नहीं हैं। पिछले दिनों दादरी में हुई घटना के बाद जिस प्रकार से सम्मान, पुरस्कार वापसी का अभियान शुरू हुआ उसी दौर में उन्होंने अपनी टिप्पणियां लिखनी शुरू कीं, जो कि पुस्तक में संकलित हैं। अपात् काल में भवानीप्रसाद मिश्र ने अपना विरोध प्रतिदिन तीन कविताएं लिखकर किया था, जिसे उन्होंने ‘त्रिकाल संध्याह्ण का नाम दिया था, लगभग उसी प्रकार भगवान सिंह ने पांच अक्तूबर 2015 से तीस दिसंबर 2015 तक नित्यप्रति तमाम मुद्दों पर जम कर बहस की । मंच था ‘सोशल मीडिया’- ‘सीधे फेसबुक पर पाठकों की प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करते हुए पुस्तक लिखने का यह शायद पहला प्रयोग हो। मित्रों ने जिस मुक्त भाव से स्वागत किया और अपनी उदार टिप्पणियों से मेरा उत्साहवर्द्धन किया वह मेरे लिए भी अविश्वसनीय था।’ इन टिप्पणियों में भगवान सिंह ने ‘डेविल्स एडवोकेट’ की भूमिका निभाते हुए उन सभी प्रश्नों-मुद्दों को विस्तार से उठाया, जिसे वामपंथी लेखक लगातार रटते रहे हैं, और फिर उन्हीं प्रश्नों के उत्तर भी पूरी संजीदगी से तर्कों-उदाहरणों से दिए हैं।
इस पूरे प्रकरण में शायद ही कोई ऐसा प्रश्न छूटा हो जो अब तक मार्क्सवादी विचारक उठाते रहे हैं। लेखक मार्क्स, एंगेल्स, हीगेल, नीत्शे को साथ-साथ उद्धृत भी करता चलता है, ताकि प्रमाणों में कहीं किसी तरह के संशय की गुंजाइश न रह जाए। पिछले कई दशकों से लेखक स्वयं मार्क्सवादी होने के कारण उस भाषा और मुहावरे को अंदर से जानता है जिसमें वामपंथी ‘बुद्धिजीवी’ बहस करते हैं, इसलिए यह समूची बहस बड़ी रोचक भी बन पड़ी है और एकदम वेधक भी- सीधे-सीधे जवाब। 1930 के दशक से ही साहित्य में वामपंथी विचार का दबदबा रहा है, इसलिए अज्ञेय को अपवाद मान छोड़ दें तो वामपंथ की पूंछ पकड़े बिना शायद ही कोई रचनाकार साहित्यिक भवसागर की वैतरणी को पार कर सका हो। लेकिन इस साहित्य के ‘यथार्थह्ण की असलियत जब भगवान सिंह उघाड़ते हैं तो काफी कुछ साफ हो जाता है- ‘जिसे हम अपना साहित्य कहते हैं वह हमारी भाषा में उनका साहित्य है। उनका साहित्य भी नहीं उनका साहित्य लिखने की कोशिश मात्र है, जो न हमारे लोगों के काम का है, न उनके। हां, अगर उसमें इस बात का चित्रण है कि हम कितने गर्हित हैं, तो इस पर वे तालियां बजाना नहीं भूलते। इसे हमारे लेखक दाद समझ लेते हैं और अपना जीवन सार्थक मान लेते हैं। हमने औपनिवेशिक मानसिकता के कारण अग्रणी देशों जैसा बनने की कोशिश में उनकी नकल की।’
कहा तो यह जाता रहा है कि साहित्य, राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत रही। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद तमाम ‘क्रांतिकारी बुद्धिजीवी’ सत्ता के पिछलग्गू बने रहे, सत्ता का ‘आशीर्वाद’ पाने की आकांक्षा में याचक बने रहे और सत्ता द्वारा पुरस्कृत सम्मानित होकर ‘बड़े साहित्यकार’ बनते रहे। साहित्य के ‘समाजशास्त्र’ और समाज के प्रति उत्तरदायी या ‘सामाजिक सरोकारों’ की बात तो खूब कही गई, लेकिन जैसे राजनीतिक नारों से न समाज का कुछ भला हुआ, न गरीबी हटी। वैसे ही इस साहित्य से समाज में कुछ बदला नहीं। लेखक की सफलता की कसौटी जो उसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से तय होनी थी वह पुरस्कारों से ही होने लगी- ‘मैं उस व्याधि को समझा रहा था जिसके चलते लिखा बहुत कुछ जा रहा है पर समझ तक नहीं पहुंच रहा है और लेखक पुरस्कारों को पाने और खोने को, अनूदित होने और न होने को लेखकीय सफलता की कसौटी मानने लगे हैं।
हमें अपने पुराने कलारूपों में आज की चुनौतियों के अनुसार कुछ निखार लाना था और इस दिशा में प्रयोग करते हुए एक नया सौंदर्यशास्त्र विकसित करना था, वह नहीं किया। राजनीति करने लगे। राजनीतिक घटियापन को साहित्यिक चुनौतियों से अधिक प्राथमिकता देने लगे’- भगवान सिंह जब यह सवाल उठाते हैं तो वे सीधे-सीधे प्रहार करते हैं, कोई लच्छेदार भाषा या लक्षणा-व्यंजना में बात नहीं करते, ‘अभिधा का सौंदर्य’ बताने वालों से अभिधा में ही बात करते हैं- ‘इसीलिए लंबे समय तक इसमें दो तत्त्व हावी रहे, एक विदेशी परामर्श, विदेशों पर निर्भरता और दूसरे किसी न किसी तरह व्यापक जनाधार की तलाश, जो विदेशी भाषा, सामंती जीवन शैली और बौद्धिक स्नॉबरी में रहते संभव ही न थी।’
भगवान सिंह जब यह कहते हैं, ‘इसी बीच किसी ‘दूरदर्शी’ ने यह सुझा दिया कि यदि द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान लिया जाए तो पूरा मुसलिम जनमत हमारे साथ आ जाएगा और एक झटके में व्यापक जनाधार मिल जाएगा। इसे लपक लिया गया और इसके परिणामस्वरूप मुसलिम लीग की सोच का प्रवेश कम्युनिस्ट पार्टी में हुआ’ तो इसका जवाब आज भी किसी कम्युनिस्टि नेता के पास नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी की सोच केवल लीग में समर्थन तक ही सीमित नहीं रही बल्कि इससे भी आगे विभाजन के समय जो रक्तपात हुआ उसके संदर्भ में भी कम्युनिस्ट नेता डांगे का जो उत्तर था उसे राज थापर के माध्यम से उद्धृत करते हैं कि कम्युनिस्ट नेता डांगे यह कहने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाए कि इस रक्तपात और हिंसा से ही क्रांति का आना सरल होगा – ‘तो यह थी तुम्हारी क्रांति की समझ और यह था मानवीय संवेदना का रूप। यह था देशप्रेम और पीड़ितों-दुखियारों का पक्ष। डांगे के ही कार्यकाल में आपात-काल आया था और उन्होंने ही उसका समर्थन किया था।’
इतिहास, ‘इतिहास-बोध’ और ‘इतिहास-दृष्टि’ भी ऐसे ही पद हैं जो स्वातंत्र्योत्तर बौद्धिक विमर्श में बार-बार इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। इतिहास और विशेष रूप से भारतीय इतिहास तमाम बहसों-मुबाहिसों और सहमति-असहमतियों का केंद्र बिंदु रहा है। अलीगढ़ स्कूल के इतिहासकारों ने बाकी इतिहासकारों के इतिहास दृष्टि को पुनरुत्थानवादी और भाववादी बता कर नए इतिहास-लेखक की जरूरत बताई। इतिहास में तथ्यों की बजाय उसकी व्याख्या पर जोर दिया गया और तटस्थता की जगह दृष्टि का महत्त्व हो गया। भगवान सिंह ने भारतीय और मानव सभ्यता का गहन अध्ययन किया है इससे कोई असहमत नहीं हो सकता लेकिन जब-जब उन जैसे इतिहास के अध्येताओं ने इतिहास की खोज-पड़ताल की है तब-तब उन पर ‘पेशेवर’ इतिहासकार न होने की बात कह कर उनकी मान्यताओं और खोजों को अमान्य कह कर खारिज करने का प्रयास किया गया। १