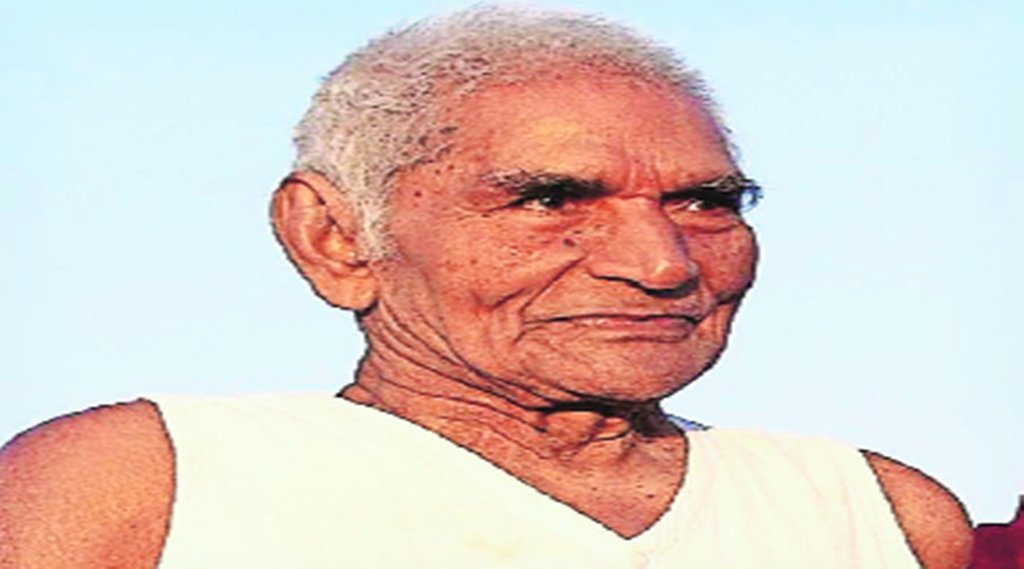भारतीय समाज-रचना के केंद्र में संवेदना की तात्विकता और केंद्रीयता की शिनाख्त को आज समाज विज्ञान के अध्येता नए सिरे से रेखांकित कर रहे हैं। इस रेखांकन के साथ हम देश में सामाजिक आंदोलनों के बारे में जब जानते-पढ़ते हैं, तो हम एक नई और भिन्न समझ की जमीन पर खड़े होकर अपनी सामाजिकता को परख रहे होते हैं। स्वाधीनता संघर्ष को अहिंसक निकष पर कसते हुए महात्मा गांधी ने रचनात्मक मूल्यों और कार्यों को अगर बराबर की अहमियत दी तो वह भारतीय समाज और लोक परंपरा के साथ यकीनी जुड़ाव के कारण ही।
अच्छी बात यह कि यह जुड़ाव उनके बाद भी कायम रहा, यह यकीन उनके बाद भी बहाल रहा। दिलचस्प यह कि महाराष्ट्र के जिस वर्धा में चले गांधी के सेवाग्राम और विनोबा के पवनार के प्रयोग को जिस शख्स ने और करीब लाया, उसने उस जगह से कुछ ही दूरी पर अपनी प्रयोगस्थली बनाई और अतीत से निकलकर समकाल की चिंताओं के बीच करुणा और संवेदना की बात करता रहा। दरअसल, हम बात कर रहे हैं बाबा आमटे की। कुष्ठ रोगियों के लिए सेवाभाव के साथ उन्होंने एक संवेदना-विरोधी दौर में मानवीय मर्यादाओं की दरकारों को नए पुरुषार्थ की शक्ल दी।
महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगनघाट में समाजसेवी बाबा आमटे का जन्म 26 दिसंबर, 1914 को एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता देवीदास आमटे ब्रितानी दौर के भारत में एक शक्तिशाली नौकरशाह और जिले के धनी जमींदार थे। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। बाबा आमटे को बचपन से ही बहुत प्यार मिला, खासकर अपने पिता से।
इसी लाड में माता-पिता व परिवार के अन्य सदस्य उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे। संपन्नता के बीच जीवन में अभाव तो खैर कोई नहीं ही था, कई असमान्य शौक भी उनके पूरे हुए। मसलन उस समय उनके पास अपनी बंदूक तक थी। उच्च शिक्षा उन्होंने विधिशास्त्र में पूरी की। रुतबे वाले परिवार से आने के कारण उनके पास काम की कभी कमी नहीं रही। उन्होंने अपने पैतृक शहर में वकालत की और काफी सफल वकील बने।
1946 में उनकी शादी साधना गुलशास्त्री से हुई। दोनों पति-पत्नी के साथ एक सामान्य बात यह थी कि दोनों की दिलचस्पी सामाजिक कार्यों के प्रति थी। आमटे महात्मा गांधी और विनोबा भावे से बहुत प्रभावित थे। आमटे ने उनके देश के गांवों में अभावों में जीने वाले लोगों की असली समस्याओं को समझने की कोशिश की। वे देश के स्वाधीनता संघर्ष में भी शरीक हुए। कई बार जेल भी गए। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो आमटे ने पूरे देश में जेल में डाले गए नेताओं का मुकदमा लड़ने के लिए वकीलों को संगठित किया।
इसी दौरान उनके जीवन ने तब नई दिशा ली जब उन्होंने एक कुष्ठरोगी को देखा। इसके बाद वे वकालत छोड़ पूरी तरह समाज सेवा से जुड़ गए। उन्होंने कुष्ठ रोगियों के बारे में जानकारी जुटाई और वर्धा से कुछ दूर वरोडा (चंद्रपुर) में आनंदवन नाम से एक आश्रम स्थापित किया। आमटे ने आनंदवन के अलावा और भी कई केंद्र और संस्थाएं कुष्ठरोगियों की सेवा के लिए बनाए।
उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 1985 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और 1988 में असम से गुजरात तक दो बार ‘भारत जोड़ो’ आंदोलन चलाया। नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर बांध निर्माण और इसके कारण हजारों आदिवासियों के विस्थापन का विरोध करने के लिए 1989 में बाबा आमटे ने बांध बनने से डूब जाने वाले क्षेत्र में ‘निजी बल’ (आंतरिक बल) नामक छोटा आश्रम बनाया। उन्होंने अपनी संवेदना को कविताई में पिरोते हुए साहित्य के क्षेत्र में भी नया प्रयोग किया। आमटे को 1971 में पद्मश्री, 1986 में पद्म विभूषण और 1988 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला था।