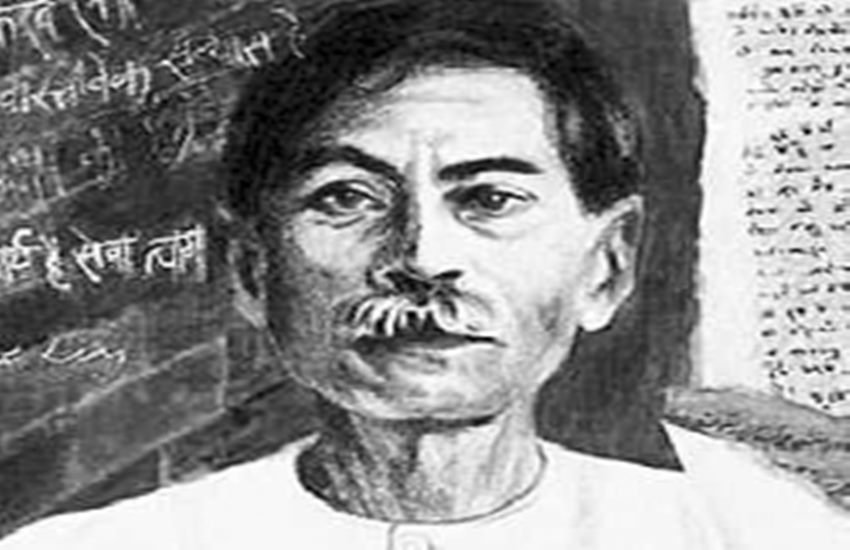प्रेमचंद साहित्य के गंभीर अध्येता कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद के जीवन काल में प्रकाशित ‘गोदान’ के प्रथम संस्करण को प्रकाशित करा कर एक बड़ा काम किया है। ‘गोदान’ का प्रथम संस्करण ‘सरस्वती प्रेस’ बनारस और नाथूराम प्रेमी की प्रकाशन संस्था ‘हिंदी ग्रंथ-रत्नाकर कार्यालय’ बंबई के संयुक्त प्रकाशन में दस जून 1936 को प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद ने जनवरी-फरवरी 1932 में गोदान लिखना शुरू किया था, जो लगभग चार साल बाद 1936 में पूरा हुआ। प्रेमचंद की जीवनकाल में प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘प्रेमचंद की उपन्यास कला’ में जनार्दन प्रसाद झा ‘द्विज’ ने लिखा है कि प्रेमचंद ने इसका नाम ‘गौ-दान’ रखा था, पर मेरे कहने से ‘गौ’ के स्थान पर ‘गो’ यानी ‘गो-दान’ कर दिया था।
‘गो-दान’ प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास के प्रकाशन के बाद वे मुश्किल से चार महीने जीवित रहे। उनके जीवनकाल में इसका दूसरा संस्करण नहीं आया था। बाद के वर्षों में ‘गो-दान’ के कई संस्करण निकले। कॉपीराइट से मुक्त होने के बाद आज कई प्रकाशक ‘गो-दान’ को छाप रहे हैं। यह अपने आप में कम आश्चर्य नहीं है कि ‘गो-दान’ के संस्करण-दर-संस्करण निकले और आज भी निकल रहे हैं, पर किसी प्रकाशक ने ‘गो-दान’ के मूल पाठ से नए संस्करणों को जांचने का प्रयास नहीं किया। गोयनका बताते हैं कि ‘गो-दान’ के पाठ में प्रेमचंद के पुत्रों के प्रकाशन काल में ही परिवर्तन आना शुरू हो गया था। सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित ‘गो-दान’ के 1972 के संस्करण और उसके प्रथम संस्करण के पाठों को मिला कर गोयनका ने बताया है कि 1972 के संस्करण में कई तरह के परिवर्तन हुए हैं।
हालांकि अधिकतर परिवर्तन कंपोजीटर और प्रूफरीडर की लापरवाही के कारण हुए हैं। इधर के संस्करणों में तो अब ‘गो-दान’ की जगह ‘गोदान’ ही छप रहा है। मूल ‘गो-दान’ की तुलना में ‘गोदान’ अधिक प्रचलित हो गया है। ‘गो-दान’ का ‘गोदान’ या ‘ये’ का ‘ए’ हो जाना या विरामचिह्नों में परिवर्तन कोई ऐसी भूल नहीं है, जिससे ‘गो-दान’ का पाठ बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है। गोयनका ने खुद स्वीकार किया है कि ‘‘गो-दान’ के साधारण पाठक के लिए इस पाठांतर का कोई महत्त्व नहीं है और न उपन्यास को पढ़ने में उसे कोई बाधा या अवरोध की अनुभूति हो सकती है।’’ पर यह बात सत्य है कि ‘गो-दान’ हिंदी उपन्यास का शिखर और गौरव है। वह श्रेष्ठ भारतीय उपन्यासों में से एक है। क्लासिक का दर्जा पा चुके इस उपन्यास को मूल रूप में संरक्षित करना हमारा अनिवार्य साहित्यिक दायित्व है।
‘गो-दान’ के मूल पाठ के सामने आ जाने से पाठकों और अध्येताओं के लिए भिन्न-भिन्न संस्करणों में हो रहे परिवर्तनों को चिह्नित करना आसान हो जाएगा। इस लिहाज से ‘गो-दान’ के प्रथम संस्करण के प्रकाशन का ऐतिहासिक महत्त्व है। अब आने वाली पीढ़ियों के लिए ‘गो-दान’ के मूल रूप को, खासकर उसकी भाषिक संरचना को बरकरार रखना संभव हो पाएगा।
‘गो-दान’ की मूल पांडुलिपि के दो ड्राफ्ट आज भी सुरक्षित हैं। पहले ड्राफ्ट में अंगरेजी में लिखी हुई बारह बिंदुओं की एक रूपरेखा मिलती है। यह एक तरह से ‘गो-दान’ का सार-संकेत (सिनॉप्सिस) है। इससे पता चलता है कि प्रेमचंद किसी रचना को लिखने से पहले उसका अंगरेजी में एक रूपरेखा तैयार कर लेते थे। ‘गो-दान’ की इस आरंभिक रूपरेखा को ‘गो-दान’ से मिलाने के बाद यह भी स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद रचना-कर्म के दौरान उस रूपरेखा में अपेक्षित बदलाव भी करते थे। यहां इस बात को भी रेखांकित करना आवश्यक है कि प्रेमचंद अपनी उर्दू-हिंदी की रचनाओं की रूपरेखा या सार-संकेत अंगरेजी में ही बनाते थे।
यानी, वे अपनी रचनाओं की विषय-वस्तु की कल्पना अंगरेजी में ही किया करते थे। उनकी रचनाओं की पांडुलिपि के साथ मिले अंगरेजी की रूपरेखा के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि उर्दू-हिंदी के इस महान लेखक के विचार का माध्यम हिंदी या उर्दू न होकर अंगरेजी थी।
प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ कर भले ही यह विश्वास करना मुश्किल हो कि वे मूल रूप से अंगरेजी में सोचते थे, पर अंगरेजी में तैयार रूपरेखा इसी सत्य को उद्घाटित करती है। अंगरेजी में रूपरेखा का संबंध सिर्फ ‘गो-दान’ से संबंधित नहीं है, बल्कि उनकी दूसरी रचनाओं- उपन्यासों और कहानियों- की पांडुलिपि में भी प्राय: अंगरेजी में ही रूपरेखा मिलती है। प्रेमचंद मूल रूप से अंगरेजी में ही सोचते-विचारते थे, यह बात उनकी रचनाओं की मूल पांडुलिपियों से बहुत स्पष्ट हो जाती है। प्रेमचंद से संबंधित इस सत्य पर हमें परदा नहीं डालना चाहिए। गोयनका भले ही इस सत्य को सामने लाना न चाहें, पर जब तथ्य प्रकाश में आ जाते हैं तो वे अनुसंधानकर्ता की इच्छा से स्वतंत्र हो जाते हैं।
एक बड़ा प्रश्न यह है कि अपनी रचनाओं की एक मुकम्मल रूपरेखा तैयार कर लेने के बाद भी प्रेमचंद को लिखते समय उस आरंभिक रूपरेखा में कई परिवर्तन क्यों करने पड़ते थे, इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है कि प्रेमचंद सृजन-कर्म के दौरान प्रेमचंद किसी पूर्व रूपरेखा की जगह रचना की स्वाभाविक परिणति को अधिक तरजीह देते थे। शायद यही कारण है कि वे एक महान रचनाकार बन सके और उनकी रचनाएं अपार लोकप्रियता के साथ साहित्यिक श्रेष्ठता के उच्च मानदंड पर भी खरी उतरती हैं।
प्रेमचंद आरंभिक रूपरेखा को आधार बना कर ही रचना में प्रवृत्त होते थे, पर बहुत जल्दी ही पूर्वनिर्धारित पीछे छूट जाता था और रचना अपने स्वाभाविक विकास पथ पर आगे बढ़ जाती थी। प्रेमचंद की रचनाएं महान इसलिए भी बन पार्इं, क्योंकि वे पूर्व निर्धारित रूपरेखा से अलग ढंग से विकसित हुई हैं। प्रेमचंद की रचनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि कोई भी अच्छी रचना- उपन्यास या कहानी- फार्मूलाबद्ध ढंग से या बंधे-बंधाए खांचे में रह कर लिखी ही नहीं जा सकती है। जब यह बात कही जाती है कि कोई बड़ी रचना विचारधारा का अतिक्रमण करती है तो इसके मूल में भी यही बात है। कोई भी महान रचना विचारधारा में ‘फिट’ हो ही नहीं सकती है। रचना की महानता विचारधारा के पालन में नहीं, बल्कि उसके अतिक्रमण में है।
कोई भी लेखक अपनी विचारधारा के अनुरूप किसी रचना की आरंभिक रूपरेखा तो तैयार कर सकता है, पर रचना धीरे-धीरे अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया में विकसित होने लगती है। जब लेखक अपनी विचारधारा के हस्तक्षेप से रचना के विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया को बाधित करता है तो रचना का कमजोर होना निश्चित है। इसलिए कोई भी बड़ा लेखक विचारधारात्मक हस्तक्षेप द्वारा रचना के विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लेखक की विचारधारा और रचना के यथार्थवाद में समानधर्मिता का होना आवश्यक नहीं है। कम से कम महान रचनाकार और महान रचना में तो यह समानधर्मिता प्राय: नहीं मिलती है। प्रसिद्ध लेखक बाल्जाक का उदाहरण हमारे सामने है।
शायद इसीलिए एंगेल्स ने कहा था कि ‘यथार्थवाद लेखक के विचारों के बावजूद प्रकट हो सकता है।’ आगे चल कर लुकाच ने एंगेल्स के इस कथन के संदर्भ में बाल्जाक और टॉलस्टाय के उपन्यासों में लेखक की विचारधारा और रचना के यथार्थवाद के बीच परस्पर विरोधी संबंध को व्याख्यायित किया है।
किसी रचना के आधार पर लेखक को उसकी अपनी मूल विचारधारा से अलग मान लेना या लेखक की विचारधारा के आधार पर रचना की विचारधारा निर्धारित करना और फिर उसका मूल्यांकन करना दोनों अन्याय है। यह अन्याय हिंदी आलोचना में खूब हुआ है। प्रेमचंद इस बात के बहुत बड़े और सटीक उदाहरण हैं कि लेखक पर विचारधाराओं का प्रभाव हो सकता है, पर उसकी रचनाएं किसी विचारधारा की वाहक नहीं हो सकतीं। प्रेमचंद को कोई आर्यसमाजी, गांधीवादी या मार्क्सवादी सिद्ध करने की लाख कोशिश करे, पर प्रेमचंद इन विचारधाराओं के कारण नहीं, इनके बावजूद महान हैं। उनकी रचनाओं में व्यापक भारतीय जीवन की लय और धड़कन है। इस जीवन की लय और धड़कन के प्रति जब तक हमारी आस्था बनी रहेगी, प्रेमचंद की महानता अक्षुण्ण रहेगी।