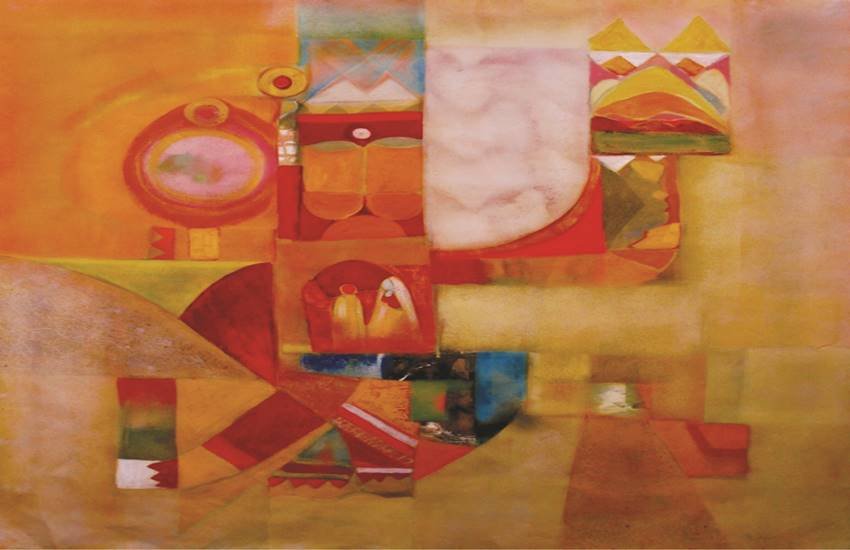इन दिनों जो साहित्य दुनिया की भाषाओं में लिखा जा रहा है, और जिससे हम कमोबेश परिचित हैं, वह कलाओं के साथ एक सहकारी भाव से लिखा जा रहा है : रचनाशील कई लेखक-कवि अब विभिन्न कला माध्यमों में गहरी रुचि ले रहे हैं। फिल्म-संगीत-नृत्य-नाटक- चित्रकला-मूर्तिशिल्प आदि में। और जाहिर है कि इस रुचि के प्रभाव से उनका लेखन प्रभावित भी हो रहा है। आने-जाने की सुविधाओं ने बहुत कुछ को प्रत्यक्ष तौर पर देखने-परखने के अवसर भी दिए हैं। सो, घर बैठे गूगल में कुछ सर्च करने से लेकर, स्वयं बहुतेरी यात्राओं द्वारा कुछ खोजने-पाने का क्रम जारी है। अचरज नहीं कि यात्रा-वृत्तांतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। यह भी कि साहित्य की विधाएं, प्रमुखत: अब केवल कविता-कहानी-निबंध-उपन्यास-नाटक ही नहीं हैं; उनमें डायरी, यात्रा संस्मरण, जीवनियां, आत्मकथाएं, संस्मरण, आदि जोरदार ढंग से शामिल हो गए हैं। और ये विधाएं पलट कर कहानियों, उपन्यासों, कविताओं को भी प्रभावित कर रही हैं।
कुछ समय पहले हिंदी में ही गीतांजलिश्री का एक उपन्यास आया है, ‘रेत समाधि’। इसे पढ़ते हुए आपको कई विधाओं का एक अलग तरह का स्वाद मिलेगा। और भाषा के साथ कई तरह के खेल करके- व्यंग्य-विनोद करके, एक नई, बोधगम्य, अर्थ-वाहक, बहुस्तरीय भाषा की निर्मिति भी आपकी आनंदित करेगी। दरअसल, ऐतिहासिक, पौराणिक से होते हुए आधुनिक, उत्तर-आधुनिक और फिर ‘आज’ के जिस दौर में हम पहुंचे हैं, उसमें स्वयं भाषा के साथ कई प्रकार के प्रयोग करके मनुष्य-मन के तल-अतल को, उसके तहखानों को, उसके विस्तृत परिसर को, खंगालने का काम लगातार जारी है। कह सकते हैं कि, भविष्य में इसमें और तेजी आएगी।
अगर नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत लेखकों की कृतियों से साहित्य की दशा-दिशा का कुछ संकेत अब भी मिलता हो, तो पिछले दशक-डेढ़ दशक के पुरस्कृत लेखकों में से कुछ को याद कर लेना अच्छा होगा। स्वेतलाना एलेक्सीविच (2015), बॉब डिलन (2016), काजुओ इशिगुरो (2017), थोड़ा और पीछे जाएं तो डोरिस लेसिंग, ओरहान पामुक, टॉमस ट्रांसत्रोमर, एलिस मुनरो जैसे नाम दिखाई पड़ेंगे। अब कठिन नहीं है, इनके बारे में कई तरह की जानकारियां प्राप्त करना। ये सभी साहित्य का एक नया वैविध्य रचने वाले हैं। उक्रेनी-बेलोरूसी स्वेतलाना एलेक्सीविच को नोबेल की घोषणा होने पर लोगों को भारी अचरज हुआ था, क्योंकि उनका लेखन एक श्रेष्ठ पत्रकारिता की श्रेणी में भी गिना जा सकता है, और बॉब डिलन के नाम की घोषणा पर तो एक विवाद ही छिड़ गया था। वे गायक-कवि हैं, बंगाल के बाउल से भी प्रभावित रहे हैं, सुने ज्यादा गए हैं, पढ़े कम। वह तो मानो वाचिक परंपरा को भी पुनर्नवा करने वाले हैं। और बाउल के जरिए, अपने देश के बाहर के एक ‘लोक’ से भी रिश्ता बनाने वाले।
यह वैविध्य चकित करने वाला है। चामत्कारिक है।
हमारी पीढ़ी बड़ी हुई थी रवींद्र, शरत, प्रेमचंद, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, यशपाल, अज्ञेय और ताल्स्तॉय, चेखव, दोस्तोएवस्की, तुर्गनेव, टॉमस मान, सार्त्र, कामू आदि को पढ़ते हुए। न जाने और कितने ही नाम जुड़ते चले गए थे, एब्सर्ड थिएटर वाले। अमेरिकी, जापानी उपन्यासकारों के भी। जो भी आया, मिला, दिखा, मित्रों से पता चला, हम पढ़ते रहे, रूसी कवियों को, पास्तरनाक, मांदलस्ताम आदि को। बहुत लंबी दूरी है। पर, इसमें सच्चाई है कि क्या तो विश्व साहित्य, क्या जापानी-चीनी साहित्य, क्या भारतीय भाषाओं का साहित्य, क्या हमारा अपना हिंदी का लेखन, जिन विधियों को पाया-खोजा गया, वे बहुत भिन्न हैं, पहले की विधियों से।
कब नहीं बदला साहित्य का स्वरूप! कभी-कभी वह तेजी से बदला है, किसी सदी विशेष में अधिक-जैसे उन्नीसवीं-बीसवीं सदी में। और इक्सीसवी के पहले चरण में ही हम बहुत-से परिवर्तन देख रहे हैं। तेज गति वाले। वस्तु से परिवर्तन तो तेजी से टेक्नालॉजी के कारण भी हो रहे हैं। ये लिखने में भी घटित हो रहे हैं- रचनाकारों की दुनिया में, और पाठकों की दुनिया में भी घटित हो रहे हैं। ई-बुक्स, किंडल और यू ट्यूब में आप रचनाएं पढ़ भी सकते हैं, और सुन भी सकते हैं। कागज पर लिखने और कंप्यूटर पर लिखे जाने में कुछ फर्क तो है ही। ‘गूगल’ में अब विश्व साहित्य की प्रमुख और समकालीन कृतियां उपलब्ध हैं- कई भाषाओं की। तमाम जानकारियां लेखकों-कवियों के बारे में, साहित्यिक प्रवृत्तियों और आंदोलनों के बारे में भी। यानी ‘एक जगह’ बहुत कुछ इकठ्ठा है।
एक सुविधा हुई है तत्काल चीजों के बारे में जान लेने की : विविध विषयों को खंगालने में। एक-दूसरे के पड़ोस में है सब कुछ : आप जयशंकर प्रसाद के बारे में जान लीजिए- उन्हीं के कालखंड के संगीतकारों, चित्रकारों-नृत्यकारों के बारे में भी जान लीजिए, पुरातत्त्वविदों के बारे में मालूम कर लीजिए। यानी किसी लेखक-कवि का जीवन-अवधि के समांतर दुनिया का कोई भी विषय छू लीजिए। पर, यह तो अतीत और वर्तमान के साहित्य की बातें हुर्इं, भविष्य का साहित्य, क्या और कैसा होगा।
नहीं, कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अनुमान लगाए जा सकते हैं। कुछ अटकलें भी। एक तो यही कि महाकाव्यों का जमाना वैसे भी चला-सा गया है, बड़े वृहदाकार उपन्यासों आदि का भी। तो पहला अनुमान यह कि कृतियों का आकार संभवत: कुछ छोटा होता जाएगा। कविता की दुनिया में यह विशेष रूप से घटित हो रहा है, आगे भी शायद घटित होगा। लंबी कविताएं लिखी कहां जा रही हैं? सवाल यह भी है कि क्या आधुनिक, उत्तर-आधुनिक के बाद कोई और प्रवृत्ति या विचार-सरणी उभरेगी! साहित्य के अध्ययन-अध्यापन, पठन-पाठन का रूप कितना और किस प्रकार बदलेगा! क्या कहा जा सकता है, सिवाय इसके कि साहित्य का परिचय, जितना खुलता गया है, रचना-विधियों, विषय-वस्तुओं आदि के मामले में वह भी और अधिक खुलेगा। रचना-विधियों या प्रयोगों की दिशा में कुछ बहुत नया तो शायद देखने को नहीं मिलेगा, पर यह संभव है कि एक ही कृति में विविध विषयों, और अभिस्थियों का ‘सम्मेलन’ या ‘सम्मिलिन’ दिखाई पड़ सकता है, जैसा कि काजुओ इशिगुरो की कृतियों में दिखाई पड़ा है। और हमारे यहां भी उपन्यासों में उसके लक्षण दिखाई ही पड़े हैं : अलका सरावगी, गीतांजलिश्री आदि के उपन्यासों में।
और जैसा कि होता ही रहा है, और आगे भी होता ही रहेगा, कि अतीत के साहित्य का भविष्य में एक नई तरह का अध्ययन, पठन, इंटरप्रेटेशन जारी रहेगा। वह सिर्फ साहित्य की दुनिया में ही नहीं होगा, वह होगा कलाओं में भी- नाटक-संगीत-फिल्म-नृत्य के जरिए भी। अकेले नाटक की ही बात कहें तो शेक्सपियर हों या कालिदास उनका इंटरप्रेटेशन जिस तरह से जारी है, वह भविष्य में और अधिक बढ़ने वाला है। हमारे यहां ही रतन थियाम की ‘ऋतुसंहार’ की प्रस्तुति को देख लीजिए या कावलम नारायण पणिक्कर द्वारा भास के नाटकों की प्रस्तुति को- या फिर मुंबई के अतुल कुमार की प्रस्तुतियों में से शेक्सपियर की एक प्रस्तुति को ‘पिया बहुरुपिया’ नाम की- जो बहुत चर्चित हुई है, बहुत सराही भी गई है। पुरानी विधियों को पुनर्नवा करके, और नई विधियों को खोज कर भविष्य में अगर कलाओं की दुनिया, साहित्य को नई तरह से खोजने-पाने का काम करेगी, तो स्वयं साहित्य भी तो कलाओं के इस पड़ोस में, नई विधियों, नई अभिव्यक्तियों की खोज करेगा। यह सहज स्वाभाविक है। और हां, प्रकृति, उसके उपादानों से साहित्य एक नए तरह का संबंध बनाएगा, ऐसा मेरा सोचना है।