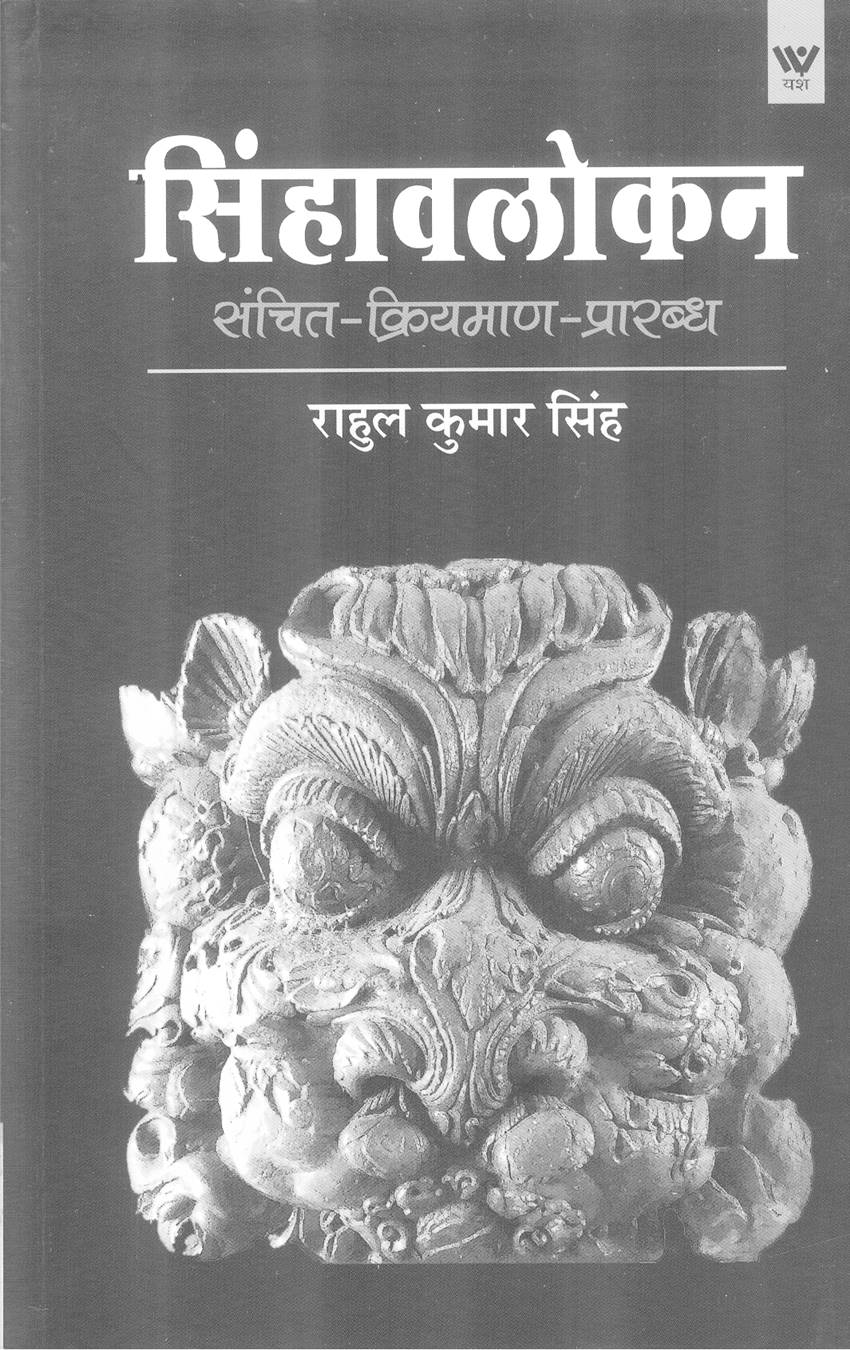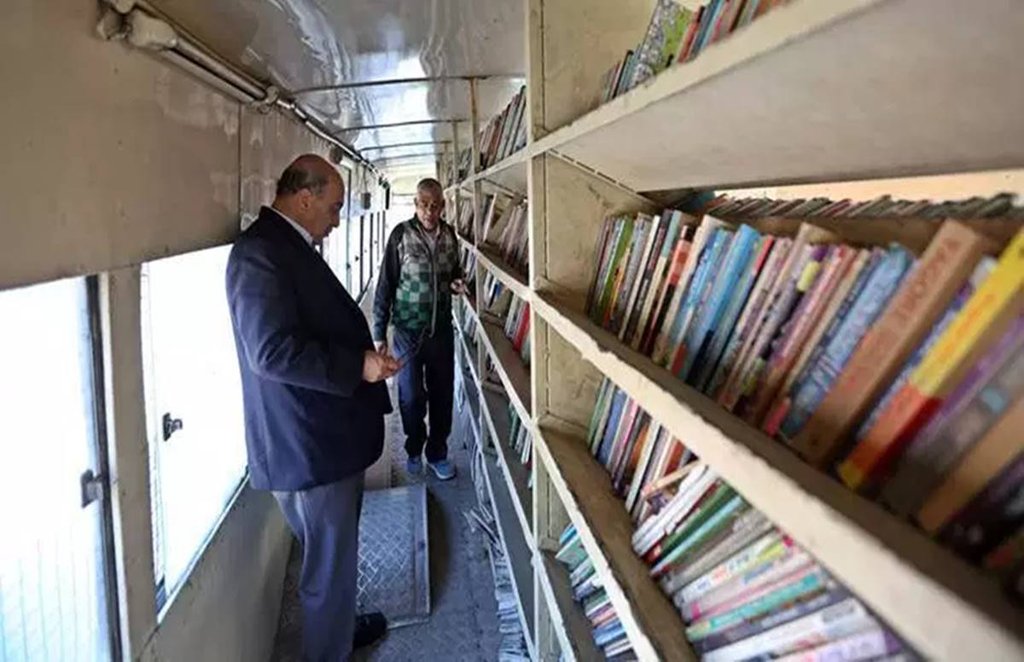हिंदी और हिंदी साहित्य से गांधीजी का हार्दिक संबंध था। इंग्लैंड में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद गांधीजी को यह बहुत खलने वाली बात लगी कि जिस भारत में अनेक समृद्ध भाषाएं दीर्घकाल से विद्यमान रही हैं, वहां पर शिक्षा का माध्यम एक विदेशी भाषा को रखा जाय। यह न तो दक्षता-निर्माण की दृष्टि से उचित था, न राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं अस्मिता की दृष्टि से। इस मुद्दे पर अंग्रेजी को आधुनिकता के लिए अपरिहार्य मानने वाले अनेक भारतीय बौद्धिकों से बिल्कुल अलग हट कर गांधीजी ने स्वदेशी भाषाओं का पक्ष लिया और हर प्रांत में वहां की संबद्ध भाषा में शिक्षा दिए जाने का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया।
भाषा के अलावा साहित्य का भी गांधी के चिंतन में महत्त्वपूर्ण स्थान था। जहां उन्होंने अपने व्यक्तित्व से अपने समय के देशी-विदेशी कई छोटे-बड़े साहित्यकारों के लेखन को प्रभावित किया, वहीं उनके चिंतन के निर्माण में साहित्य की भी काफी नियामक भूमिका रही। उन्हें भारत के प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक के साहित्य का अच्छा ज्ञान था। इसके अतिरिक्त विदेशी साहित्यकारों को भी उन्होंने यथेष्ट रूप में पढ़ा था। रूसी साहित्यकार टॉल्सटॉय का उन पर प्रभाव सर्वविदित है। लेकिन उन पर उससे अधिक भारत के मध्यकालीन भक्त कवियों- नरसी मेहता, अखा भगत, भोजा भगत, मीरांबाई, तुलसी, कबीर आदि का प्रभाव पड़ा था। साथ ही साहित्य पढ़ने के क्रम में साहित्य के संबंध में गांधीजी का अपना दृष्टिकोण भी विकसित हुआ था। उनसे प्रभावित साहित्यिक रचनाशीलता को लेकर तो हिंदी में काफी काम हुआ है, लेकिन उनके साहित्य संबंधी सरोकारों को लेकर बहुत कम चर्चा हुई है। इस पुस्तक का तीसरा अध्याय गांधीजी के इसी पत्र से संबद्ध है। श्रीभगवान सिंह ने अपनी इस पुस्तक में हिंदी और हिंदी साहित्य तथा इनसे संबद्ध विषयों पर गांधीजी के गहन विमर्श की व्यापक प्रस्तुति के साथ ही अपना मौलिक चिंतन भी हम सबसे साझा किया है और कतिपय बहुप्रचारित मिथकों का सच उजागर किया है।
गांधी का साहित्य और भाषा चिंतन : श्रीभगवान सिंह; सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी; 130 रुपए।
कथा कहे बलराम
लराम की तरह ही हैं उनकी कहानियां- सादगी, सहजता और सच्चाई। वे अक्सर आडंबररहित सहजता की छाप छोड़ती हैं। भोगी हुई यातना भी उनके यहां प्रदर्शन के लिए नहीं है। बलराम की कुछ कहानियां ऐसी हैं, जिनमें रचनाशीलता सहज वेग के साथ उतरी और कथाकार के रूप में उनकी सामर्थ्य, सार्थकता और संभावनाओं को उजागर कर गर्इं। बलराम की कहानियां पढ़ने के बाद ग्राम परिवेश ही उनका सृजन परिवेश लगता है। बलराम को कहानी कहना आता है, उनकी अपनी खास शैली है। कहानियां सहज, बहुत सहज ढंग से शुरू होती और मैदानी नदी-सी शांत-गंभीर बहती चली जाती हैं। अर्थ, समाज, राजनीति, पारिवारिक संबंध और व्यवस्था के कुचक्रों के उलझाव में फंसे किशोर, युवा और वृद्ध, बलराम की कहानियों के प्राय: मुख्य पात्र होते हैं। गांव के दुष्चक्रों से निकल कर ये पात्र शहर और महानगर में फैले और- और बड़े दुष्चक्रों में फंस जाते हैं। इस तरह कहानी की मामूली-सी घटना से निकल कर ये पात्र सामाजिक सोद्देश्यता लेकर ज्वलंत आधुनिक समस्याओं तक जा पहुंचते हैं। बलराम की कहानियों में अंतर्वस्तु की विविधता है, लेकिन अत्मनिरपेक्ष नहीं। उनके नायकों में अक्सर लेखक का संघर्ष सातत्य नैतिक विजन का काम करता है। वह हारता है और धूल झाड़ कर खड़ा हो जाता है। अपमान, उपेक्षा, मानसिक उत्पीड़न, संबंधों में बिखराव और टूटने-जुड़ने के बावजूद उनके व्यक्तित्व का विघटन नहीं होता।
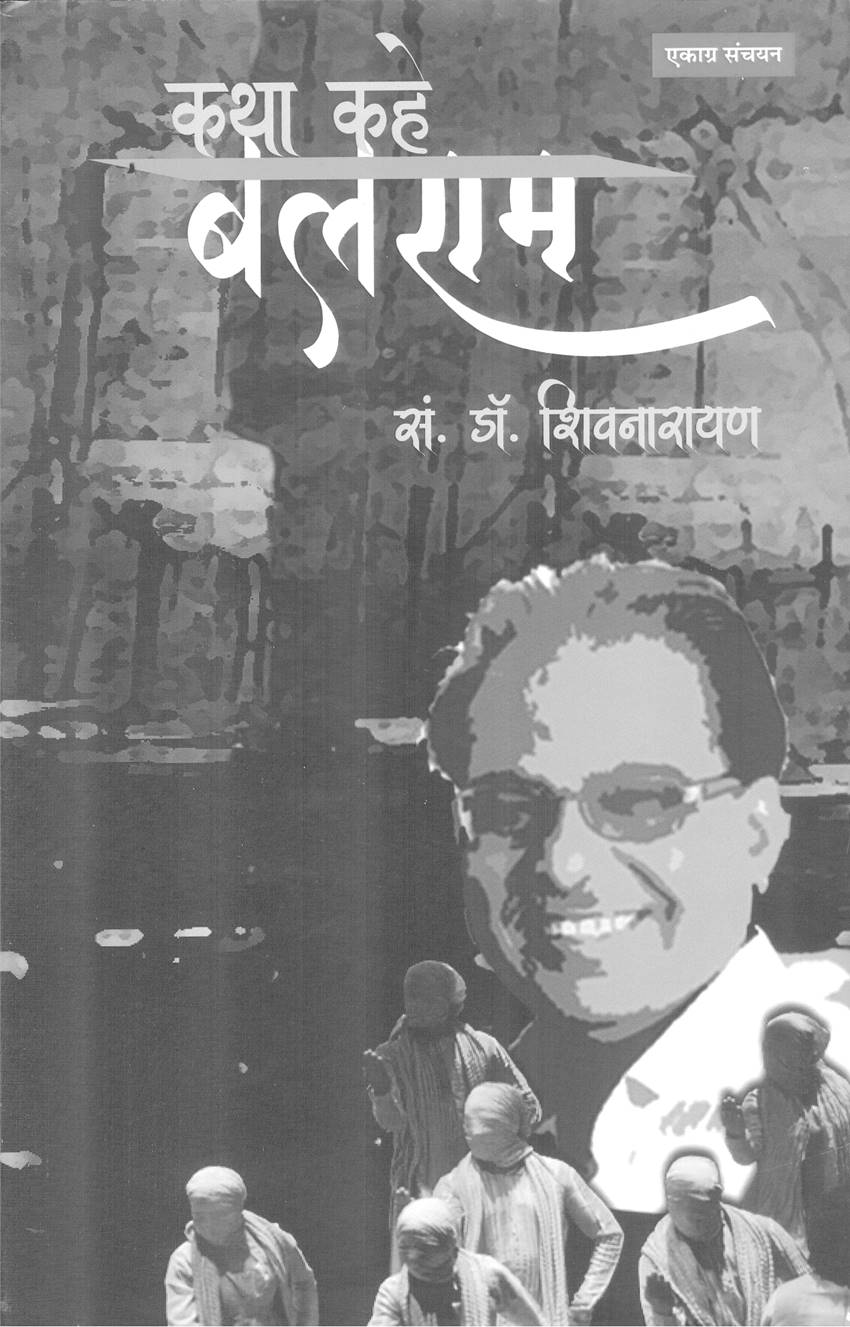
अघोर पुरुष
मीनाथ पांडेय रचित उपन्यास ‘अघोर पुरुष’ जीवनीपरक उपन्यासों की साहित्य-परंपरा का महत्त्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास के केंद्रीय व्यक्तित्व हैं काशी क्षेत्र की अघोर परंपरा के सिद्ध-पुरुष संत कीनाराम। इस उपन्यास का देशकाल है मुगलकालीन भारतीय इतिहास का वह काल-खंड, जिसमें अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति के विपरीत मुगल साम्राज्य की अंतर्कलह और औरंगजेब की कट्टर सांप्रदायिक नीति हिंदुस्तान के सामाजिक ढांचे को छिन्न-भिन्न कर रही थी। एक तेजस्वी और समावेशी इतिहास-पुरुष के आगमन का इससे उपयुक्त समय भला क्या हो सकता था। लोक विश्रुत संत कीनाराम के आख्यान को केवल जनश्रुतियों-किंवदंतियों और अपर्याप्त जीवन-वृत्त के बल पर रचना संभव नहीं था। इसलिए लेखक ने शोधपरक दृष्टि के साथ आवश्यक कल्पनाशीलता के समावेशन से एक उद्देश्यपूर्ण कृति रचने में सफलता प्राप्त की है। आज जब संत-समाज की राजनीतिक संलग्नता सवालों के दायरे में है, अघोर पुरुष का केंद्रीय व्यक्तित्व एक ऐसा संत है जिसके चिंतन और चिंता का विषय परलोक नहीं, इहलोक है; जिसकी लीलाभूमि मात्र तीन लोक से न्यारी काशी नहीं, यह समूचा महादेश है; और उसकी विचारभूमि के केंद्र में है महादेश भारत की सामाजिक संस्कृति। सिद्ध-पुरुष संत कीनाराम की जीवन-कथा के माध्यम से सांस्कृतिक अस्मिता का देशज विमर्श रचता तथा उसका संगत और समीचीन समालोचन प्रस्तुत करता है यह उपन्यास है।
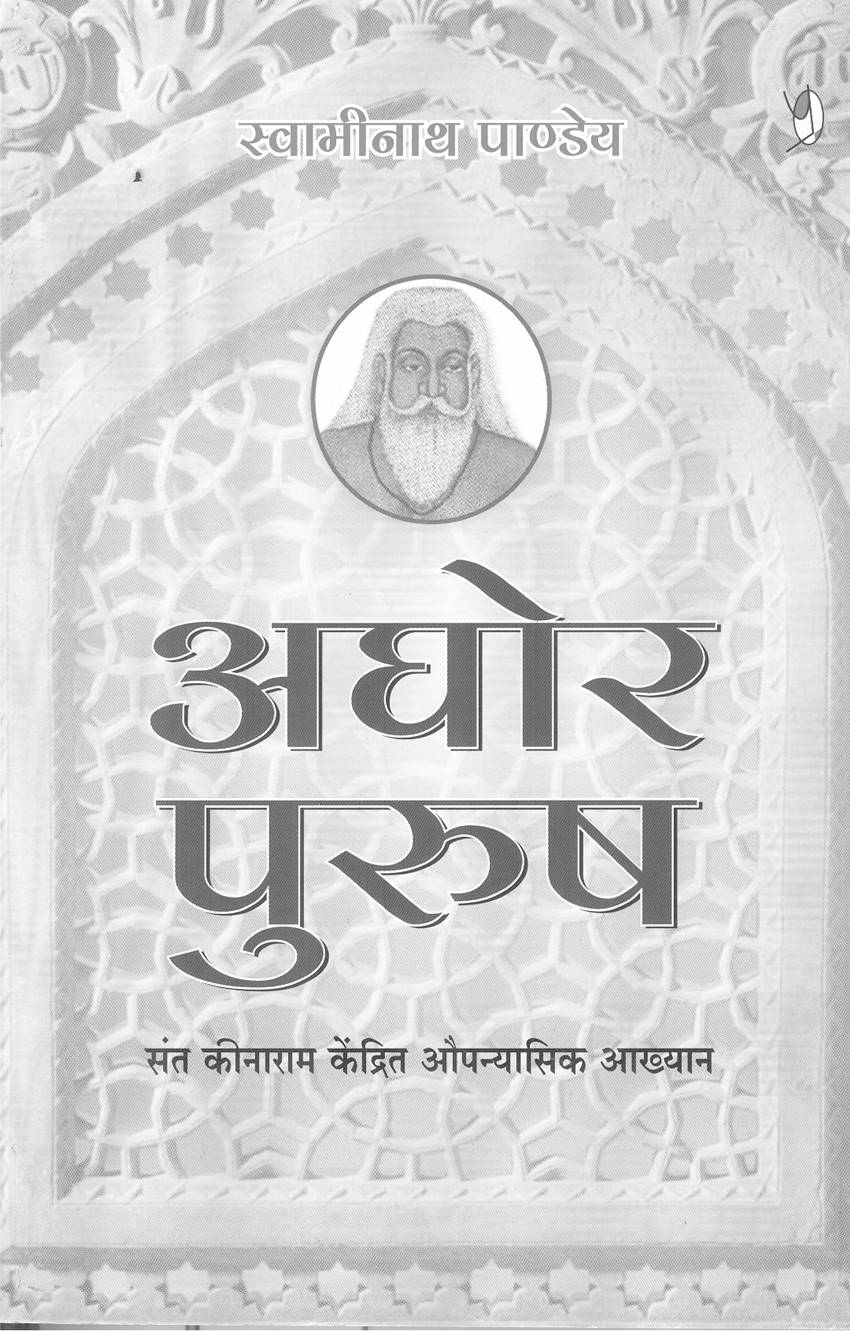
सिंहावलोकन
स किताब में मेले, रंगमंच, सिनेमा, मिथक और भाषा जैसे घटकों में कला, संस्कृति, धरोहर, इतिहास, परंपरा के आंचलिक वैशिष्ट्य की पहचान होती है। इस दृष्टि से यहां विविधरंगी छत्तीसगढ़ के उत्तरी सरगुजा अंचल और दक्षिणी बस्तर अंचल के समावेशी संतुलन का ध्यान रखते हुए सांस्कृतिक कारकों के कई अनछुए लेकिन महत्त्वपूर्ण पक्षों को रेखांकित किया गया है। साथ ही प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर प्रदेश के आंचलिक परिप्रेक्ष्य को राष्ट्रीयता और वैश्विक संदर्भों में भी यथास्थान स्पर्श किया गया है। संग्रह में वैचारिक टिप्पणियां तथा पुरातत्व से संबंधिक गंभीर किंतु रोचक लेख भी हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ की विशिष्टता के साथ विश्वजनीन सभ्यता-संस्कृति के प्रतिमानों का आत्मीय स्पंदन महसूस किया जा सकता है। पुस्तक में सांस्कृतिक मूल्यों के साथ एकमेव होकर डूबने-उतराते समष्टि की झलकियां मिलती हैं और वहीं पथ आलोकित करती हैं। सभ्यता शिशु ठहरता है अपने पूर्वकृत संचित से प्रारब्ध करने का मार्ग प्रशस्त करने और क्रियमाण पग बढ़ाता है। यह सिंहावलोकन, देश के भेद और काल के प्रवाह में बोध की समग्रता का आग्रह है।