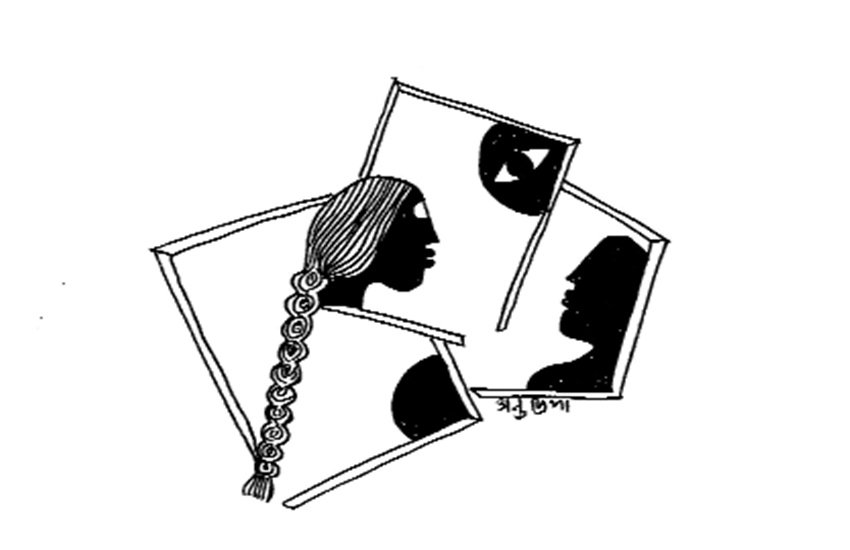हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल सरोजिनी देवी नेत्र चिकित्सालय में 21 मरीजों के मोतियाबिंद के आपरेशन हुआ। इनमें से सात के आंखों की रोशनी चली गई और तेरह के आंखों में गंभीर संक्रमण हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि सर्जरी में अनियमितता नहीं हुई, बल्कि मरीजों को जो बोतल चढ़ाया गया, वह प्रदूषित था। किसी न किसी राज्य से अक्सर खबरें आती रहती हैं। यह घटना तो सरकारी अस्पताल में हुई है, लेकिन अधिकतर घटनाएं शिविरों या निजी अस्पतालों में होती हैं। संक्रमण के लिए न केवल संक्रमित सलाइन, मिलावटी दवाएं बल्कि एकदम प्रत्यक्ष दिख जानेवाले कारण भी मौजूद होते हैं। मसलन, साफ सुथरे बिस्तर बेड का अभाव, साफ सफाई की बदहाल व्यवस्था, मरीजों की देखभाल के नाम पर तैनात अप्रशिक्षित कर्मी, सीमित संख्या में उपलब्धता के चलते अस्पतालों में अत्यधिक भीड़। इस प्रकार के संक्रमण के कारण मरीजों की दुर्दशा और उन्हें झेलने पड़ते जोखिम जहां एक बात है, वहीं मूल प्रश्न यह है कि कब तक लोगों को मोतियाबिंद जैसे आपरेशनों के लिए बदइंतजामी वाले सरकारी अस्पताल या शिविरों में इलाज में से एक को चुनना पड़ेगा?
अभी कुछ माह पहले की बात है कि जब अंबाला के एक अस्पताल में अवैध तरीके से लगाए गए एक शिविर में मोतियाबिंद के आपरेशन में सोलह लोगों के आंखों की रोशनी चली गई थी। मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में अलग-अलग शिविरों में चालीस लोगों की आंखें खराब हो गर्इं। दो साल पहले छत्तीसगढ़ में नसबंदी आॅपरेशन के दौरान कई महिलाओं की मौत हो गई थी। जांच में आया कि आपरेशन के बाद दी गई दवा मिलावटी थी।
शिविरों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, उनकी जांच करना आदि मामले तो ठीक हैं, लेकिन मोतियाबिंद या नसबंदी जैसे आपरेशन के जएि आंखों की रोशनी छीनना या जान को जोखिम में डाल करना अपराध है। आए दिन शिविरों में हो रही मौतों की खबरें आती हैं। लेकिन, उन घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया जाता। ऐसे शिविरों में आमतौर गरीब लोग आते हैं। इस वजह से भी सरकारें लापरवाह बनी रहती हैं। रोशनी जाने के बावजूद पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिए कहीं भागदौड़ नहीं कर पाता। इसके अलावा, शिविर लगाने के नाम सरकारी अस्पताल हों या निजी, सब जगह पैसे का भी घोटाला होता है।
भारत में आम जनता के लिए स्वास्थ्य का बजट भी बहुत कम है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का महज एक फीसद बजट होता है, जबकि चीन में सकल घरेलू उत्पाद का तीन फीसद स्वास्थ्य पर खर्च होता है। अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद का 8.3 फीसद और ब्रिटेन में यह आंकड़ा 9.6 फीसद तक होता है। एक अनुमान के अनुसार भारत स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च के हिसाब से दुनिया के 184 देशों में 178 वें स्थान पर है। निम्न आयवाले देश -बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी वह पीछे है।
विशेषज्ञ लंबे समय से भारत में स्वास्थ्य का बजट सकल घरेलू उत्पाद का फीसद करने की जरूरत जता रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि वह सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम पांच फीसद होना चाहिए। हम यह भी देख रहे हैं केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने के बाद जिस तरह सामाजिक कल्याण के अन्य मदों में कटौती हो रही है, वह खतरा यहां पर भी मंडरा रहा है।
अभी कितना कुछ किया जाना बाकी है, इसे महिलाओं के स्वास्थ्य की बात से समझा जा सकता है। राजधानी दिल्ली में हर चौथी महिला अपनी जान पर खेलकर बच्चे को जन्म देती है। करीब दो करोड़ की आबादी वाले इस शहर में सरकारी अस्पताल में सिर्फ आठ हजार बिस्तर उपलब्ध हैं। दिल्ली की तीस फीसद महिलाओं का प्रसव अप्रशिक्षित दाइयां कराती हैं जिनमें एक चौथाई महिलाएं प्रसव के दौरान अपनी जान गवां बैठती हैं। दिल्ली के आसपास के ग्रामीण इलाकों की स्थिति और भी खराब है। यहां उचित चिकित्सा सुविधा के अभाव में बयालीस फीसद से भी अधिक महिलाएं घरों में ही बच्चों को जन्म देने के लिए विवश हैं। यह स्थिति तब है, जब हम जानते हैं कि भारत में मातृ मृत्यु-दर काफी खराब है।
तुलना करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मातृ मृत्यु-दर पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी बदतर है। यहां प्रति एक लाख पर बच्चा जनते समय चार सौ पचास माताओं की मृत्यु हो जाती है, जबकि पाकिस्तान में यह दर तीन सौ बीस है। इन तथ्यों पर भी कई बार सर्वेक्षण हुए हैं। भारतीय महिलाओं में खून की कमी होती है, हिमोग्लोबिन की मात्रा सात या आठ प्रतिशत होती है और यह गर्भवती के लिए खतरनाक स्थिति मानी जाती है। अगर केस बिगड़ गया तो अस्पतालों में उसे संभाल लेने की गुंजाइश होती है लेकिन घर में चाह कर भी ऐन मौके पर बचाना असंभव होगा।
प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप को अधिक पुष्ट करने और उसमें आवंटन बढ़ाने जैसे असल मुद्दे से सरकार कब तक भागती रहेगी और जब भी ऐसी दुर्घटना सामने आए तो कुछ व्यक्तियों को सजा देकर जवाबदेही से बचती रहेगी ? स्वास्थ्य का सवाल और इलाज का हक एक गम्भीर समस्या का रूप ले चुका है। बीमार इंसान को इलाज का हक मिलना ही चाहिए। और हमारे देश में अभी भी आलम यह है कि स्वास्थ्य नागरिकों का मूल अधिकार तो छोड़िए, कानूनी अधिकार भी नहीं है। कानूनविदों के मुताबिक स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार में शामिल माना जाता है।
उच्चतम न्यायालय ने भी इस विचार को आंशिक स्वीकृति दी है, मगर इसे लेकर स्पष्ट प्रावधान न होने के चलते कोई नागरिक यह दावा नहीं कर सकता कि स्वास्थ्य सुविधाएं पाना उसका बुनियादी अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों की सेहत और उसकी जिंदगी से जुड़े खतरों को प्राथमिकता के साथ ले। ऐसा करने में नाकाम रहने पर ही अदालतों को दखल देना पड़ता है।
ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि भारत के पास संसाधनों की कमी है। यह दरअसल राजनीतिक इच्छाशक्ति का सवाल है। अगर एक छोटा सा देश क्यूबा – जो खुद उसी तरह आर्थिक संकट और अमेरिकी घेराबंदी की मार झेलते हुए – हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिलाने में और विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से दुनिया के लिए नजीर बन सकता है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता!