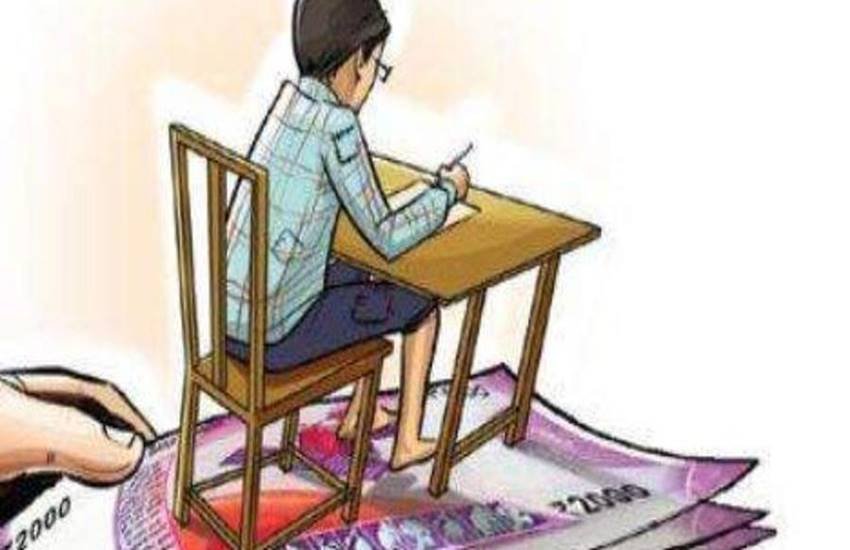समान शिक्षा से सरोकार रखने वालों के लिए हाल ही में दो अहम् खबरें आई हैं। पहली खबर के मुताबिक कोरोनावायरस की वजह से देश से बाहर पढ़ने जाने वाले बच्चों पर खर्चे में सत्तर फीसदी की कमी आई है। यानी पिछले वर्ष अप्रैल में ढाई सौ मिलियन डॉलर की जगह इस बार सिर्फ अठहत्तर मिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा देश से बाहर गई है। 2018 में सात लाख भारतीय बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, आॅस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर आदि देशों में पढ़ने गए थे। अगर इसमें विदेशों में सैर-सपाटे के लिए जाने वालों को भी जोड़ लें, तो उसमें भी बहत्तर फीसदी की कमी आई है।
दूसरी खबर है महंगे निजी स्कूलों को छोड़ कर सरकारी स्कूलों में दाखिले की दौड़। अभी सिर्फ पंजाब से आंकड़े मिले हैं, जहां लगभग दो लाख स्कूली बच्चों ने निजी स्कूलों को छोड़ कर सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया है। आगे और भी बढ़ने की उम्मीद है। ये सभी बच्चे निम्न मध्यवर्ग, मजदूर, गरीब तबकों से ताल्लुक रखते हैं। पूर्णबंदी की वजह से आर्थिक स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं और निजी स्कूलों की फीस और खर्च वहन कर पाना आसान नहीं है। यह पूरे देश की तस्वीर का बयान है।
इन दोनों खबरों से ही शिक्षा में बड़े बदलाव के रास्ते खोजे जा सकते हैं। आखिर हजारों-लाखों बच्चे भारत के लगभग आठ सौ विश्वविद्यालयों को छोड़ कर विदेश क्यों भागते हैं? वह भी बहुत ऊंची फीस देकर? क्या हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, प्रबंधन कालेज, कंप्यूटर संस्थाएं और दूसरे विषयों की पढ़ाई में इतनी गिरावट आ चुकी है? वैसी ही स्थिति सरकारी स्कूलों को छोड़ कर अंग्रेजी स्कूलों में भागने की दौड़, जहां बस्ता, दाखिला, किताब, कॉपी प्रोजेक्ट, कंप्यूटर, लेबोरेट्री आदि के नाम पर फीस से जेब खाली की जाती है।
लेकिन सच यह भी है कि शिक्षा की हालत दिनोंदिन और बिगड़ रही है। लगभग सभी अध्ययन बताते हैं कि आठवीं कक्षा का छात्र तीसरी का गणित हल नहीं कर सकता और पांचवी का बच्चा दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकता। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता का आकलन करने वाली क्यूएस की सूची पर यकीन किया जाए तो इस साल दुनिया के एक हजार विश्वविद्यालय में भारत के सिर्फ इक्कीस हैं।
खैर मौजूदा कोरोना की चुनौती ने पूरे शिक्षा जगत को और बड़ी चिंता में डाल दिया है। दिल्ली जैसे महानगरों में आनन-फानन में आॅनलाइन शिक्षा की वकालत लॉकडाउन के पहले चरण में मार्च के अंत में ही शुरू कर दी गई थी। इसे वातानुकूल कक्ष में रहने वाले अमीरों की नासमझी कहें या देश की जमीनी स्थितियों से अनभिज्ञता। नतीजा सिफर रहा।
दिल्ली के चंद नामी स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो सरकारी स्कूलों के जो आंकड़े सामने आए उसमें मुश्किल से तीस फीसदी स्कूली बच्चे ही आॅनलाइन कक्षा में शामिल हो पाए। बहुत सारे बच्चों के पास अलग से मोबाइल नहीं रहता, न इंटरनेट की सुविधाएं हैं। महंगे स्मार्टफोन खरीदना सबके लिए आसान नहीं! घर का माहौल एक बड़ा सवाल है। खासतौर पर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों का परिवार जैसे घरों में रहते हैं, उसमें कम जगह, संसाधनों के अभाव के साथ-साथ पढ़ाई के लिए आवश्यक एकाग्रता में बाधा एक सामान्य-सी बात है।
देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि गरीब बच्चे और मुसीबत में फंस गए हैं। न केवल बच्चों के लिए, बल्कि शिक्षकों के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। न अभ्यास है, न प्रशिक्षण। इसलिए ऐसे किसी विकल्प को जल्दबाजी में लागू करना शिक्षा को और बर्बाद करेगा।
प्रश्न उठता है कि फिर विकल्प क्या है? नई स्थितियों में शिक्षकों और अभिभावकों की एक सक्रिय भूमिका सामने आ सकती है। वह इस रूप में कि उनके पास उनके घरों में ही या स्कूल में अलग-अलग बुला कर पुस्तकें दे दी जाएं। संभव हो तो हर स्कूल में एक पुस्तकालय की शुरुआत की जाए, जिसमें बच्चों के मनोरंजन, खेल और कहानी, नाटक की विविध अच्छी किताबें हों। बच्चों को किताब का चस्का अगर लग जाए तो वे पाठ्यक्रम की किताबों से कई गुना ज्यादा खुद ही पढ़ लेते हैं। वे स्वाध्याय और आत्मनिर्भर रहना, बनना भी सीखेंगे।
बहरहाल, आगे पढ़ाई के लिए आखिर हमारे बच्चे विदेशी विश्वविद्यालयों की तरफ क्यों भागते हैं? बहुत सारे अनुभवों के बाद कुछ बातें समान रूप से सामने आई हैं कि इन सभी देशों में यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया में शिक्षा सस्थानों की विशेषता अच्छा पुस्तकालय है। विविध किताबों से भरे हुए। मनमर्जी घर ले जाने के लिए और उनकी रुचि के अनुसार और पुस्तकें मंगाने के लिए भी। दूसरा अहम् पक्ष है शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच एक आत्मीय रिश्ता।
बच्चों को जो काम दिया जाता है, शिक्षक उसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर उन्हें समझाते हैं, न कि महीनों तक उनकी कॉपियों को देखने से भी बचें। यही कारण है कि फ्रांस में पढ़ने वाली दो बच्चियों ने बताया कि उनको छुट्टी वाले दिन भी स्कूल जाने का मन करता है, जबकि हमारे यहां बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। याद किया जा सकता है कि रवींद्रनाथ ठाकुर ने सौ वर्ष पहले ऐसे स्कूलों को पाठशाला की बजाय ‘जेलसाला’ कहा था।
कोरोना समय में जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, उसमें स्कूलों में दाखिले के विकल्प के कमजोर पड़ने की भी गुंजाइश बन रही है। हालांकि ऐसी आवाजें भी उठ रही हैं कि जहां बाजार, माल, रेस्टोरेंट और मंदिर, मस्जिद तक खोलने के लिए लोगों ने कहा, वहीं स्कूल खोलने की एक भी आवाज नहीं आ रही। हाल के सर्वे बताते हैं कि बहुत सारे अभिभावक कोरोनावायरस की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। निश्चित रूप से बच्चों के विकास में स्कूल-कॉलेज की एक भूमिका होती है, लेकिन शर्त यह भी है कि स्कूल और कॉलज वैसा मुक्त, प्रभावी वातावरण दें।
अगर किन्हीं वजहों से स्कूल-कॉलेज की नियमित पढ़ाई में बाधा आ रही है तो सरकार एक नीतिगत घोषणा कर सकती है कि जो अभिभावक समर्थ हैं, घर पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनके लिए स्कूल अनिवार्य नहीं है। इससे स्कूलों पर दाखिले का दबाव भी कम होगा। जब भी स्कूल में ऐसे बच्चे अपनी सुविधा से दाखिला लेना चाहें, स्कूल इनकी परीक्षा लेकर दाखिला दे।
एक काम यह भी किया जा सकता है कि आठवीं या पांचवी की कोई राष्ट्रीय परीक्षा या राज्य परीक्षा हो। वह प्रमाण-पत्र भी एक मानक का काम करे। इसके कई फायदे हैं। बच्चों को सुबह-सुबह उठा कर बस की तरफ दौड़ाना, फिर घंटे-दो घंटे तक बस से स्कूल, सड़कों पर मारामारी, फिर लौटने तक उनमें एक थकान। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में ‘घर स्कूल’ के परिणाम अच्छे साबित हुए हैं।