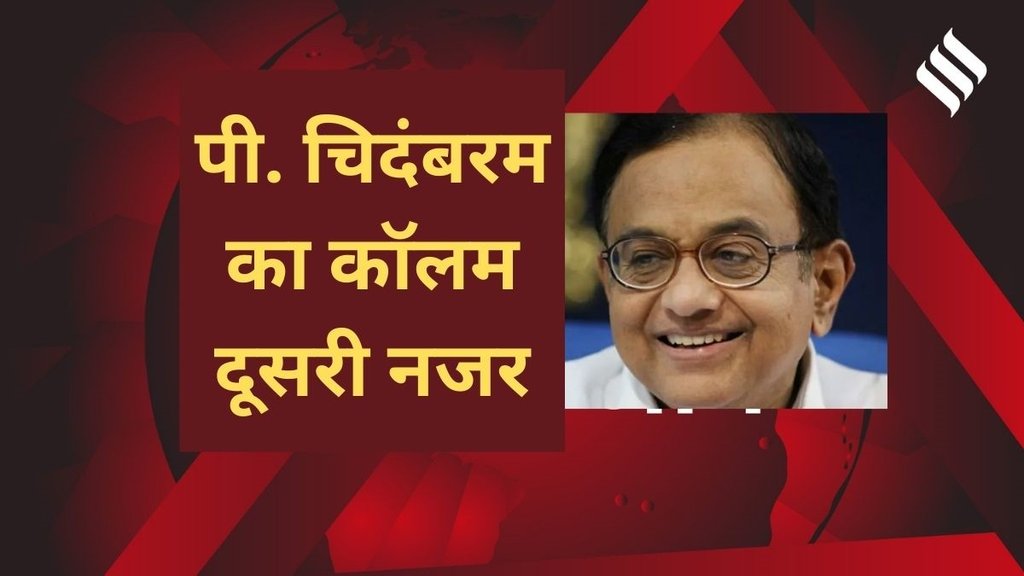तमिल में एक कहावत है कि जब भूख सताती है तो दसों गुण फुर्र हो जाते हैं। वे दस गुण हैं- सम्मान, कुल, शिक्षा, उदारता, ज्ञान, दान, तपस्या, प्रयास, दृढ़ता और इच्छा। आधुनिक समय में, चुनावों के समय ये दसों- और इससे अधिक- गुण गायब हो जाते हैं। माना कि बजट 2025-26 दिल्ली चुनाव से ठीक पहले और बिहार चुनाव से कुछ महीने पहले पेश किया गया। मगर, मैंने शायद ही कभी ऐसा बजट देखा है, जिसमें सरकार एक वर्ष में जितना दे सकती है, वह सब कुछ, सिर्फ कुछ लोगों को इस उम्मीद में दे दे कि सत्तारूढ़ पार्टी को उससे उनके वोट हासिल हो सकते हैं। ठीक यही बात माननीय वित्तमंत्री ने बजट में की।
वित्तमंत्री ने हिसाब लगाया- या शायद उन्हें बताया गया होगा कि उन्हें इसकी खोज करनी चाहिए- कि उनके पास बांटने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का खजाना है। उन्होंने इस पैसे को ‘ढूंढ़ा’ और वह सारा पैसा उन 3.2 करोड़ लोगों (143 करोड़ लोगों की आबादी में से) को देने का फैसला कर लिया, जो आयकर देते हैं। यह बहुत सामान्य-सा विवरण है कि 3.2 करोड़ आयकरदाताओं में मध्यवर्ग, अमीर, बहुत अमीर और अतिशय अमीर शामिल हैं। तमिल कहावत में निहित दस गुणों के साथ-साथ, समता, सामाजिक न्याय और वितरण में निष्पक्षता जैसे शासन के आधुनिक मूल्यों को भी हवा में उड़ा दिया गया।
राजनीति से प्रेरित बजट
जिस वक्त बजट की कवायद शुरू हुई, उस वक्त वित्तमंत्री राजस्व में गिरावट के दबाव में थीं। वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया कि केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियां 2024-25 के बजट अनुमानों से लगभग साठ हजार करोड़ रुपए कम रहेंगी। इसके अलावा, अगर वित्तमंत्री 2024-25 के राजकोषीय घाटे में थोड़ा सुधार करना चाहती हैं, तो वित्त मंत्रालय को कम से कम तिरालीस हजार करोड़ रुपए जुटाने होंगे। यानी कुल मिलाकर, लगभग एक लाख करोड़ रुपए जुटाने होंगे। दिल्ली चुनाव नजदीक थे, तय किया गया कि अगर छूट देने पर विचार करेंगे, तो इसके लिए 2025-26 में अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी।
इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि आयकर में ‘छूट’ सरकार के शीर्ष स्तर पर तय की गई थी। करदाताओं के किस वर्ग को इसका लाभ मिलना चाहिए? अरे वाह (जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा), हर आयकरदाता को इसका लाभ मिलना चाहिए! इसलिए, करयोग्य आय की सीमा को सात लाख रुपए से बढ़ाकर बारह लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया। वित्तमंत्री ने कहा कि इस पर एक लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।
बजट पर कुल्हाड़ी
यह निर्णय लिए जाने के बाद, 2024-25 के व्यय में कटौती करने और 2025-26 में नागरिकों के अन्य वर्गों को किसी भी तरह की राहत से वंचित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था: मनरेगा श्रमिकों (सबसे गरीब), दिहाड़ी मजदूरों, गैर-आयकर भुगतान करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों, औद्योगिक श्रमिकों, एमएसएमई, गृहिणियों, पेंशनभोगियों और बेरोजगार युवाओं को नजरअंदाज कर दिया गया। वित्तमंत्री ने कुल्हाड़ी चलाई और विदेश मंत्रालय से लेकर शिक्षा, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण और शहरी विकास तक के मंत्रालयों से मौजूदा और अगले वर्षों के पूंजी और राजस्व व्यय दोनों में बेरहमी से कटौती कर दी। इसके अलावा, एक लाख करोड़ रुपए छोड़ने के बावजूद, उन्होंने बस यह मान लिया कि 2025-26 में केंद्र सरकार को शुद्ध कर प्राप्तियां 2024-25 की तरह ग्यारह फीसद की दर से बढ़ेंगी।
आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, युवा बेरोजगारी 10.2 फीसद है और स्रातकों की बेरोजगारी तेरह फीसद है। बजट दस्तावेजों में रोजगार सृजन योजनाओं पर व्यय की आठ पंक्तियां हैं, जिनमें बहुचर्चित उत्पादकता से जुड़ी निवेश (पीएलआइ) योजनाओं की पांच पंक्तियां शामिल हैं। आठ पंक्तियों में 2024-25 के लिए बजट अनुमान 28,318 करोड़ रुपए था, लेकिन संशोधित अनुमान केवल 20,035 करोड़ रुपए है। रोजगार सृजन कार्यक्रम एक बहुत बड़ी विफलता है।
निचले तबके के आधे लोग
पीएलएफएस के अनुसार, पिछले सात वर्षों में वेतनभोगी पुरुष कर्मचारियों का मासिक वेतन 12,665 रुपए से घटकर 11,858 रुपए हो गया है और स्वरोजगार करने वाले पुरुष कर्मचारियों का वेतन 9,454 रुपए से घटकर 8,591 रुपए हो गया है। महिला कर्मचारियों के मामले में भी इसी तरह की गिरावट आई है। घरेलू उपभोग सर्वेक्षण के अनुसार, औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) 4,226 रुपए (ग्रामीण) और 6,996 रुपए (शहरी) था। यह भारत की पूरी आबादी का औसत है। अगर कोई आबादी के निचले पचास फीसद के लिए एमपीसीई की गणना करता है, तो यह कम होगा, और आबादी के निचले पच्चीस फीसद के लिए, यह और भी कम होगा। चार लोगों का परिवार 44000-7000 रुपए (या इससे कम) के प्रति व्यक्ति मासिक व्यय पर कैसे जी सकता है, जिसमें भोजन, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, किराया, परिवहन, ऋण चुकाना, मनोरंजन, सामाजिक दायित्व और आपात स्थितियों पर व्यय शामिल होगा?
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत को वर्ष 2030 तक हर साल 78.5 लाख गैर-कृषि रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। भारत का विनिर्माण क्षेत्र पिछले दस वर्षों में कम हो गया है: 2014 में सकल घरेलू उत्पाद के 15.07 फीसद से 2023 में 12.93 फीसद (स्रोत: विश्व बैंक)। वैश्विक विनिर्माण व्यापार में भारत का हिस्सा 2.8 फीसद था, जबकि चीन का 28.8 फीसद था। विनिर्माण क्षेत्र ने बेरोजगारों, दिहाड़ी मजदूरों या स्वरोजगार करने वाले श्रमिकों को रोजगार देने के लिए आवश्यक संख्या में रोजगार सृजित नहीं किए हैं। ‘मेड इन इंडिया’ एक और बहुत बड़ी विफलता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर्याप्त गति से नहीं बढ़ पा रही है। सरकार की नीतियों (जो 1 फरवरी, 2025 के वित्तमंत्री के भाषण में परिलक्षित होती है) के परिणामस्वरूप, एक छोटा-सा हिस्सा बहुत अमीर बन सकता है और मध्यवर्ग (अधिकतम 30 फीसद आबादी) आरामदायक जीवन जी सकता है। हालांकि, सरकार पर निचले पचास फीसद भारतीयों को क्रूरतापूर्वक त्याग देने का आरोप है।
(जारी)