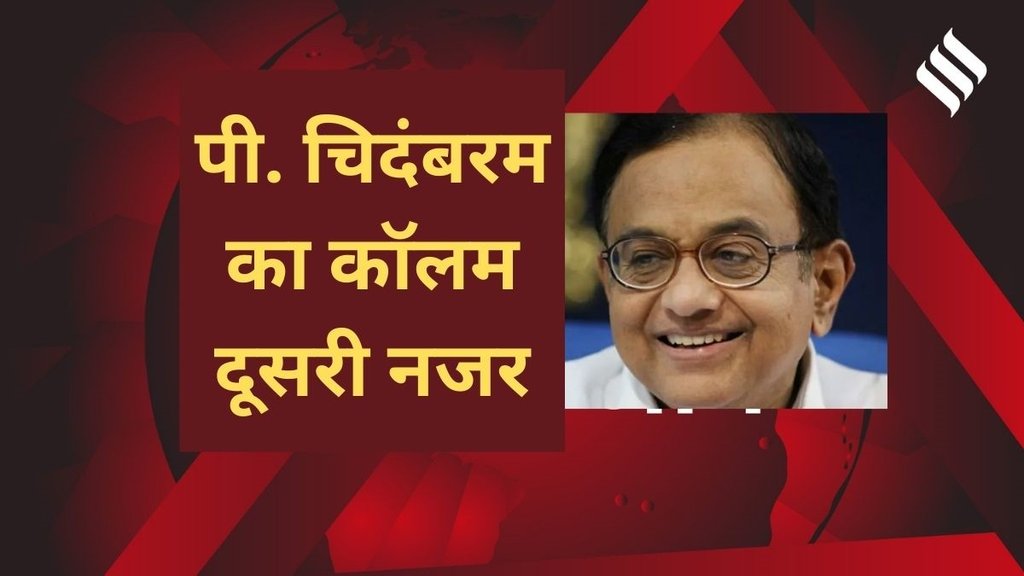उन लोगों की तारीफ करता हूं, जो मुझे सोचने के लिए उकसाते हैं। हो सकता है कि मैं उनके कुछ विचारों से सहमत न हो पाऊं, लेकिन मुझे खुशी होती है कि वे मुझे थोड़ा ठहरने, सोचने और फिर से सोचने को मजबूर करते हैं। ऐसे बहुत थोड़े से लोग हैं। हमें आभारी होना चाहिए कि हमारे बीच एनआर नारायणमूर्ति और एसएन सुब्रह्मण्यन जैसे लोग हैं। उन्होंने दुनिया में अपनी जगह बनाई है और अपने लंबे और प्रतिष्ठित करिअर के दौरान उन्होंने अपने मन की बात कहने की गुणवत्ता विकसित की है। लोग नारायणमूर्ति और सुब्रह्मण्यन को सुनते और उस पर प्रतिक्रिया देते हैं- थोड़े आक्रामक ढंग से!
भिन्न विश्व-दृष्टि
नारायणमूर्ति और सुब्रह्मण्यन दोनों को संपत्ति विरासत में नहीं मिली। न ही वे सरकारी या औद्योगिक कर्मचारी हैं, जिन्हें वेतन या मजदूरी मिलती है। वे योग्य पेशेवर हैं और इंजीनियर से पहली पीढ़ी के उद्यमी बन चुके हैं। इस तरह, उनके उद्यमों के मुनाफे में उनका हिस्सा बनता है। उनका दुनिया को देखने का नजरिया ‘उत्तराधिकारियों’ और ‘कर्मचारियों’ के विचारों से अलग है। नतीजतन, कामकाजी जीवन में संतुलन को लेकर भी उनका दृष्टिकोण अलग है।
उत्तराधिकारी नीचे से काम करके ऊपर तक नहीं पहुंचते। वे जानते हैं, और व्यवसाय में हर कोई जानता है, कि उत्तराधिकारी एक दिन शीर्ष पर पहुंचेंगे। मुझे डर है कि लगभग एक दर्जन पुराने परिवारों को छोड़कर, अधिकांश उत्तराधिकारियों ने मूल्य या धन नहीं बनाया है। कुछ ने, दुर्भाग्य से, मूल्य और धन को नष्ट कर दिया। केवल 1991 से पहले और आज के भारत के शीर्ष दस व्यापारिक घरानों की सूचियों की तुलना करें। पहली पीढ़ी के अधिकतर उद्यमियों ने धन बनाया है। जहां तक श्रमिकों और कर्मचारियों का संबंध है, उनमें से अधिकतर वेतन/ मजदूरी (और उसमें आवधिक संशोधन) पाकर संतुष्ट हैं। उनके पास न तो कौशल है और न ही अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ने की महत्त्वाकांक्षा है। मैंने देखा कि मोटे तौर पर उत्तराधिकारियों और कर्मचारियों ने ही नारायणमूर्ति और सुब्रह्मण्यन की उस टिप्पणी की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति को हफ्ते में कितने घंटे काम करना चाहिए।
नियम सामान्य नहीं है
नारायणमूर्ति ने हफ्ते में सत्तर घंटे काम करने की वकालत की थी। सुब्रह्मण्यन ने कथित तौर पर हफ्ते में नब्बे घंटे काम करने की बात कही। मेरा मानना है कि उन्होंने जो कहा वह उनके मुताबिक अपमानजनक नहीं था। नारायणमूर्ति ने कहा कि, ‘भारत की कार्य उत्पादकता दुनिया में सबसे कम है… इसलिए, मेरा अनुरोध है कि हमारे युवाओं को कहना चाहिए कि यह मेरा देश है, मैं सप्ताह में सत्तर घंटे काम करना चाहता हूं।’ जब उनकी इस टिप्पणी पर तीखी बहस छिड़ गई, तो उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। सुब्रह्मण्यन ने एक वीडियो में कहा कि, ‘ईमानदारी से कहूं तो मुझे खेद है कि मैं आपसे रविवार को काम नहीं ले पा रहा हूं। मुझे आपसे रविवार को काम करवाने में बहुत खुशी होगी, मैं रविवार को काम करता हूं।’
औद्योगिक श्रमिकों के लिए आठ घंटे के कार्य दिवस का कानून पहली बार 1918 में जर्मनी में बना था। तब से ‘आठ घंटे श्रम, आठ घंटे मनोरंजन और आठ घंटे आराम’ एक सार्वभौम आदर्श बन गया है। 8-8-8 का सिद्धांत अच्छा है, हालांकि मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता, जो दिन में आठ घंटे ‘मनोरंजन’ पर खर्च करता हो। मुझे लगता है कि ‘मनोरंजन’ में खाना, कपड़े धोना, व्यायाम करना, खेल खेलना, फिल्में देखना, अखबार और किताबें पढ़ना, खरीदारी करना, गपशप करना आदि शामिल हैं। अगर आप इसे इस तरह देखें, तो ‘मनोरंजन’ के लिए आठ घंटे पर्याप्त नहीं लगते हैं!
अधिकतर औद्योगिक कर्मचारी एक ही तरह के काम दोहराते रहते हैं। कुछ ही नए कौशल सीखते और अधिक जटिल काम करने का हुनर सीखने के लिए स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हैं। जब ‘डेस्क जाब’ प्रचलित हो गई, तो नियोक्ताओं ने 8-8-8 मानदंड की नकल की। अधिकतर डेस्क कर्मचारी भी दोहराए जाने वाले काम करते हैं। इसलिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि अधिकांश श्रमिकों/ कर्मचारियों के लिए 8-8-8 मानदंड को अपनाना समझ से परे है। स्वचालन, रोबोटिक्स और एआइ आने के बाद, काम के घंटे कम हो सकते हैं। उन्हें लंबे समय तक काम करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। मगर उन्हें अधिक उत्पादक बनने के लिए औजारों, तकनीकी और प्रणाली की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि नारायणमूर्ति और सुब्रह्मण्यन की टिप्पणियां ऐसे श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए नहीं थीं।
इसके विपरीत, किसान, खासकर स्वरोजगार वाले किसान 8-8-8 के मानदंड का पालन नहीं करते हैं। खेती के काम में, आठ घंटे दिन के काम की अवधि दस या बारह घंटे तक बढ़ सकती है। इसी तरह, डाक्टर, वकील, न्यायाधीश, आर्किटेक्ट, वैज्ञानिक, अभिनेता आदि जैसे पेशेवर दिन में सिर्फ आठ घंटे काम नहीं करते हैं। मैं ऐसे पेशेवरों को जानता हूं, जिनके काम के घंटे दिन के बारह घंटे तक बढ़ जाते हैं और शनिवार और कई मामलों में रविवार को भी बढ़ जाते हैं। कुछ सफल पेशेवर लंबे काम के घंटों के बारे में शिकायत करते हैं, जिसे उन्होंने स्वेच्छा से अपनाया है। इसलिए तथाकथित मानदंड सभी लोगों पर लागू एक समान नियम नहीं है।
संतुलन की तलाश
मुझे दिन में लंबे समय तक काम करना अच्छा लगता है, मगर मेरे लिए ‘काम’ की परिभाषा में वकालत करना, संसदीय कार्य, पढ़ना, लिखना, बोलना, जनता की बातें सुनना, पार्टी कार्यकर्ताओं से बातें करना और चुनिंदा सामाजिक समारोहों में भाग लेना शामिल है। मैं हर उस घंटे को ‘काम का घंटा’ मानता हूं, जब मैं सो नहीं रहा होता हूं। कार्य-जीवन का संतुलन एक ऐसी चीज है, जिसे हर व्यक्ति को खुद खोजना पड़ता है, और मुझे खुशी है कि मैंने अपना संतुलन खोज लिया है। मुझे लगता है कि, बड़ी कामयाबी हासिल करने और शीर्ष पर पहुंचने के बाद, नारायणमूर्ति और सुब्रह्मण्यन ने यह योग्यता अर्जित की है कि वे भारतीयों से काम के ‘लंबे’ घंटों के बारे में बात कर सकें। मुझे नहीं लगता कि इसका वित्तीय लाभ से कोई लेना-देना है, जैसा कि कुछ ‘ट्रोल’ और ‘मीम्स’ द्वारा बताया गया है।
मैं ऐसे कई पुरुषों और महिलाओं को जानता हूं, जो बड़ी आय या बहुत अधिक धन से अप्रभावित हैं: वे एक सादा जीवन जीते हैं, सादा खाना खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, साफ-सुथरे कपड़े पहनते हैं, मगर दिखावटी नहीं, विनम्र और दयालु हैं। मेरा मानना है कि नारायणमूर्ति और सुब्रह्मण्यन महत्त्वाकांक्षी युवा पीढ़ी को यह सबक सिखाने के लिए प्रेरित कर रहे थे कि उत्पादक काम के लंबे घंटे ही विकासशील देश को वास्तव में समृद्ध और लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मेरे विचार से, नारायणमूर्ति और सुब्रह्मण्यन द्वारा की गई टिप्पणियों में कुछ भी विवादास्पद नहीं था। अगर कुछ है तो यह कि उनकी बातें लोगों को सोचने के लिए उकसाती हैं, जिनका अनपेक्षित प्रभाव हो सकता है। इसे कामकाजी जीवन में संतुलन की खोज की दृष्टि से कोई बुरी बात नहीं कहा जा सकता है!